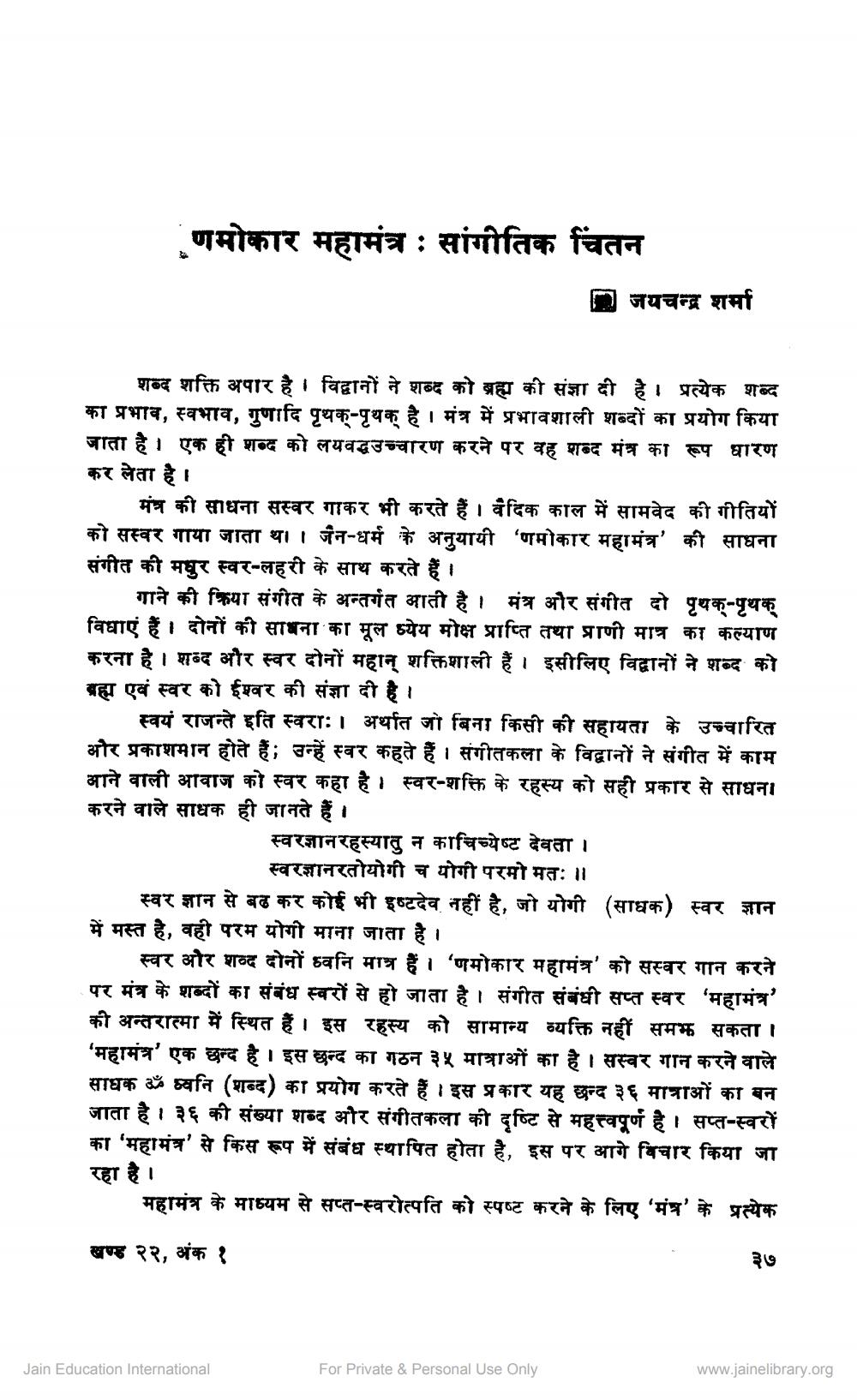________________
णमोकार महामंत्र : सांगीतिक चिंतन
0 जयचन्द्र शर्मा
शब्द शक्ति अपार है। विद्वानों ने शब्द को ब्रह्म की संज्ञा दी है। प्रत्येक शब्द का प्रभाव, स्वभाव, गुणादि पृथक्-पृथक् है । मंत्र में प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक ही शब्द को लयवद्धउच्चारण करने पर वह शब्द मंत्र का रूप धारण कर लेता है।
मंत्र की साधना सस्वर गाकर भी करते हैं। वैदिक काल में सामवेद की गीतियों को सस्वर गाया जाता था। जैन-धर्म के अनुयायी ‘णमोकार महामंत्र' की साधना संगीत की मधर स्वर-लहरी के साथ करते हैं।
गाने की क्रिया संगीत के अन्तर्गत आती है। मंत्र और संगीत दो पृथक्-पृथक् विधाएं हैं। दोनों की साधना का मूल ध्येय मोक्ष प्राप्ति तथा प्राणी मात्र का कल्याण करना है। शब्द और स्वर दोनों महान् शक्तिशाली हैं। इसीलिए विद्वानों ने शब्द को ब्रह्म एवं स्वर को ईश्वर की संज्ञा दी है।
स्वयं राजन्ते इति स्वराः। अर्थात जो बिना किसी की सहायता के उच्चारित और प्रकाशमान होते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं । संगीतकला के विद्वानों ने संगीत में काम आने वाली आवाज को स्वर कहा है। स्वर-शक्ति के रहस्य को सही प्रकार से साधना करने वाले साधक ही जानते हैं।
स्वरज्ञानरहस्यातु न काचिच्येष्ट देवता।
स्वरज्ञानरतोयोगी च योगी परमो मतः ॥ स्वर ज्ञान से बढ़ कर कोई भी इष्टदेव नहीं है, जो योगी (साधक) स्वर ज्ञान में मस्त है, वही परम योगी माना जाता है।
स्वर और शब्द दोनों ध्वनि मात्र हैं। ‘णमोकार महामंत्र' को सस्वर गान करने पर मंत्र के शब्दों का संबंध स्वरों से हो जाता है। संगीत संबंधी सप्त स्वर 'महामंत्र' की अन्तरात्मा में स्थित हैं। इस रहस्य को सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। 'महामंत्र' एक छन्द है । इस छन्द का गठन ३५ मात्राओं का है । सस्वर गान करने वाले साधक ॐ ध्वनि (शब्द) का प्रयोग करते हैं । इस प्रकार यह छन्द ३६ मात्राओं का बन जाता है । ३६ की संख्या शब्द और संगीतकला की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । सप्त-स्वरों का 'महामंत्र' से किस रूप में संबंध स्थापित होता है, इस पर आगे विचार किया जा
महामंत्र के माध्यम से सप्त-स्वरोत्पति को स्पष्ट करने के लिए 'मंत्र' के प्रत्येक
खण्ड २२, अंक १
३७
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org