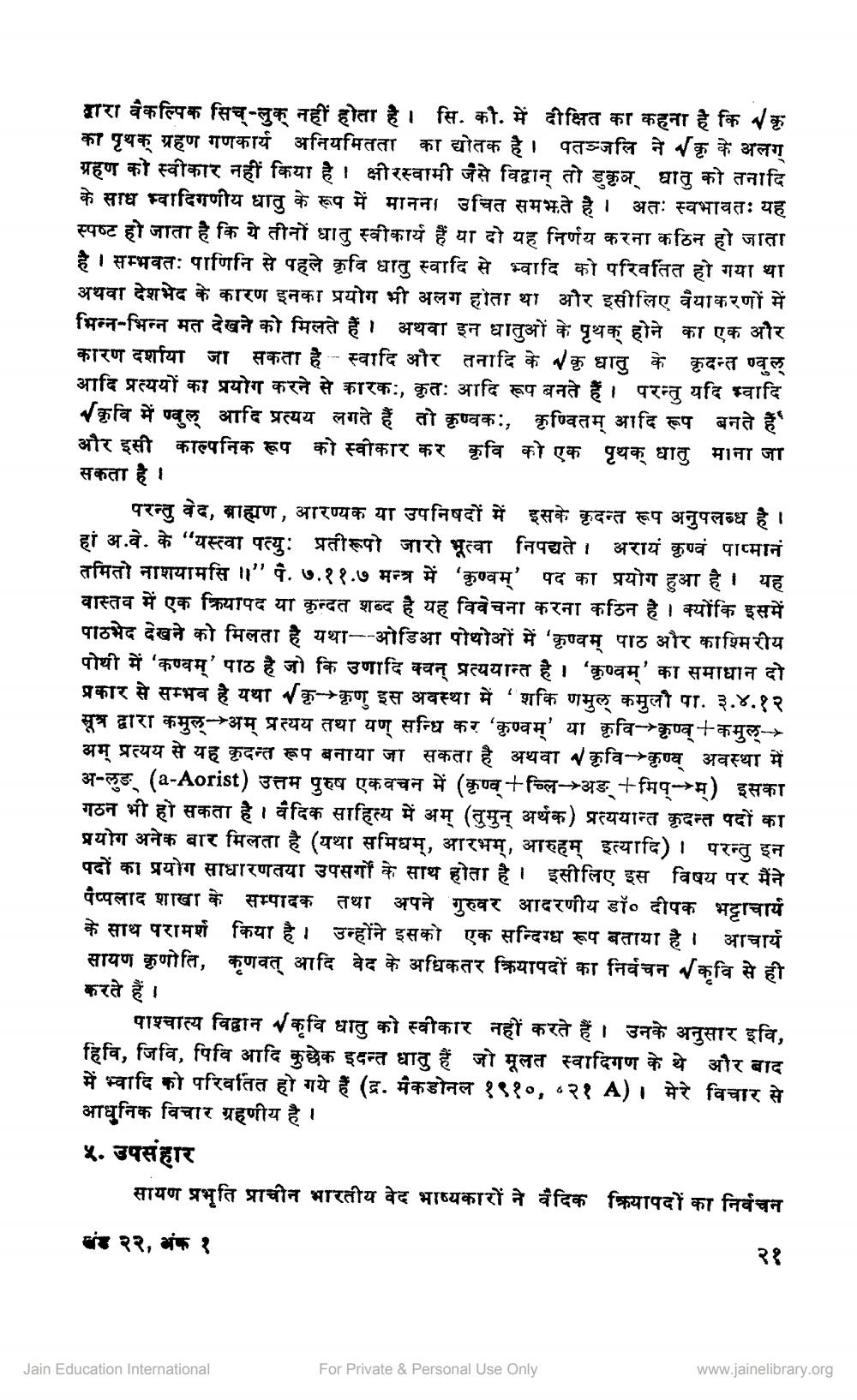________________
धातु को तनादि
अतः स्वभावतः यह
द्वारा वैकल्पिक सिच् लुक् नहीं होता है । सि. को में दीक्षित का कहना है कि / कृ का पृथक् ग्रहण गणकार्य अनियमितता का द्योतक है । पतञ्जलि ने √ कृ के अलग् ग्रहण को स्वीकार नहीं किया है। क्षीरस्वामी जैसे विद्वान् तो डुकृञ के साध भ्वादिगणीय धातु के रूप में मानना उचित समझते है । स्पष्ट हो जाता है कि ये तीनों धातु स्वीकार्य हैं या दो यह निर्णय करना कठिन हो जाता है । सम्भवतः पाणिनि से पहले कृवि धातु स्वादि से भ्वादि को परिवर्तित हो गया था अथवा देशभेद के कारण इनका प्रयोग भी अलग होता था और इसीलिए वैयाकरणों में भिन्न-भिन्न मत देखने को मिलते हैं । अथवा इन धातुओं के पृथक् होने का एक और कारण दर्शाया जा सकता है- स्वादि और तनादि के / कृ धातु के कृदन्त ण्वुल् आदि प्रत्ययों का प्रयोग करने से कारकः कृतः आदि रूप बनते हैं । परन्तु यदि स्वादि कृवि में ण्वुल् आदि प्रत्यय लगते हैं तो कृण्वकः, कृण्वितम् आदि रूप बनते हैं ' और इसी काल्पनिक रूप को स्वीकार कर कृवि को एक पृथक् धातु माना जा सकता है ।
1
परन्तु वेद, ब्राह्मण, आरण्यक या उपनिषदों में इसके कृदन्त रूप अनुपलब्ध है । हां अ. वे के "यस्त्वा पत्युः प्रतीरूपो जारो भूत्वा निपद्यते । अरायं कृण्वं पाप्मानं तमितो नाशयामसि ।।" पं. ७.११.७ मन्त्र में 'कृण्वम्' पद का प्रयोग हुआ है । यह वास्तव में एक क्रियापद या कृन्दत शब्द है यह विवेचना करना कठिन है । क्योंकि इसमें पाठभेद देखने को मिलता है यथा-ओडिआ पोथोओं में 'कृण्वम् पाठ और काश्मिरीय पोथी में 'कण्वम्' पाठ है जो कि उणादि क्वन् प्रत्ययान्त है । 'कृण्वम्' का समाधान दो प्रकार से सम्भव है यथा कृकृणु इस अवस्था में शकि णमुल् कमुलौ पा. ३.४.१२ सूत्र द्वारा कमुल् अम् प्रत्यय तथा यण् सन्धि कर 'कृण्वम्' या कृवि कृण्व् +कमुल् अम् प्रत्यय से यह कृदन्त रूप बनाया जा सकता है अथवा / कृवि कृण्य् अवस्था में अ-लुङ, (a-Aorist) उत्तम पुरुष एकवचन में (कृण्व् + च्लि अ + मिम् ) इसका गठन भी हो सकता है । वैदिक साहित्य में अम् (तुमुन् अर्थक) प्रत्ययान्त कृदन्त पदों का प्रयोग अनेक बार मिलता है (यथा समिधम्, आरभम्, आरुहम् इत्यादि) । परन्तु इन पदों का प्रयोग साधारणतया उपसर्गों के साथ होता है । इसीलिए इस विषय पर मैंने पैप्पलाद शाखा के सम्पादक तथा अपने गुरुवर आदरणीय डॉ० दीपक भट्टाचार्य के साथ परामर्श किया है । उन्होंने इसको एक सन्दिग्ध रूप बताया है । आचार्य सायण कृणोति, कृणवत् आदि वेद के अधिकतर क्रियापदों का निर्वचन / कृवि से ही करते हैं ।
पाश्चात्य विद्वान / कृवि धातु को स्वीकार नहीं करते हैं । उनके अनुसार इवि, हिवि, जिवि, पिवि आदि कुछेक इदन्त धातु हैं जो मूलत स्वादिगण के थे और बाद में भ्वादि को परिवर्तित हो गये हैं (द्र. मैकडोनल १९१०, ०२१ A ) । मेरे विचार से
आधुनिक विचार ग्रहणीय है ।
५. उपसंहार
सायण प्रभृति प्राचीन भारतीय वेद भाष्यकारों ने वैदिक क्रियापदों का निर्वचन
खंड २२, अंक १
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
२१
www.jainelibrary.org