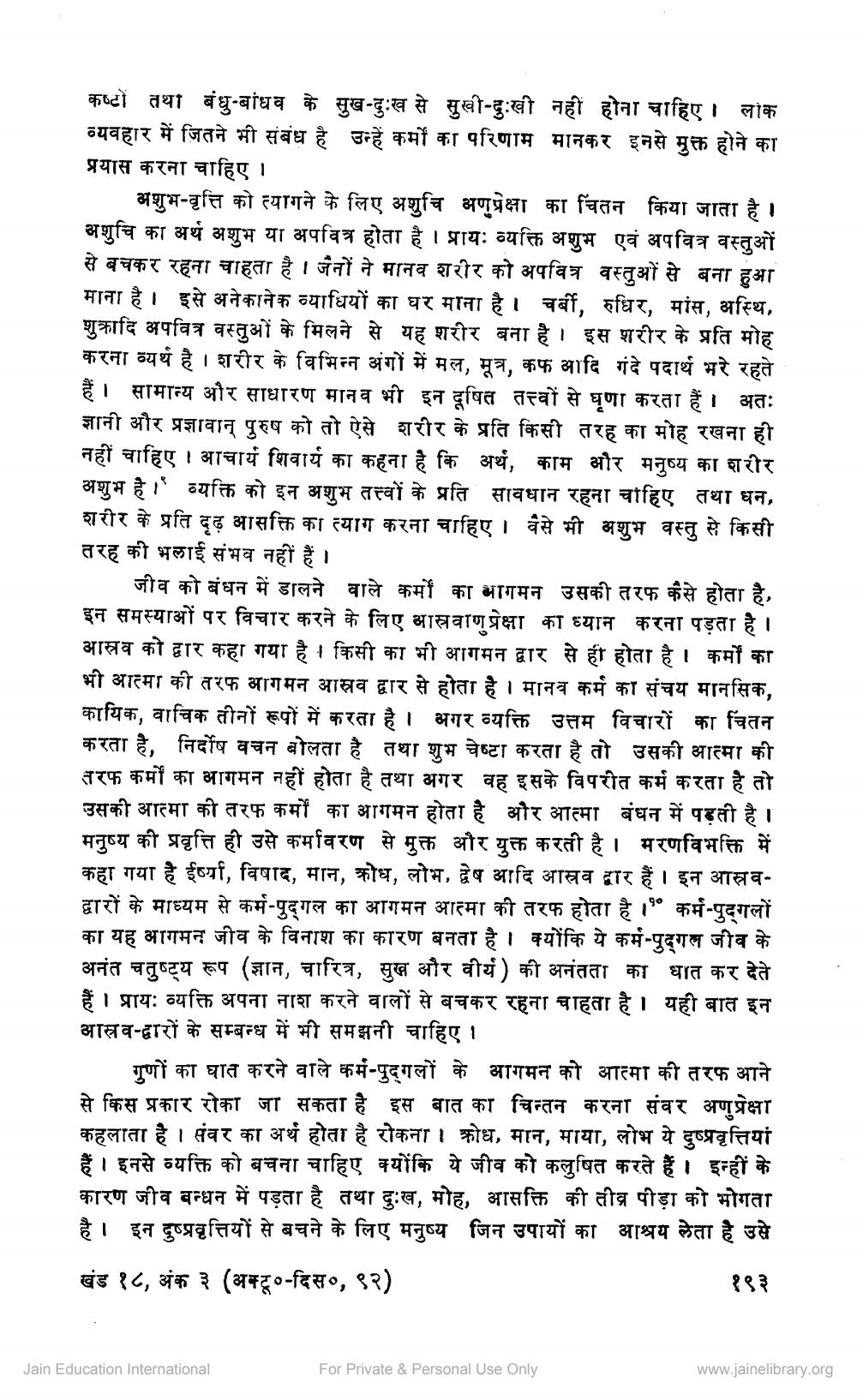________________
कष्टों तथा बंधु-बांधव के व्यवहार में जितने भी संबंध है प्रयास करना चाहिए ।
अशुभ वृत्ति को त्यागने के लिए अशुचि अणुप्रेक्षा का चिंतन किया जाता है । अशुचि का अर्थ अशुभ या अपवित्र होता है । प्रायः व्यक्ति अशुभ एवं अपवित्र वस्तुओं से बचकर रहना चाहता है । जैनों ने मानव शरीर को अपवित्र वस्तुओं से बना हुआ माना है । इसे अनेकानेक व्याधियों का घर माना है । चर्बी, रुधिर, मांस, अस्थि, शुक्रादि अपवित्र वस्तुओं के मिलने से यह शरीर बना है । इस शरीर के प्रति मोह करना व्यर्थ है । शरीर के विभिन्न अंगों में मल, मूत्र, कफ आदि गंदे पदार्थ भरे रहते हैं । सामान्य और साधारण मानव भी इन दूषित तत्त्वों से घृणा करता हैं । अतः ज्ञानी और प्रज्ञावान् पुरुष को तो ऐसे शरीर के प्रति किसी तरह का मोह रखना ही नहीं चाहिए । आचार्य शिवार्य का कहना है कि अर्थ, काम और मनुष्य का शरीर अशुभ है ।" व्यक्ति को इन अशुभ तत्त्वों के प्रति सावधान रहना चाहिए तथा धन, शरीर के प्रति दृढ़ आसक्ति का त्याग करना चाहिए। वैसे भी अशुभ वस्तु से किसी तरह की भलाई संभव नहीं हैं ।
सुख-दुःख से सुखी - दुःखी नहीं होना चाहिए । लोक उन्हें कर्मों का परिणाम मानकर इनसे मुक्त होने का
जीव को बंधन में डालने वाले कर्मों का आगमन उसकी तरफ कैसे होता है, इन समस्याओं पर विचार करने के लिए आस्रवाणुप्रेक्षा का ध्यान करना पड़ता है । आस्रव को द्वार कहा गया है । किसी का भी आगमन द्वार से ही होता है । कर्मों का भी आत्मा की तरफ आगमन आस्रव द्वार से होता है। मानव कर्म का संचय मानसिक, कायिक, वाचिक तीनों रूपों में करता है । अगर व्यक्ति उत्तम विचारों का चिंतन करता है, निर्दोष वचन बोलता है तथा शुभ चेष्टा करता है तो उसकी आत्मा की तरफ कर्मों का आगमन नहीं होता है तथा अगर वह इसके विपरीत कर्म करता है तो उसकी आत्मा की तरफ कर्मों का आगमन होता है और आत्मा बंधन में पड़ती है । मनुष्य की प्रवृत्ति ही उसे कर्मावरण से मुक्त और युक्त करती है । मरणविभक्ति में कहा गया है ईर्ष्या, विषाद, मान, क्रोध, लोभ, द्वेष आदि आस्रव द्वार हैं । इन आस्रवद्वारों के माध्यम से कर्म- पुद्गल का आगमन आत्मा की तरफ होता है ।" कर्म- पुद्गलों का यह आगमन जीव के विनाश का कारण बनता है । क्योंकि ये कर्म- पुद्गल जीव के अनंत चतुष्ट्य रूप ( ज्ञान, चारित्र, सुख और वीर्य ) की अनंतता का घात कर देते हैं । प्रायः व्यक्ति अपना नाश करने वालों से बचकर रहना चाहता है । यही बात इन आस्रव द्वारों के सम्बन्ध में भी समझनी चाहिए ।
गुणों का घात करने वाले कर्म-पुद्गलों के आगमन को आत्मा की तरफ आने से किस प्रकार रोका जा सकता है इस बात का चिन्तन करना संवर अणुप्रेक्षा कहलाता है । संवर का अर्थ होता है रोकना । क्रोध, मान, माया, लोभ ये दुष्प्रवृत्तियां हैं । इनसे व्यक्ति को बचना चाहिए क्योंकि ये जीव को कलुषित करते हैं । इन्हीं के कारण जीव बन्धन में पड़ता है तथा दुःख, मोह, आसक्ति की तीव्र पीड़ा को भोगता है । इन दुष्प्रवृत्तियों से बचने के लिए मनुष्य जिन उपायों का आश्रय लेता है उसे
खंड १८, अंक ३ (अक्टू० - दिस०, ९२ )
१९३
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org