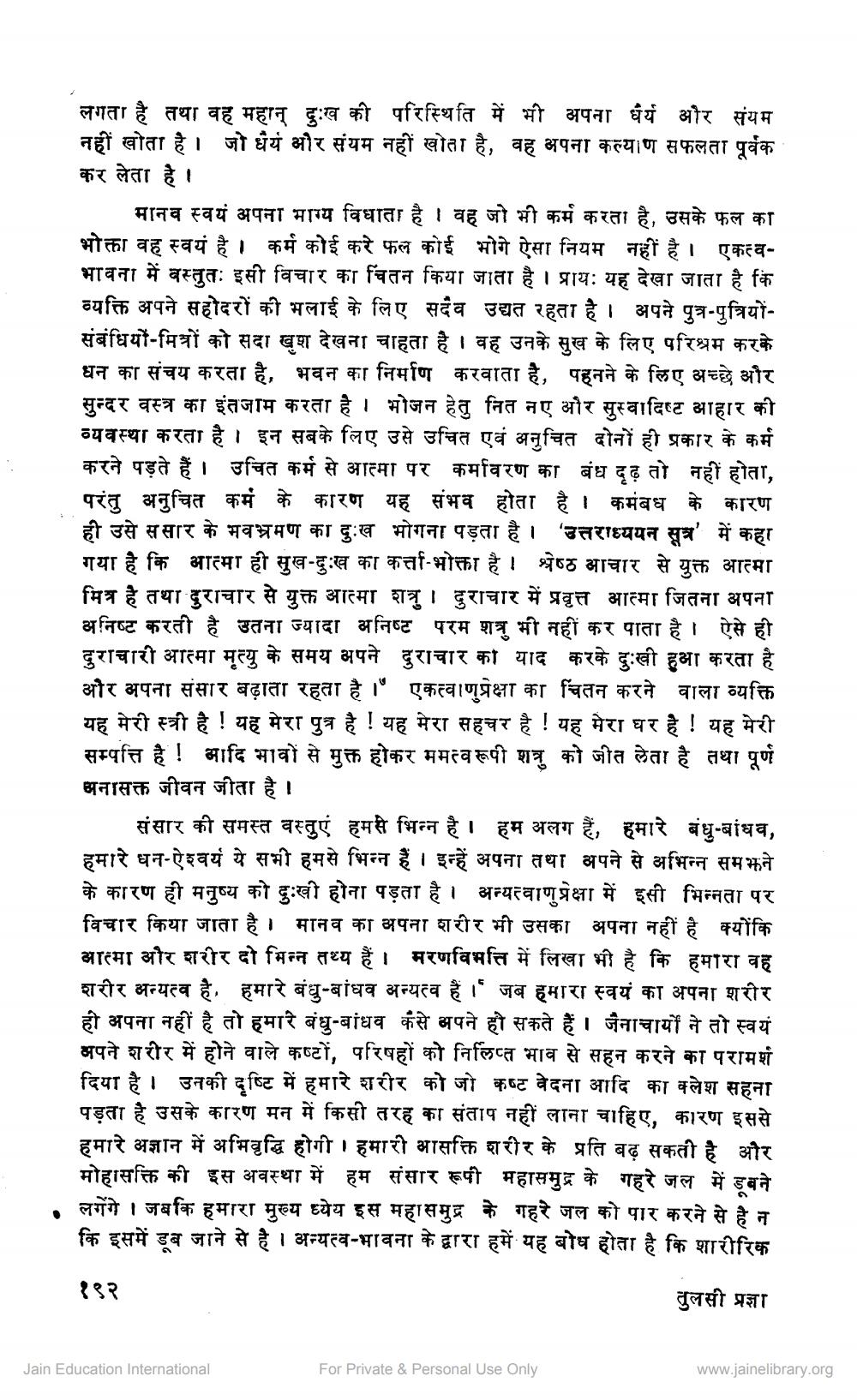________________
लगता है तथा वह महान् दुःख की परिस्थिति में भी अपना धैर्य और संयम नहीं खोता है। जो धैर्य और संयम नहीं खोता है, वह अपना कल्याण सफलता पूर्वक कर लेता है।
__ मानव स्वयं अपना भाग्य विधाता है । वह जो भी कर्म करता है, उसके फल का भोक्ता वह स्वयं है। कर्म कोई करे फल कोई भोगे ऐसा नियम नहीं है। एकत्वभावना में वस्तुतः इसी विचार का चिंतन किया जाता है । प्रायः यह देखा जाता है कि व्यक्ति अपने सहोदरों की भलाई के लिए सदैव उद्यत रहता है। अपने पुत्र-पुत्रियोंसंबंधियों-मित्रों को सदा खुश देखना चाहता है । वह उनके सुख के लिए परिश्रम करके धन का संचय करता है, भवन का निर्माण करवाता है, पहनने के लिए अच्छे और सुन्दर वस्त्र का इंतजाम करता है । भोजन हेतु नित नए और सुस्वादिष्ट आहार की व्यवस्था करता है। इन सबके लिए उसे उचित एवं अनुचित दोनों ही प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। उचित कर्म से आत्मा पर कर्मावरण का बंध दृढ़ तो नहीं होता, परंतु अनुचित कर्म के कारण यह संभव होता है। कमंबध के कारण ही उसे ससार के भवभ्रमण का दुःख भोगना पड़ता है। 'उत्तराध्ययन सूत्र' में कहा गया है कि आत्मा ही सुख-दुःख का कर्ता-भोक्ता है । श्रेष्ठ आचार से युक्त आत्मा मित्र है तथा दुराचार से युक्त आत्मा शत्रु । दुराचार में प्रवृत्त आत्मा जितना अपना अनिष्ट करती है उतना ज्यादा अनिष्ट परम शत्रु भी नहीं कर पाता है। ऐसे ही दुराचारी आत्मा मृत्यु के समय अपने दुराचार को याद करके दुःखी हुआ करता है और अपना संसार बढ़ाता रहता है । एकत्वाणुप्रेक्षा का चिंतन करने वाला व्यक्ति यह मेरी स्त्री है ! यह मेरा पुत्र है ! यह मेरा सहचर है ! यह मेरा घर है ! यह मेरी सम्पत्ति है ! आदि भावों से मुक्त होकर ममत्वरूपी शत्रु को जीत लेता है तथा पूर्ण अनासक्त जीवन जीता है ।
संसार की समस्त वस्तुएं हमसे भिन्न है। हम अलग हैं, हमारे बंधु-बांधव, हमारे धन-ऐश्वर्य ये सभी हमसे भिन्न हैं । इन्हें अपना तथा अपने से अभिन्न समझने के कारण ही मनुष्य को दुःखी होना पड़ता है। अन्यत्वाणुप्रेक्षा में इसी भिन्नता पर विचार किया जाता है। मानव का अपना शरीर भी उसका अपना नहीं है क्योंकि आत्मा और शरीर दो भिन्न तथ्य हैं। मरणविभत्ति में लिखा भी है कि हमारा वह शरीर अन्यत्व है, हमारे बंधु-बांधव अन्यत्व हैं । जब हमारा स्वयं का अपना शरीर ही अपना नहीं है तो हमारे बंधु-बांधव कसे अपने हो सकते हैं । जैनाचार्यों ने तो स्वयं अपने शरीर में होने वाले कष्टों, परिषहों को निलिप्त भाव से सहन करने का परामर्श दिया है। उनकी दृष्टि में हमारे शरीर को जो कष्ट वेदना आदि का क्लेश सहना पड़ता है उसके कारण मन में किसी तरह का संताप नहीं लाना चाहिए, कारण इससे हमारे अज्ञान में अभिवृद्धि होगी। हमारी आसक्ति शरीर के प्रति बढ़ सकती है और मोहासक्ति की इस अवस्था में हम संसार रूपी महासमुद्र के गहरे जल में डूबने लगेंगे । जबकि हमारा मुख्य ध्येय इस महासमुद्र के गहरे जल को पार करने से है न कि इसमें डूब जाने से है । अन्यत्व-भावना के द्वारा हमें यह बोध होता है कि शारीरिक
१९२
तुलसी प्रज्ञा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org