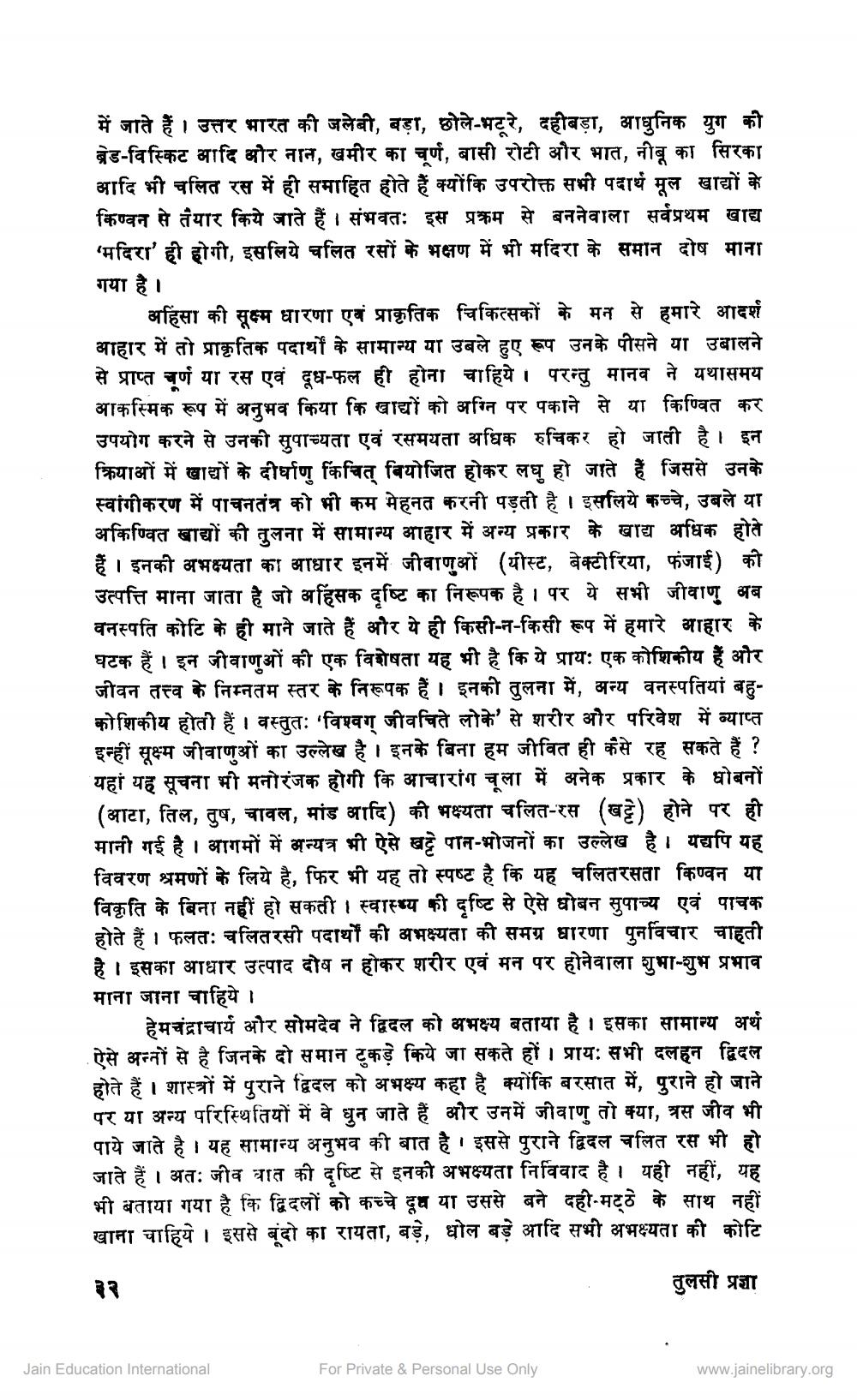________________
में जाते हैं । उत्तर भारत की जलेबी, बड़ा, छोले-भटूरे, दहीबड़ा, आधुनिक युग की ब्रेड-विस्किट आदि और नान, खमीर का चूर्ण, बासी रोटी और भात, नीबू का सिरका आदि भी चलित रस में ही समाहित होते हैं क्योंकि उपरोक्त सभी पदार्थ मूल खाद्यों के किण्वन से तैयार किये जाते हैं। संभवतः इस प्रक्रम से बननेवाला सर्वप्रथम खाद्य 'मदिरा' ही होगी, इसलिये चलित रसों के भक्षण में भी मदिरा के समान दोष माना गया है।
अहिंसा की सूक्ष्म धारणा एवं प्राकृतिक चिकित्सकों के मन से हमारे आदर्श आहार में तो प्राकृतिक पदार्थों के सामान्य या उबले हुए रूप उनके पीसने या उबालने से प्राप्त चूर्ण या रस एवं दूध-फल ही होना चाहिये । परन्तु मानव ने यथासमय आकस्मिक रूप में अनुभव किया कि खाद्यों को अग्नि पर पकाने से या किण्वित कर उपयोग करने से उनकी सुपाच्यता एवं रसमयता अधिक रुचिकर हो जाती है। इन क्रियाओं में खाद्यों के दीर्घाणु किंचित् वियोजित होकर लघु हो जाते हैं जिससे उनके स्वांगीकरण में पाचनतंत्र को भी कम मेहनत करनी पड़ती है । इसलिये कच्चे, उबले या अकिण्वित खाद्यों की तुलना में सामान्य आहार में अन्य प्रकार के खाद्य अधिक होते हैं । इनकी अभक्ष्यता का आधार इनमें जीवाणुओं (यीस्ट, बेक्टीरिया, फंजाई) को उत्पत्ति माना जाता है जो अहिंसक दृष्टि का निरूपक है । पर ये सभी जीवाणु अब वनस्पति कोटि के ही माने जाते हैं और ये ही किसी-न-किसी रूप में हमारे आहार के घटक हैं । इन जीवाणुओं की एक विशेषता यह भी है कि ये प्राय: एक कोशिकीय हैं और जीवन तत्त्व के निम्नतम स्तर के निरूपक हैं। इनकी तुलना में, अन्य वनस्पतियां बहुकोशिकीय होती हैं । वस्तुतः 'विश्वग् जीवचिते लोके' से शरीर और परिवेश में व्याप्त इन्हीं सूक्ष्म जीवाणुओं का उल्लेख है । इनके बिना हम जीवित ही कैसे रह सकते हैं ? यहां यह सूचना भी मनोरंजक होगी कि आचारांग चूला में अनेक प्रकार के धोबनों (आटा, तिल, तुष, चावल, मांड आदि) की भक्ष्यता चलित-रस (खट्टे) होने पर ही मानी गई है । आगमों में अन्यत्र भी ऐसे खट्टे पान-भोजनों का उल्लेख है। यद्यपि यह विवरण श्रमणों के लिये है, फिर भी यह तो स्पष्ट है कि यह चलितरसता किण्वन या विकृति के बिना नहीं हो सकती । स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसे धोबन सुपाच्य एवं पाचक होते हैं। फलतः चलितरसी पदार्थों की अभक्ष्यता की समग्र धारणा पुनर्विचार चाहती है । इसका आधार उत्पाद दोष न होकर शरीर एवं मन पर होनेवाला शुभा-शुभ प्रभाव माना जाना चाहिये।
हेमचंद्राचार्य और सोमदेव ने द्विदल को अभक्ष्य बताया है । इसका सामान्य अर्थ ऐसे अन्नों से है जिनके दो समान टुकड़े किये जा सकते हों। प्रायः सभी दलहन द्विदल होते हैं । शास्त्रों में पुराने द्विदल को अभक्ष्य कहा है क्योंकि बरसात में, पुराने हो जाने पर या अन्य परिस्थितियों में वे धुन जाते हैं और उनमें जीवाणु तो क्या, त्रस जीव भी पाये जाते है। यह सामान्य अनुभव की बात है। इससे पुराने द्विदल चलित रस भी हो जाते हैं । अतः जीव वात की दृष्टि से इनको अभक्ष्यता निर्विवाद है। यही नहीं, यह भी बताया गया है कि द्विदलों को कच्चे दूध या उससे बने दही-मठे के साथ नहीं खाना चाहिये । इससे बूंदो का रायता, बड़े, धोल बड़े आदि सभी अभक्ष्यता की कोटि
३२
तुलसी प्रज्ञा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org