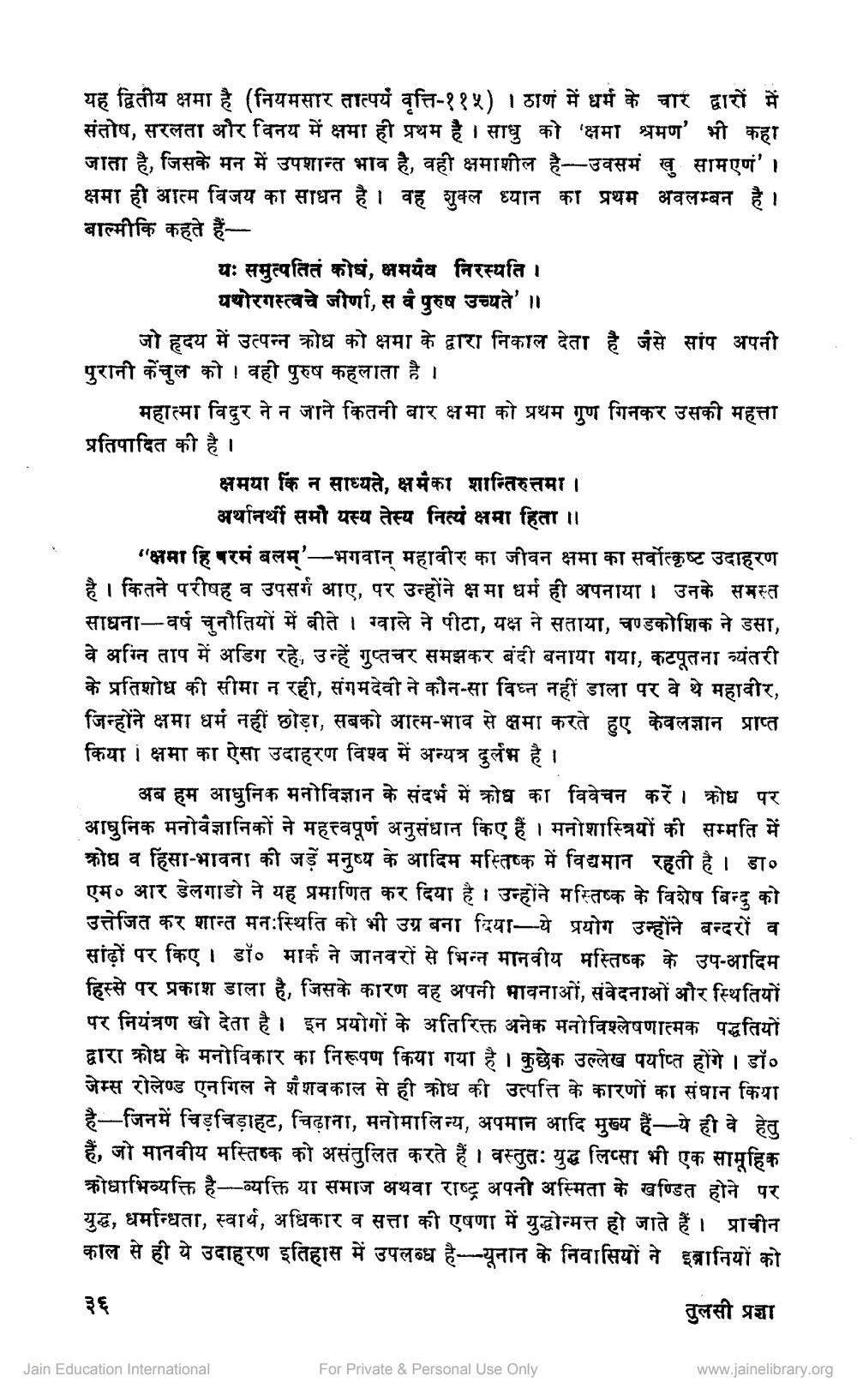________________
यह द्वितीय क्षमा है ( नियमसार तात्पर्यं वृत्ति- ११५) । ठाणं में धर्म के चार द्वारों में संतोष, सरलता और विनय में क्षमा ही प्रथम है । साधु को 'क्षमा श्रमण' भी कहा जाता है, जिसके मन में उपशान्त भाव है, वही क्षमाशील है – उवसमं खु सामएणं' । क्षमा ही आत्म विजय का साधन है । वह शुक्ल ध्यान का प्रथम अवलम्बन है । बाल्मीकि कहते हैं—
यः समुत्पतितं कोघं, क्षमयैव निरस्यति । यथोरगस्त्वचे जीर्णा, स वै पुरुष उच्यते ' ॥
जो हृदय में उत्पन्न क्रोध को क्षमा के द्वारा निकाल देता है जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुल को । वही पुरुष कहलाता है ।
महात्मा विदुर ने न जाने कितनी बार क्षमा को प्रथम गुण गिनकर उसकी महत्ता प्रतिपादित की है ।
क्षमया किं न साध्यते, क्षमका शान्तिरुत्तमा । अर्थानर्थी समौ यस्य तेस्य नित्यं क्षमा हिता ॥
"क्षमा हि परमं बलम्' - भगवान् महावीर का जीवन क्षमा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है । कितने परीषह व उपसर्ग आए, पर उन्होंने क्षमा धर्म ही अपनाया । उनके समस्त साधना - वर्ष चुनौतियों में बीते । ग्वाले ने पीटा, यक्ष ने सताया, चण्डकोशिक ने डसा,
अग्नि ताप में अडिग रहे, उन्हें गुप्तचर समझकर बंदी बनाया गया, कटपूतना व्यंतरी के प्रतिशोध की सीमा न रही, संगमदेवी ने कौन-सा विघ्न नहीं डाला पर वे थे महावीर, जिन्होंने क्षमा धर्म नहीं छोड़ा, सबको आत्म-भाव से क्षमा करते हुए केवलज्ञान प्राप्त किया । क्षमा का ऐसा उदाहरण विश्व में अन्यत्र दुर्लभ है ।
Jain Education International
अब हम आधुनिक मनोविज्ञान के संदर्भ में क्रोध का विवेचन करें। क्रोध पर • आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने महत्त्वपूर्ण अनुसंधान किए हैं । मनोशास्त्रियों की सम्मति में क्रोध व हिंसा - भावना की जड़ें मनुष्य के आदिम मस्तिष्क में विद्यमान रहती है डा० एम० आर डेलगाडो ने यह प्रमाणित कर दिया है । उन्होंने मस्तिष्क के विशेष बिन्दु को उत्तेजित कर शान्त मनःस्थिति को भी उग्र बना दिया - ये प्रयोग उन्होंने बन्दरों व सांढ़ों पर किए । डॉ० मार्क ने जानवरों से भिन्न मानवीय मस्तिष्क के उप-आदिम हिस्से पर प्रकाश डाला है, जिसके कारण वह अपनी भावनाओं, संवेदनाओं और स्थितियों पर नियंत्रण खो देता है । इन प्रयोगों के अतिरिक्त अनेक मनोविश्लेषणात्मक पद्धतियों द्वारा क्रोध के मनोविकार का निरूपण किया गया है । कुछेक उल्लेख पर्याप्त होंगे। डॉ० जेम्स रोलेण्ड एनगिल ने शैशवकाल से ही क्रोध की उत्पत्ति के कारणों का संधान किया है— जिनमें चिड़चिड़ाहट, चिढ़ाना, मनोमालिन्य, अपमान आदि मुख्य हैं—ये ही वे हेतु हैं, जो मानवीय मस्तिष्क को असंतुलित करते हैं । वस्तुतः युद्ध लिप्सा भी एक सामूहिक क्रोधाभिव्यक्ति है— व्यक्ति या समाज अथवा राष्ट्र अपनी अस्मिता के खण्डित होने पर युद्ध, धर्मान्धता, स्वार्थ, अधिकार व सत्ता की एषणा में युद्धोन्मत्त हो जाते हैं । प्राचीन काल से ही ये उदाहरण इतिहास में उपलब्ध है ---यूनान के निवासियों ने इब्रानियों को
३६
तुलसी प्रज्ञा
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org