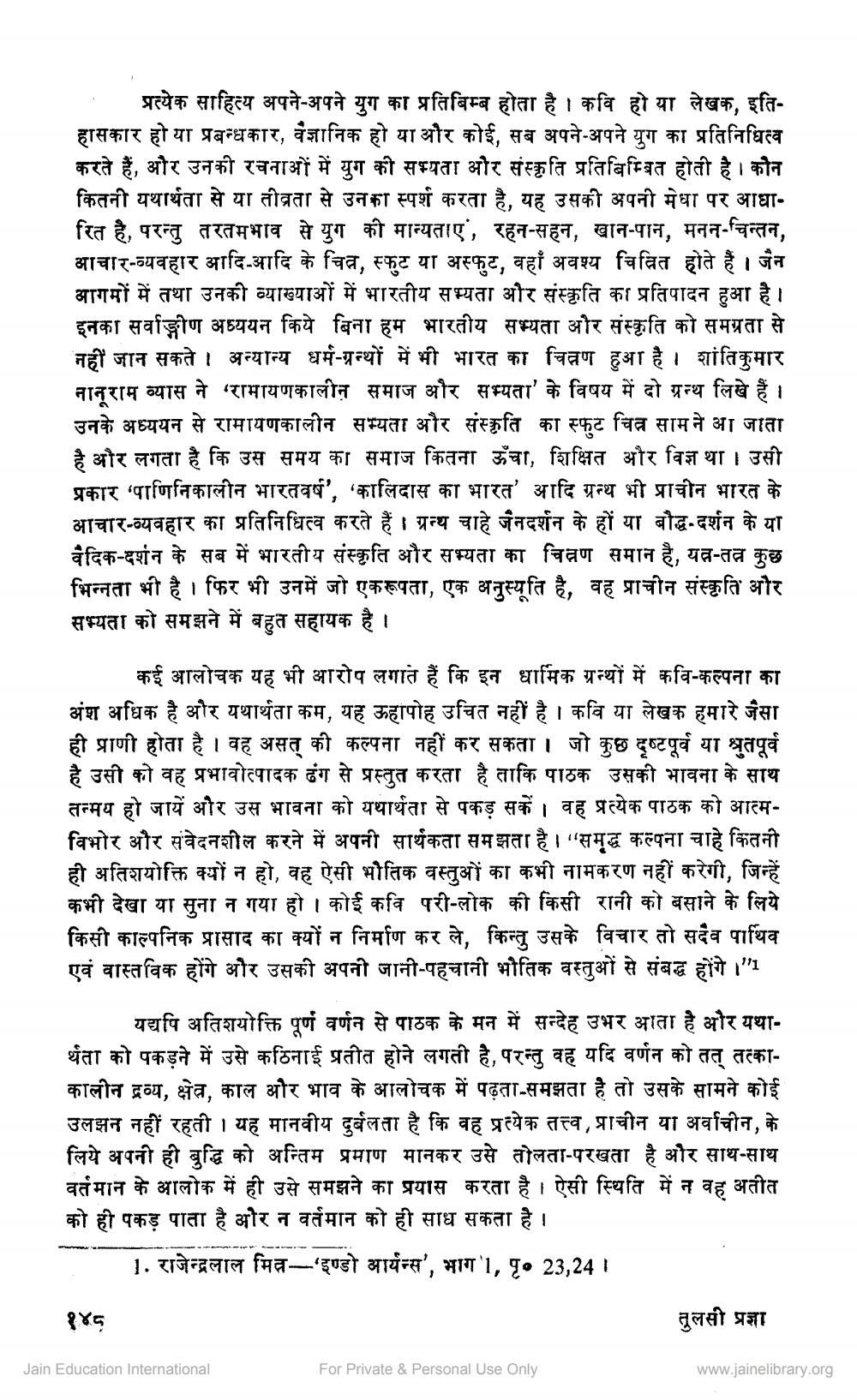________________
- प्रत्येक साहित्य अपने-अपने युग का प्रतिबिम्ब होता है । कवि हो या लेखक, इतिहासकार हो या प्रबन्धकार, वैज्ञानिक हो या और कोई, सब अपने-अपने युग का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनकी रचनाओं में युग की सभ्यता और संस्कृति प्रतिबिम्बित होती है। कौन कितनी यथार्थता से या तीव्रता से उनका स्पर्श करता है, यह उसकी अपनी मेधा पर आधारित है, परन्तु तरतमभाव से युग की मान्यताएं, रहन-सहन, खान-पान, मनन-चिन्तन, आचार-व्यवहार आदि-आदि के चित्र, स्फुट या अस्फुट, वहाँ अवश्य चित्रित होते हैं । जैन आगमों में तथा उनकी व्याख्याओं में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रतिपादन हुआ है। इनका सर्वाङ्गीण अध्ययन किये बिना हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समग्रता से नहीं जान सकते। अन्यान्य धर्म-ग्रन्थों में भी भारत का चित्रण हुआ है। शांतिकुमार नानूराम व्यास ने 'रामायणकालीन समाज और सभ्यता' के विषय में दो ग्रन्थ लिखे हैं । उनके अध्ययन से रामायणकालीन सभ्यता और संस्कृति का स्फुट चित्र सामने आ जाता है और लगता है कि उस समय का समाज कितना ऊँचा, शिक्षित और विज्ञ था। उसी प्रकार पाणिनिकालीन भारतवर्ष', 'कालिदास का भारत' आदि ग्रन्थ भी प्राचीन भारत के आचार-व्यवहार का प्रतिनिधित्व करते हैं । ग्रन्थ चाहे जनदर्शन के हों या बौद्ध दर्शन के या वैदिक-दर्शन के सब में भारतीय संस्कृति और सभ्यता का चित्रण समान है, यत्र-तत्र कुछ भिन्नता भी है । फिर भी उनमें जो एकरूपता, एक अनुस्यूति है, वह प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को समझने में बहुत सहायक है।
कई आलोचक यह भी आरोप लगाते हैं कि इन धार्मिक ग्रन्थों में कवि-कल्पना का अंश अधिक है और यथार्थता कम, यह ऊहापोह उचित नहीं है । कवि या लेखक हमारे जैसा ही प्राणी होता है। वह असत की कल्पना नहीं कर सकता। जो कुछ दृष्टपूर्व या श्रुतपूर्व है उसी को वह प्रभावोत्पादक ढंग से प्रस्तुत करता है ताकि पाठक उसकी भावना के साथ तन्मय हो जायें और उस भावना को यथार्थता से पकड़ सकें। वह प्रत्येक पाठक को आत्मविभोर और संवेदनशील करने में अपनी सार्थकता समझता है । “समृद्ध कल्पना चाहे कितनी ही अतिशयोक्ति क्यों न हो, वह ऐसी भौतिक वस्तुओं का कभी नामकरण नहीं करेगी, जिन्हें कभी देखा या सुना न गया हो । कोई कवि परी-लोक की किसी रानी को बसाने के लिये किसी काल्पनिक प्रासाद का क्यों न निर्माण कर ले, किन्तु उसके विचार तो सदैव पार्थिव एवं वास्तविक होंगे और उसकी अपनी जानी-पहचानी भौतिक वस्तुओं से संबद्ध होंगे।"
यद्यपि अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन से पाठक के मन में सन्देह उभर आता है और यथार्थता को पकड़ने में उसे कठिनाई प्रतीत होने लगती है, परन्तु वह यदि वर्णन को तत् तत्काकालीन द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के आलोचक में पढ़ता-समझता है तो उसके सामने कोई उलझन नहीं रहती । यह मानवीय दुर्बलता है कि वह प्रत्येक तत्त्व, प्राचीन या अर्वाचीन, के लिये अपनी ही बुद्धि को अन्तिम प्रमाण मानकर उसे तोलता-परखता है और साथ-साथ वर्तमान के आलोक में ही उसे समझने का प्रयास करता है। ऐसी स्थिति में न वह अतीत को ही पकड़ पाता है और न वर्तमान को ही साध सकता है।
1. राजेन्द्रलाल मित्र-'इण्डो आर्यन्स', भाग'1, पृ० 23,24।
१४८
तुलसी प्रज्ञा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org