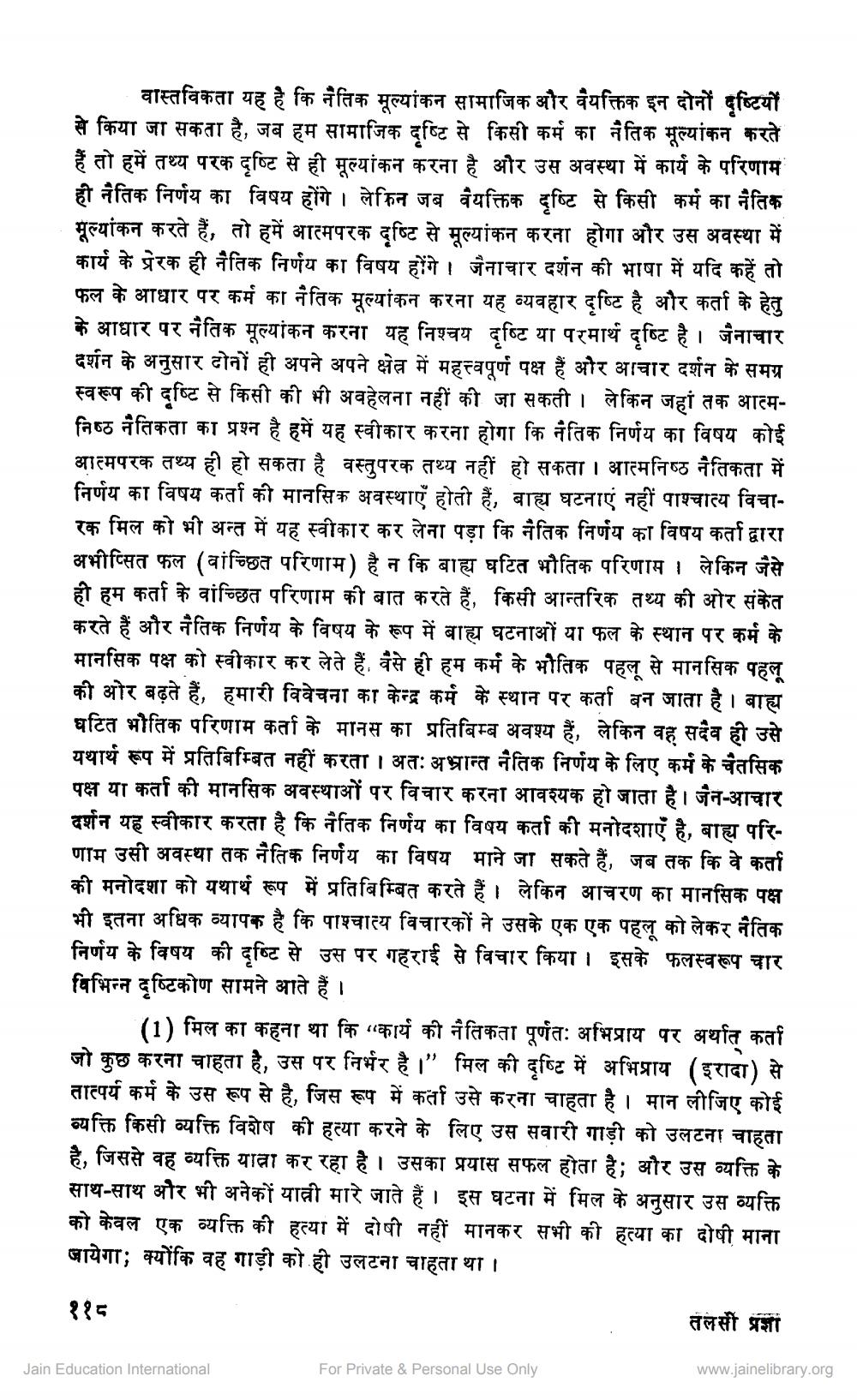________________
वास्तविकता यह है कि नैतिक मूल्यांकन सामाजिक और वैयक्तिक इन दोनों दृष्टियों से किया जा सकता है, जब हम सामाजिक दृष्टि से किसी कर्म का नैतिक मूल्यांकन करते हैं तो हमें तथ्य परक दृष्टि से ही मूल्यांकन करना है और उस अवस्था में कार्य के परिणाम ही नैतिक निर्णय का विषय होंगे। लेकिन जब वैयक्तिक दृष्टि से किसी कर्म का नैतिक मूल्यांकन करते हैं, तो हमें आत्मपरक दृष्टि से मूल्यांकन करना होगा और उस अवस्था में कार्य के प्रेरक ही नैतिक निर्णय का विषय होंगे। जैनाचार दर्शन की भाषा में यदि कहें तो फल के आधार पर कर्म का नैतिक मूल्यांकन करना यह व्यवहार दृष्टि है और कर्ता के हेतु के आधार पर नैतिक मूल्यांकन करना यह निश्चय दृष्टि या परमार्थ दृष्टि है। जैनाचार दर्शन के अनुसार दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं और आचार दर्शन के समग्र स्वरूप की दृष्टि से किसी की भी अवहेलना नहीं की जा सकती। लेकिन जहां तक आत्मनिष्ठ नैतिकता का प्रश्न है हमें यह स्वीकार करना होगा कि नैतिक निर्णय का विषय कोई आत्मपरक तथ्य ही हो सकता है वस्तुपरक तथ्य नहीं हो सकता । आत्मनिष्ठ नैतिकता में निर्णय का विषय कर्ता की मानसिक अवस्थाएँ होती हैं, बाह्य घटनाएं नहीं पाश्चात्य विचारक मिल को भी अन्त में यह स्वीकार कर लेना पड़ा कि नैतिक निर्णय का विषय कर्ता द्वारा अभीप्सित फल (वांच्छित परिणाम) है न कि बाह्य घटित भौतिक परिणाम । लेकिन जैसे ही हम कर्ता के वांच्छित परिणाम की बात करते हैं, किसी आन्तरिक तथ्य की ओर संकेत करते हैं और नैतिक निर्णय के विषय के रूप में बाह्य घटनाओं या फल के स्थान पर कर्म के मानसिक पक्ष को स्वीकार कर लेते हैं. वैसे ही हम कर्म के भौतिक पहलू से मानसिक पहलू की ओर बढ़ते हैं, हमारी विवेचना का केन्द्र कर्म के स्थान पर कर्ता बन जाता है। बाह्य घटित भौतिक परिणाम कर्ता के मानस का प्रतिबिम्ब अवश्य हैं, लेकिन वह सदैव ही उसे यथार्थ रूप में प्रतिबिम्बित नहीं करता। अतः अभ्रान्त नैतिक निर्णय के लिए कर्म के चैतसिक पक्ष या कर्ता की मानसिक अवस्थाओं पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। जैन-आचार दर्शन यह स्वीकार करता है कि नैतिक निर्णय का विषय कर्ता की मनोदशाएं है, बाह्य परिणाम उसी अवस्था तक नैतिक निर्णय का विषय माने जा सकते हैं, जब तक कि वे कर्ता की मनोदशा को यथार्थ रूप में प्रतिबिम्बित करते हैं। लेकिन आचरण का मानसिक पक्ष भी इतना अधिक व्यापक है कि पाश्चात्य विचारकों ने उसके एक एक पहलू को लेकर नैतिक निर्णय के विषय की दृष्टि से उस पर गहराई से विचार किया। इसके फलस्वरूप चार विभिन्न दृष्टिकोण सामने आते हैं ।
(1) मिल का कहना था कि “कार्य की नैतिकता पूर्णतः अभिप्राय पर अर्थात कर्ता जो कुछ करना चाहता है, उस पर निर्भर है।" मिल की दृष्टि में अभिप्राय (इरादा) से तात्पर्य कर्म के उस रूप से है, जिस रूप में कर्ता उसे करना चाहता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष की हत्या करने के लिए उस सवारी गाड़ी को उलटना चाहता है, जिससे वह व्यक्ति यात्रा कर रहा है। उसका प्रयास सफल होता है; और उस व्यक्ति के साथ-साथ और भी अनेकों यात्री मारे जाते हैं। इस घटना में मिल के अनुसार उस व्यक्ति को केवल एक व्यक्ति की हत्या में दोषी नहीं मानकर सभी की हत्या का दोषी माना जायेगा; क्योंकि वह गाड़ी को ही उलटना चाहता था।
तलसी प्रज्ञा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org