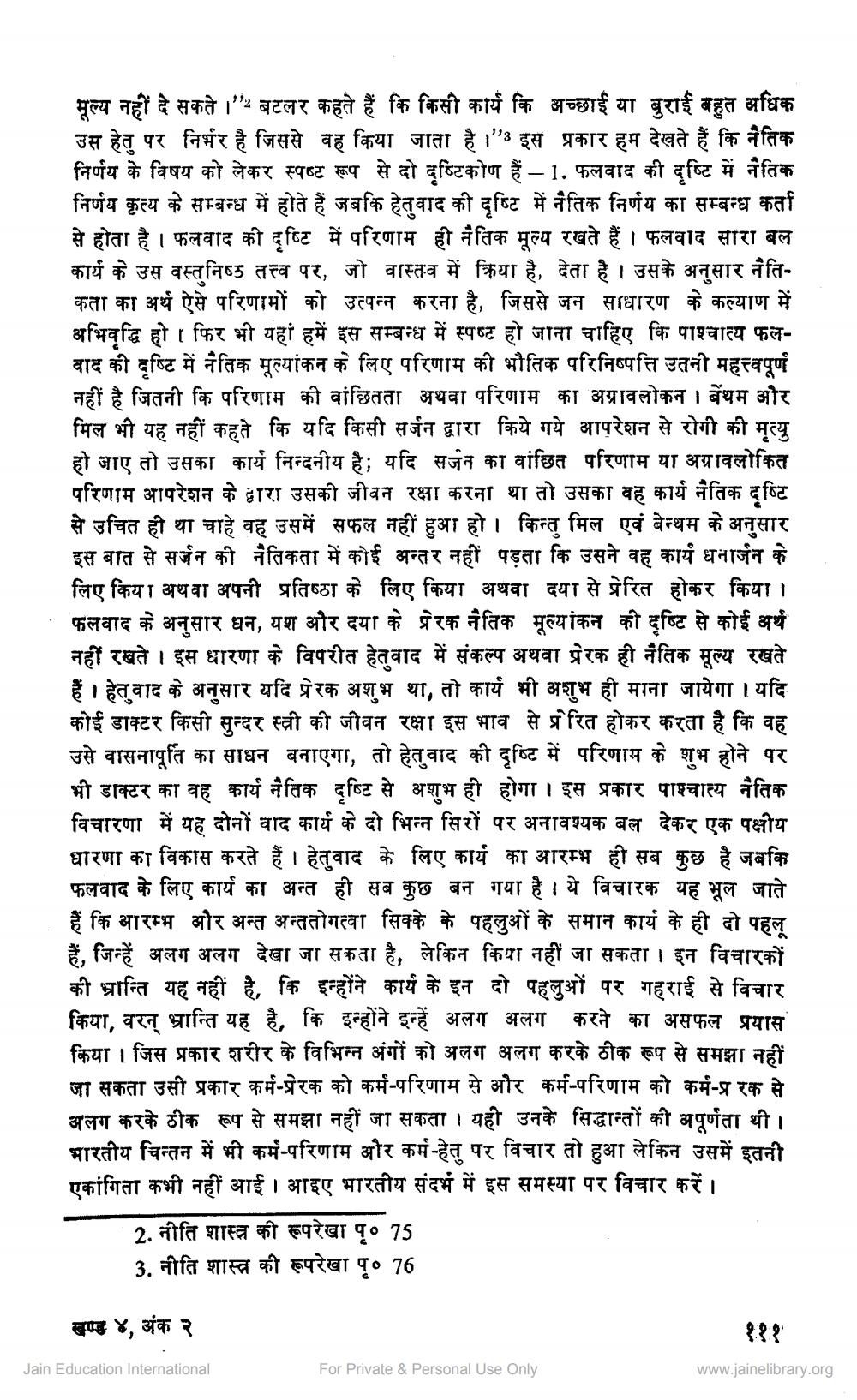________________
मूल्य नहीं दे सकते ।"2 बटलर कहते हैं कि किसी कार्य कि अच्छाई या बुराई बहुत अधिक उस हेतु पर निर्भर है जिससे वह किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नैतिक निर्णय के विषय को लेकर स्पष्ट रूप से दो दृष्टिकोण हैं - 1. फलवाद की दृष्टि में नैतिक निर्णय कृत्य के सम्बन्ध में होते हैं जबकि हेतुवाद की दृष्टि में नैतिक निर्णय का सम्बन्ध कर्ता से होता है । फलवाद की दृष्टि में परिणाम ही नैतिक मूल्य रखते हैं । फलवाद सारा बल कार्य के उस वस्तुनिष्ठ तत्त्व पर, जो वास्तव में क्रिया है, देता है । उसके अनुसार नैतिकता का अर्थ ऐसे परिणामों को उत्पन्न करना है, जिससे जन साधारण के कल्याण में अभिवृद्धि हो । फिर भी यहां हमें इस सम्बन्ध में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पाश्चात्य फलवाद की दृष्टि में नैतिक मूल्यांकन के लिए परिणाम की भौतिक परिनिष्पत्ति उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है जितनी कि परिणाम की वांछितता अथवा परिणाम का अग्रावलोकन । बेंथम और मिल भी यह नहीं कहते कि यदि किसी सर्जन द्वारा किये गये आपरेशन से रोगी की मृत्यु हो जाए तो उसका कार्य निन्दनीय है; यदि सर्जन का वांछित परिणाम या अग्रावलोकित परिणाम आपरेशन के द्वारा उसकी जीवन रक्षा करना था तो उसका वह कार्य नैतिक दृष्टि से उचित ही था चाहे वह उसमें सफल नहीं हुआ हो। किन्तु मिल एवं बेन्थम के अनुसार इस बात से सर्जन की नैतिकता में कोई अन्तर नहीं पड़ता कि उसने वह कार्य धनार्जन के लिए किया अथवा अपनी प्रतिष्ठा के लिए किया अथवा दया से प्रेरित होकर किया। फलवाद के अनुसार धन, यश और दया के प्रेरक नैतिक मूल्यांकन की दृष्टि से कोई अर्थ नहीं रखते । इस धारणा के विपरीत हेतुवाद में संकल्प अथवा प्रेरक ही नैतिक मूल्य रखते हैं । हेतुवाद के अनुसार यदि प्रेरक अशुभ था, तो कार्य भी अशुभ ही माना जायेगा । यदि कोई डाक्टर किसी सुन्दर स्त्री की जीवन रक्षा इस भाव से प्रेरित होकर करता है कि वह उसे वासनापूर्ति का साधन बनाएगा, तो हेतुवाद की दृष्टि में परिणाम के शुभ होने पर भी डाक्टर का वह कार्य नैतिक दृष्टि से अशुभ ही होगा। इस प्रकार पाश्चात्य नैतिक विचारणा में यह दोनों वाद कार्य के दो भिन्न सिरों पर अनावश्यक बल देकर एक पक्षीय धारणा का विकास करते हैं । हेतुवाद के लिए कार्य का आरम्भ ही सब कुछ है जबकि फलवाद के लिए कार्य का अन्त ही सब कुछ बन गया है । ये विचारक यह भूल जाते हैं कि आरम्भ और अन्त अन्ततोगत्वा सिक्के के पहलुओं के समान कार्य के ही दो पहल हैं, जिन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, लेकिन किया नहीं जा सकता। इन विचारकों की भ्रान्ति यह नहीं है, कि इन्होंने कार्य के इन दो पहलुओं पर गहराई से विचार किया, वरन् भ्रान्ति यह है, कि इन्होंने इन्हें अलग अलग करने का असफल प्रयास किया। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों को अलग अलग करके ठीक रूप से समझा नहीं जा सकता उसी प्रकार कर्म-प्रेरक को कर्म-परिणाम से और कर्म-परिणाम को कर्म-प्ररक से अलग करके ठीक रूप से समझा नहीं जा सकता । यही उनके सिद्धान्तों की अपूर्णता थी। भारतीय चिन्तन में भी कर्म-परिणाम और कर्म-हेतु पर विचार तो हुआ लेकिन उसमें इतनी एकांगिता कभी नहीं आई। आइए भारतीय संदर्भ में इस समस्या पर विचार करें।
2. नीति शास्त्र की रूपरेखा पृ० 75 3. नीति शास्त्र की रूपरेखा पृ० 76
खण्ड ४, अंक २
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org