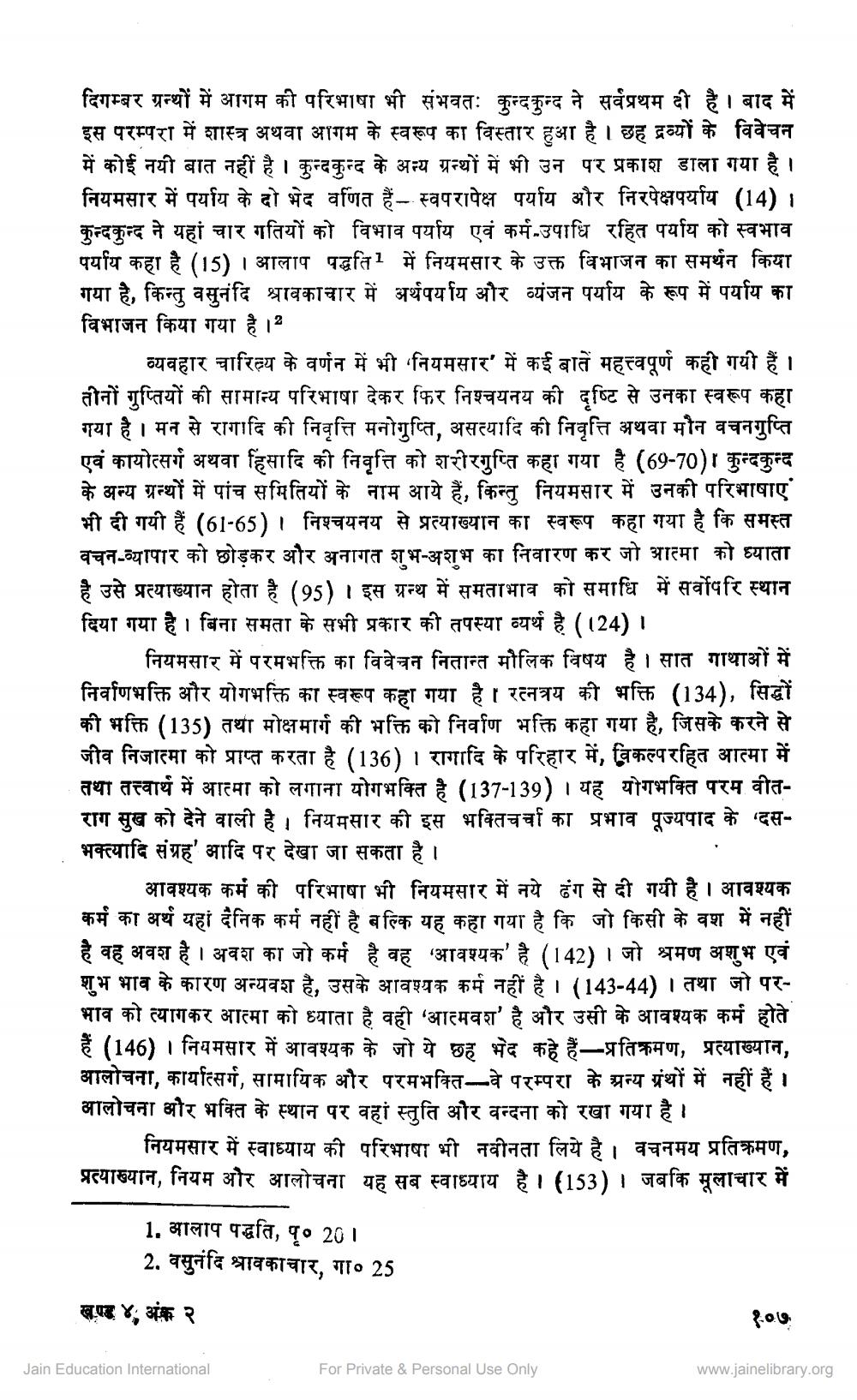________________
दिगम्बर ग्रन्थों में आगम की परिभाषा भी संभवतः कुन्दकुन्द ने सर्वप्रथम दी है। बाद में इस परम्परा में शास्त्र अथवा आगम के स्वरूप का विस्तार हुआ है । छह द्रव्यों के विवेचन में कोई नयी बात नहीं है । कुन्दकुन्द के अन्य ग्रन्थों में भी उन पर प्रकाश डाला गया है। नियमसार में पर्याय के दो भेद वणित हैं- स्वपरापेक्ष पर्याय और निरपेक्षपर्याय (14)। कुन्दकुन्द ने यहां चार गतियों को विभाव पर्याय एवं कर्म-उपाधि रहित पर्याय को स्वभाव पर्याय कहा है (15) । आलाप पद्धति में नियमसार के उक्त विभाजन का समर्थन किया गया है, किन्तु वसुनंदि श्रावकाचार में अर्थपर्याय और व्यंजन पर्याय के रूप में पर्याय का विभाजन किया गया है।
व्यवहार चारित्र्य के वर्णन में भी नियमसार' में कई बातें महत्त्वपूर्ण कही गयी हैं । तीनों गुप्तियों की सामान्य परिभाषा देकर फिर निश्चयनय की दृष्टि से उनका स्वरूप कहा गया है । मन से रागादि की निवृत्ति मनोगुप्ति, असत्यादि की निवृत्ति अथवा मौन वचनगुप्ति एवं कायोत्सर्ग अथवा हिंसादि की निवृत्ति को शरीरगुप्ति कहा गया है (69-70) कुन्दकुन्द के अन्य ग्रन्थों में पांच समितियों के नाम आये हैं, किन्तु नियमसार में उनकी परिभाषाएं भी दी गयी हैं (61-65)। निश्चयनय से प्रत्याख्यान का स्वरूप कहा गया है कि समस्त वचन-व्यापार को छोड़कर और अनागत शुभ-अशुभ का निवारण कर जो आत्मा को ध्याता है उसे प्रत्याख्यान होता है (95) । इस ग्रन्थ में समताभाव को समाधि में सर्वोपरि स्थान दिया गया है। बिना समता के सभी प्रकार की तपस्या व्यर्थ है (124)।
नियमसार में परमभक्ति का विवेचन नितान्त मौलिक विषय है। सात गाथाओं में निर्वाणभक्ति और योगभक्ति का स्वरूप कहा गया है। रत्नत्रय की भक्ति (134), सिद्धों की भक्ति (135) तथा मोक्षमार्ग की भक्ति को निर्वाण भक्ति कहा गया है, जिसके करने से जीव निजात्मा को प्राप्त करता है (136) । रागादि के परिहार में, विकल्परहित आत्मा में तथा तत्त्वार्थ में आत्मा को लगाना योगभक्ति है (137-139) । यह योगभक्ति परम वीतराग सुख को देने वाली है। नियमसार की इस भक्तिचर्चा का प्रभाव पूज्यपाद के 'दसभक्त्यादि संग्रह' आदि पर देखा जा सकता है।
आवश्यक कर्म की परिभाषा भी नियमसार में नये ढंग से दी गयी है । आवश्यक कर्म का अर्थ यहां दैनिक कर्म नहीं है बल्कि यह कहा गया है कि जो किसी के वश में नहीं है वह अवश है । अवश का जो कर्म है वह 'आवश्यक' है (142)। जो श्रमण अशुभ एवं शुभ भाव के कारण अन्यवश है, उसके आवश्यक कर्म नहीं है । (143-44) । तथा जो परभाव को त्यागकर आत्मा को ध्याता है वही 'आत्मवश' है और उसी के आवश्यक कर्म होते हैं (146) । नियमसार में आवश्यक के जो ये छह भेद कहे हैं-प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, कार्यात्सर्ग, सामायिक और परमभक्ति-वे परम्परा के अन्य ग्रंथों में नहीं हैं। आलोचना और भक्ति के स्थान पर वहां स्तुति और वन्दना को रखा गया है।
नियमसार में स्वाध्याय की परिभाषा भी नवीनता लिये है। वचनमय प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, नियम और आलोचना यह सब स्वाध्याय है। (153)। जबकि मूलाचार में
1. आलाप पद्धति, पृ० 20।
2. वसुनंदि श्रावकाचार, गा० 25 खण्ड ४, अंक २
१०७
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org