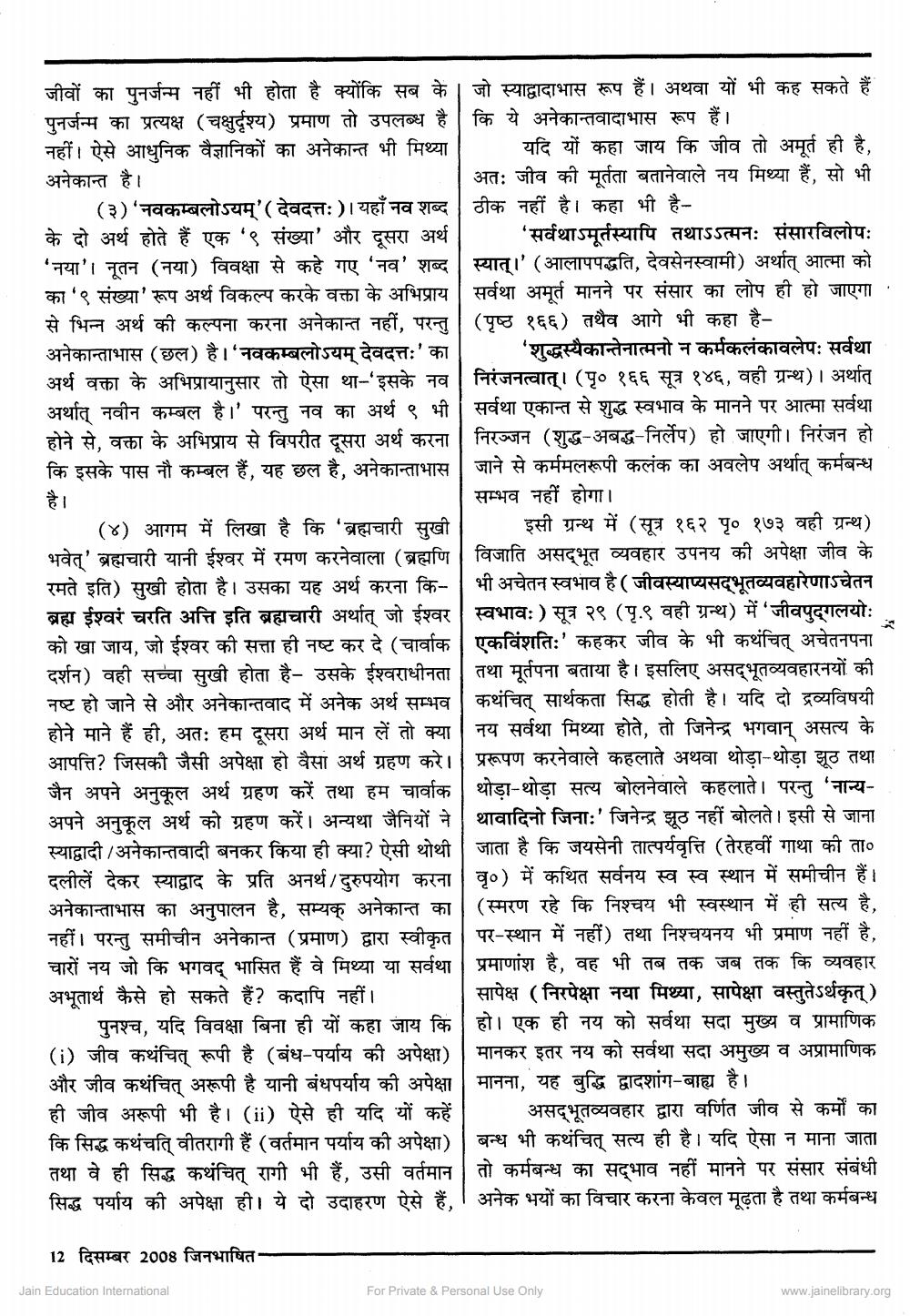________________
जीवों का पुनर्जन्म नहीं भी होता है क्योंकि सब के | जो स्याद्वादाभास रूप हैं। अथवा यों भी कह सकते हैं पुनर्जन्म का प्रत्यक्ष (चक्षुर्दृश्य) प्रमाण तो उपलब्ध है | कि ये अनेकान्तवादाभास रूप हैं। नहीं। ऐसे आधुनिक वैज्ञानिकों का अनेकान्त भी मिथ्या | यदि यों कहा जाय कि जीव तो अमूर्त ही है, अनेकान्त है।
अतः जीव की मूर्तता बतानेवाले नय मिथ्या हैं, सो भी (३) 'नवकम्बलोऽयम्' (देवदत्तः)। यहाँ नव शब्द | ठीक नहीं है। कहा भी हैके दो अर्थ होते हैं एक '९ संख्या' और दूसरा अर्थ 'सर्वथाऽमूर्तस्यापि तथाऽऽत्मनः संसारविलोपः 'नया'। नूतन (नया) विवक्षा से कहे गए 'नव' शब्द | स्यात्।' (आलापपद्धति, देवसेनस्वामी) अर्थात् आत्मा को का '९ संख्या' रूप अर्थ विकल्प करके वक्ता के अभिप्राय | सर्वथा अमूर्त मानने पर संसार का लोप ही हो जाएगा .. से भिन्न अर्थ की कल्पना करना अनेकान्त नहीं, परन्तु | | (पृष्ठ १६६) तथैव आगे भी कहा हैअनेकान्ताभास (छल) है। 'नवकम्बलोऽयम् देवदत्तः' का 'शुद्धस्यैकान्तेनात्मनो न कर्मकलंकावलेपः सर्वथा अर्थ वक्ता के अभिप्रायानुसार तो ऐसा था-'इसके नव | निरंजनत्वात्। (पृ० १६६ सूत्र १४६, वही ग्रन्थ)। अर्थात् अर्थात् नवीन कम्बल है।' परन्तु नव का अर्थ ९ भी | सर्वथा एकान्त से शुद्ध स्वभाव के मानने पर आत्मा सर्वथा होने से, वक्ता के अभिप्राय से विपरीत दूसरा अर्थ करना निरञ्जन (शुद्ध-अबद्ध-निर्लेप) हो जाएगी। निरंजन हो कि इसके पास नौ कम्बल हैं, यह छल है, अनेकान्ताभास | जाने से कर्ममलरूपी कलंक का अवलेप अर्थात् कर्मबन्ध
सम्भव नहीं होगा। (४) आगम में लिखा है कि 'ब्रह्मचारी सुखी इसी ग्रन्थ में (सूत्र १६२ पृ० १७३ वही ग्रन्थ) भवेत्' ब्रह्मचारी यानी ईश्वर में रमण करनेवाला (ब्रह्मणि | विजाति असद्भूत व्यवहार उपनय की अपेक्षा जीव के रमते इति) सुखी होता है। उसका यह अर्थ करना कि- | भी अचेतन स्वभाव है (जीवस्याप्यसद्भूतव्यवहारेणाऽचेतन ब्रह्म ईश्वरं चरति अत्ति इति ब्रह्मचारी
स्वभावः) सूत्र २९ (पृ.९ वही ग्रन्थ) में 'जीवपुद्गलयोः . को खा जाय, जो ईश्वर की सत्ता ही नष्ट कर दे (चार्वाक | एकविंशतिः' कहकर जीव के भी कथंचित् अचेतनपना दर्शन) वही सच्चा सुखी होता है- उसके ईश्वराधीनता | तथा मूर्तपना बताया है। इसलिए असद्भूतव्यवहारनयों की नष्ट हो जाने से और अनेकान्तवाद में अनेक अर्थ सम्भव | कथंचित् सार्थकता सिद्ध होती है। यदि दो द्रव्यविषयी होने माने हैं ही, अतः हम दूसरा अर्थ मान लें तो क्या | नय सर्वथा मिथ्या होते, तो जिनेन्द्र भगवान् असत्य के आपत्ति? जिसकी जैसी अपेक्षा हो वैसा अर्थ ग्रहण करे। प्ररूपण करनेवाले कहलाते अथवा थोड़ा-थोड़ा झूठ तथा जैन अपने अनुकूल अर्थ ग्रहण करें तथा हम चार्वाक | थोड़ा-थोड़ा सत्य बोलनेवाले कहलाते। परन्तु 'नान्यअपने अनुकूल अर्थ को ग्रहण करें। अन्यथा जैनियों ने | थावादिनो जिनाः' जिनेन्द्र झूठ नहीं बोलते। इसी से जाना स्याद्वादी /अनेकान्तवादी बनकर किया ही क्या? ऐसी थोथी | जाता है कि जयसेनी तात्पर्यवृत्ति (तेरहवीं गाथा की ता० दलीलें देकर स्याद्वाद के प्रति अनर्थ / दुरुपयोग करना | वृ०) में कथित सर्वनय स्व स्व स्थान में समीचीन हैं। अनेकान्ताभास का अनुपालन है, सम्यक अनेकान्त का (स्मरण रहे कि निश्चय भी स्वस्थान में ही सत्य है, नहीं। परन्तु समीचीन अनेकान्त (प्रमाण) द्वारा स्वीकृत | पर-स्थान में नहीं) तथा निश्चयनय भी प्रमाण नहीं है, चारों नय जो कि भगवद् भासित हैं वे मिथ्या या सर्वथा | प्रमाणांश है, वह भी तब तक जब तक कि व्यवहार अभूतार्थ कैसे हो सकते हैं? कदापि नहीं।
सापेक्ष (निरपेक्षा नया मिथ्या, सापेक्षा वस्तुतेऽर्थकृत्) पुनश्च, यदि विवक्षा बिना ही यों कहा जाय कि हो। एक ही नय को सर्वथा सदा मुख्य व प्रामाणिक (i) जीव कथंचित् रूपी है (बंध-पर्याय की अपेक्षा) | मानकर इतर नय को सर्वथा सदा अमुख्य व अप्रामाणिक
और जीव कथंचित अरूपी है यानी बंधपर्याय की अपेक्षा। मानना, यह बुद्धि द्वादशांग-बाह्य है। ही जीव अरूपी भी है। (ii) ऐसे ही यदि यों कहें | असद्भूतव्यवहार द्वारा वर्णित जीव से कर्मों का कि सिद्ध कथंचति वीतरागी हैं (वर्तमान पर्याय की अपेक्षा) | बन्ध भी कथंचित् सत्य ही है। यदि ऐसा न माना जाता तथा वे ही सिद्ध कथंचित् रागी भी हैं, उसी वर्तमान | तो कर्मबन्ध का सद्भाव नहीं मानने पर संसार संबंधी सिद्ध पर्याय की अपेक्षा ही। ये दो उदाहरण ऐसे हैं, | अनेक भयों का विचार करना केवल मूढ़ता है तथा कर्मबन्ध
12 दिसम्बर 2008 जिनभाषित
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org