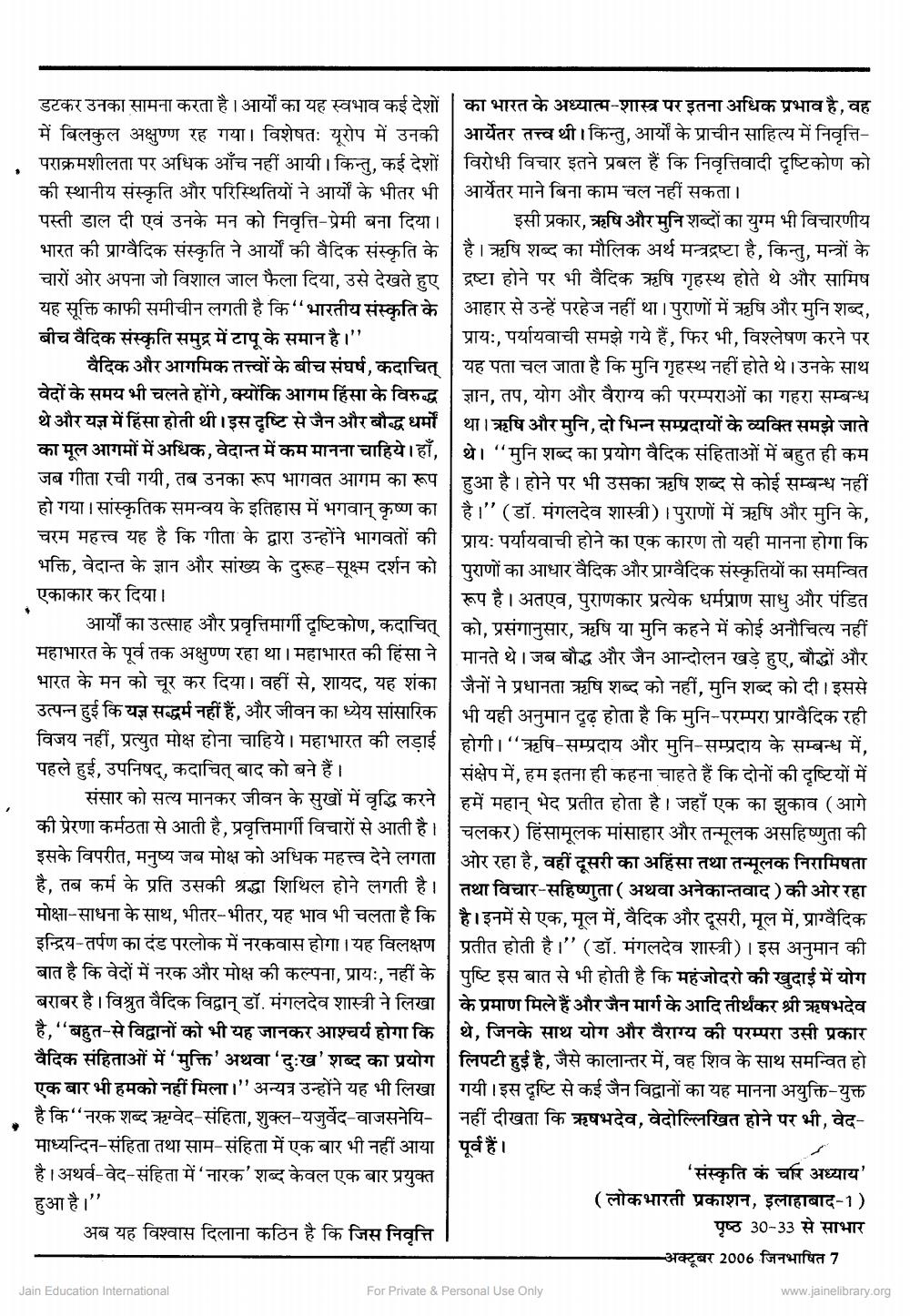________________
"
.
$
डटकर उनका सामना करता है। आर्यों का यह स्वभाव कई देशों में बिलकुल अक्षुण्ण रह गया । विशेषतः यूरोप में उनकी पराक्रमशीलता पर अधिक आँच नहीं आयी। किन्तु, कई देशों की स्थानीय संस्कृति और परिस्थितियों ने आर्यों के भीतर भी पस्ती डाल दी एवं उनके मन को निवृत्ति प्रेमी बना दिया । भारत की प्राग्वैदिक संस्कृति ने आर्यों की वैदिक संस्कृति के चारों ओर अपना जो विशाल जाल फैला दिया, उसे देखते हुए यह सूक्ति काफी समीचीन लगती है कि "भारतीय संस्कृति के
वैदिक संस्कृति समुद्र में टापू के समान है।"
वैदिक और आगमिक तत्त्वों के बीच संघर्ष, कदाचित् वेदों के समय भी चलते होंगे, क्योंकि आगम हिंसा के विरुद्ध थे और यज्ञ में हिंसा होती थी। इस दृष्टि से जैन और बौद्ध धर्मों का मूल आगमों में अधिक, वेदान्त में कम मानना चाहिये । हाँ, जब गीता रची गयी, तब उनका रूप भागवत आगम का रूप हो गया। सांस्कृतिक समन्वय के इतिहास में भगवान् कृष्ण का चरम महत्त्व यह है कि गीता के द्वारा उन्होंने भागवतों की भक्ति, वेदान्त के ज्ञान और सांख्य के दुरूह - सूक्ष्म दर्शन को एकाकार कर दिया।
आर्यों का उत्साह और प्रवृत्तिमार्गी दृष्टिकोण, कदाचित् महाभारत के पूर्व तक अक्षुण्ण रहा था। महाभारत की हिंसा ने भारत के मन को चूर कर दिया। वहीं से, शायद, यह शंका उत्पन्न हुई कि यज्ञ सद्धर्म नहीं हैं, और जीवन का ध्येय सांसारिक विजय नहीं, प्रत्युत मोक्ष होना चाहिये। महाभारत की लड़ाई पहले हुई, उपनिषद्, कदाचित् बाद को बने हैं।
संसार को सत्य मानकर जीवन के सुखों में वृद्धि करने की प्रेरणा कर्मठता से आती है, प्रवृत्तिमार्गी विचारों से आती है। इसके विपरीत, मनुष्य जब मोक्ष को अधिक महत्त्व देने लगता है, तब कर्म के प्रति उसकी श्रद्धा शिथिल होने लगती है। मोक्षा - साधना के साथ, भीतर-भीतर, यह भाव भी चलता है कि इन्द्रिय-तर्पण का दंड परलोक में नरकवास होगा। यह विलक्षण बात है कि वेदों में नरक और मोक्ष की कल्पना, प्रायः, नहीं के बराबर है। विश्रुत वैदिक विद्वान् डॉ. मंगलदेव शास्त्री ने लिखा है, "बहुत-से विद्वानों को भी यह जानकर आश्चर्य होगा कि वैदिक संहिताओं में 'मुक्ति' अथवा 'दुःख' शब्द का प्रयोग एक बार भी हमको नहीं मिला।" अन्यत्र उन्होंने यह भी लिखा है कि " नरक शब्द ऋग्वेद संहिता, शुक्ल यजुर्वेद - वाजसनेयिमाध्यन्दिन - संहिता तथा साम-संहिता में एक बार भी नहीं आया है। अथर्ववेद संहिता में 'नारक' शब्द केवल एक बार प्रयुक्त हुआ है।"
अब यह विश्वास दिलाना कठिन है कि जिस निवृत्ति
Jain Education International
| का भारत के अध्यात्म-शास्त्र पर इतना अधिक प्रभाव है, वह आर्येतर तत्त्व थी। किन्तु, आर्यों के प्राचीन साहित्य में निवृत्तिविरोधी विचार इतने प्रबल हैं कि निवृत्तिवादी दृष्टिकोण को आर्येतर माने बिना काम चल नहीं सकता ।
इसी प्रकार, ऋषि और मुनि शब्दों का युग्म भी विचारणीय है । ऋषि शब्द का मौलिक अर्थ मन्त्रद्रष्टा है, किन्तु, मन्त्रों के द्रष्टा होने पर भी वैदिक ऋषि गृहस्थ होते थे और सामिष आहार से उन्हें परहेज नहीं था। पुराणों में ऋषि और मुनि शब्द, प्रायः, पर्यायवाची समझे गये हैं, फिर भी, विश्लेषण करने पर यह पता चल जाता है कि मुनि गृहस्थ नहीं होते थे। उनके साथ ज्ञान, तप, योग और वैराग्य की परम्पराओं का गहरा सम्बन्ध था। ऋषि और मुनि, दो भिन्न सम्प्रदायों के व्यक्ति समझे जाते थे । “मुनि शब्द का प्रयोग वैदिक संहिताओं में बहुत ही कम हुआ है। होने पर भी उसका ऋषि शब्द से कोई सम्बन्ध नहीं है।" (डॉ. मंगलदेव शास्त्री) । पुराणों में ऋषि और मुनि के, प्रायः पर्यायवाची होने का एक कारण तो यही मानना होगा कि पुराणों का आधार वैदिक और प्राग्वैदिक संस्कृतियों का समन्वित रूप है। अतएव, पुराणकार प्रत्येक धर्मप्राण साधु और पंडित को, प्रसंगानुसार, ऋषि या मुनि कहने में कोई अनौचित्य नहीं मानते थे । जब बौद्ध और जैन आन्दोलन खड़े हुए, बौद्धों और जैनों ने प्रधानता ऋषि शब्द को नहीं, मुनि शब्द को दी। इससे भी यही अनुमान दृढ़ होता है कि मुनि-परम्परा प्राग्वैदिक रही होगी। " ऋषि - सम्प्रदाय और मुनि-सम्प्रदाय के सम्बन्ध में, संक्षेप में, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि दोनों की दृष्टियों में हमें महान् भेद प्रतीत होता है। जहाँ एक का झुकाव (आगे चलकर) हिंसामूलक मांसाहार और तन्मूलक असहिष्णुता की ओर रहा है, वहीं दूसरी का अहिंसा तथा तन्मूलक निरामिषता तथा विचार सहिष्णुता ( अथवा अनेकान्तवाद) की ओर रहा है । इनमें से एक, मूल में, वैदिक और दूसरी, मूल में, प्राग्वैदिक प्रतीत होती है।" (डॉ. मंगलदेव शास्त्री) । इस अनुमान की पुष्टि इस बात से भी होती है कि महंजोदरो की खुदाई में योग के प्रमाण मिले हैं और जैन मार्ग के आदि तीर्थंकर श्री ऋषभदेव थे, जिनके साथ योग और वैराग्य की परम्परा उसी प्रकार लिपटी हुई है, जैसे कालान्तर में, वह शिव के साथ समन्वित हो गयी। इस दृष्टि से कई जैन विद्वानों का यह मानना अयुक्ति-युक्त नहीं दीखता कि ऋषभदेव, वेदोल्लिखित होने पर भी, वेदपूर्व हैं ।
For Private & Personal Use Only
'संस्कृति कं चरि अध्याय' ( लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद - 1 )
पृष्ठ 30-33 से साभार
-अक्टूबर 2006 जिनभाषित 7
www.jainelibrary.org