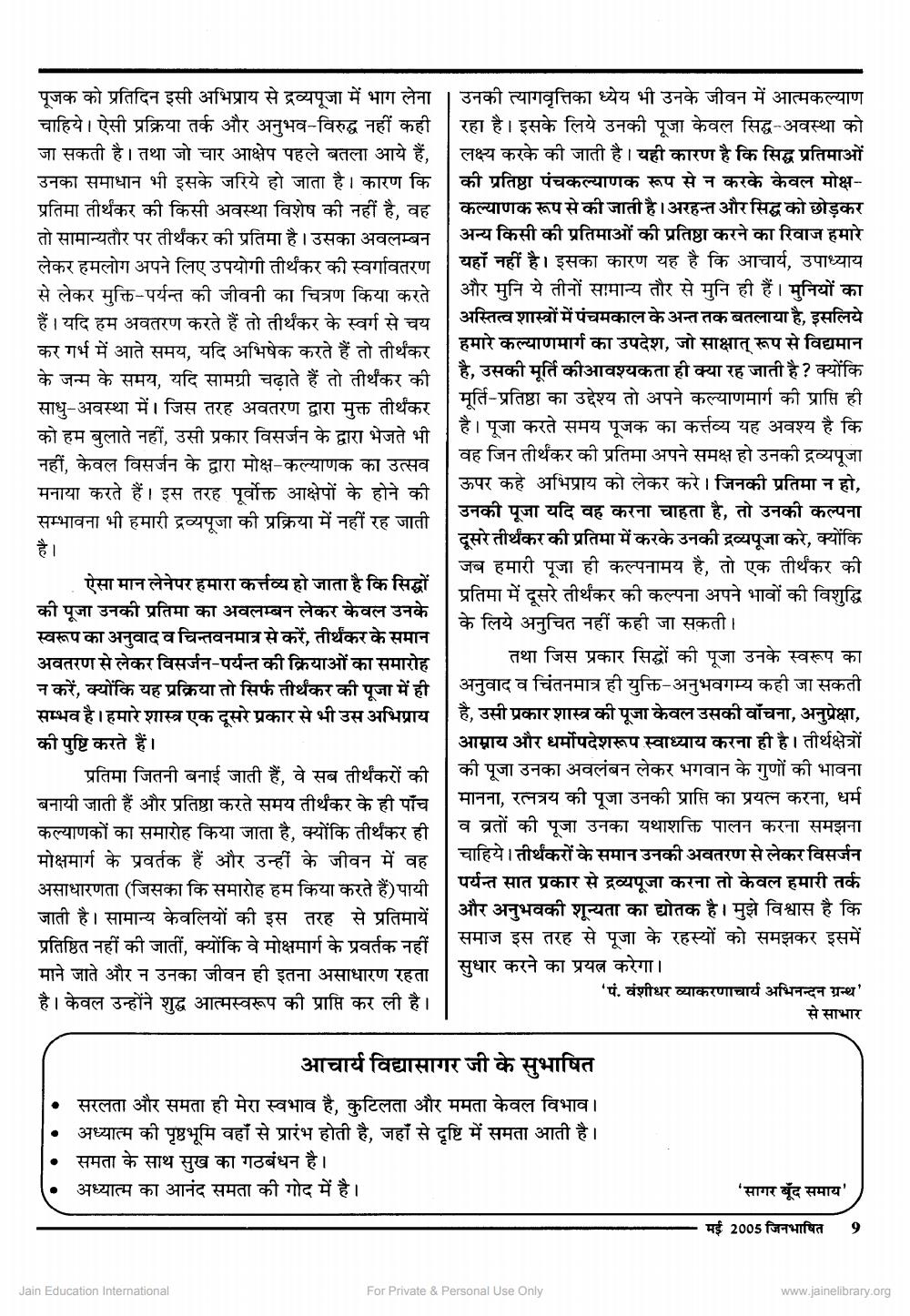________________
पूजक को प्रतिदिन इसी अभिप्राय से द्रव्यपूजा में भाग लेना चाहिये। ऐसी प्रक्रिया तर्क और अनुभव- विरुद्ध नहीं कही जा सकती है । तथा जो चार आक्षेप पहले बतला आये हैं, उनका समाधान भी इसके जरिये हो जाता है। कारण कि प्रतिमा तीर्थंकर की किसी अवस्था विशेष की नहीं है, वह तो सामान्यतौर पर तीर्थंकर की प्रतिमा है। उसका अवलम्बन लेकर हमलोग अपने लिए उपयोगी तीर्थंकर की स्वर्गावतरण से लेकर मुक्ति - पर्यन्त की जीवनी का चित्रण किया करते हैं। यदि हम अवतरण करते हैं तो तीर्थंकर के स्वर्ग से चय कर गर्भ में आते समय, यदि अभिषेक करते हैं तो तीर्थंकर
जन्म के समय, यदि सामग्री चढ़ाते हैं तो तीर्थंकर की साधु-अवस्था में। जिस तरह अवतरण द्वारा मुक्त तीर्थंकर को हम बुलाते नहीं, उसी प्रकार विसर्जन के द्वारा भेजते भी नहीं, केवल विसर्जन के द्वारा मोक्ष कल्याणक का उत्सव मनाया करते हैं । इस तरह पूर्वोक्त आक्षेपों के होने की सम्भावना भी हमारी द्रव्यपूजा की प्रक्रिया में नहीं रह जाती
है ।
ऐसा मान लेने पर हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि सिद्धों की पूजा उनकी प्रतिमा का अवलम्बन लेकर केवल उनके स्वरूप का अनुवाद व चिन्तवनमात्र से करें, तीर्थंकर के समान अवतरण से लेकर विसर्जन- पर्यन्त की क्रियाओं का समारोह न करें, क्योंकि यह प्रक्रिया तो सिर्फ तीर्थंकर की पूजा में ही सम्भव है। हमारे शास्त्र एक दूसरे प्रकार से भी उस अभिप्राय की पुष्टि करते हैं ।
प्रतिमा जितनी बनाई जाती हैं, वे सब तीर्थंकरों की बनायी जाती हैं और प्रतिष्ठा करते समय तीर्थंकर के ही पाँच कल्याणकों का समारोह किया जाता है, क्योंकि तीर्थंकर ही मोक्षमार्ग के प्रवर्तक हैं और उन्हीं के जीवन में वह असाधारणता (जिसका कि समारोह हम किया करते हैं) पायी जाती है। सामान्य केवलियों की इस तरह से प्रतिमायें प्रतिष्ठित नहीं की जातीं, क्योंकि वे मोक्षमार्ग के प्रवर्तक नहीं माने जाते और न उनका जीवन ही इतना असाधारण रहता है । केवल उन्होंने शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति कर ली है।
·
·
। उनकी त्यागवृत्तिका ध्येय भी उनके जीवन में आत्मकल्याण रहा है। इसके लिये उनकी पूजा केवल सिद्ध-अवस्था को लक्ष्य करके की जाती है। यही कारण है कि सिद्ध प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा पंचकल्याणक रूप से न करके केवल मोक्षकल्याणक रूप से की जाती है। अरहन्त और सिद्ध को छोड़कर अन्य किसी की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करने का रिवाज हमारे यहाँ नहीं है। इसका कारण यह है कि आचार्य, उपाध्याय और मुनि ये तीनों सामान्य तौर से मुनि ही हैं। मुनियों का अस्तित्व शास्त्रों में पंचमकाल के अन्त तक बतलाया है, इसलिये हमारे कल्याणमार्ग का उपदेश, जो साक्षात् रूप से विद्यमान है, उसकी मूर्ति की आवश्यकता ही क्या रह जाती है ? क्योंकि मूर्ति - प्रतिष्ठा का उद्देश्य तो अपने कल्याणमार्ग की प्राप्ति ही है। पूजा करते समय पूजक का कर्त्तव्य यह अवश्य है वह जिन तीर्थंकर की प्रतिमा अपने समक्ष हो उनकी द्रव्यपूजा ऊपर कहे अभिप्राय को लेकर करे। जिनकी प्रतिमा न हो, उनकी पूजा यदि वह करना चाहता है, तो उनकी कल्पना दूसरे तीर्थंकर की प्रतिमा में करके उनकी द्रव्यपूजा करे, क्योंकि जब हमारी पूजा ही कल्पनामय है, तो एक तीर्थंकर की प्रतिमा में दूसरे तीर्थंकर की कल्पना अपने भावों की विशुद्धि के लिये अनुचित नहीं कही जा सकती।
Jain Education International
तथा जिस प्रकार सिद्धों की पूजा उनके स्वरूप का अनुवाद व चिंतनमात्र ही युक्ति- अनुभवगम्य कही जा सकती है, उसी प्रकार शास्त्र की पूजा केवल उसकी वाँचना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेशरूप स्वाध्याय करना ही है। तीर्थक्षेत्रों की पूजा उनका अवलंबन लेकर भगवान के गुणों की भावना मानना, रत्नत्रय की पूजा उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करना, धर्म व व्रतों की पूजा उनका यथाशक्ति पालन करना समझना चाहिये। तीर्थंकरों के समान उनकी अवतरण से लेकर विसर्जन पर्यन्त सात प्रकार से द्रव्यपूजा करना तो केवल हमारी तर्क और अनुभवकी शून्यता का द्योतक है। मुझे विश्वास है कि समाज इस तरह से पूजा के रहस्यों को समझकर इसमें सुधार करने का प्रयत्न करेगा।
आचार्य विद्यासागर जी के सुभाषित
सरलता और समता ही मेरा स्वभाव है, कुटिलता और ममता केवल विभाव । अध्यात्म की पृष्ठभूमि वहाँ से प्रारंभ होती है, जहाँ से दृष्टि में समता आती है। समता के साथ सुख का गठबंधन है ।
अध्यात्म का आनंद समता की गोद में है ।
For Private & Personal Use Only
'पं. वंशीधर व्याकरणाचार्य अभिनन्दन ग्रन्थ ' से साभार
'सागर बूँद समाय'
मई 2005 जिनभाषित
9
www.jainelibrary.org