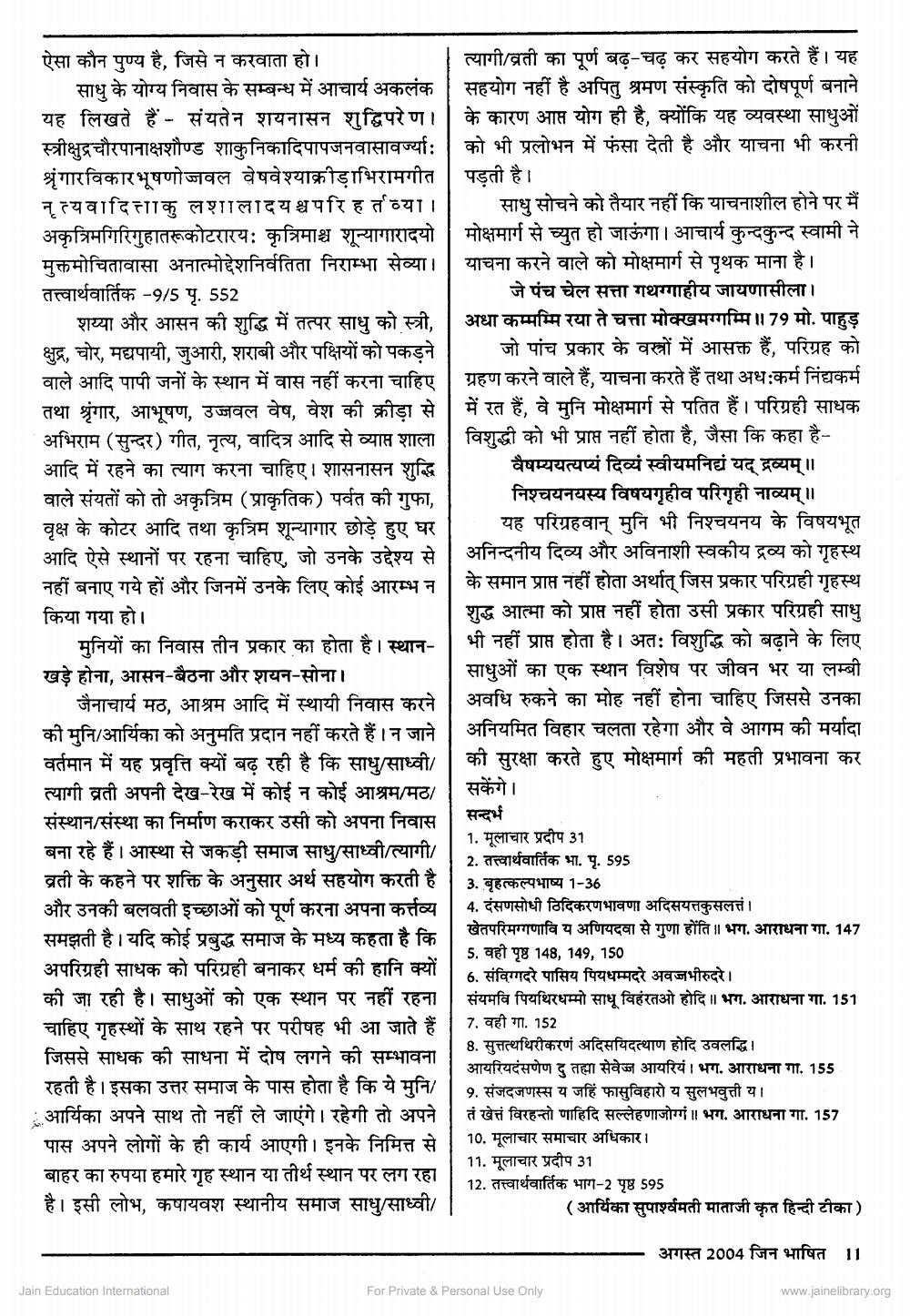________________
ऐसा कौन पुण्य है, जिसे न करवाता हो।
| त्यागी/व्रती का पूर्ण बढ़-चढ़ कर सहयोग करते हैं। यह ___ साधु के योग्य निवास के सम्बन्ध में आचार्य अकलंक | सहयोग नहीं है अपितु श्रमण संस्कृति को दोषपूर्ण बनाने यह लिखते हैं - संयतेन शयनासन शुद्धिपरे ण। | के कारण आप्त योग ही है, क्योंकि यह व्यवस्था साधुओं स्त्रीक्षुद्रचौरपानाक्षशौण्ड शाकुनिकादिपापजनवासावाः | को भी प्रलोभन में फंसा देती है और याचना भी करनी श्रृंगार विकार भूषणोज्जवल वेषवेश्याक्रीड़ाभिरामगीत | पड़ती है। नृत्य वादित्ता कु लशालादयश्च परि ह त व्या।। साधु सोचने को तैयार नहीं कि याचनाशील होने पर मैं अकृत्रिमगिरिगुहातरूकोटरारयः कृत्रिमाश्च शून्यागारादयो | मोक्षमार्ग से च्युत हो जाऊंगा। आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी ने मुक्तमोचितावासा अनात्मोद्देशनिर्वतिता निराम्भा सेव्या। | याचना करने वाले को मोक्षमार्ग से पृथक माना है। तत्त्वार्थवार्तिक -9/5 पृ. 552
जे पंच चेल सत्ता गथग्गाहीय जायणासीला। शय्या और आसन की शद्धि में तत्पर साधु को स्त्री, | अधा कम्मम्मि रया ते चत्ता मोक्खमग्गम्मि॥79 मो. पाहुड़ क्षुद्र, चोर, मद्यपायी, जुआरी, शराबी और पक्षियों को पकड़ने | जो पांच प्रकार के वस्त्रों में आसक्त हैं, परिग्रह को वाले आदि पापी जनों के स्थान में वास नहीं करना चाहिए | ग्रहण करने वाले हैं, याचना करते हैं तथा अध:कर्म निंद्यकर्म तथा श्रृंगार, आभूषण, उज्जवल वेष, वेश की क्रीड़ा से | में रत हैं, वे मुनि मोक्षमार्ग से पतित हैं। परिग्रही साधक अभिराम (सुन्दर) गीत, नृत्य, वादित्र आदि से व्याप्त शाला | विशुद्धी को भी प्राप्त नहीं होता है, जैसा कि कहा हैआदि में रहने का त्याग करना चाहिए। शासनासन शुद्धि वैषम्ययत्ययं दिव्यं स्वीयमनिद्यं यद् द्रव्यम्॥ वाले संयतों को तो अकृत्रिम (प्राकृतिक) पर्वत की गुफा,
निश्चयनयस्य विषयगृहीव परिगृही नाव्यम्॥ वृक्ष के कोटर आदि तथा कृत्रिम शून्यागार छोड़े हुए घर
___यह परिग्रहवान् मुनि भी निश्चयनय के विषयभूत आदि ऐसे स्थानों पर रहना चाहिए, जो उनके उद्देश्य से । अनिन्दनीय दिव्य और अविनाशी स्वकीय द्रव्य को गृहस्थ नहीं बनाए गये हों और जिनमें उनके लिए कोई आरम्भ न के समान प्राप्त नहीं होता अर्थात् जिस प्रकार परिग्रही गृहस्थ किया गया हो।
शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं होता उसी प्रकार परिग्रही साधु ___ मुनियों का निवास तीन प्रकार का होता है। स्थान- भी नहीं प्राप्त होता है। अतः विशुद्धि को बढ़ाने के लिए खड़े होना, आसन-बैठना और शयन-सोना।
साधुओं का एक स्थान विशेष पर जीवन भर या लम्बी ___ जैनाचार्य मठ, आश्रम आदि में स्थायी निवास करने | अवधि रुकने का मोह नहीं होना चाहिए जिससे उनका की मुनि/आर्यिका को अनुमति प्रदान नहीं करते हैं। न जाने अनियमित विहार चलता रहेगा और वे आगम की मर्यादा वर्तमान में यह प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है कि साध/साध्वी/ की सुरक्षा करते हुए मोक्षमार्ग की महती प्रभावना कर त्यागी व्रती अपनी देख-रेख में कोई न कोई आश्रम/मठ/ |
सकेंगे। संस्थान/संस्था का निर्माण कराकर उसी को अपना निवास
सन्दर्भ
1. मूलाचार प्रदीप 31 बना रहे हैं। आस्था से जकड़ी समाज साधु/साध्वी/त्यागी/
2. तत्त्वार्थवार्तिक भा. पृ. 595 व्रती के कहने पर शक्ति के अनसार अर्थ सहयोग करती है
3. बृहत्कल्पभाष्य 1-36 और उनकी बलवती इच्छाओं को पूर्ण करना अपना कर्तव्य 4. दंसणसोधी ठिदिकरणभावणा अदिसयत्तकुसलत्तं । समझती है। यदि कोई प्रबुद्ध समाज के मध्य कहता है कि
खेतपरिमग्गणावि य अणियदवा से गुणा होंति ॥ भग. आराधना गा. 147
5. वही पृष्ठ 148, 149, 150 अपरिग्रही साधक को परिग्रही बनाकर धर्म की हानि क्यों
6. संविग्गदरे पासिय पियधम्मदरे अवज्जभीरुदरे। की जा रही है। साधुओं को एक स्थान पर नहीं रहना | संयमवि पियथिरधम्मो साधू विहरतओ होदि॥ भग. आराधना गा. 151 चाहिए गृहस्थों के साथ रहने पर परीषह भी आ जाते हैं | 7. वही गा. 152
8. सुत्तत्थथिरीकरणं अदिसयिदत्थाण होदि उवलद्धि। जिससे साधक की साधना में दोष लगने की सम्भावना
आयरियदंसणेण दु तह्मा सेवेज्ज आयरियं । भग. आराधना गा. 155 रहती है। इसका उत्तर समाज के पास होता है कि ये मुनि
9. संजदजणस्स य जहिं फासुविहारो य सुलभवुत्ती य। : आर्यिका अपने साथ तो नहीं ले जाएंगे। रहेगी तो अपने तं खेत्तं विरहन्तो णाहिदि सल्लेहणाजोगं ।। भग. आराधना गा. 157 पास अपने लोगों के ही कार्य आएगी। इनके निमित्त से |
10. मूलाचार समाचार अधिकार।
11. मूलाचार प्रदीप 31 बाहर का रुपया हमारे गृह स्थान या तीर्थ स्थान पर लग रहा
12. तत्त्वार्थवार्तिक भाग-2 पृष्ठ 595 है। इसी लोभ, कषायवश स्थानीय समाज साधु/साध्वी/
(आर्यिका सुपार्श्वमती माताजी कृत हिन्दी टीका)
अगस्त 2004 जिन भाषित 11
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org