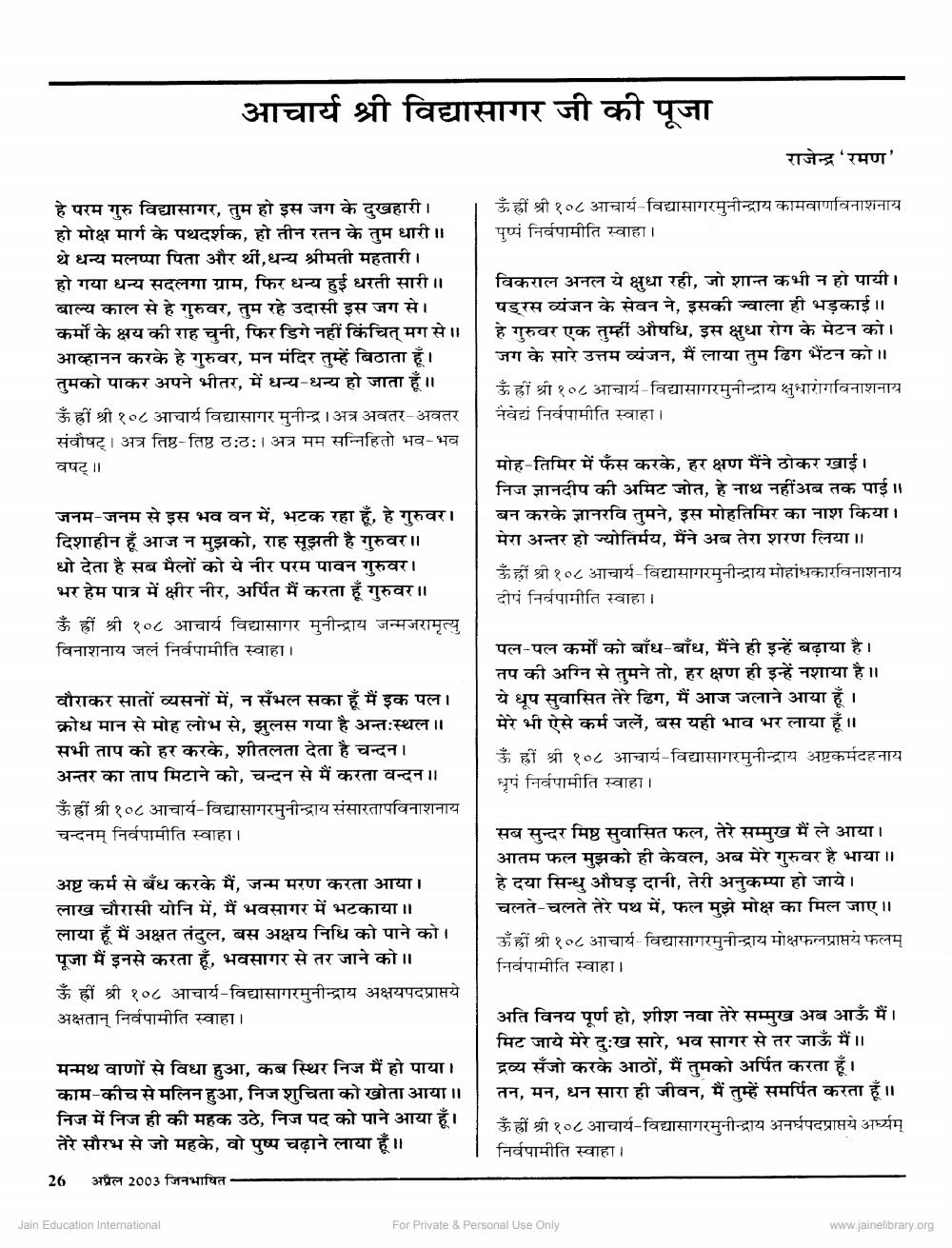________________
आचार्य श्री विद्यासागर जी की पूजा
राजेन्द्र 'रमण'
हे परम गुरु विद्यासागर, तुम हो इस जग के दुखहारी। । ऊँ ह्रीं श्री १०८ आचार्य-विद्यासागरमुनीन्द्राय कामवाणविनाशनाय हो मोक्ष मार्ग के पथदर्शक, हो तीन रतन के तुम धारी॥ | पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा। थे धन्य मलप्पा पिता और थीं,धन्य श्रीमती महतारी। हो गया धन्य सदलगा ग्राम, फिर धन्य हई धरती सारी॥ विकराल अनल ये क्षुधा रही, जो शान्त कभी न हो पायी। बाल्य काल से हे गुरुवर, तुम रहे उदासी इस जग से। पड्रस व्यंजन के सेवन ने, इसकी ज्वाला ही भड़काई।। कर्मों के क्षय की राह चुनी, फिर डिगे नहीं किंचित् मग से। हे गुरुवर एक तुम्ही औषधि, इस क्षुधा रोग के मेटन को। आव्हानन करके हे गुरुवर, मन मंदिर तुम्हें बिठाता हूँ। जग के सारे उत्तम व्यंजन, मैं लाया तुम ढिग भैंटन को। तुमको पाकर अपने भीतर, में धन्य-धन्य हो जाता हूँ॥
ऊँ ह्रीं श्री १०८ आचार्य विद्यासागरमुनीन्द्राय क्षुधारोगविनाशनाय ॐ ह्रीं श्री १०८ आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र। अत्र अवतर-अवतर नवयं निर्वपामीति स्वाहा। संवौषट् । अत्र तिष्ठ-तिष्ठ ठ:ठः। अत्र मम सन्निहितो भव-भव वषट् ।।
मोह-तिमिर में फंस करके, हर क्षण मैंने ठोकर खाई।
निज ज्ञानदीप की अमिट जोत, हे नाथ नहींअब तक पाई। जनम-जनम से इस भव वन में, भटक रहा हूँ, हे गुरुवर। बन करके ज्ञानरवि तुमने, इस मोहतिमिर का नाश किया। दिशाहीन हूँ आज न मुझको, राह सूझती है गुरुवर। मेरा अन्तर हो ज्योतिर्मय, मैंने अब तेरा शरण लिया। धो देता है सब मैलों को ये नीर परम पावन गुरुवर।
ऊँ ह्रीं श्री १०८ आचार्य-विद्यासागरमनीन्द्राय मोहांधकारविनाशनाय भर हेम पात्र में क्षीर नीर, अर्पित मैं करता हूँ गुरुवर॥
दीपं निर्वपामीति स्वाहा। ऊँ ह्रीं श्री १०८ आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्मजरामृत्यु विनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा।
पल-पल कर्मों को बाँध-बाँध, मैंने ही इन्हें बढ़ाया है।
तप की अग्नि से तुमने तो, हर क्षण ही इन्हें नशाया है। वौराकर सातों व्यसनों में, न सँभल सका हूँ मैं इक पल। ये धूप सुवासित तेरे ढिग, मैं आज जलाने आया हूँ। क्रोध मान से मोह लोभ से, झुलस गया है अन्तःस्थल। मेरे भी ऐसे कर्म जलें, बस यही भाव भर लाया हूँ। सभी ताप को हर करके, शीतलता देता है चन्दन।
ॐ ह्रीं श्री १०८ आचार्य-विद्यासागरमनीन्द्राय अष्टकर्मदहनाय अन्तर का ताप मिटाने को, चन्दन से मैं करता वन्दन।।
धूपं निर्वपामीति स्वाहा। ऊँ ह्रीं श्री १०८ आचार्य-विद्यासागरमुनीन्द्राय संसारतापविनाशनाय चन्दनम् निर्वपामीति स्वाहा।
सब सुन्दर मिष्ठ सुवासित फल, तेरे सम्मुख मैं ले आया।
आतम फल मुझको ही केवल, अब मेरे गुरुवर है भाया। अष्ट कर्म से बँध करके मैं, जन्म मरण करता आया। हे दया सिन्धु औघड़ दानी, तेरी अनुकम्पा हो जाये। लाख चौरासी योनि में, मैं भवसागर में भटकाया। चलते-चलते तेरे पथ में, फल मुझे मोक्ष का मिल जाए। लाया हूँ मैं अक्षत तंदुल, बस अक्षय निधि को पाने को।
ऊँ ह्रीं श्री १०८ आचार्य विद्यासागरमनीन्द्राय मोक्षफलप्राप्तय फलम पूजा मैं इनसे करता हूँ, भवसागर से तर जाने को।
निर्वपामीति स्वाहा। ऊँ ह्रीं श्री १०८ आचार्य-विद्यासागरमुनीन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा।
अति विनय पूर्ण हो, शीश नवा तेरे सम्मुख अब आऊँ मैं।
मिट जाये मेरे दुःख सारे, भव सागर से तर जाऊँ मैं ।। मन्मथ वाणों से विधा हुआ, कब स्थिर निज मैं हो पाया। द्रव्य सँजो करके आठों, मैं तुमको अर्पित करता हूँ। काम-कीच से मलिन हुआ, निज शुचिता को खोता आया। तन, मन, धन सारा ही जीवन, मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ। निज में निज ही की महक उठे, निज पद को पाने आया हूँ।
ऊँ ह्रीं श्री १०८ आचार्य-विद्यासागरमुनीन्द्राय अनर्घपदप्राप्तये अय॑म् तेरे सौरभ से जो महके, वो पुष्प चढ़ाने लाया हूँ॥
निर्वपामीति स्वाहा। 26 अप्रैल 2003 जिनभाषित
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org