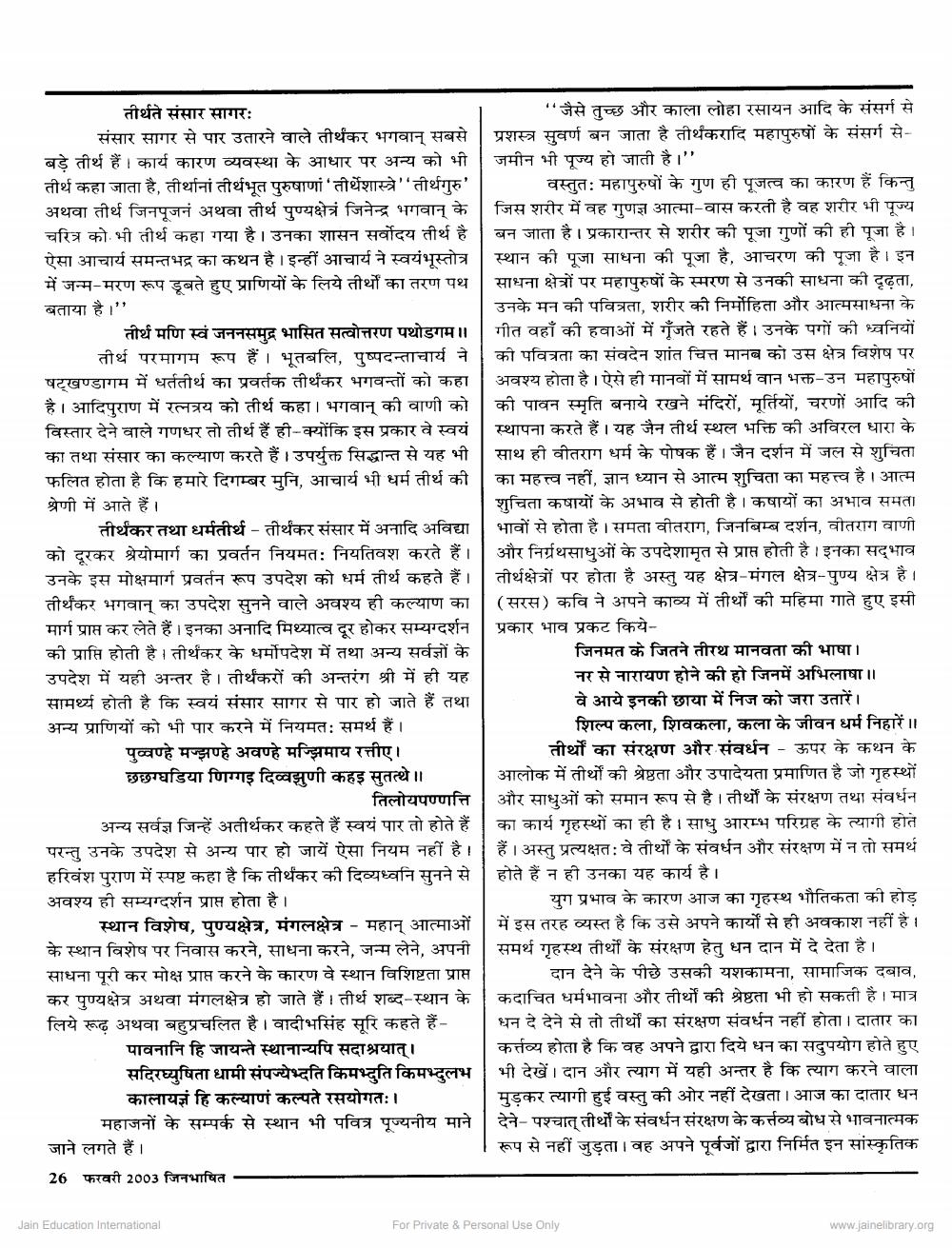________________
तीर्थते संसार सागरः
संसार सागर से पार उतारने वाले तीर्थंकर भगवान् सबसे बड़े तीर्थ हैं। कार्य कारण व्यवस्था के आधार पर अन्य को भी तीर्थ कहा जाता है, तीर्थानां तीर्थभूत पुरुषाणां 'तीर्थेशास्त्रे 'तीर्थगुरु' अथवा तीर्थ जिनपूजनं अथवा तीर्थ पुण्यक्षेत्रं जिनेन्द्र भगवान् के चरित्र को भी तीर्थ कहा गया है। उनका शासन सर्वोदय तीर्थ है। ऐसा आचार्य समन्तभद्र का कथन है। इन्हीं आचार्य ने स्वयंभूस्तोत्र में जन्म-मरण रूप डूबते हुए प्राणियों के लिये तीर्थों का तरण पथ बताया है।"
तीर्थ मणि स्वं जननसमुद्र भासित सत्वोत्तरण पथोडगम ॥ तीर्थ परमागम रूप हैं। भूतबलि, पुष्पदन्ताचार्य ने षट्खण्डागम में धर्ततीर्थ का प्रवर्तक तीर्थंकर भगवन्तों को कहा है। आदिपुराण में रत्नत्रय को तीर्थ कहा। भगवान् की वाणी को विस्तार देने वाले गणधर तो तीर्थ हैं ही क्योंकि इस प्रकार वे स्वयं का तथा संसार का कल्याण करते हैं। उपर्युक्त सिद्धान्त से यह भी फलित होता है कि हमारे दिगम्बर मुनि, आचार्य भी धर्म तीर्थ की श्रेणी में आते हैं।
तीर्थंकर तथा धर्मतीर्थ तीर्थंकर संसार में अनादि अविद्या को दूरकर श्रेयोमार्ग का प्रवर्तन नियमतः नियतिवश करते हैं। उनके इस मोक्षमार्ग प्रवर्तन रूप उपदेश को धर्म तीर्थ कहते हैं। तीर्थंकर भगवान् का उपदेश सुनने वाले अवश्य ही कल्याण का मार्ग प्राप्त कर लेते हैं। इनका अनादि मिथ्यात्व दूर होकर सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होती है। तीर्थंकर के धर्मोपदेश में तथा अन्य सर्वज्ञों के उपदेश में यही अन्तर है। तीर्थंकरों की अन्तरंग श्री में ही यह सामर्थ्य होती है कि स्वयं संसार सागर से पार हो जाते हैं तथा अन्य प्राणियों को भी पार करने में नियमत: समर्थ हैं।
पुव्वण्हे मन्झहे अवण्हे मन्त्रिमाय रतीए । छछग्घडिया णिग्गड़ दिव्वझुणी कहइ सुतत्थे । तिलोयपण्णत्ति अन्य सर्वज्ञ जिन्हें अतीर्थकर कहते हैं स्वयं पार तो होते हैं परन्तु उनके उपदेश से अन्य पार हो जायें ऐसा नियम नहीं है। हरिवंश पुराण में स्पष्ट कहा है कि तीर्थंकर की दिव्यध्वनि सुनने से अवश्य ही सम्यग्दर्शन प्राप्त होता है।
,
स्थान विशेष पुण्यक्षेत्र, मंगलक्षेत्र महान् आत्माओं के स्थान विशेष पर निवास करने, साधना करने, जन्म लेने, अपनी साधना पूरी कर मोक्ष प्राप्त करने के कारण वे स्थान विशिष्टता प्राप्त कर पुण्यक्षेत्र अथवा मंगलक्षेत्र हो जाते हैं। तीर्थ शब्द-स्थान के लिये रूद अथवा बहुप्रचलित है। बादीभसिंह सूरि कहते हैं
पावनानि हि जायन्ते स्थानान्यपि सदाश्रयात् ।
" जैसे तुच्छ और काला लोहा रसायन आदि के संसर्ग से प्रशस्त्र सुवर्ण बन जाता है तीर्थंकरादि महापुरुषों के संसर्ग सेजमीन भी पूज्य हो जाती है।"
वस्तुत: महापुरुषों के गुण ही पूजत्व का कारण हैं किन्तु जिस शरीर में वह गुणज्ञ आत्मा-वास करती है वह शरीर भी पूज्य बन जाता है। प्रकारान्तर से शरीर की पूजा गुणों की ही पूजा है। स्थान की पूजा साधना की पूजा है, आचरण की पूजा है। इन साधना क्षेत्रों पर महापुरुषों के स्मरण से उनकी साधना की दृढ़ता, उनके मन की पवित्रता, शरीर की निर्मोहिता और आत्मसाधना के गीत वहाँ की हवाओं में गूँजते रहते हैं। उनके पगों की ध्वनियों की पवित्रता का संवदेन शांत चित्त मानब को उस क्षेत्र विशेष पर अवश्य होता है। ऐसे ही मानवों में सामर्थ वान भक्त उन महापुरुषों की पावन स्मृति बनाये रखने मंदिरों, मूर्तियों चरणों आदि की स्थापना करते हैं। यह जैन तीर्थ स्थल भक्ति की अविरल धारा के साथ ही वीतराग धर्म के पोषक हैं। जैन दर्शन में जल से शुचिता का महत्त्व नहीं, ज्ञान ध्यान से आत्म शुचिता का महत्त्व है। आत्म शुचिता कषायों के अभाव से होती है। कषायों का अभाव समता भावों से होता है। समता वीतराग, जिनबिम्ब दर्शन, वीतराग वाणी और निर्ग्रथसाधुओं के उपदेशामृत से प्राप्त होती है। इनका सद्भाव तीर्थक्षेत्रों पर होता है अस्तु यह क्षेत्र मंगल क्षेत्र- पुण्य क्षेत्र है। (सरस) कवि ने अपने काव्य में तीर्थों की महिमा गाते हुए इसी प्रकार भाव प्रकट किये
-
सदिरध्युषिता धामी संपज्येभ्दति किमभ्दुति किमभ्दुलभ कालायज्ञं हि कल्याणं कल्पते रसयोगतः ।
Jain Education International
युग प्रभाव के कारण आज का गृहस्थ भौतिकता की होड़ में इस तरह व्यस्त है कि उसे अपने कार्यों से ही अवकाश नहीं है। समर्थ गृहस्थ तीर्थों के संरक्षण हेतु धन दान में दे देता है।
दान देने के पीछे उसकी यशकामना, सामाजिक दबाव, कदाचित धर्मभावना और तीर्थों की श्रेष्ठता भी हो सकती है। मात्र धन दे देने से तो तीर्थों का संरक्षण संवर्धन नहीं होता। दातार का कर्त्तव्य होता है कि वह अपने द्वारा दिये धन का सदुपयोग होते हुए भी देखें। दान और त्याग में यही अन्तर है कि त्याग करने वाला मुड़कर त्यागी हुई वस्तु की ओर नहीं देखता। आज का दातार धन
महाजनों के सम्पर्क से स्थान भी पवित्र पूज्यनीय माने देने- पश्चात् तीर्थों के संवर्धन संरक्षण के कर्त्तव्य बोध से भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ता । वह अपने पूर्वजों द्वारा निर्मित इन सांस्कृतिक
जाने लगते हैं।
26 फरवरी 2003 जिनभाषित
जिनमत के जितने तीरथ मानवता की भाषा । नर से नारायण होने की हो जिनमें अभिलाषा ॥ वे आये इनकी छाया में निज को जरा उतारें।
शिल्प कला, शिवकला, कला के जीवन धर्म निहारें ।। तीर्थों का संरक्षण और संबर्धन ऊपर के कथन के आलोक में तीर्थों की श्रेष्ठता और उपादेयता प्रमाणित है जो गृहस्थों और साधुओं को समान रूप से है। तीर्थों के संरक्षण तथा संवर्धन का कार्य गृहस्थों का ही है। साधु आरम्भ परिग्रह के त्यागी होते हैं। अस्तु प्रत्यक्षत: वे तीर्थों के संवर्धन और संरक्षण में न तो समर्थ होते हैं न ही उनका यह कार्य है।
For Private & Personal Use Only
-
www.jainelibrary.org