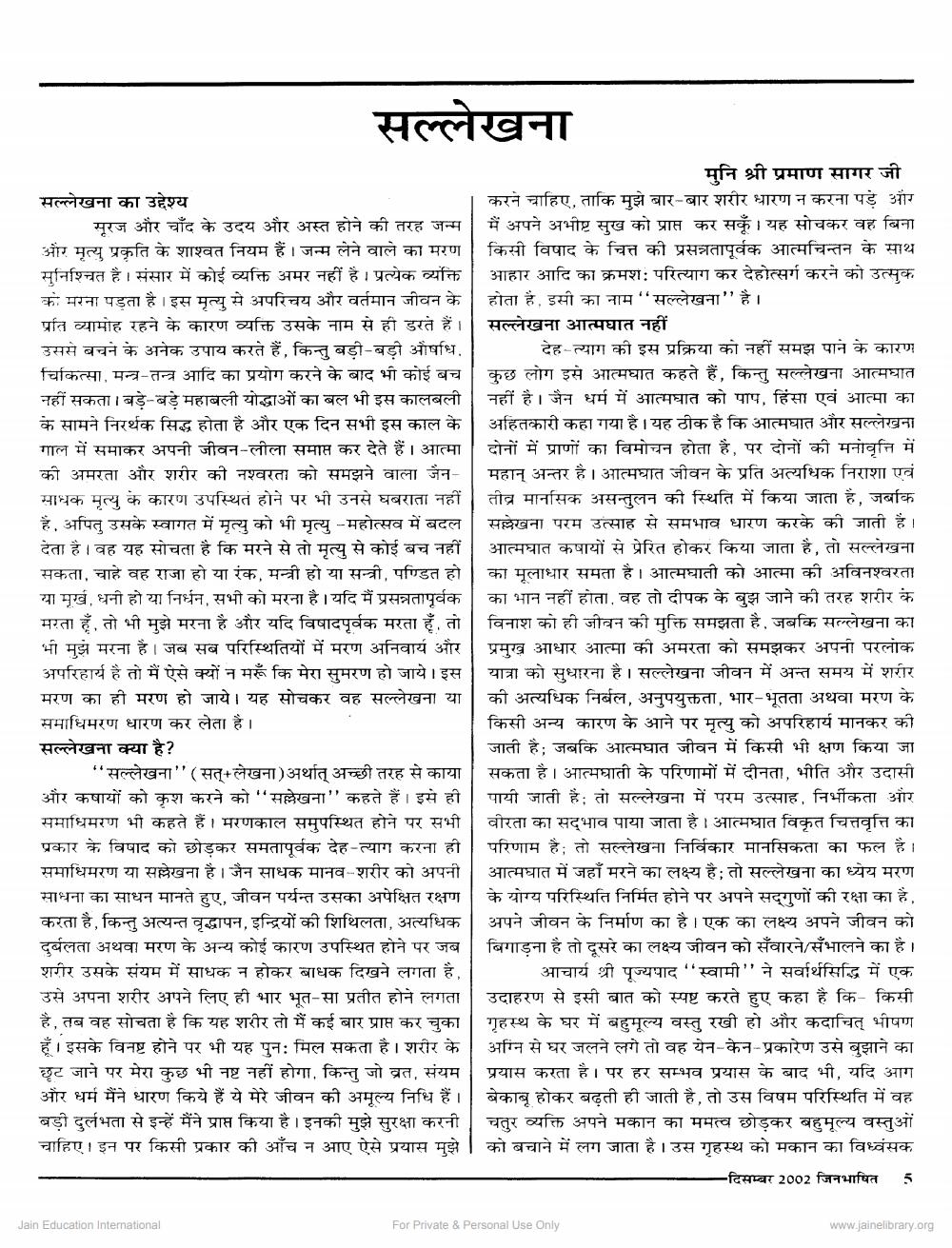________________
सल्लेखना
मुनि श्री प्रमाण सागर जी सल्लेखना का उद्देश्य
करने चाहिए, ताकि मुझे बार-बार शरीर धारण न करना पड़े और सूरज और चाँद के उदय और अस्त होने की तरह जन्म | मैं अपने अभीष्ट सुख को प्राप्त कर सकूँ। यह सोचकर वह बिना और मृत्यु प्रकृति के शाश्वत नियम हैं। जन्म लेने वाले का मरण किसी विषाद के चित्त की प्रसन्नतापूर्वक आत्मचिन्तन के साथ निश्चित है। संसार में कोई व्यक्ति अमर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति | आहार आदि का क्रमश: परित्याग कर देहोत्सर्ग करने को उत्सुक के मरना पड़ता है। इस मृत्यु से अपरिचय और वर्तमान जीवन के | होता है, इसी का नाम "सल्लेखना' है। प्रति व्यामोह रहने के कारण व्यक्ति उसके नाम से ही डरते हैं। | सल्लेखना आत्मघात नहीं उससे बचने के अनेक उपाय करते हैं, किन्तु बड़ी-बड़ी औषधि, | देह त्याग की इस प्रक्रिया को नहीं समझ पाने के कारण चिकित्सा, मन्त्र-तन्त्र आदि का प्रयोग करने के बाद भी कोई बच | कुछ लोग इसे आत्मघात कहते हैं, किन्तु सल्लेखना आत्मघात नहीं सकता। बड़े-बड़े महाबली योद्धाओं का बल भी इस कालबली नहीं है। जैन धर्म में आत्मघात को पाप, हिंसा एवं आत्मा का के सामने निरर्थक सिद्ध होता है और एक दिन सभी इस काल के अहितकारी कहा गया है। यह ठीक है कि आत्मघात और सल्लेखना गाल में समाकर अपनी जीवन-लीला समाप्त कर देते हैं। आत्मा दोनों में प्राणों का विमोचन होता है, पर दोनों की मनोवृत्ति में की अमरता और शरीर की नश्वरता को समझने वाला जैन- महान् अन्तर है। आत्मघात जीवन के प्रति अत्यधिक निराशा एवं साधक मृत्यु के कारण उपस्थित होने पर भी उनसे घबराता नहीं तीव्र मानसिक असन्तुलन की स्थिति में किया जाता है, जबकि है, अपितु उसके स्वागत में मृत्यु को भी मृत्यु -महोत्सव में बदल सल्लेखना परम उत्साह से समभाव धारण करके की जाती है। देता है। वह यह सोचता है कि मरने से तो मृत्यु से कोई बच नहीं आत्मघात कषायों से प्रेरित होकर किया जाता है, तो सल्लेखना सकता, चाहे वह राजा हो या रंक, मन्त्री हो या सन्त्री, पण्डित हो | का मूलाधार समता है। आत्मघाती को आत्मा की अविनश्वरता या मूर्ख, धनी हो या निर्धन, सभी को मरना है। यदि मैं प्रसन्नतापूर्वक | का भान नहीं होता, वह तो दीपक के बुझ जाने की तरह शरीर के मरता हूँ, तो भी मुझे मरना है और यदि विषादपूर्वक मरता हूँ, तो | विनाश को ही जीवन की मुक्ति समझता है, जबकि सल्लेखना का भी मुझे मरना है। जब सब परिस्थितियों में मरण अनिवार्य और | प्रमुख आधार आत्मा की अमरता को समझकर अपनी परलोक अपरिहार्य है तो मैं ऐसे क्यों न मरूँ कि मेरा सुमरण हो जाये। इस | यात्रा को सुधारना है। सल्लेखना जीवन में अन्त समय में शरीर मरण का ही मरण हो जाये। यह सोचकर वह सल्लेखना या की अत्यधिक निर्बल, अनुपयुक्तता, भार-भूतता अथवा मरण के समाधिमरण धारण कर लेता है।
किसी अन्य कारण के आने पर मृत्यु को अपरिहार्य मानकर की सल्लेखना क्या है?
जाती है। जबकि आत्मघात जीवन में किसी भी क्षण किया जा "सल्लेखना" (सत्+लेखना)अर्थात् अच्छी तरह से काया | सकता है। आत्मघाती के परिणामों में दीनता, भीति और उदासी और कषायों को कृश करने को "सल्लेखना" कहते हैं। इसे ही | पायी जाती है; तो सल्लेखना में परम उत्साह, निर्भीकता और समाधिमरण भी कहते हैं। मरणकाल समुपस्थित होने पर सभी | वीरता का सद्भाव पाया जाता है। आत्मघात विकृत चित्तवृत्ति का प्रकार के विषाद को छोड़कर समतापूर्वक देह-त्याग करना ही परिणाम है; तो सल्लेखना निर्विकार मानसिकता का फल है। समाधिमरण या सल्लेखना है। जैन साधक मानव शरीर को अपनी आत्मघात में जहाँ मरने का लक्ष्य है; तो सल्लेखना का ध्येय मरण साधना का साधन मानते हुए, जीवन पर्यन्त उसका अपेक्षित रक्षण के योग्य परिस्थिति निर्मित होने पर अपने सद्गुणों की रक्षा का है, करता है, किन्तु अत्यन्त वृद्धापन, इन्द्रियों की शिथिलता, अत्यधिक | अपने जीवन के निर्माण का है। एक का लक्ष्य अपने जीवन को दुर्बलता अथवा मरण के अन्य कोई कारण उपस्थित होने पर जब बिगाड़ना है तो दूसरे का लक्ष्य जीवन को सँवारने/सँभालने का है। शरीर उसके संयम में साधक न होकर बाधक दिखने लगता है, आचार्य श्री पूज्यपाद "स्वामी' ने सर्वार्थसिद्धि में एक उसे अपना शरीर अपने लिए ही भार भूत-सा प्रतीत होने लगता | उदाहरण से इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि- किसी है, तब वह सोचता है कि यह शरीर तो मैं कई बार प्राप्त कर चुका | गृहस्थ के घर में बहुमूल्य वस्तु रखी हो और कदाचित् भीषण हूँ। इसके विनष्ट होने पर भी यह पुनः मिल सकता है। शरीर के अग्नि से घर जलने लगे तो वह येन-केन-प्रकारेण उसे बुझाने का छूट जाने पर मेरा कुछ भी नष्ट नहीं होगा. किन्तु जो व्रत, संयम प्रयास करता है। पर हर सम्भव प्रयास के बाद भी, यदि आग और धर्म मैंने धारण किये हैं ये मेरे जीवन की अमूल्य निधि हैं। बेकाबू होकर बढ़ती ही जाती है, तो उस विषम परिस्थिति में वह बड़ी दुर्लभता से इन्हें मैंने प्राप्त किया है। इनकी मुझे सुरक्षा करनी | चतुर व्यक्ति अपने मकान का ममत्व छोड़कर बहुमूल्य वस्तुओं चाहिए। इन पर किसी प्रकार की आँच न आए ऐसे प्रयास मुझे | को बचाने में लग जाता है। उस गृहस्थ को मकान का विध्वंसक
- -दिसम्बर 2002 जिनभाषित 5
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org