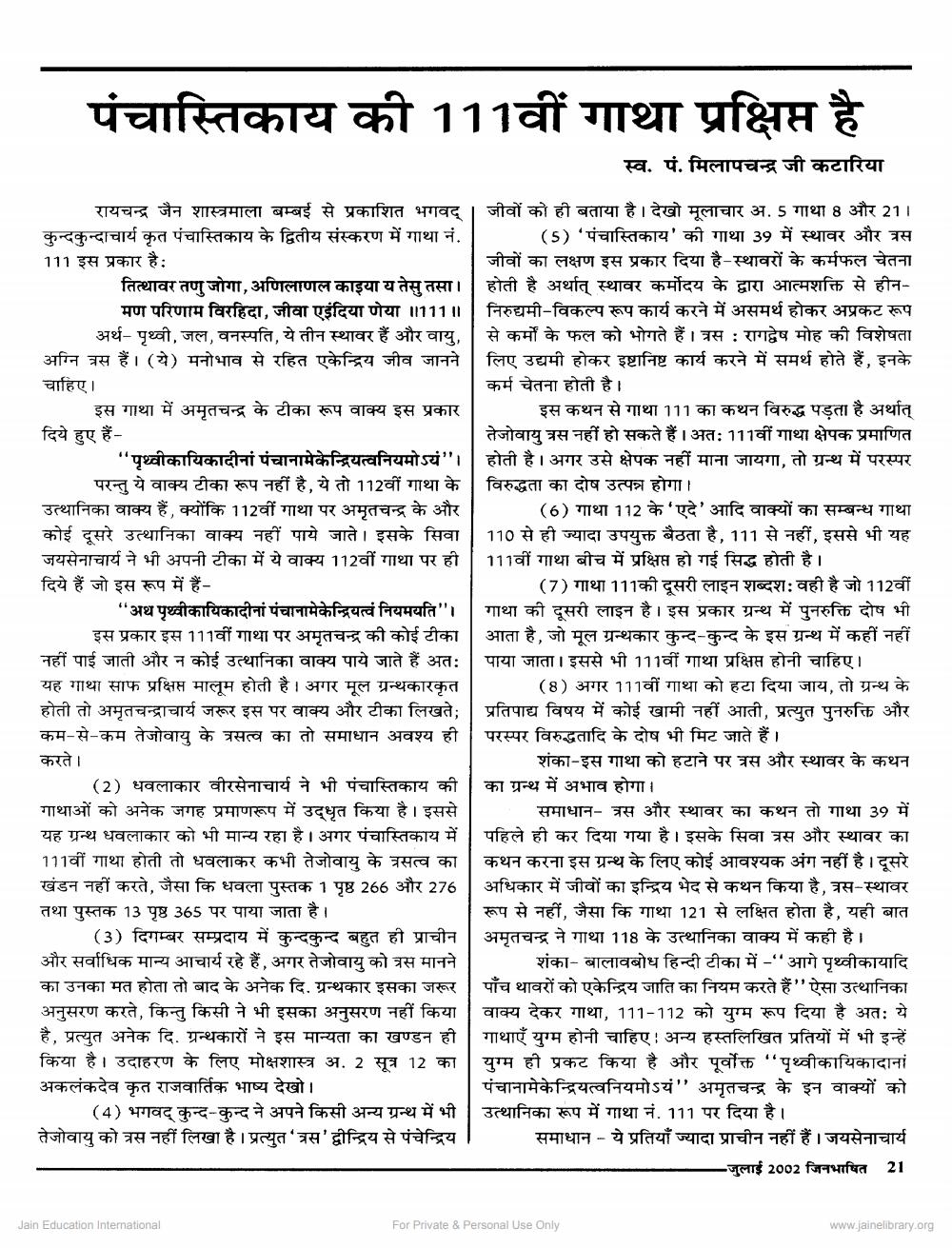________________
पंचास्तिकाय की 111वीं गाथा प्रक्षिप्त है
स्व. पं. मिलापचन्द्र जी कटारिया
रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला बम्बई से प्रकाशित भगवद् | जीवों को ही बताया है। देखो मूलाचार अ.5 गाथा 8 और 21। कुन्दकुन्दाचार्य कृत पंचास्तिकाय के द्वितीय संस्करण में गाथा नं. (5) 'पंचास्तिकाय' की गाथा 39 में स्थावर और त्रस 111 इस प्रकार है:
जीवों का लक्षण इस प्रकार दिया है-स्थावरों के कर्मफल चेतना तित्थावर तणु जोगा, अणिलाणल काइया य तेसु तसा। होती है अर्थात् स्थावर कर्मोदय के द्वारा आत्मशक्ति से हीन
मण परिणाम विरहिदा, जीवा एइंदिया णेया 1110 | निरुद्यमी-विकल्प रूप कार्य करने में असमर्थ होकर अप्रकट रूप
अर्थ- पृथ्वी, जल, वनस्पति, ये तीन स्थावर हैं और वायु, | से कर्मों के फल को भोगते हैं। त्रस : रागद्वेष मोह की विशेषता अग्नि त्रस हैं। (ये) मनोभाव से रहित एकेन्द्रिय जीव जानने लिए उद्यमी होकर इष्टानिष्ट कार्य करने में समर्थ होते हैं, इनके चाहिए।
कर्म चेतना होती है। इस गाथा में अमृतचन्द्र के टीका रूप वाक्य इस प्रकार इस कथन से गाथा 111 का कथन विरुद्ध पड़ता है अर्थात् दिये हुए हैं
तेजोवायु त्रस नहीं हो सकते हैं। अत: 111वीं गाथा क्षेपक प्रमाणित "पृथ्वीकायिकादीनां पंचानामेकेन्द्रियत्वनियमोऽयं"। होती है। अगर उसे क्षेपक नहीं माना जायगा, तो ग्रन्थ में परस्पर
परन्तु ये वाक्य टीका रूप नहीं है, ये तो 112वीं गाथा के | विरुद्धता का दोष उत्पन्न होगा। उत्थानिका वाक्य हैं, क्योंकि 112वीं गाथा पर अमृतचन्द्र के और | (6) गाथा 112 के 'एदे' आदि वाक्यों का सम्बन्ध गाथा कोई दूसरे उत्थानिका वाक्य नहीं पाये जाते। इसके सिवा | 110 से ही ज्यादा उपयुक्त बैठता है, 111 से नहीं, इससे भी यह जयसेनाचार्य ने भी अपनी टीका में ये वाक्य 112वीं गाथा पर ही | 111वीं गाथा बीच में प्रक्षिप्त हो गई सिद्ध होती है। दिये हैं जो इस रूप में हैं
(7) गाथा 111की दूसरी लाइन शब्दश: वही है जो 112वीं “अथ पृथ्वीकायिकादीनां पंचानामेकेन्द्रियत्वं नियमयति"। | गाथा की दूसरी लाइन है। इस प्रकार ग्रन्थ में पुनरुक्ति दोष भी
इस प्रकार इस 111वीं गाथा पर अमृतचन्द्र की कोई टीका आता है, जो मूल ग्रन्थकार कुन्द-कुन्द के इस ग्रन्थ में कहीं नहीं नहीं पाई जाती और न कोई उत्थानिका वाक्य पाये जाते हैं अत: पाया जाता। इससे भी 111वीं गाथा प्रक्षिप्त होनी चाहिए। यह गाथा साफ प्रक्षिप्त मालूम होती है। अगर मूल ग्रन्थकारकृत (8) अगर 111वीं गाथा को हटा दिया जाय, तो ग्रन्थ के होती तो अमृतचन्द्राचार्य जरूर इस पर वाक्य और टीका लिखते; प्रतिपाद्य विषय में कोई खामी नहीं आती, प्रत्युत पुनरुक्ति और कम-से-कम तेजोवायु के त्रसत्व का तो समाधान अवश्य ही | परस्पर विरुद्धतादि के दोष भी मिट जाते हैं। करते।
शंका-इस गाथा को हटाने पर त्रस और स्थावर के कथन (2) धवलाकार वीरसेनाचार्य ने भी पंचास्तिकाय की का ग्रन्थ में अभाव होगा। गाथाओं को अनेक जगह प्रमाणरूप में उद्धृत किया है। इससे समाधान- त्रस और स्थावर का कथन तो गाथा 39 में यह ग्रन्थ धवलाकार को भी मान्य रहा है। अगर पंचास्तिकाय में पहिले ही कर दिया गया है। इसके सिवा त्रस और स्थावर का 111वीं गाथा होती तो धवलाकर कभी तेजोवायु के त्रसत्व का कथन करना इस ग्रन्थ के लिए कोई आवश्यक अंग नहीं है। दूसरे खंडन नहीं करते, जैसा कि धवला पुस्तक 1 पृष्ठ 266 और 276 अधिकार में जीवों का इन्द्रिय भेद से कथन किया है, त्रस-स्थावर तथा पुस्तक 13 पृष्ठ 365 पर पाया जाता है।
रूप से नहीं, जैसा कि गाथा 121 से लक्षित होता है, यही बात (3) दिगम्बर सम्प्रदाय में कुन्दकुन्द बहुत ही प्राचीन | अमृतचन्द्र ने गाथा 118 के उत्थानिका वाक्य में कही है। और सर्वाधिक मान्य आचार्य रहे हैं, अगर तेजोवायु को त्रस मानने शंका- बालावबोध हिन्दी टीका में -"आगे पृथ्वीकायादि का उनका मत होता तो बाद के अनेक दि. ग्रन्थकार इसका जरूर पाँच थावरों को एकेन्द्रिय जाति का नियम करते हैं" ऐसा उत्थानिका अनुसरण करते, किन्तु किसी ने भी इसका अनुसरण नहीं किया वाक्य देकर गाथा, 111-112 को युग्म रूप दिया है अतः ये है, प्रत्युत अनेक दि. ग्रन्थकारों ने इस मान्यता का खण्डन ही | गाथाएँ युग्म होनी चाहिए। अन्य हस्तलिखित प्रतियों में भी इन्हें किया है। उदाहरण के लिए मोक्षशास्त्र अ. 2 सूत्र 12 का | युग्म ही प्रकट किया है और पूर्वोक्त "पृथ्वीकायिकादानां अकलंकदेव कृत राजवार्तिक भाष्य देखो।
पंचानामेकेन्द्रियत्वनियमोऽयं" अमृतचन्द्र के इन वाक्यों को (4) भगवद् कुन्द-कुन्द ने अपने किसी अन्य ग्रन्थ में भी | उत्थानिका रूप में गाथा नं. 111 पर दिया है। तेजोवायु को त्रस नहीं लिखा है। प्रत्युत त्रस' द्वीन्द्रिय से पंचेन्द्रिय । समाधान- ये प्रतियाँ ज्यादा प्राचीन नहीं हैं। जयसेनाचार्य
-जुलाई 2002 जिनभाषित 21
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org