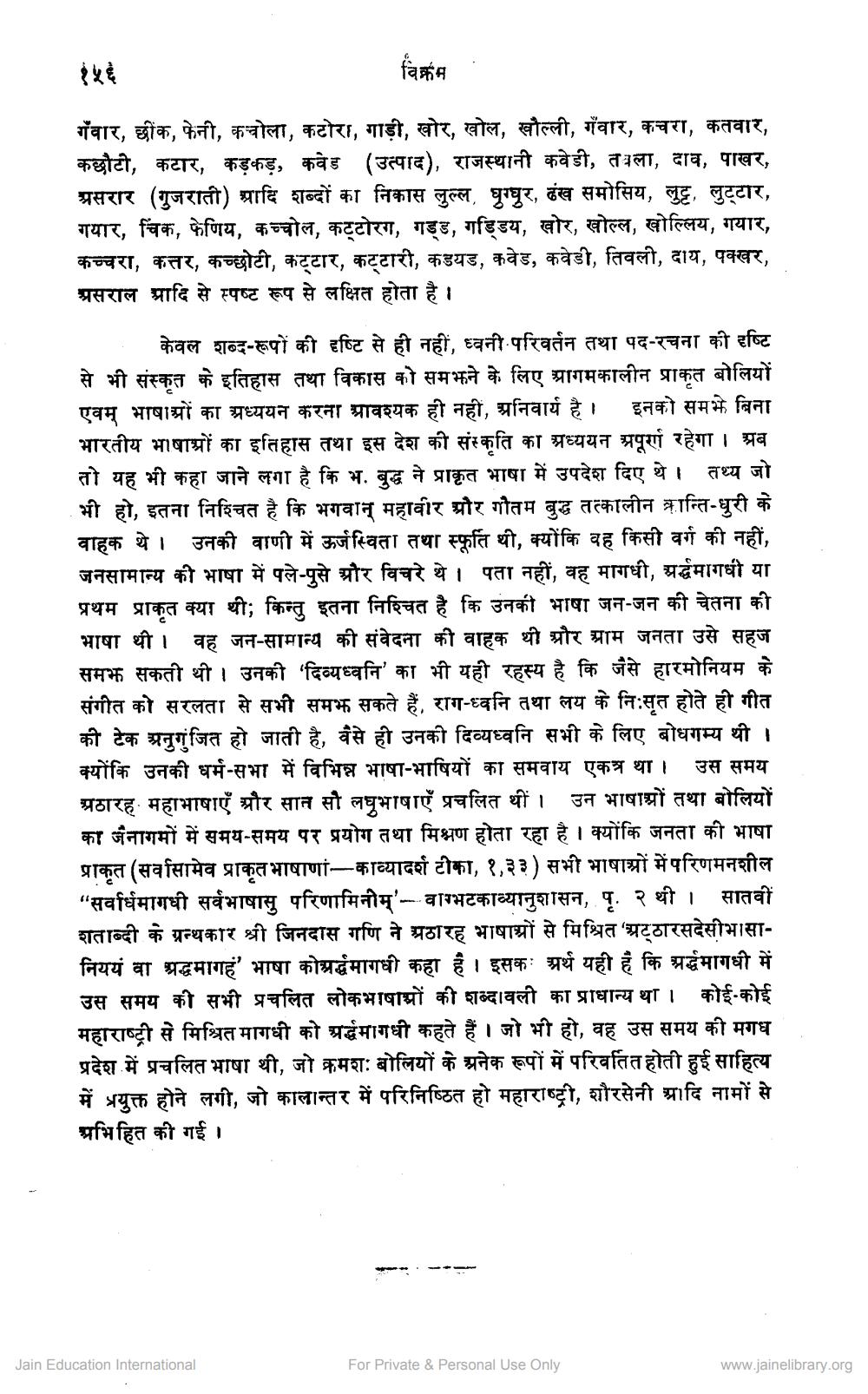________________
विक्रम
गॅवार, छींक, फेनी, कचोला, कटोरा, गाड़ी, खोर, खोल, खौल्ली, गँवार, कचरा, कतवार, कछौटी, कटार, कड़कड़, कवेड (उत्पाद), राजस्थानी कवेडी, तबला, दाव, पाखर, असरार (गुजराती) आदि शब्दों का निकास लुल्ल, घुग्घुर, ढंख समोसिय, लुट, लुट्टार, गयार, चिंक, फेणिय, कच्चोल, कट्टोरग, गड्ड, गड्डिय, खोर, खोल्ल, खोल्लिय, गयार, कच्चरा, कत्तर, कच्छोटी, कट्टार, कट्टारी, कडयड, कवेड, कवेडी, तिवली, दाय, पक्खर, असराल आदि से स्पष्ट रूप से लक्षित होता है।
केवल शब्द-रूपों की दृष्टि से ही नहीं, ध्वनी परिवर्तन तथा पद-रचना की दृष्टि से भी संस्कृत के इतिहास तथा विकास को समझने के लिए आगमकालीन प्राकृत बोलियों एवम् भाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। इनको समझे बिना भारतीय भाषाओं का इतिहास तथा इस देश की संस्कृति का अध्ययन अपूर्ण रहेगा। अब तो यह भी कहा जाने लगा है कि भ. बुद्ध ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। तथ्य जो भी हो, इतना निश्चित है कि भगवान महावीर और गौतम बद्ध तत्कालीन क्रान्ति-धरी के वाहक थे। उनकी वाणी में ऊर्जस्विता तथा स्फूर्ति थी, क्योंकि वह किसी वर्ग की नहीं, जनसामान्य की भाषा में पले-पुसे और विचरे थे। पता नहीं, वह मागधी, अर्द्धमागधी या प्रथम प्राकृत क्या थी; किन्तु इतना निश्चित है कि उनकी भाषा जन-जन की चेतना की भाषा थी। वह जन-सामान्य की संवेदना की वाहक थी और आम जनता उसे सहज समझ सकती थी। उनकी 'दिव्यध्वनि' का भी यही रहस्य है कि जैसे हारमोनियम के संगीत को सरलता से सभी समझ सकते हैं, राग-ध्वनि तथा लय के नि:सृत होते ही गीत की टेक अनुगुंजित हो जाती है, वैसे ही उनकी दिव्यध्वनि सभी के लिए बोधगम्य थी। क्योंकि उनकी धर्म-सभा में विभिन्न भाषा-भाषियों का समवाय एकत्र था। उस समय अठारह महाभाषाएँ और सात सौ लघुभाषाएँ प्रचलित थीं। उन भाषाओं तथा बोलियों का जैनागमों में समय-समय पर प्रयोग तथा मिश्रण होता रहा है । क्योंकि जनता की भाषा प्राकृत (सर्वासामेव प्राकृतभाषाणां-काव्यादर्श टीका, १,३३) सभी भाषाओं में परिणमनशील "सर्वार्धमागधी सर्वभाषासु परिणामिनीम्'- वाग्भटकाव्यानुशासन, पृ. २ थी। सातवीं शताब्दी के ग्रन्थकार श्री जिनदास गणि ने अठारह भाषाओं से मिश्रित 'अट्ठारसदेसीभासानिययं वा अद्धमागह' भाषा कोअर्द्धमागधी कहा है । इसका अर्थ यही है कि अर्द्धमागधी में उस समय की सभी प्रचलित लोकभाषाओं की शब्दावली का प्राधान्य था। कोई-कोई महाराष्ट्री से मिश्रित मागधी को अर्द्धमागधी कहते हैं । जो भी हो, वह उस समय की मगध प्रदेश में प्रचलित भाषा थी, जो क्रमशः बोलियों के अनेक रूपों में परिवर्तित होती हुई साहित्य में प्रयुक्त होने लगी, जो कालान्तर में परिनिष्ठित हो महाराष्ट्री, शौरसेनी आदि नामों से अभिहित की गई।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org