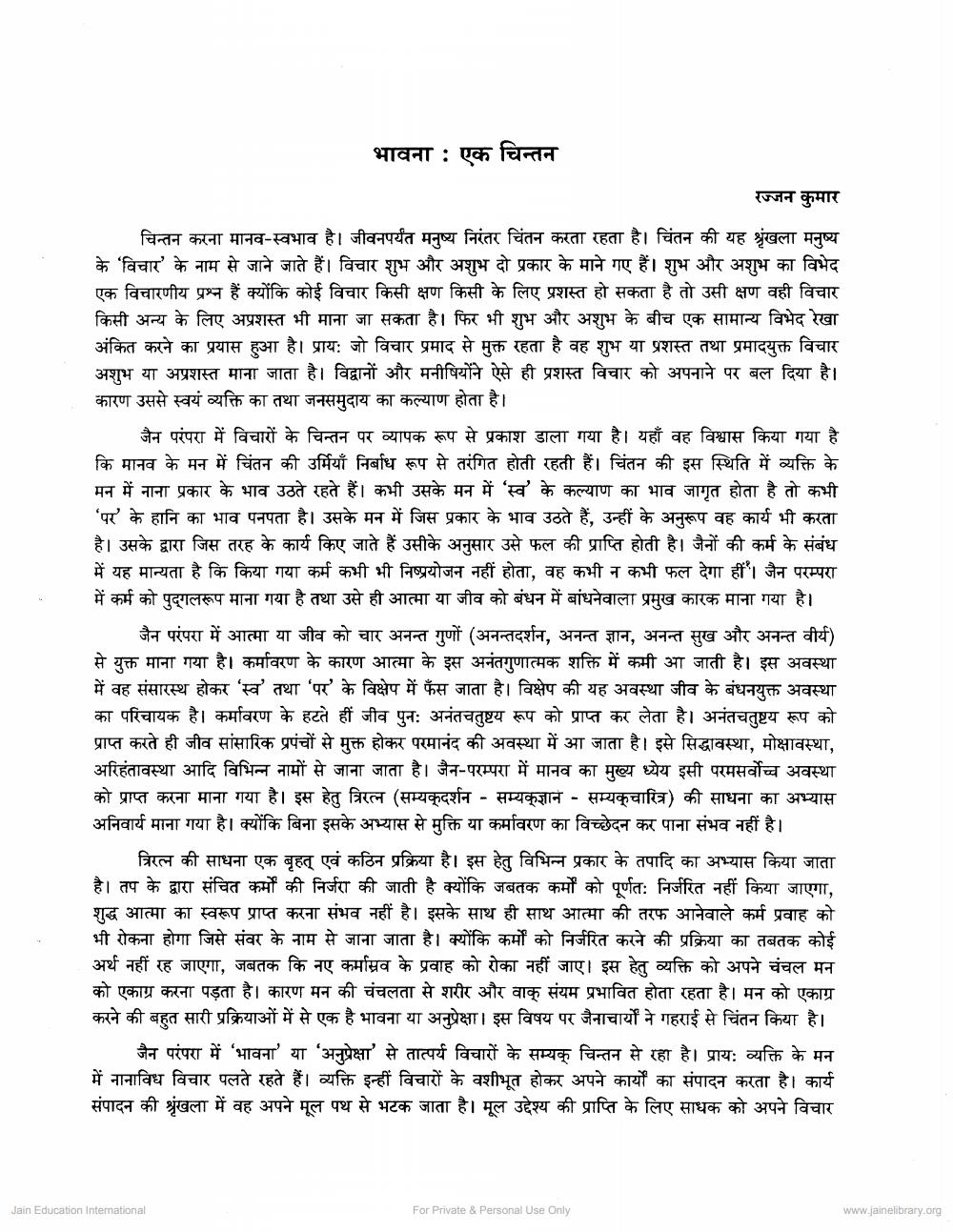________________
भावना एक चिन्तन :
रज्जन कुमार
चिन्तन करना मानव स्वभाव है। जीवनपर्यंत मनुष्य निरंतर चिंतन करता रहता है। चिंतन की यह श्रृंखला मनुष्य के 'विचार' के नाम से जाने जाते हैं विचार शुभ और अशुभ दो प्रकार के माने गए हैं। शुभ और अशुभ का विभेद एक विचारणीय प्रश्न हैं क्योंकि कोई विचार किसी क्षण किसी के लिए प्रशस्त हो सकता है तो उसी क्षण वही विचार किसी अन्य के लिए अप्रशस्त भी माना जा सकता है। फिर भी शुभ और अशुभ के बीच एक सामान्य विभेद रेखा अंकित करने का प्रयास हुआ है। प्रायः जो विचार प्रमाद से मुक्त रहता है वह शुभ या प्रशस्त तथा प्रमादयुक्त विचार अशुभ या अप्रशस्त माना जाता है। विद्वानों और मनीषियोंने ऐसे ही प्रशस्त विचार को अपनाने पर बल दिया है। कारण उससे स्वयं व्यक्ति का तथा जनसमुदाय का कल्याण होता है।
जैन परंपरा में विचारों के चिन्तन पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला गया है। यहाँ वह विश्वास किया गया है। कि मानव के मन में चिंतन की उर्मियों निर्वाध रूप से तरंगित होती रहती हैं चिंतन की इस स्थिति में व्यक्ति के मन में नाना प्रकार के भाव उठते रहते हैं। कभी उसके मन में 'स्व' के कल्याण का भाव जागृत होता है तो कभी 'पर' के हानि का भाव पनपता है। उसके मन में जिस प्रकार के भाव उठते हैं, उन्हीं के अनुरूप वह कार्य भी करता है। उसके द्वारा जिस तरह के कार्य किए जाते हैं उसीके अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है। जैनों की कर्म के संबंध में यह मान्यता है कि किया गया कर्म कभी भी निष्प्रयोजन नहीं होता, वह कभी न कभी फल देगा हीं। जैन परम्परा में कर्म को पुद्गलरूप माना गया है तथा उसे ही आत्मा या जीव को बंधन में बांधनेवाला प्रमुख कारक माना गया है।
जैन परंपरा में आत्मा या जीव को चार अनन्त गुणों (अनन्तदर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य ) से युक्त माना गया है। कर्मावरण के कारण आत्मा के इस अनंतगुणात्मक शक्ति में कमी आ जाती है। इस अवस्था में वह संसारस्थ होकर 'स्व' तथा 'पर' के विक्षेप में फँस जाता है। विक्षेप की यह अवस्था जीव के बंधनयुक्त अवस्था का परिचायक है। कर्मावरण के हटते हीं जीव पुनः अनंतचतुष्टय रूप को प्राप्त कर लेता है। अनंतचतुष्टय रूप को प्राप्त करते ही जीव सांसारिक प्रपंचों से मुक्त होकर परमानंद की अवस्था में आ जाता है। इसे सिद्धावस्था, मोक्षावस्था, अरिहंतावस्था आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैन परम्परा में मानव का मुख्य ध्येय इसी परमसर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करना माना गया है। इस हेतु त्रिरत्न (सम्यक्दर्शन सम्यक्ज्ञान सम्यक्चारित्र) की साधना का अभ्यास अनिवार्य माना गया है। क्योंकि बिना इसके अभ्यास से मुक्ति या कर्मावरण का विच्छेदन कर पाना संभव नहीं है।
-
त्रिरत्न की साधना एक बृहत् एवं कठिन प्रक्रिया है । इस हेतु विभिन्न प्रकार के तपादि का अभ्यास किया जाता है तप के द्वारा संचित कर्मों की निर्जरा की जाती है क्योंकि जबतक कर्मों को पूर्णतः निर्जरित नहीं किया जाएगा, शुद्ध आत्मा का स्वरूप प्राप्त करना संभव नहीं है। इसके साथ ही साथ आत्मा की तरफ आनेवाले कर्म प्रवाह को भी रोकना होगा जिसे संवर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि कर्मों को निर्जरित करने की प्रक्रिया का तबतक कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, जबतक कि नए कर्मास्रव के प्रवाह को रोका नहीं जाए। इस हेतु व्यक्ति को अपने चंचल मन को एकाग्र करना पड़ता है कारण मन की चंचलता से शरीर और वाक् संयम प्रभावित होता रहता है। मन को एकाग्र करने की बहुत सारी प्रक्रियाओं में से एक है भावना या अनुप्रेक्षा । इस विषय पर जैनाचार्यों ने गहराई से चिंतन किया है।
Jain Education International
जैन परंपरा में 'भावना' या 'अनुप्रेक्षा' से तात्पर्य विचारों के सम्यक् चिन्तन से रहा है। प्रायः व्यक्ति के मन में नानाविध विचार पलते रहते हैं। व्यक्ति इन्हीं विचारों के वशीभूत होकर अपने कार्यों का संपादन करता है। कार्य संपादन की श्रृंखला में वह अपने मूल पथ से भटक जाता है। मूल उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधक को अपने विचार
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org