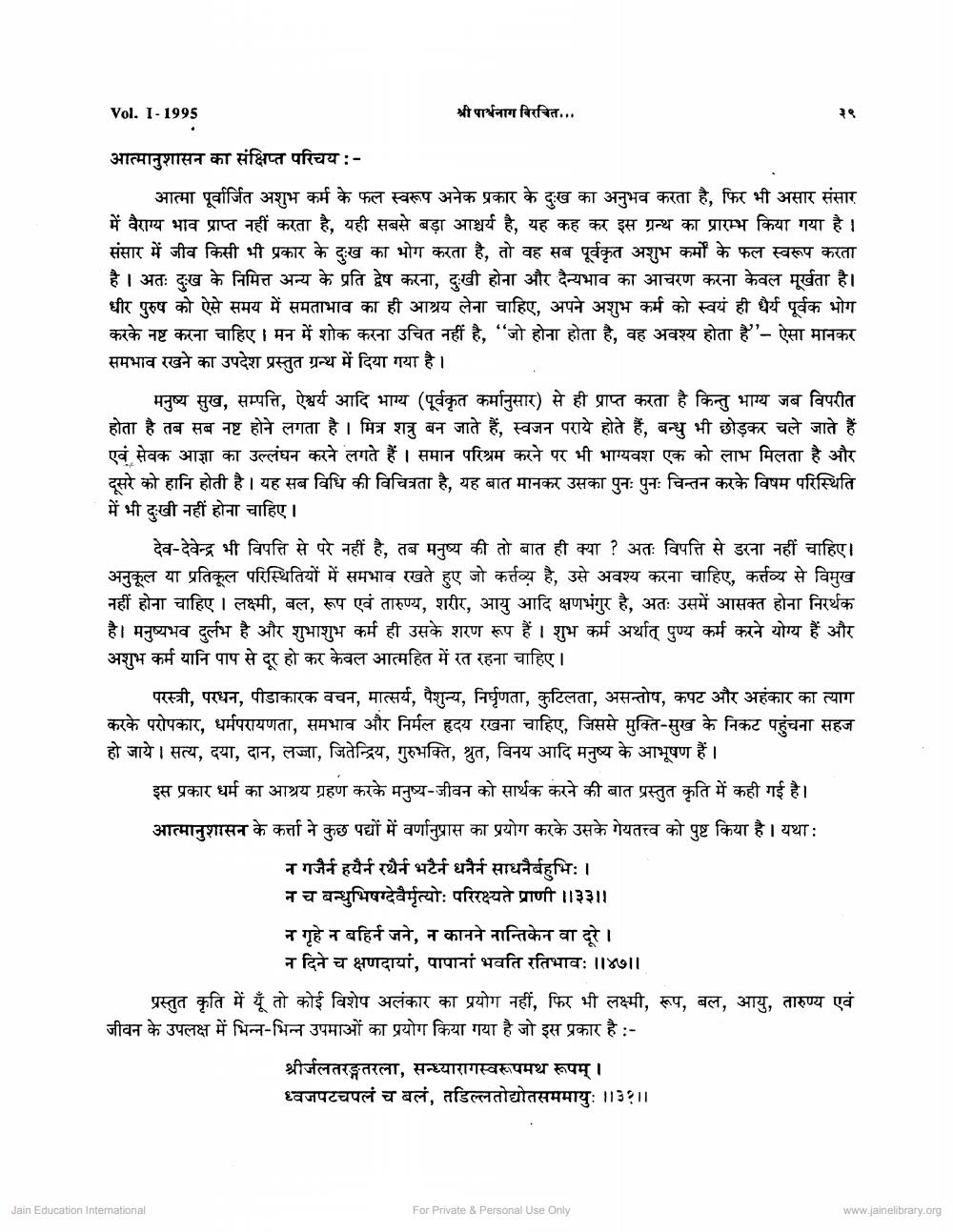________________
Vol. I-1995
श्री पार्थनाग विरचित...
आत्मानुशासन का संक्षिप्त परिचय :
आत्मा पूर्वार्जित अशुभ कर्म के फल स्वरूप अनेक प्रकार के दुःख का अनुभव करता है, फिर भी असार संसार में वैराग्य भाव प्राप्त नहीं करता है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, यह कह कर इस ग्रन्थ का प्रारम्भ किया गया है। संसार में जीव किसी भी प्रकार के दुःख का भोग करता है, तो वह सब पूर्वकृत अशुभ कर्मों के फल स्वरूप करता है। अतः दुख के निमित्त अन्य के प्रति द्वेष करना, दुःखी होना और दैन्यभाव का आचरण करना केवल मूर्खता है। धीर पुरुष को ऐसे समय में समताभाव का ही आश्रय लेना चाहिए, अपने अशुभ कर्म को स्वयं ही धैर्य पूर्वक भोग करके नष्ट करना चाहिए। मन में शोक करना उचित नहीं है, “जो होना होता है, वह अवश्य होता है"- ऐसा मानकर समभाव रखने का उपदेश प्रस्तुत ग्रन्थ में दिया गया है।
मनुष्य सुख, सम्पत्ति, ऐश्वर्य आदि भाग्य (पूर्वकृत कर्मानुसार) से ही प्राप्त करता है किन्तु भाग्य जब विपरीत होता है तब सब नष्ट होने लगता है। मित्र शत्रु बन जाते हैं, स्वजन पराये होते हैं, बन्धु भी छोड़कर चले जाते हैं एवं सेवक आज्ञा का उल्लंघन करने लगते हैं। समान परिश्रम करने पर भी भाग्यवश एक को लाभ मिलता है और दूसरे को हानि होती है। यह सब विधि की विचित्रता है, यह बात मानकर उसका पुनः पुनः चिन्तन करके विषम परिस्थिति में भी दुःखी नहीं होना चाहिए।
देव-देवेन्द्र भी विपत्ति से परे नहीं है, तब मनुष्य की तो बात ही क्या ? अतः विपत्ति से डरना नहीं चाहिए। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में समभाव रखते हुए जो कर्त्तव्य है, उसे अवश्य करना चाहिए, कर्त्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए । लक्ष्मी, बल, रूप एवं तारुण्य, शरीर, आयु आदि क्षणभंगुर है, अतः उसमें आसक्त होना निरर्थक है। मनुष्यभव दुर्लभ है और शुभाशुभ कर्म ही उसके शरण रूप हैं। शुभ कर्म अर्थात् पुण्य कर्म करने योग्य हैं और अशुभ कर्म यानि पाप से दूर हो कर केवल आत्महित में रत रहना चाहिए।
परस्त्री, परधन, पीडाकारक वचन, मात्सर्य, पैशुन्य, निघृणता, कुटिलता, असन्तोष, कपट और अहंकार का त्याग करके परोपकार, धर्मपरायणता, समभाव और निर्मल हृदय रखना चाहिए, जिससे मुक्ति-सुख के निकट पहुंचना सहज हो जाये। सत्य, दया, दान, लज्जा, जितेन्द्रिय, गुरुभक्ति, श्रुत, विनय आदि मनुष्य के आभूषण हैं।
इस प्रकार धर्म का आश्रय ग्रहण करके मनुष्य-जीवन को सार्थक करने की बात प्रस्तुत कृति में कही गई है। आत्मानुशासन के कर्ता ने कुछ पद्यों में वर्णानुप्रास का प्रयोग करके उसके गेयतत्त्व को पुष्ट किया है। यथा :
न गजैन हयैर्न रथैर्न भटैर्न धनैर्न साधनैर्बहुभिः । न च बन्धुभिषग्देवैर्मृत्योः परिरक्ष्यते प्राणी ॥३३॥ न गृहे न बहिर्न जने, न कानने नान्तिकेन वा दरे ।
न दिने च क्षणदायां, पापानां भवति रतिभावः ॥४७।। प्रस्तुत कृति में यूँ तो कोई विशेष अलंकार का प्रयोग नहीं, फिर भी लक्ष्मी, रूप, बल, आयु, तारुण्य एवं जीवन के उपलक्ष में भिन्न-भिन्न उपमाओं का प्रयोग किया गया है जो इस प्रकार है :
श्रीर्जलतरङ्गतरला, सन्ध्यारागस्वरूपमथ रूपम् । ध्वजपटचपलं च बलं, तडिल्लतोद्योतसममायुः ।। ३१।।
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org