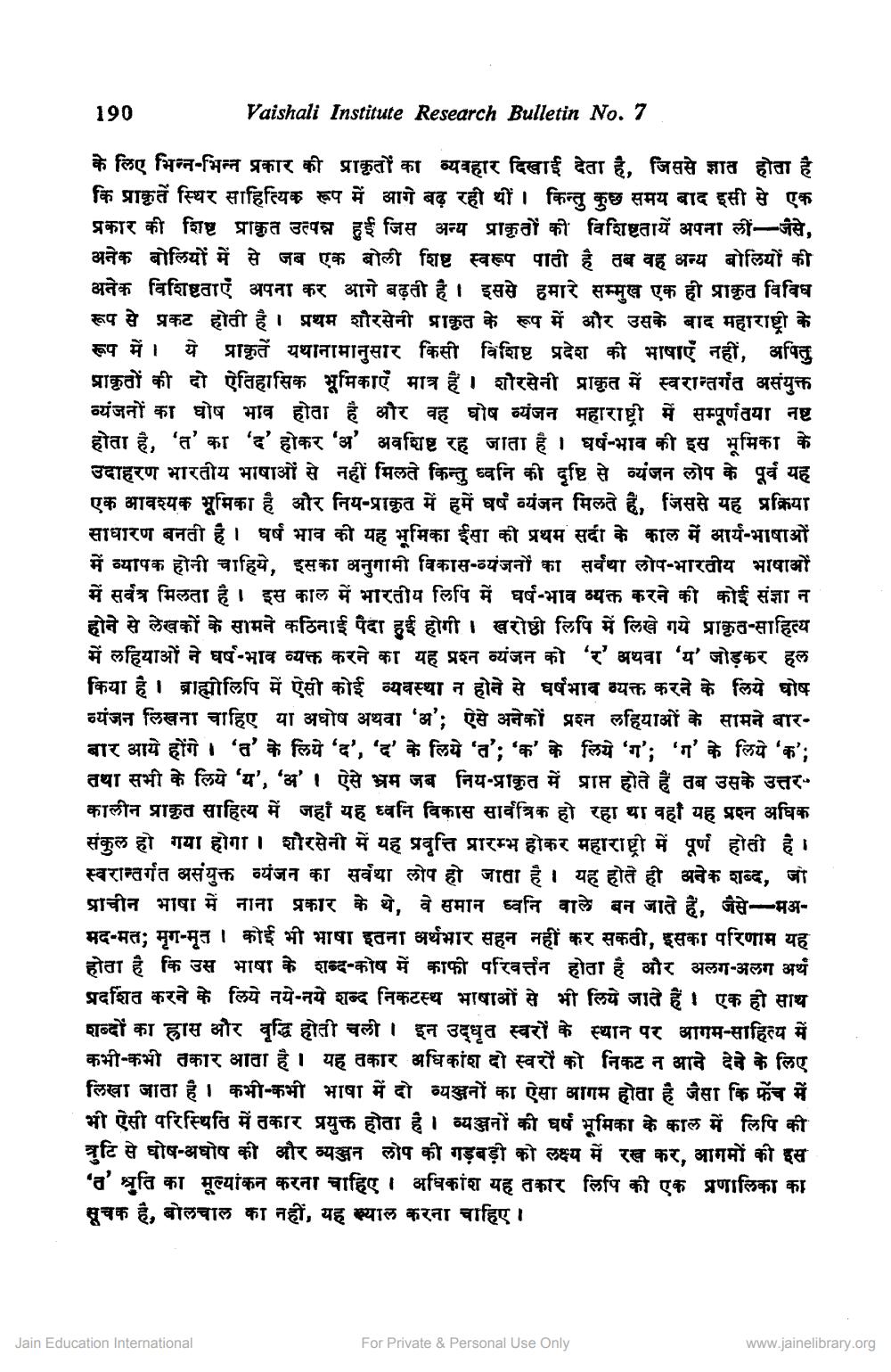________________
190
Vaishali Institute Research Bulletin No. 7
के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की प्राकृतों का व्यवहार दिखाई देता है, जिससे ज्ञात होता है कि प्राकृतें स्थिर साहित्यिक रूप में आगे बढ़ रही थीं। किन्तु कुछ समय बाद इसी से एक प्रकार की शिष्ट प्राकृत उत्पन्न हुई जिस अन्य प्राकृतों की विशिष्टतायें अपना लीं-जैसे, अनेक बोलियों में से जब एक बोली शिष्ट स्वरूप पाती है तब वह अन्य बोलियों की अनेक विशिष्टताएं अपना कर आगे बढ़ती है। इससे हमारे सम्मुख एक ही प्राकृत विविध रूप से प्रकट होती है। प्रथम शौरसेनी प्राकृत के रूप में और उसके बाद महाराष्ट्री के रूप में। ये प्राकृतें यथानामानुसार किसी विशिष्ट प्रदेश की भाषाएं नहीं, अपितु प्राकृतों की दो ऐतिहासिक भूमिकाएँ मात्र है। शौरसेनी प्राकृत में स्वरान्तर्गत असंयुक्त व्यंजनों का घोष भाव होता है और वह घोष व्यंजन महाराष्ट्री में सम्पूर्णतया नष्ट होता है, 'त' का 'द' होकर 'अ' अवशिष्ट रह जाता है । घर्ष-भाव की इस भूमिका के उदाहरण भारतीय भाषाओं से नहीं मिलते किन्तु ध्वनि की दृष्टि से व्यंजन लोप के पूर्व यह एक आवश्यक भूमिका है और निय-प्राकृत में हमें घर्ष व्यंजन मिलते हैं, जिससे यह प्रक्रिया साधारण बनती है। वर्ष भाव को यह भूमिका ईसा की प्रथम सदी के काल में आर्य भाषाओं में व्यापक होनी चाहिये, इसका अनुगामी विकास-व्यंजनों का सर्वथा लोप-भारतीय भाषाओं में सर्वत्र मिलता है। इस काल में भारतीय लिपि में घर्ष-भाव व्यक्त करने की कोई संज्ञा न होने से लेखकों के सामने कठिनाई पैदा हुई होगी। खरोष्ठी लिपि में लिखे गये प्राकृत-साहित्य में लहियाओं ने घर्ष-भाव व्यक्त करने का यह प्रश्न व्यंजन को 'र' अथवा 'य' जोड़कर हल किया है। ब्राह्मीलिपि में ऐसी कोई व्यवस्था न होने से घर्षभाव व्यक्त करने के लिये घोष व्यंजन लिखना चाहिए या अघोष अथवा 'अ'; ऐसे अनेकों प्रश्न लहियाओं के सामने बारबार आये होंगे । 'त' के लिये 'द', 'द' के लिये 'त'; 'क' के लिये 'ग'; 'ग' के लिये 'क'; तथा सभी के लिये 'य', 'अ' | ऐसे भ्रम जब निय-प्राकृत में प्राप्त होते हैं तब उसके उत्तरकालीन प्राकृत साहित्य में जहाँ यह ध्वनि विकास सार्वत्रिक हो रहा था वहाँ यह प्रश्न अधिक संकुल हो गया होगा। शौरसेनी में यह प्रवृत्ति प्रारम्भ होकर महाराष्ट्री में पूर्ण होती है। स्वरान्तर्गत असंयुक्त व्यंजन का सर्वथा लोप हो जाता है। यह होते ही अनेक शब्द, जो प्राचीन भाषा में नाना प्रकार के थे. वे समान ध्वनि वाले बन जाते हैं. जैसे-मअमद-मत; मृग-मृत । कोई भी भाषा इतना अर्थभार सहन नहीं कर सकती, इसका परिणाम यह होता है कि उस भाषा के शब्द-कोष में काफी परिवर्तन होता है और अलग-अलग अर्थ प्रदर्शित करने के लिये नये-नये शब्द निकटस्थ भाषाओं से भी लिये जाते हैं। एक ही साथ शब्दों का ह्रास और वृद्धि होती चली। इन उद्धृत स्वरों के स्थान पर आगम-साहित्य में कभी-कभी तकार आता है। यह तकार अधिकांश दो स्वरों को निकट न आने देने के लिए लिखा जाता है। कभी-कभी भाषा में दो व्यञ्जनों का ऐसा आगम होता है जैसा कि फ्रेंच में भी ऐसी परिस्थिति में तकार प्रयुक्त होता है। व्यञ्जनों की घर्ष भूमिका के काल में लिपि की त्रुटि से घोष-अघोष की और व्यञ्जन लोप की गड़बड़ी को लक्ष्य में रख कर, आगमों की इस '' श्रुति का मूल्यांकन करना चाहिए । अधिकांश यह तकार लिपि की एक प्रणालिका का सूचक है, बोलचाल का नहीं, यह ख्याल करना चाहिए।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org