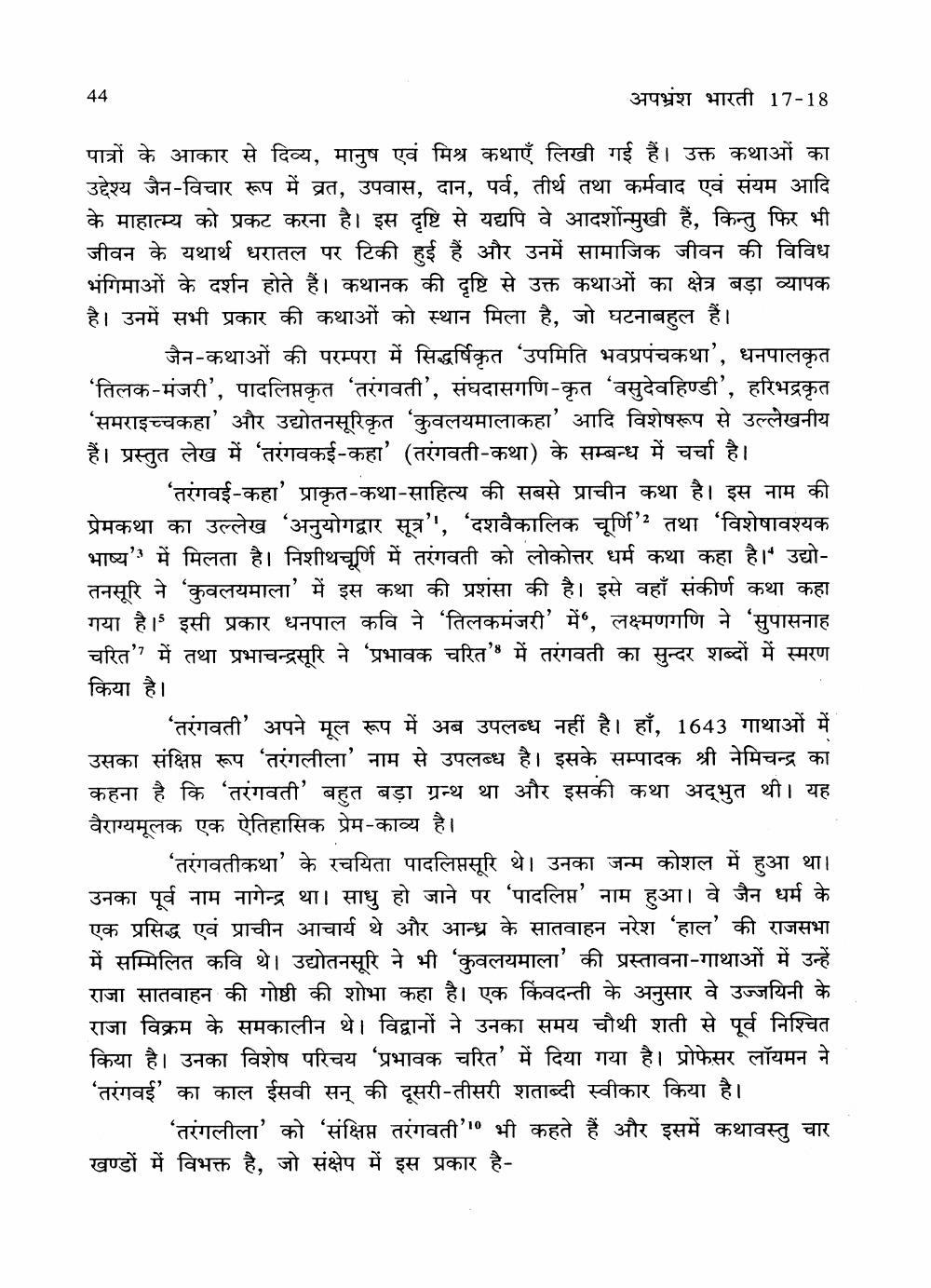________________
44
अपभ्रंश भारती 17-18
पात्रों के आकार से दिव्य, मानुष एवं मिश्र कथाएँ लिखी गई हैं। उक्त कथाओं का उद्देश्य जैन-विचार रूप में व्रत, उपवास, दान, पर्व, तीर्थ तथा कर्मवाद एवं संयम आदि के माहात्म्य को प्रकट करना है। इस दृष्टि से यद्यपि वे आदर्शोन्मुखी हैं, किन्तु फिर भी जीवन के यथार्थ धरातल पर टिकी हुई हैं और उनमें सामाजिक जीवन की विविध भंगिमाओं के दर्शन होते हैं। कथानक की दृष्टि से उक्त कथाओं का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। उनमें सभी प्रकार की कथाओं को स्थान मिला है, जो घटनाबहुल हैं।
जैन-कथाओं की परम्परा में सिद्धर्षिकृत ‘उपमिति भवप्रपंचकथा', धनपालकृत 'तिलक-मंजरी', पादलिप्तकृत 'तरंगवती', संघदासगणि-कृत 'वसुदेवहिण्डी', हरिभद्रकृत ‘समराइच्चकहा' और उद्योतनसूरिकृत 'कुवलयमालाकहा' आदि विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। प्रस्तुत लेख में 'तरंगवकई-कहा' (तरंगवती-कथा) के सम्बन्ध में चर्चा है।
'तरंगवई-कहा' प्राकृत-कथा-साहित्य की सबसे प्राचीन कथा है। इस नाम की प्रेमकथा का उल्लेख 'अनुयोगद्वार सूत्र'', 'दशवैकालिक चूर्णि' तथा 'विशेषावश्यक भाष्य'' में मिलता है। निशीथचूर्णि में तरंगवती को लोकोत्तर धर्म कथा कहा है।' उद्योतनसूरि ने 'कुवलयमाला' में इस कथा की प्रशंसा की है। इसे वहाँ संकीर्ण कथा कहा गया है। इसी प्रकार धनपाल कवि ने 'तिलकमंजरी' में", लक्ष्मणगणि ने 'सुपासनाह चरित'' में तथा प्रभाचन्द्रसूरि ने ‘प्रभावक चरित' में तरंगवती का सुन्दर शब्दों में स्मरण किया है।
'तरंगवती' अपने मूल रूप में अब उपलब्ध नहीं है। हाँ, 1643 गाथाओं में उसका संक्षिप्त रूप 'तरंगलीला' नाम से उपलब्ध है। इसके सम्पादक श्री नेमिचन्द्र का कहना है कि 'तरंगवती' बहुत बड़ा ग्रन्थ था और इसकी कथा अद्भुत थी। यह वैराग्यमूलक एक ऐतिहासिक प्रेम-काव्य है।
'तरंगवतीकथा' के रचयिता पादलिप्तसूरि थे। उनका जन्म कोशल में हुआ था। उनका पूर्व नाम नागेन्द्र था। साधु हो जाने पर ‘पादलिप्त' नाम हुआ। वे जैन धर्म के एक प्रसिद्ध एवं प्राचीन आचार्य थे और आन्ध्र के सातवाहन नरेश ‘हाल' की राजसभा में सम्मिलित कवि थे। उद्योतनसूरि ने भी 'कुवलयमाला' की प्रस्तावना-गाथाओं में उन्हें राजा सातवाहन की गोष्ठी की शोभा कहा है। एक किंवदन्ती के अनुसार वे उज्जयिनी के राजा विक्रम के समकालीन थे। विद्वानों ने उनका समय चौथी शती से पूर्व निश्चित किया है। उनका विशेष परिचय ‘प्रभावक चरित' में दिया गया है। प्रोफेसर लॉयमन ने 'तरंगवई' का काल ईसवी सन् की दूसरी-तीसरी शताब्दी स्वीकार किया है।
तरंगलीला' को 'संक्षिप्त तरंगवती' भी कहते हैं और इसमें कथावस्तु चार खण्डों में विभक्त है, जो संक्षेप में इस प्रकार है