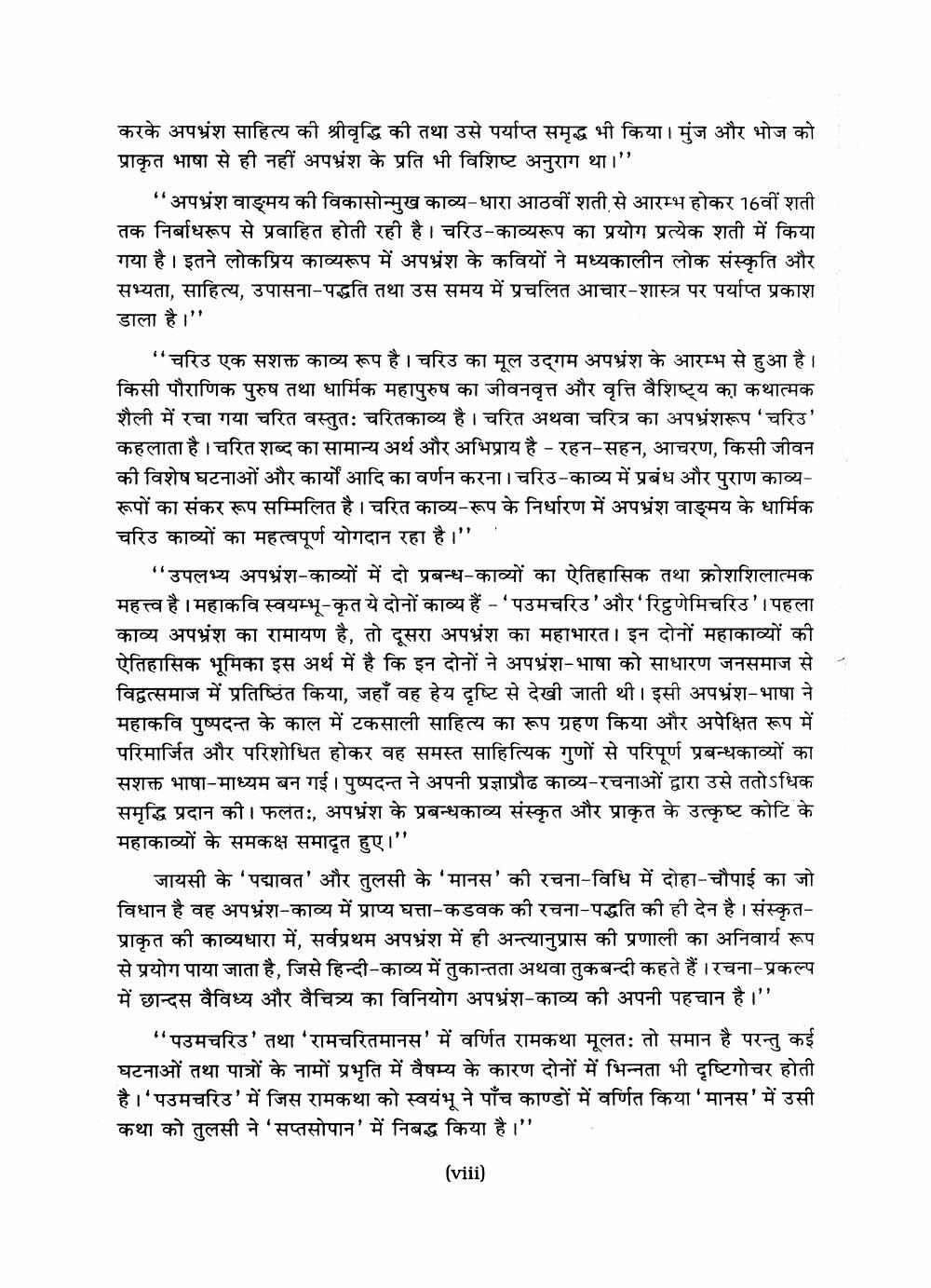________________
करके अपभ्रंश साहित्य की श्रीवृद्धि की तथा उसे पर्याप्त समृद्ध भी किया। मुंज और भोज को प्राकृत भाषा से ही नहीं अपभ्रंश के प्रति भी विशिष्ट अनुराग था।"
"अपभ्रंश वाङ्मय की विकासोन्मुख काव्य-धारा आठवीं शती से आरम्भ होकर 16वीं शती तक निर्बाधरूप से प्रवाहित होती रही है। चरिउ-काव्यरूप का प्रयोग प्रत्येक शती में किया गया है। इतने लोकप्रिय काव्यरूप में अपभ्रंश के कवियों ने मध्यकालीन लोक संस्कृति और सभ्यता, साहित्य, उपासना-पद्धति तथा उस समय में प्रचलित आचार-शास्त्र पर पर्याप्त प्रकाश डाला है।"
"चरिउ एक सशक्त काव्य रूप है । चरिउ का मूल उद्गम अपभ्रंश के आरम्भ से हुआ है। किसी पौराणिक पुरुष तथा धार्मिक महापुरुष का जीवनवृत्त और वृत्ति वैशिष्ट्य का कथात्मक शैली में रचा गया चरित वस्तुत: चरितकाव्य है। चरित अथवा चरित्र का अपभ्रंशरूप 'चरिउ' कहलाता है । चरित शब्द का सामान्य अर्थ और अभिप्राय है - रहन-सहन, आचरण, किसी जीवन की विशेष घटनाओं और कार्यों आदि का वर्णन करना। चरिउ-काव्य में प्रबंध और पुराण काव्यरूपों का संकर रूप सम्मिलित है। चरित काव्य-रूप के निर्धारण में अपभ्रंश वाङ्मय के धार्मिक चरिउ काव्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।''
"उपलभ्य अपभ्रंश-काव्यों में दो प्रबन्ध-काव्यों का ऐतिहासिक तथा क्रोशशिलात्मक महत्त्व है । महाकवि स्वयम्भू-कृत ये दोनों काव्य हैं - 'पउमचरिउ' और 'रिट्ठणेमिचरिउ' । पहला काव्य अपभ्रंश का रामायण है, तो दूसरा अपभ्रंश का महाभारत। इन दोनों महाकाव्यों की ऐतिहासिक भूमिका इस अर्थ में है कि इन दोनों ने अपभ्रंश-भाषा को साधारण जनसमाज से - विद्वत्समाज में प्रतिष्ठित किया. जहाँ वह हेय दृष्टि से देखी जाती थी। इसी अपभ्रंश-भाषा ने महाकवि पुष्पदन्त के काल में टकसाली साहित्य का रूप ग्रहण किया और अपेक्षित रूप में परिमार्जित और परिशोधित होकर वह समस्त साहित्यिक गणों से परिपूर्ण प्रबन्धकाव्यों का सशक्त भाषा-माध्यम बन गई। पष्पदन्त ने अपनी प्रज्ञाप्रौढ काव्य-रचनाओं द्वारा उसे ततोऽधिक समद्धि प्रदान की। फलतः अपभ्रंश के प्रबन्धकाव्य संस्कृत और प्राकत के उत्कृष्ट कोटि के महाकाव्यों के समकक्ष समादृत हुए।"
जायसी के 'पद्मावत' और तुलसी के 'मानस' की रचना-विधि में दोहा-चौपाई का जो विधान है वह अपभ्रंश-काव्य में प्राप्य घत्ता-कडवक की रचना-पद्धति की ही देन है। संस्कृतप्राकृत की काव्यधारा में, सर्वप्रथम अपभ्रंश में ही अन्त्यानुप्रास की प्रणाली का अनिवार्य रूप से प्रयोग पाया जाता है, जिसे हिन्दी-काव्य में तुकान्तता अथवा तुकबन्दी कहते हैं । रचना-प्रकल्प में छान्दस वैविध्य और वैचित्र्य का विनियोग अपभ्रंश-काव्य की अपनी पहचान है।''
"पउमचरिउ' तथा 'रामचरितमानस' में वर्णित रामकथा मूलत: तो समान है परन्तु कई घटनाओं तथा पात्रों के नामों प्रभृति में वैषम्य के कारण दोनों में भिन्नता भी दृष्टिगोचर होती है। 'पउमचरिउ' में जिस रामकथा को स्वयंभू ने पाँच काण्डों में वर्णित किया 'मानस' में उसी कथा को तुलसी ने 'सप्तसोपान' में निबद्ध किया है।"
(viii)