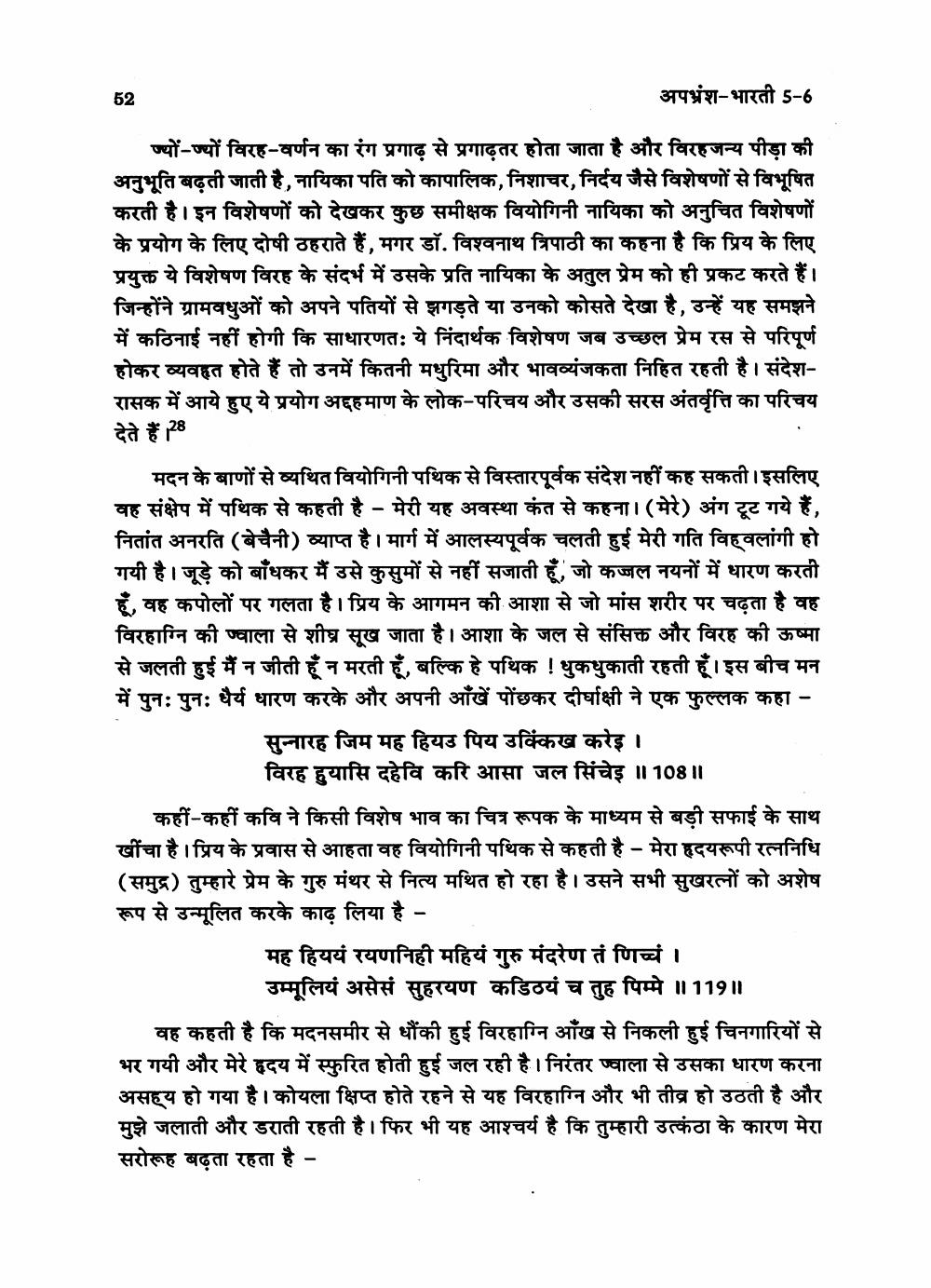________________
अपभ्रंश - भारती 5-6
ज्यों-ज्यों विरह-वर्णन का रंग प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर होता जाता है और विरहजन्य पीड़ा की अनुभूति बढ़ती जाती है, नायिका पति को कापालिक, निशाचर, निर्दय जैसे विशेषणों से विभूषित करती है। इन विशेषणों को देखकर कुछ समीक्षक वियोगिनी नायिका को अनुचित विशेषणों के प्रयोग के लिए दोषी ठहराते हैं, मगर डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी का कहना है कि प्रिय के लिए प्रयुक्त ये विशेषण विरह के संदर्भ में उसके प्रति नायिका के अतुल प्रेम को ही प्रकट करते हैं। जिन्होंने ग्रामवधुओं को अपने पतियों से झगड़ते या उनको कोसते देखा है, उन्हें यह समझने में कठिनाई नहीं होगी कि साधारणतः ये निंदार्थक विशेषण जब उच्छल प्रेम रस से परिपूर्ण होकर व्यवहृत होते हैं तो उनमें कितनी मधुरिमा और भावव्यंजकता निहित रहती है। संदेशरासक में आये हुए ये प्रयोग अद्दहमाण के लोक-परिचय और उसकी सरस अंतर्वृत्ति का परिचय देते हैं 28
52
'टूट'
मदन के बाणों से व्यथित वियोगिनी पथिक से विस्तारपूर्वक संदेश नहीं कह सकती। इसलिए वह संक्षेप में पथिक से कहती है मेरी यह अवस्था कंत से कहना। (मेरे) अंग गये हैं, नितांत अनरति (बेचैनी) व्याप्त है। मार्ग में आलस्यपूर्वक चलती हुई मेरी गति विह्वलांगी हो गयी है। जूड़े को बाँधकर मैं उसे कुसुमों से नहीं सजाती हूँ, जो कज्जल नयनों में धारण करती हूँ, वह कपोलों पर गलता है। प्रिय के आगमन की आशा से जो मांस शरीर पर चढ़ता है वह विरहाग्नि की ज्वाला से शीघ्र सूख जाता है। आशा के जल से संसिक्त और विरह की ऊष्मा से जलती हुई मैं न जीती हूँ न मरती हूँ, बल्कि हे पथिक ! धुकधुकाती रहती हूँ। इस बीच मन में पुनः पुनः धैर्य धारण करके और अपनी आँखें पोंछकर दीर्घाक्षी ने एक फुल्लक कहा -
-
सुन्नारह जिम मह हियउ पिय उक्किख करेई ।
विरह हुयासि दहेवि करि आसा जल सिंचेइ ॥ 108 ॥
कहीं-कहीं कवि ने किसी विशेष भाव का चित्र रूपक के माध्यम से बड़ी सफाई के साथ खींचा है। प्रिय के प्रवास से आहता वह वियोगिनी पथिक से कहती है- मेरा हृदयरूपी रत्ननिधि (समुद्र) तुम्हारे प्रेम के गुरु मंथर से नित्य मथित हो रहा है। उसने सभी सुखरत्नों को अशेष रूप से उन्मूलित करके काढ़ लिया है।
-
मह हिययं रयणनिही महियं गुरु मंदरेण तं णिच्चं ।
उम्मूलियं असेसं सुहरयण कडिठयं च तुह पिम्मे ॥ 119 ॥
वह कहती है कि मदनसमीर से धौंकी हुई विरहाग्नि आँख से निकली हुई चिनगारियों से भर गयी और मेरे हृदय में स्फुरित होती हुई जल रही है। निरंतर ज्वाला से उसका धारण करना असह्य हो गया है। कोयला क्षिप्त होते रहने से यह विरहाग्नि और भी तीव्र हो उठती है और मुझे जलाती और डराती रहती है। फिर भी यह आश्चर्य है कि तुम्हारी उत्कंठा के कारण मेरा सरोरूह बढ़ता रहता है
-