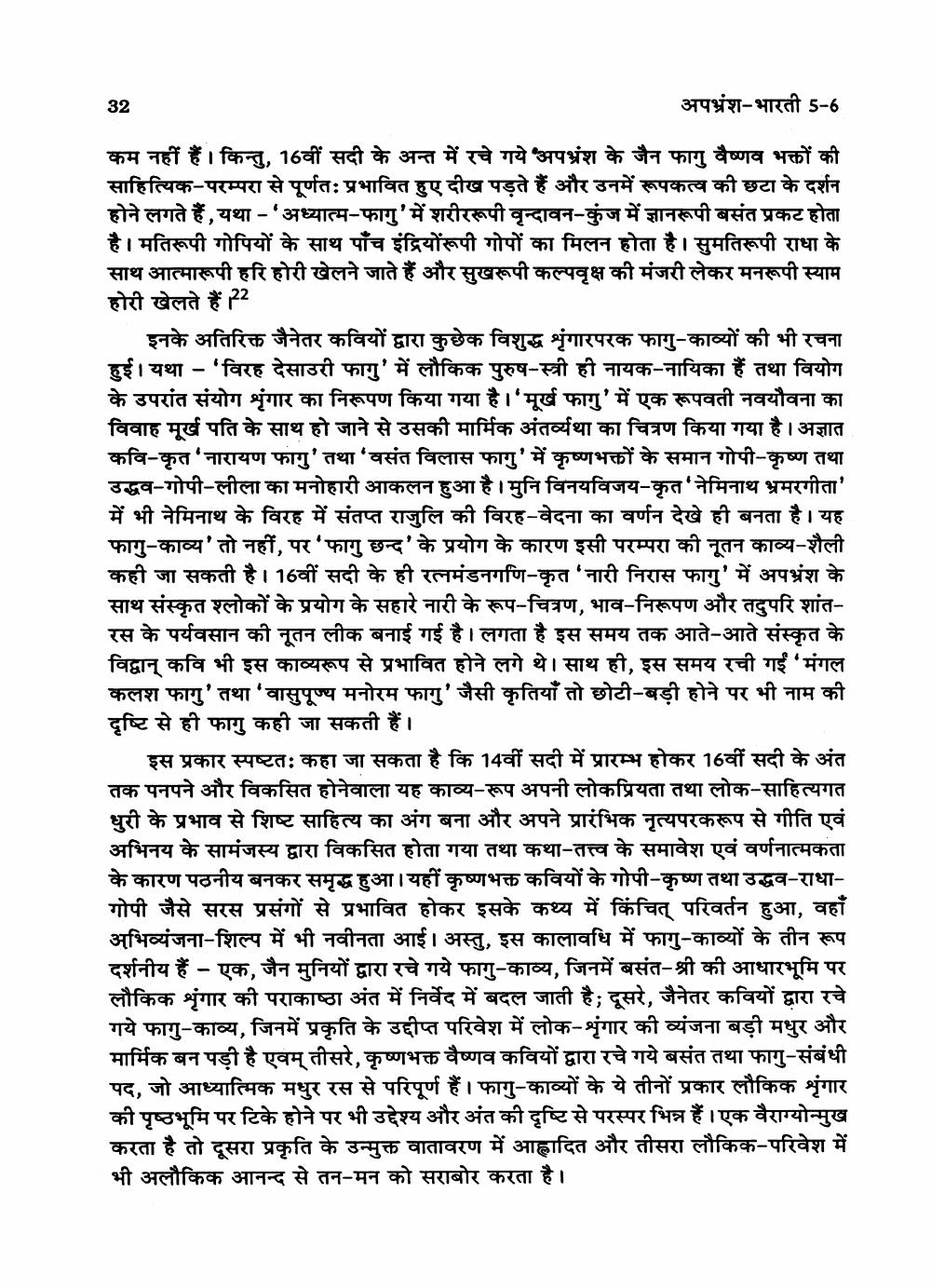________________
32
अपभ्रंश-भारती 5-6
कम नहीं हैं। किन्तु, 16वीं सदी के अन्त में रचे गये 'अपभ्रंश के जैन फाग वैष्णव भक्तों की साहित्यिक-परम्परा से पूर्णतःप्रभावित हुए दीख पड़ते हैं और उनमें रूपकत्व की छटा के दर्शन होने लगते हैं, यथा - 'अध्यात्म-फागु' में शरीररूपी वृन्दावन-कुंज में ज्ञानरूपी बसंत प्रकट होता है। मतिरूपी गोपियों के साथ पाँच इंद्रियोंरूपी गोपों का मिलन होता है। सुमतिरूपी राधा के साथ आत्मारूपी हरि होरी खेलने जाते हैं और सुखरूपी कल्पवृक्ष की मंजरी लेकर मनरूपी स्याम होरी खेलते हैं
इनके अतिरिक्त जैनेतर कवियों द्वारा कुछेक विशुद्ध शृंगारपरक फागु-काव्यों की भी रचना हुई। यथा - 'विरह देसाउरी फागु' में लौकिक पुरुष-स्त्री ही नायक-नायिका हैं तथा वियोग के उपरांत संयोग श्रृंगार का निरूपण किया गया है। मूर्ख फागु' में एक रूपवती नवयौवना का विवाह मूर्ख पति के साथ हो जाने से उसकी मार्मिक अंतर्व्यथा का चित्रण किया गया है। अज्ञात कवि-कृत 'नारायण फागु' तथा 'वसंत विलास फागु' में कृष्णभक्तों के समान गोपी-कृष्ण तथा उद्धव-गोपी-लीला का मनोहारी आकलन हुआ है। मुनि विनयविजय-कृत 'नेमिनाथ भ्रमरगीता' में भी नेमिनाथ के विरह में संतप्त राजुलि की विरह-वेदना का वर्णन देखे ही बनता है। यह फागु-काव्य' तो नहीं, पर 'फागु छन्द' के प्रयोग के कारण इसी परम्परा की नूतन काव्य-शैली कही जा सकती है। 16वीं सदी के ही रत्नमंडनगणि-कृत 'नारी निरास फागु' में अपभ्रंश के साथ संस्कृत श्लोकों के प्रयोग के सहारे नारी के रूप-चित्रण, भाव-निरूपण और तदुपरि शांतरस के पर्यवसान की नूतन लीक बनाई गई है। लगता है इस समय तक आते-आते संस्कृत के विद्वान् कवि भी इस काव्यरूप से प्रभावित होने लगे थे। साथ ही, इस समय रची गई 'मंगल कलश फागु' तथा 'वासुपूण्य मनोरम फागु' जैसी कृतियाँ तो छोटी-बड़ी होने पर भी नाम की दृष्टि से ही फागु कही जा सकती हैं।
इस प्रकार स्पष्टतः कहा जा सकता है कि 14वीं सदी में प्रारम्भ होकर 16वीं सदी के अंत तक पनपने और विकसित होनेवाला यह काव्य-रूप अपनी लोकप्रियता तथा लोक-साहित्यगत धुरी के प्रभाव से शिष्ट साहित्य का अंग बना और अपने प्रारंभिक नृत्यपरकरूप से गीति एवं अभिनय के सामंजस्य द्वारा विकसित होता गया तथा कथा-तत्त्व के समावेश एवं वर्णनात्मकता के कारण पठनीय बनकर समृद्ध हुआ। यहीं कृष्णभक्त कवियों के गोपी-कृष्ण तथा उद्धव-राधागोपी जैसे सरस प्रसंगों से प्रभावित होकर इसके कथ्य में किंचित् परिवर्तन हुआ, वहाँ अभिव्यंजना-शिल्प में भी नवीनता आई। अस्तु, इस कालावधि में फागु-काव्यों के तीन रूप दर्शनीय हैं - एक, जैन मुनियों द्वारा रचे गये फागु-काव्य, जिनमें बसंत-श्री की आधारभूमि पर लौकिक शृंगार की पराकाष्ठा अंत में निर्वेद में बदल जाती है। दूसरे, जैनेतर कवियों द्वारा रचे गये फागु-काव्य, जिनमें प्रकृति के उद्दीप्त परिवेश में लोक-श्रृंगार की व्यंजना बड़ी मधुर और मार्मिक बन पड़ी है एवम् तीसरे, कृष्णभक्त वैष्णव कवियों द्वारा रचे गये बसंत तथा फागु-संबंधी पद, जो आध्यात्मिक मधुर रस से परिपूर्ण हैं। फागु-काव्यों के ये तीनों प्रकार लौकिक शृंगार की पृष्ठभूमि पर टिके होने पर भी उद्देश्य और अंत की दृष्टि से परस्पर भिन्न हैं । एक वैराग्योन्मुख करता है तो दूसरा प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में आह्लादित और तीसरा लौकिक-परिवेश में भी अलौकिक आनन्द से तन-मन को सराबोर करता है।