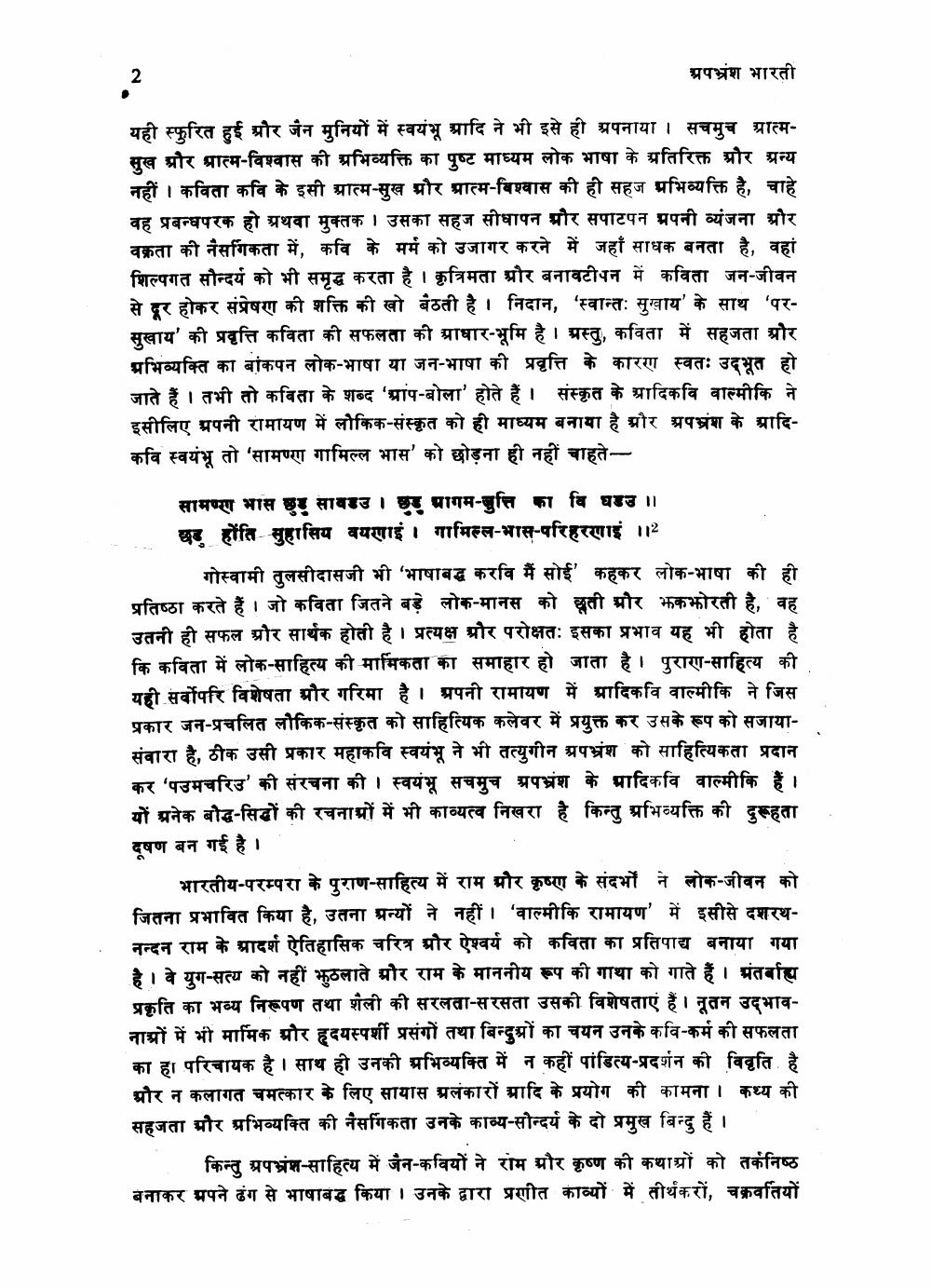________________
अपभ्रंश भारती
यही स्फुरित हुई और जैन मुनियों में स्वयंभू आदि ने भी इसे ही अपनाया। सचमुच प्रात्मसुख और प्रात्म-विश्वास की अभिव्यक्ति का पुष्ट माध्यम लोक भाषा के अतिरिक्त और अन्य नहीं । कविता कवि के इसी प्रात्म-सुख और प्रात्म-विश्वास की ही सहज अभिव्यक्ति है, चाहे वह प्रबन्धपरक हो अथवा मुक्तक । उसका सहज सीधापन और सपाटपन अपनी व्यंजना और वक्रता की नैसर्गिकता में, कवि के मर्म को उजागर करने में जहाँ साधक बनता है, वहां शिल्पगत सौन्दर्य को भी समृद्ध करता है । कृत्रिमता और बनावटीपन में कविता जन-जीवन से दूर होकर संप्रेषण की शक्ति की खो बैठती है । निदान, 'स्वान्तः सुखाय' के साथ 'परसुखाय' की प्रवृत्ति कविता की सफलता की आधार-भूमि है । प्रस्तु, कविता में सहजता और अभिव्यक्ति का बांकपन लोक-भाषा या जन-भाषा की प्रवृत्ति के कारण स्वतः उद्भूत हो जाते हैं। तभी तो कविता के शब्द 'प्राप-बोला' होते हैं। संस्कृत के आदिकवि वाल्मीकि ने इसीलिए अपनी रामायण में लौकिक-संस्कृत को ही माध्यम बनाया है और अपभ्रंश के प्रादिकवि स्वयंभू तो 'सामण्ण गामिल्ल भास' को छोड़ना ही नहीं चाहते
सामण्ण भास छु, सावरउ । छुड़ मागम-सुत्ति का वि घडउ ॥ छड होति सुहासिय वयणाई। गामिल्ल-भास-परिहरणाई ॥
___गोस्वामी तुलसीदासजी भी 'भाषाबद्ध करवि मैं सोई' कहकर लोक-भाषा की ही प्रतिष्ठा करते हैं । जो कविता जितने बड़े लोक-मानस को छूती और झकझोरती है, वह उतनी ही सफल और सार्थक होती है। प्रत्यक्ष और परोक्षतः इसका प्रभाव यह भी होता है कि कविता में लोक-साहित्य की मार्मिकता का समाहार हो जाता है। पराण-साहित्य की यही सर्वोपरि विशेषता और गरिमा है। अपनी रामायण में प्रादिकवि वाल्मीकि ने जिस प्रकार जन-प्रचलित लौकिक-संस्कृत को साहित्यिक कलेवर में प्रयुक्त कर उसके रूप को सजायासंवारा है, ठीक उसी प्रकार महाकवि स्वयंभू ने भी तत्यूगीन अपभ्रंश को साहित्यिकता प्रदान कर 'पउमचरिउ' की संरचना की। स्वयंभ सचमच अपभ्रंश के प्रादिकवि वाल्मीकि हैं। गों अनेक बौद्ध-सिद्धों की रचनामों में भी काव्यत्व निखरा है किन्तु अभिव्यक्ति की दुरूहता दूषण बन गई है।
भारतीय-परम्परा के पुराण-साहित्य में राम और कृष्ण के संदर्भो ने लोक-जीवन को जितना प्रभावित किया है, उतना अन्यों ने नहीं। 'वाल्मीकि रामायण' में इसीसे दशरथनन्दन राम के आदर्श ऐतिहासिक चरित्र और ऐश्वर्य को कविता का प्रतिपाद्य बनाया गया है। वे युग-सत्य को नहीं झुठलाते और राम के माननीय रूप की गाथा को गाते हैं । अंतर्बाह्य प्रकृति का भव्य निरूपण तथा शैली की सरलता-सरसता उसकी विशेषताएं हैं। नूतन उद्भावनाओं में भी मार्मिक और हृदयस्पर्शी प्रसंगों तथा बिन्दुओं का चयन उनके कवि-कर्म की सफलता का हा परिचायक है । साथ ही उनकी अभिव्यक्ति में न कहीं पांडित्य-प्रदर्शन की विवृति है
और न कलागत चमत्कार के लिए सायास अलंकारों आदि के प्रयोग की कामना। कथ्य की सहजता और अभिव्यक्ति की नैसर्गिकता उनके काव्य-सौन्दर्य के दो प्रमुख बिन्दु हैं ।
किन्तु अपभ्रंश-साहित्य में जैन-कवियों ने राम और कृष्ण की कथानों को तर्कनिष्ठ बनाकर अपने ढंग से भाषाबद्ध किया। उनके द्वारा प्रणीत काव्यों में तीर्थंकरों, चक्रवतियों