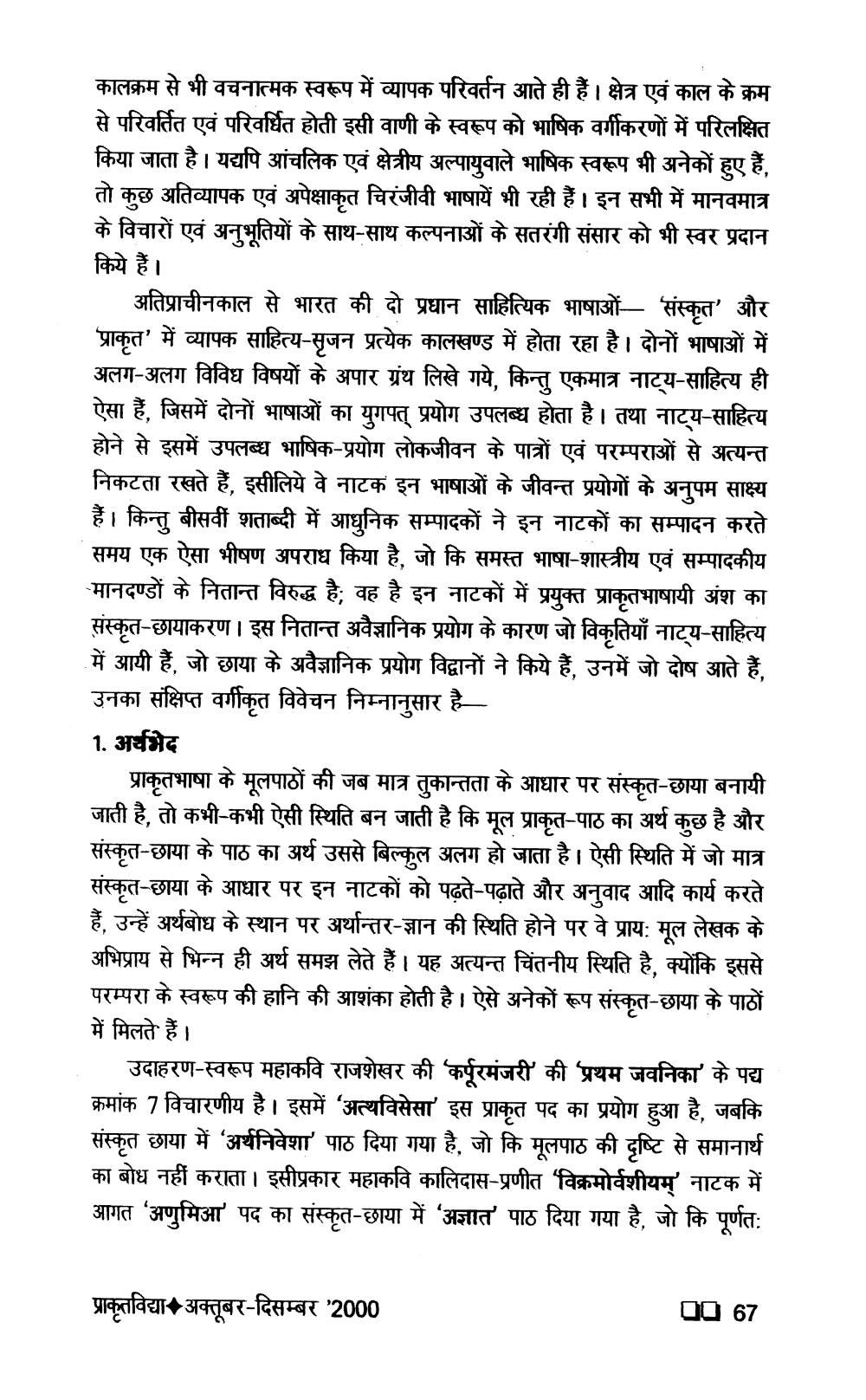________________
कालक्रम से भी वचनात्मक स्वरूप में व्यापक परिवर्तन आते ही हैं। क्षेत्र एवं काल के क्रम से परिवर्तित एवं परिवर्धित होती इसी वाणी के स्वरूप को भाषिक वर्गीकरणों में परिलक्षित किया जाता है। यद्यपि आंचलिक एवं क्षेत्रीय अल्पायुवाले भाषिक स्वरूप भी अनेकों हुए हैं, तो कुछ अतिव्यापक एवं अपेक्षाकृत चिरंजीवी भाषायें भी रही हैं। इन सभी में मानवमात्र के विचारों एवं अनुभूतियों के साथ-साथ कल्पनाओं के सतरंगी संसार को भी स्वर प्रदान किये हैं।
अतिप्राचीनकाल से भारत की दो प्रधान साहित्यिक भाषाओं- संस्कृत' और प्राकृत' में व्यापक साहित्य-सृजन प्रत्येक कालखण्ड में होता रहा है। दोनों भाषाओं में अलग-अलग विविध विषयों के अपार ग्रंथ लिखे गये, किन्तु एकमात्र नाट्य-साहित्य ही ऐसा हैं, जिसमें दोनों भाषाओं का युगपत् प्रयोग उपलब्ध होता है। तथा नाट्य-साहित्य होने से इसमें उपलब्ध भाषिक-प्रयोग लोकजीवन के पात्रों एवं परम्पराओं से अत्यन्त निकटता रखते हैं, इसीलिये वे नाटक इन भाषाओं के जीवन्त प्रयोगों के अनुपम साक्ष्य हैं। किन्तु बीसवीं शताब्दी में आधुनिक सम्पादकों ने इन नाटकों का सम्पादन करते समय एक ऐसा भीषण अपराध किया है, जो कि समस्त भाषा-शास्त्रीय एवं सम्पादकीय मानदण्डों के नितान्त विरुद्ध है; वह है इन नाटकों में प्रयुक्त प्राकृतभाषायी अंश का संस्कृत-छायाकरण। इस नितान्त अवैज्ञानिक प्रयोग के कारण जो विकृतियाँ नाट्य-साहित्य में आयी हैं, जो छाया के अवैज्ञानिक प्रयोग विद्वानों ने किये हैं, उनमें जो दोष आते हैं, उनका संक्षिप्त वर्गीकृत विवेचन निम्नानुसार है1. अर्थभेद
प्राकृतभाषा के मूलपाठों की जब मात्र तुकान्तता के आधार पर संस्कृत-छाया बनायी जाती है, तो कभी-कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि मूल प्राकृत-पाठ का अर्थ कुछ है और संस्कृत-छाया के पाठ का अर्थ उससे बिल्कुल अलग हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो मात्र संस्कृत-छाया के आधार पर इन नाटकों को पढ़ते-पढ़ाते और अनुवाद आदि कार्य करते हैं, उन्हें अर्थबोध के स्थान पर अर्थान्तर-ज्ञान की स्थिति होने पर वे प्राय: मूल लेखक के अभिप्राय से भिन्न ही अर्थ समझ लेते हैं। यह अत्यन्त चिंतनीय स्थिति है, क्योंकि इससे परम्परा के स्वरूप की हानि की आशंका होती है। ऐसे अनेकों रूप संस्कृत-छाया के पाठों में मिलते हैं।
उदाहरण-स्वरूप महाकवि राजशेखर की कर्पूरमंजरी की प्रथम जवनिका के पद्य क्रमांक 7 विचारणीय है। इसमें ‘अत्थविसेसा' इस प्राकृत पद का प्रयोग हुआ है, जबकि संस्कृत छाया में 'अर्थनिवेशा' पाठ दिया गया है, जो कि मूलपाठ की दृष्टि से समानार्थ का बोध नहीं कराता। इसीप्रकार महाकवि कालिदास-प्रणीत 'विक्रमोर्वशीयम्' नाटक में आगत 'अणुमिआ' पद का संस्कृत-छाया में 'अज्ञात' पाठ दिया गया है, जो कि पूर्णत:
प्राकृतविद्या अक्तूबर-दिसम्बर '2000
4067