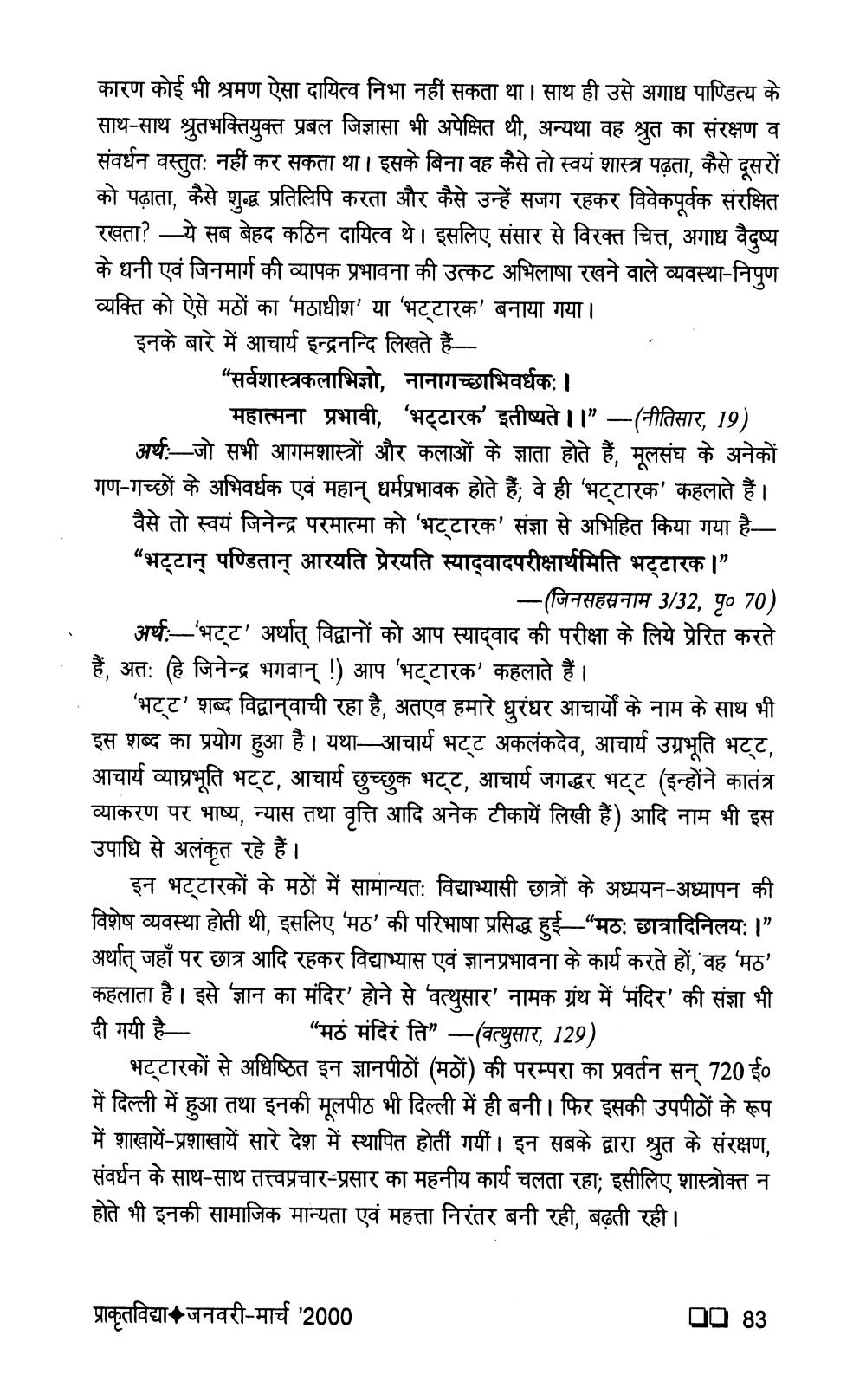________________
कारण कोई भी श्रमण ऐसा दायित्व निभा नहीं सकता था। साथ ही उसे अगाध पाण्डित्य के साथ-साथ श्रुतभक्तियुक्त प्रबल जिज्ञासा भी अपेक्षित थी, अन्यथा वह श्रुत का संरक्षण संवर्धन वस्तुतः नहीं कर सकता था। इसके बिना वह कैसे तो स्वयं शास्त्र पढ़ता, कैसे दूसरों को पढ़ाता, कैसे शुद्ध प्रतिलिपि करता और कैसे उन्हें सजग रहकर विवेकपूर्वक संरक्षित रखता? – ये सब बेहद कठिन दायित्व थे । इसलिए संसार से विरक्त चित्त, अगाध वैदुष्य धनी एवं जिनमार्ग की व्यापक प्रभावना की उत्कट अभिलाषा रखने वाले व्यवस्था - निपुण व्यक्ति को ऐसे मठों का 'मठाधीश' या 'भट्टारक' बनाया गया।
इनके बारे में आचार्य इन्द्रनन्दि लिखते हैं
“सर्वशास्त्रकलाभिज्ञो नानागच्छाभिवर्धकः ।
महात्मना प्रभावी, 'भट्टारक' इतीष्यते । । " – (नीतिसार, 19 ) अर्थ – जो सभी आगमशास्त्रों और कलाओं के ज्ञाता होते हैं, मूलसंघ के अनेकों गण-गच्छों के अभिवर्धक एवं महान् धर्मप्रभावक होते हैं; वे ही 'भट्टारक' कहलाते हैं। वैसे तो स्वयं जिनेन्द्र परमात्मा को 'भट्टारक' संज्ञा से अभिहित किया गया है— “भट्टान् पण्डितान् आरयति प्रेरयति स्याद्वादपरीक्षार्थमिति भट्टारक।” - (जिनसहस्रनाम 3/32, पृ० 70 ) अर्थ:- 'भट्ट' अर्थात् विद्वानों को आप स्याद्वाद की परीक्षा के लिये प्रेरित करते हैं, अत: (हे जिनेन्द्र भगवान् !) आप 'भट्टारक' कहलाते हैं।
‘भट्ट' शब्द विद्वान्वाची रहा है, अतएव हमारे धुरंधर आचार्यों के नाम के साथ भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है । यथा - आचार्य भट्ट अकलंकदेव, आचार्य उग्रभूति भट्ट, आचार्य व्याघ्रभूति भट्ट, आचार्य छुच्छुक भट्ट, आचार्य जगद्धर भट्ट ( इन्होंने कातंत्र व्याकरण पर भाष्य, न्यास तथा वृत्ति आदि अनेक टीकायें लिखी हैं) आदि नाम भी इस उपाधि से अलंकृत रहे हैं।
इन भट्टारकों के मठों में सामान्यतः विद्याभ्यासी छात्रों के अध्ययन-अध्यापन की विशेष व्यवस्था होती थी, इसलिए 'मठ' की परिभाषा प्रसिद्ध हुई— “मठ: छात्रादिनिलयः ।” अर्थात् जहाँ पर छात्र आदि रहकर विद्याभ्यास एवं ज्ञानप्रभावना के कार्य करते हों, वह 'मठ' कहलाता है। इसे 'ज्ञान का मंदिर' होने से 'वत्थुसार' नामक ग्रंथ में 'मंदिर' की संज्ञा भी दी गयी है— " मठं मंदिरं ति” – ( वत्थुसार, 129 )
भट्टारकों से अधिष्ठित इन ज्ञानपीठों (मठों) की परम्परा का प्रवर्तन सन् 720 ई० में दिल्ली में हुआ तथा इनकी मूलपीठ भी दिल्ली में ही बनी। फिर इसकी उपपीठों के रूप में शाखायें-प्रशाखायें सारे देश में स्थापित होतीं गयीं। इन सबके द्वारा श्रुत के संरक्षण, संवर्धन के साथ-साथ तत्त्वप्रचार-प्रसार का महनीय कार्य चलता रहा; इसीलिए शास्त्रोक्त न होते भी इनकी सामाजिक मान्यता एवं महत्ता निरंतर बनी रही, बढ़ती रही ।
प्राकृतविद्या + जनवरी-मार्च 2000
83