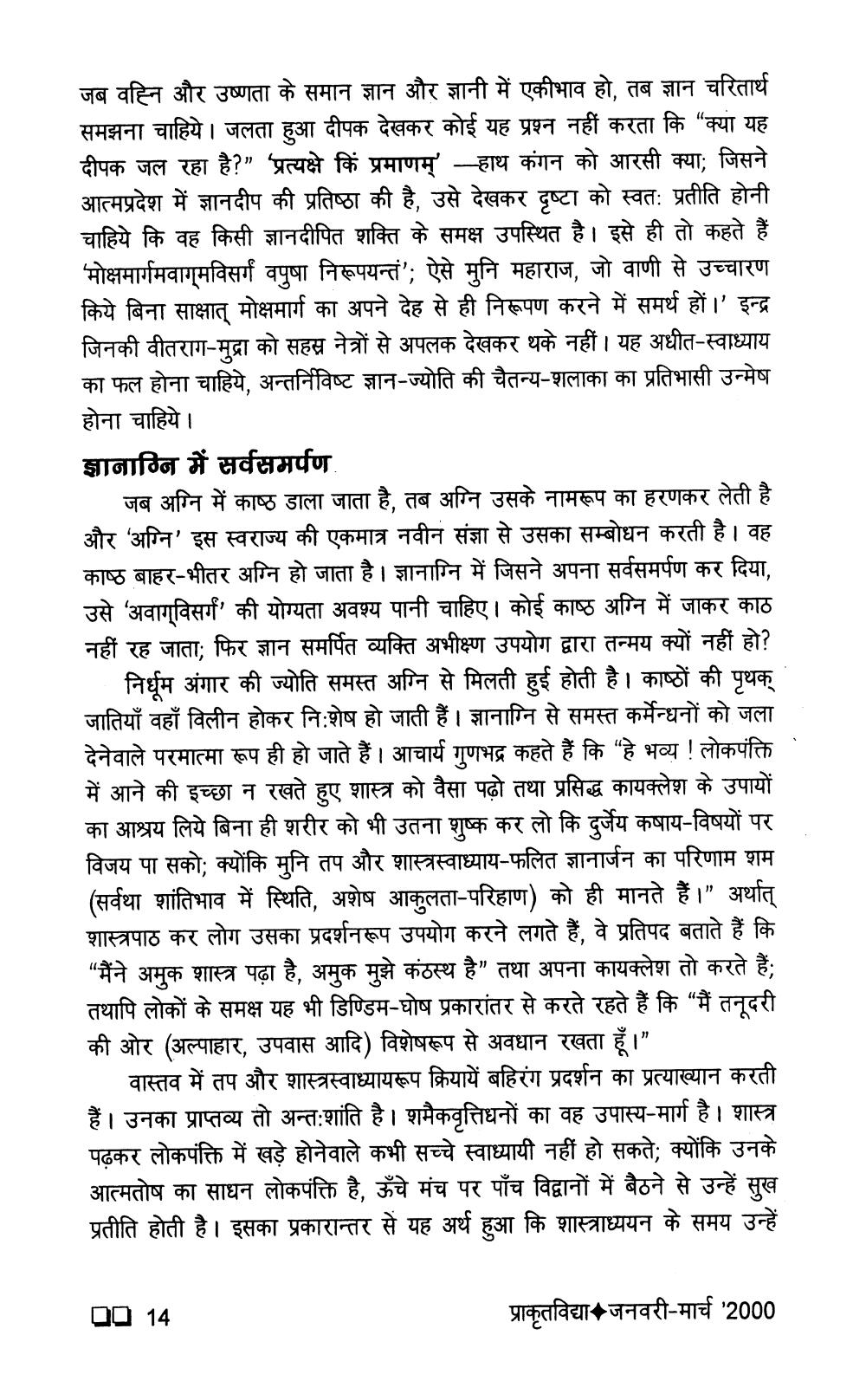________________
जब वह्नि और उष्णता के समान ज्ञान और ज्ञानी में एकीभाव हो, तब ज्ञान चरितार्थ समझना चाहिये। जलता हुआ दीपक देखकर कोई यह प्रश्न नहीं करता कि "क्या यह दीपक जल रहा है?" 'प्रत्यक्षे किं प्रमाणम्' - हाथ कंगन को आरसी क्या; जिसने आत्मप्रदेश में ज्ञानदीप की प्रतिष्ठा की है, उसे देखकर दृष्टा को स्वतः प्रतीति होनी चाहिये कि वह किसी ज्ञानदीपित शक्ति के समक्ष उपस्थित है। इसे ही तो कहते हैं 'मोक्षमार्गमवाग्मविसर्गं वपुषा निरूपयन्तं'; ऐसे मुनि महाराज, जो वाणी से उच्चारण किये बिना साक्षात् मोक्षमार्ग का अपने देह से ही निरूपण करने में समर्थ हों ।' इन्द्र जिनकी वीतराग - मुद्रा को सहस्र नेत्रों से अपलक देखकर थके नहीं । यह अधीत-स्वाध्याय का फल होना चाहिये, अन्तर्निविष्ट ज्ञान - ज्योति की चैतन्य - शलाका का प्रतिभासी उन्मेष होना चाहिये ।
ज्ञानाग्नि में सर्वसमर्पण.
1
जब अग्नि में काष्ठ डाला जाता है, तब अग्नि उसके नामरूप का हरणकर लेती है और 'अग्नि' इस स्वराज्य की एकमात्र नवीन संज्ञा से उसका सम्बोधन करती है । वह काष्ठ बाहर-भीतर अग्नि हो जाता है । ज्ञानाग्नि में जिसने अपना सर्वसमर्पण कर दिया, उसे 'अवाग्विसर्गं' की योग्यता अवश्य पानी चाहिए। कोई काष्ठ अग्नि में जाकर काठ नहीं रह जाता; फिर ज्ञान समर्पित व्यक्ति अभीक्ष्ण उपयोग द्वारा तन्मय क्यों नहीं हो ?
निर्धूम अंगार की ज्योति समस्त अग्नि से मिलती हुई होती है । काष्ठों की पृथक् जातियाँ वहाँ विलीन होकर नि:शेष हो जाती हैं । ज्ञानाग्नि से समस्त कर्मेन्धनों को जला
।
1
देनेवाले परमात्मा रूप ही हो जाते हैं । आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि "हे भव्य ! लोकपंक्ति में आने की इच्छा न रखते हुए शास्त्र को वैसा पढ़ो तथा प्रसिद्ध कायक्लेश के उपायों का आश्रय लिये बिना ही शरीर को भी उतना शुष्क कर लो कि दुर्जेय कषाय-विषयों पर विजय पा सको; क्योंकि मुनि तप और शास्त्रस्वाध्याय - फलित ज्ञानार्जन का परिणाम शम (सर्वथा शांतिभाव में स्थिति, अशेष आकुलता - परिहाण ) को ही मानते हैं।” अर्थात् शास्त्रपाठ कर लोग उसका प्रदर्शनरूप उपयोग करने लगते हैं, वे प्रतिपद बताते हैं कि “मैंने अमुक शास्त्र पढ़ा है, अमुक मुझे कंठस्थ है" तथा अपना कायक्लेश तो करते हैं; तथापि लोकों के समक्ष यह भी डिण्डिम - घोष प्रकारांतर से करते रहते हैं कि “मैं तनूदरी की ओर (अल्पाहार, उपवास आदि) विशेषरूप से अवधान रखता हूँ ।"
वास्तव में तप और शास्त्रस्वाध्यायरूप क्रियायें बहिरंग प्रदर्शन का प्रत्याख्यान करती हैं। उनका प्राप्तव्य तो अन्त:शांति है । शमैकवृत्तिधनों का वह उपास्य -मार्ग है। शास्त्र पढ़कर लोकपंक्ति में खड़े होनेवाले कभी सच्चे स्वाध्यायी नहीं हो सकते; क्योंकि उनके आत्मतोष का साधन लोकपंक्ति है, ऊँचे मंच पर पाँच विद्वानों में बैठने से उन्हें सुख प्रतीति होती है। इसका प्रकारान्तर से यह अर्थ हुआ कि शास्त्राध्ययन के समय उन्हें
014
प्राकृतविद्या जनवरी-मार्च 2000