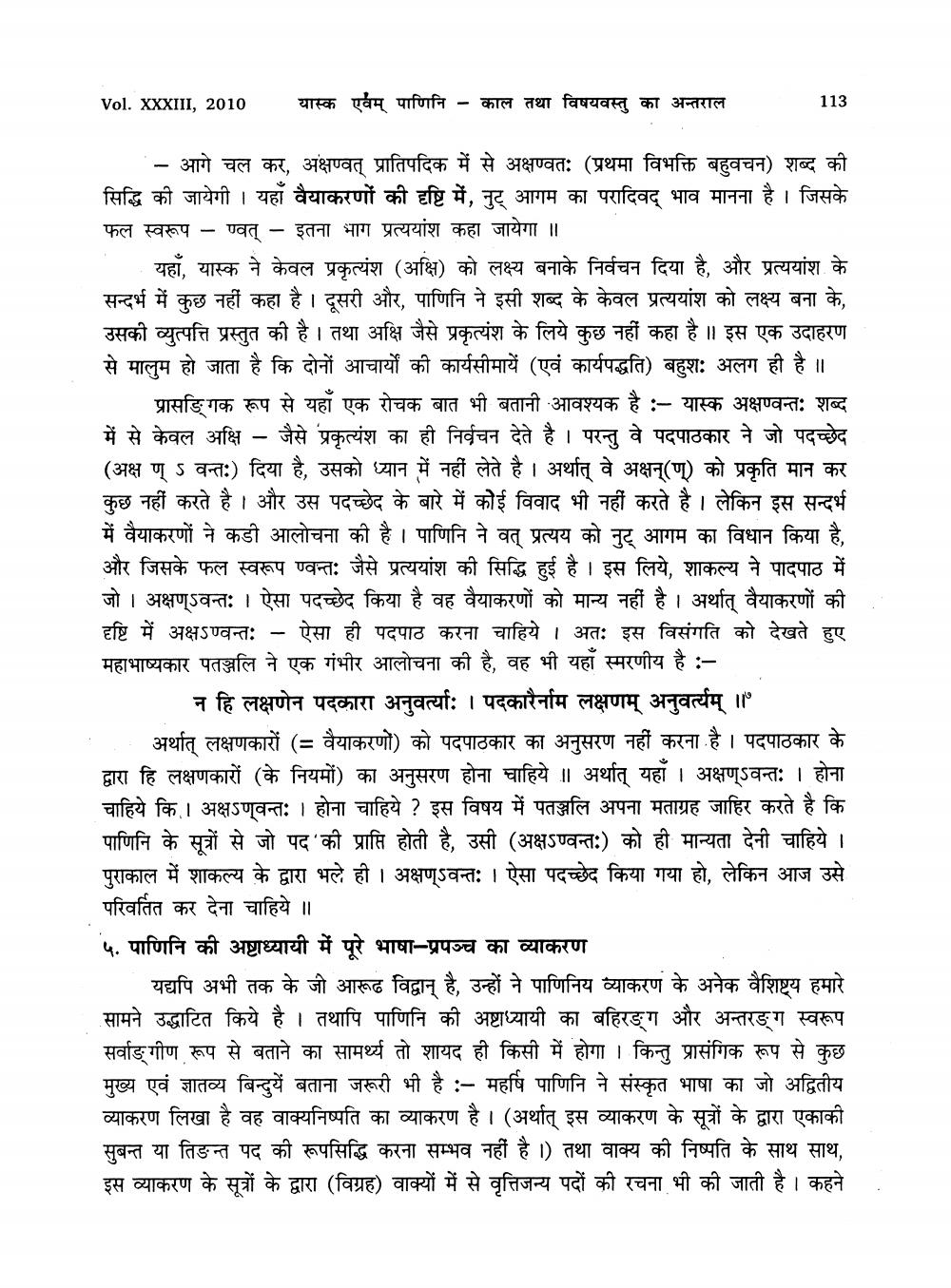________________
Vol. XXXIII, 2010
यास्क एवम् पाणिनि - काल तथा विषयवस्तु का अन्तराल
113
- आगे चल कर, अक्षण्वत् प्रातिपदिक में से अक्षण्वतः (प्रथमा विभक्ति बहुवचन) शब्द की सिद्धि की जायेगी । यहाँ वैयाकरणों की दृष्टि में, नुट आगम का परादिवद् भाव मानना है । जिसके फल स्वरूप - ण्वत् - इतना भाग प्रत्ययांश कहा जायेगा ॥
यहाँ, यास्क ने केवल प्रकृत्यंश (अक्षि) को लक्ष्य बनाके निर्वचन दिया है, और प्रत्ययांश के सन्दर्भ में कुछ नहीं कहा है। दूसरी और, पाणिनि ने इसी शब्द के केवल प्रत्ययांश को लक्ष्य बना के, उसकी व्युत्पत्ति प्रस्तुत की है । तथा अक्षि जैसे प्रकृत्यंश के लिये कुछ नहीं कहा है । इस एक उदाहरण से मालुम हो जाता है कि दोनों आचार्यों की कार्यसीमायें (एवं कार्यपद्धति) बहुशः अलग ही है ॥
प्रासङ्गिक रूप से यहाँ एक रोचक बात भी बतानी आवश्यक है :- यास्क अक्षण्वन्तः शब्द में से केवल अक्षि - जैसे प्रकृत्यंश का ही निर्वचन देते है । परन्तु वे पदपाठकार ने जो पदच्छेद (अक्ष ण् 5 वन्तः) दिया है, उसको ध्यान में नहीं लेते है । अर्थात् वे अक्षन्(ण) को प्रकृति मान कर कुछ नहीं करते है । और उस पदच्छेद के बारे में कोई विवाद भी नहीं करते है। लेकिन इस सन्दर्भ में वैयाकरणों ने कड़ी आलोचना की है। पाणिनि ने वत् प्रत्यय को नुट् आगम का विधान किया है, और जिसके फल स्वरूप ण्वन्तः जैसे प्रत्ययांश की सिद्धि हुई है । इस लिये, शाकल्य ने पादपाठ में जो । अक्षणऽवन्तः । ऐसा पदच्छेद किया है वह वैयाकरणों को मान्य नहीं है। अर्थात् वैयाकरणों की
क्षऽण्वन्तः - ऐसा ही पदपाठ करना चाहिये । अतः इस विसंगति को देखते हुए महाभाष्यकार पतञ्जलि ने एक गंभीर आलोचना की है, वह भी यहाँ स्मरणीय है :
न हि लक्षणेन पदकारा अनुवाः । पदकारैर्नाम लक्षणम् अनुवर्त्यम् ॥ अर्थात् लक्षणकारों (= वैयाकरणो) को पदपाठकार का अनुसरण नहीं करना है । पदपाठकार के द्वारा हि लक्षणकारों (के नियमों) का अनुसरण होना चाहिये ॥ अर्थात् यहाँ । अक्षणऽवन्तः । होना चाहिये कि । अक्षऽण्वन्तः । होना चाहिये ? इस विषय में पतञ्जलि अपना मताग्रह जाहिर करते है कि पाणिनि के सूत्रों से जो पद की प्राप्ति होती है, उसी (अक्षऽण्वन्तः) को ही मान्यता देनी चाहिये । पुराकाल में शाकल्य के द्वारा भले ही । अक्षणऽवन्तः । ऐसा पदच्छेद किया गया हो, लेकिन आज उसे परिवर्तित कर देना चाहिये ॥ ५. पाणिनि की अष्टाध्यायी में पूरे भाषा-प्रपञ्च का व्याकरण
यद्यपि अभी तक के जी आरूढ विद्वान् है, उन्हों ने पाणिनिय व्याकरण के अनेक वैशिष्ट्य हमारे सामने उद्घाटित किये है । तथापि पाणिनि की अष्टाध्यायी का बहिरङ्ग और अन्तरङ्ग स्वरूप सर्वाङ्गीण रूप से बताने का सामर्थ्य तो शायद ही किसी में होगा । किन्तु प्रासंगिक रूप से कुछ मुख्य एवं ज्ञातव्य बिन्दुयें बताना जरूरी भी है :- महर्षि पाणिनि ने संस्कृत भाषा का जो अद्वितीय व्याकरण लिखा है वह वाक्यनिष्पति का व्याकरण है। (अर्थात् इस व्याकरण के सूत्रों के द्वारा एकाकी सुबन्त या तिङन्त पद की रूपसिद्धि करना सम्भव नहीं है ।) तथा वाक्य की निष्पति के साथ साथ, इस व्याकरण के सूत्रों के द्वारा (विग्रह) वाक्यों में से वृत्तिजन्य पदों की रचना भी की जाती है । कहने