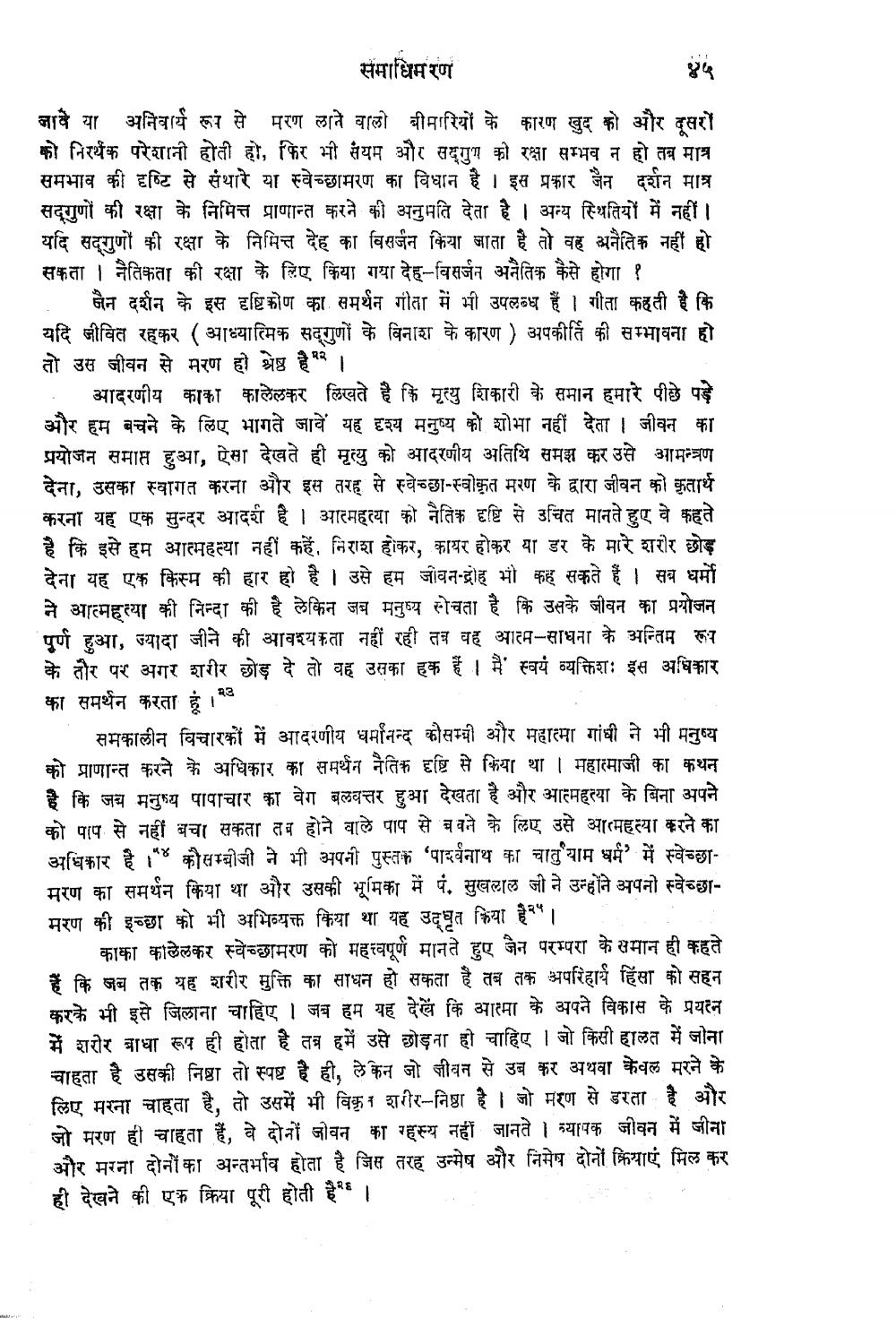________________
समाधिमरण
४५
जावे या अनिवार्य रूप से मरण लाने वाली बीमारियों के कारण खुद को और दूसरों को निरर्थक परेशानी होती हो, फिर भी संयम और सद्गुण की रक्षा सम्भव न हो तब मात्र समभाव की दृष्टि से संथारे या स्वेच्छामरण का विधान है । इस प्रकार जैन दर्शन मात्र सद्गुणों की रक्षा के निमित्त प्राणान्त करने की अनुमति देता है । अन्य स्थितियों में नहीं । यदि सद्गुणों की रक्षा के निमित्त देह का विसर्जन किया जाता है तो वह अनैतिक नहीं हो सकता । नैतिकता की रक्षा के लिए किया गया देह - विसर्जन अनैतिक कैसे होगा १
जैन दर्शन के इस दृष्टिकोण का समर्थन गीता में भी उपलब्ध हैं । गीता कहती है कि यदि जीवित रहकर ( आध्यात्मिक सद्गुणों के विनाश के कारण ) अपकीर्ति की सम्भावना हो तो उस जीवन से मरण हो श्रेष्ठ है २ ।
आदरणीय काका कालेलकर लिखते है कि मृत्यु शिकारी के समान हमारे पीछे पड़े और हम बचने के लिए भागते जावें यह दृश्य मनुष्य को शोभा नहीं देता । जीवन का प्रयोजन समाप्त हुआ, ऐसा देखते ही मृत्यु को आदरणीय अतिथि समझ कर उसे आमन्त्रण देना, उसका स्वागत करना और इस तरह से स्वेच्छा स्वीकृत मरण के द्वारा जीवन को कृतार्थ करना यह एक सुन्दर आदर्श है । आत्महत्या को नैतिक दृष्टि से उचित मानते हुए वे कहते है कि इसे हम आत्महत्या नहीं कहें, निराश होकर, कायर होकर या डर के मारे शरीर छोड़ देना यह एक किस्म की हार हो है । उसे हम जीवन-द्रोह भी कह सकते हैं । सब धर्मो ने आत्महत्या की निन्दा की है लेकिन जब मनुष्य सोचता है कि उसके जीवन का प्रयोजन पूर्ण हुआ, ज्यादा जीने की आवश्यकता नहीं रही तत्र वह आत्म-साधना के अन्तिम रूप के तौर पर अगर शरीर छोड़ दे तो वह उसका हक हैं । मैं स्वयं व्यक्तिशः इस अधिकार का समर्थन करता हूं ।
२३
समकालीन विचारकों में आदरणीय धर्मानन्द कौसम्बी और महात्मा गांधी ने भी मनुष्य को प्राणान्त करने के अधिकार का समर्थन नैतिक दृष्टि से किया था । महात्माजी का कथन है कि जब मनुष्य पापाचार का वेग बलवत्तर हुआ देखता है और आत्महत्या के बिना अपने को पाप से नहीं बचा सकता तब होने वाले पाप से बचने के लिए उसे आत्महत्या करने का अधिकार है । *४ कौसम्बीजी ने भी अपनी पुस्तक 'पार्श्वनाथ का चातु याम धर्म' में स्वेच्छामरण का समर्थन किया था और उसकी भूमिका में पं. सुखलाल जी ने उन्होंने अपनो स्वेच्छामरण की इच्छा को भी अभिव्यक्त किया था यह उद्धृत किया है२५ ।
काका कालेलकर स्वेच्छामरण को महत्त्वपूर्ण मानते हुए जैन परम्परा के समान ही कहते हैं कि जब तक यह शरीर मुक्ति का साधन हो सकता है तब तक अपरिहार्य हिंसा को सहन करके भी इसे जिलाना चाहिए । जब हम यह देखें कि आत्मा के अपने विकास के प्रयत्न में शरीर बाधा रूप ही होता है तब हमें उसे छोड़ना हो चाहिए । जो किसी हालत में जोना चाहता है उसकी निष्ठा तो स्पष्ट है ही, लेकिन जो जीवन से उब कर अथवा केवल मरने के लिए मरना चाहता है, तो उसमें भी विकृत शरीर - निष्ठा है। जो मरण से डरता है और जो मरण ही चाहता हैं, वे दोनों जीवन का रहस्य नहीं जानते । व्यापक जीवन में जीना और मरना दोनों का अन्तर्भाव होता है जिस तरह उन्मेष और निमेष दोनों क्रियाएं मिल कर ही देखने की एक क्रिया पूरी होती है ।