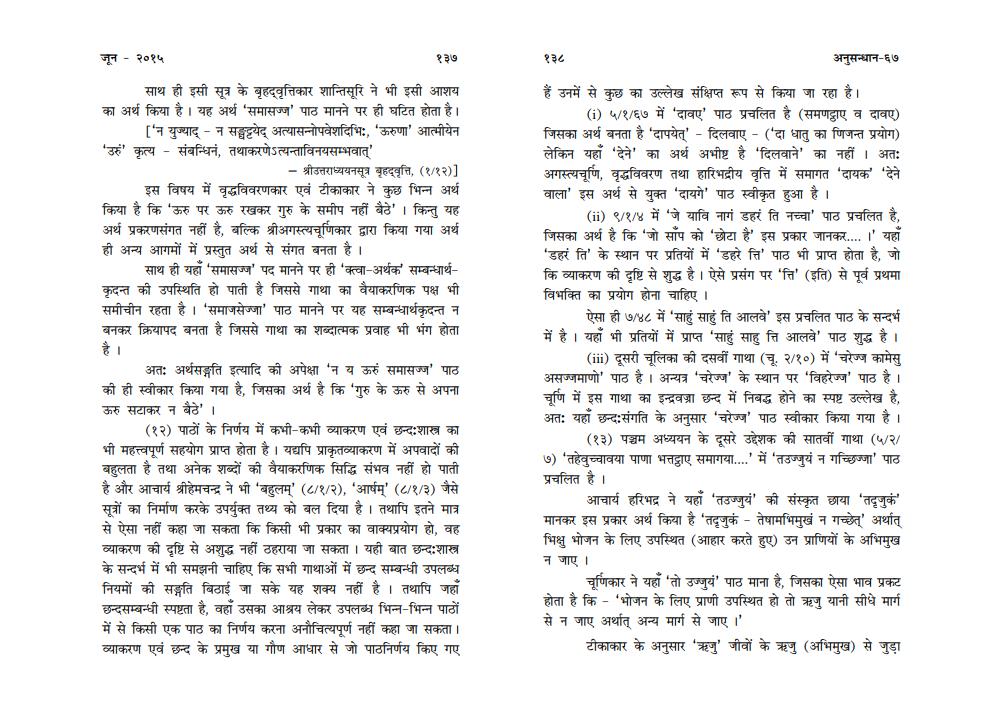________________
१३७
साथ ही इसी सूत्र के बृहद्वृत्तिकार शान्तिसूरि ने भी इसी आशय का अर्थ किया है। यह अर्थ 'समासज्ज' पाठ मानने पर ही घटित होता है। ['न युज्याद् न सङ्घट्टयेद् अत्यासन्नोपवेशदिभिः, 'ऊरुणा' आत्मीयेन "उरु' कृत्य संबन्धिनं तथाकरणेऽत्यन्ताविनयसम्भवात्'
-
जून २०१५
-
श्रीउत्तराध्ययनसूत्र बृहद्वृत्ति, ( १ / १२ ) ] इस विषय में वृद्धविवरणकार एवं टीकाकार ने कुछ भिन्न अर्थ किया है कि 'ऊरु पर ऊरु रखकर गुरु के समीप नहीं बैठे' । किन्तु यह अर्थ प्रकरणसंगत नहीं है, बल्कि श्रीअगस्त्यचूर्णिकार द्वारा किया गया अर्थ ही अन्य आगमों में प्रस्तुत अर्थ से संगत बनता है ।
साथ ही यहाँ 'समासज्ज' पद मानने पर ही 'क्त्वा अर्थक' सम्बन्धार्थकृदन्त की उपस्थिति हो पाती है जिससे गाथा का वैयाकरणिक पक्ष भी समीचीन रहता है। 'समाजसेज्जा' पाठ मानने पर यह सम्बन्धार्थकृदन्त न बनकर क्रियापद बनता है जिससे गाथा का शब्दात्मक प्रवाह भी भंग होता है ।
अतः अर्थसङ्गति इत्यादि की अपेक्षा की ही स्वीकार किया गया है, जिसका अर्थ है ऊरु सटाकर न बैठे' ।
न य ऊरुं समासज्ज' पाठ कि 'गुरु के ऊरु से अपना
(१२) पाठों के निर्णय में कभी- कभी व्याकरण एवं छन्दः शास्त्र का भी महत्त्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। यद्यपि प्राकृतव्याकरण में अपवादों की बहुलता है तथा अनेक शब्दों की वैयाकरणिक सिद्धि संभव नहीं हो पाती है और आचार्य श्रीहेमचन्द्र ने भी 'बहुलम्' (८/१/२), 'आर्षम्' (८/१/३) जैसे सूत्रों का निर्माण करके उपर्युक्त तथ्य को बल दिया है। तथापि इतने मात्र से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी भी प्रकार का वाक्यप्रयोग हो, वह व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध नहीं ठहराया जा सकता । यही बात छन्दः शास्त्र के सन्दर्भ में भी समझनी चाहिए कि सभी गाथाओं में छन्द सम्बन्धी उपलब्ध नियमों की सङ्गति बिठाई जा सके यह शक्य नहीं है । तथापि जहाँ छन्दसम्बन्धी स्पष्टता है, वहाँ उसका आश्रय लेकर उपलब्ध भिन्न-भिन्न पाठों में से किसी एक पाठ का निर्णय करना अनौचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता । व्याकरण एवं छन्द के प्रमुख या गौण आधार से जो पाठनिर्णय किए गए
१३८
अनुसन्धान-६७
हैं उनमें से कुछ का उल्लेख संक्षिप्त रूप से किया जा रहा है। (i) ५/१ / ६७ में 'दावए' पाठ प्रचलित है (समणट्टाए व दावए) जिसका अर्थ बनता है 'दापयेत्'- दिलवाए ('दा धातु का णिजन्त प्रयोग ) लेकिन यहाँ 'देने' का अर्थ अभीष्ट है 'दिलवाने' का नहीं । अतः अगस्त्यचूर्णि, वृद्धविवरण तथा हारिभद्रीय वृत्ति में समागत 'दायक' 'देने वाला' इस अर्थ से युक्त 'दायगे' पाठ स्वीकृत हुआ है।
(ii) ९ / १ / ४ में 'जे यावि नागं डहरं ति नच्चा' पाठ प्रचलित है, जिसका अर्थ है कि 'जो साँप को 'छोटा है' इस प्रकार जानकर....।' यहाँ 'डहरं ति' के स्थान पर प्रतियों में 'डहरे त्ति' पाठ भी प्राप्त होता है, जो कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। ऐसे प्रसंग पर 'त्ति' (इति) से पूर्व प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए।
ऐसा ही ७/४८ में 'साहुं साहुं ति आलवे' इस प्रचलित पाठ के सन्दर्भ में है। यहाँ भी प्रतियों में प्राप्त 'साहु साहु त्ति आलवे' पाठ शुद्ध है।
(iii) दूसरी चूलिका की दसवीं गाथा (चू. २/१०) में 'चरेज्ज कामेसु असज्जमाणो' पाठ है। अन्यत्र 'चरेज्ज' के स्थान पर 'विहरेज्ज' पाठ है 1 चूर्णि में इस गाथा का इन्द्रवज्रा छन्द में निबद्ध होने का स्पष्ट उल्लेख है, अतः यहाँ छन्द:संगति के अनुसार 'चरेज्ज' पाठ स्वीकार किया गया है ।
(१३) पञ्चम अध्ययन के दूसरे उद्देशक की सातवीं गाथा (५/२/ ७) तहेवुच्चावया पाणा भत्तट्ठाए समागया....' में 'तउज्जुयं न गच्छिज्जा' पाठ प्रचलित है।
आचार्य हरिभद्र ने यहाँ 'तउज्जयं' की संस्कृत छाया 'तदृजुकं' मानकर इस प्रकार अर्थ किया है 'तदृजुकं तेषामभिमुखं न गच्छेत्' अर्थात् भिक्षु भोजन के लिए उपस्थित (आहार करते हुए) उन प्राणियों के अभिमुख
न जाए।
-
चूर्णिकार ने यहाँ 'तो उज्जुयं' पाठ माना है, जिसका ऐसा भाव प्रकट होता है कि 'भोजन के लिए प्राणी उपस्थित हो तो ऋजु यानी सीधे मार्ग से न जाए अर्थात् अन्य मार्ग से जाए ।'
टीकाकार के अनुसार 'ऋजु' जीवों के ऋजु (अभिमुख) से जुड़ा