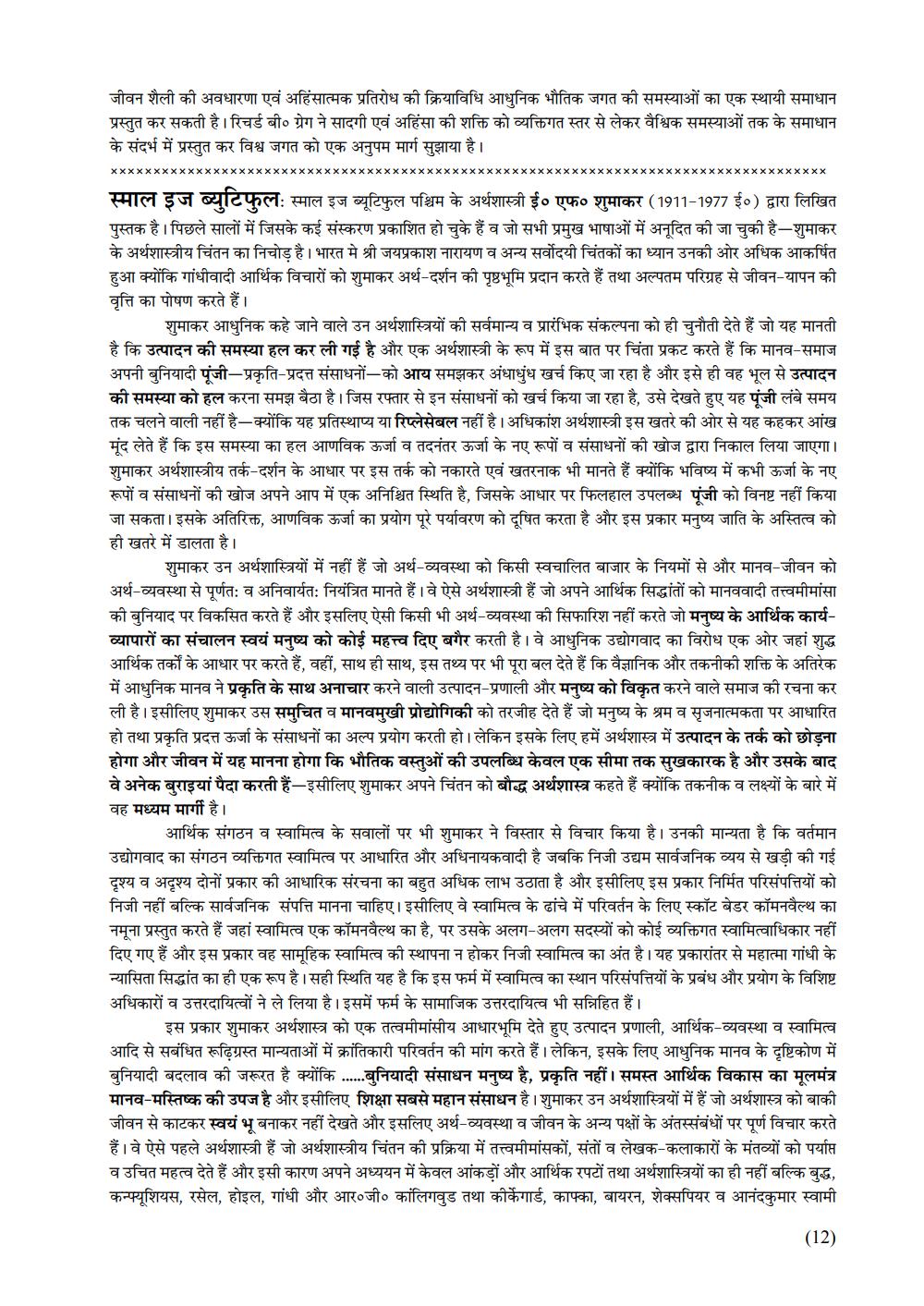________________
जीवन शैली की अवधारणा एवं अहिंसात्मक प्रतिरोध की क्रियाविधि आधुनिक भौतिक जगत की समस्याओं का एक स्थायी समाधान प्रस्तुत कर सकती है। रिचर्ड बी० ग्रेग ने सादगी एवं अहिंसा की शक्ति को व्यक्तिगत स्तर से लेकर वैश्विक समस्याओं तक के समाधान के संदर्भ में प्रस्तुत कर विश्व जगत को एक अनुपम मार्ग सुझाया है।
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
स्माल इज ब्युटिफुल: स्माल इज ब्यूटिफुल पश्चिम के अर्थशास्त्री ई० एफ० शुमाकर (1911-1977 ई०) द्वारा लिखित पुस्तक है। पिछले सालों में जिसके कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं व जो सभी प्रमुख भाषाओं में अनूदित की जा चुकी है-शुमाकर के अर्थशास्त्रीय चिंतन का निचोड़ है। भारत मे श्री जयप्रकाश नारायण व अन्य सर्वोदयी चिंतकों का ध्यान उनकी ओर अधिक आकर्षित हुआ क्योंकि गांधीवादी आर्थिक विचारों को शुमाकर अर्थ-दर्शन की पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं तथा अल्पतम परिग्रह से जीवन-यापन की वृत्ति का पोषण करते हैं।
शुमाकर आधुनिक कहे जाने वाले उन अर्थशास्त्रियों की सर्वमान्य व प्रारंभिक संकल्पना को ही चुनौती देते हैं जो यह मानती है कि उत्पादन की समस्या हल कर ली गई है और एक अर्थशास्त्री के रूप में इस बात पर चिंता प्रकट करते हैं कि मानव-समाज अपनी बुनियादी पूंजी-प्रकृति-प्रदत्त संसाधनों-को आय समझकर अंधाधुंध खर्च किए जा रहा है और इसे ही वह भूल से उत्पादन की समस्या को हल करना समझ बैठा है। जिस रफ्तार से इन संसाधनों को खर्च किया जा रहा है, उसे देखते हुए यह पूंजी लंबे समय तक चलने वाली नहीं है क्योंकि यह प्रतिस्थाप्य या रिप्लेसेबल नहीं है। अधिकांश अर्थशास्त्री इस खतरे की ओर से यह कहकर आंख मूंद लेते हैं कि इस समस्या का हल आणविक ऊर्जा व तदनंतर ऊर्जा के नए रूपों व संसाधनों की खोज द्वारा निकाल लिया जाएगा। शुमाकर अर्थशास्त्रीय तर्क-दर्शन के आधार पर इस तर्क को नकारते एवं खतरनाक भी मानते हैं क्योंकि भविष्य में कभी ऊर्जा के नए रूपों व संसाधनों की खोज अपने आप में एक अनिश्चित स्थिति है, जिसके आधार पर फिलहाल उपलब्ध पूंजी को विनष्ट नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, आणविक ऊर्जा का प्रयोग पूरे पर्यावरण को दूषित करता है और इस प्रकार मनुष्य जाति के अस्तित्व को ही खतरे में डालता है।
शुमाकर उन अर्थशास्त्रियों में नहीं हैं जो अर्थ-व्यवस्था को किसी स्वचालित बाजार के नियमों से और मानव-जीवन को अर्थ-व्यवस्था से पूर्णत: व अनिवार्यतः नियंत्रित मानते हैं। वे ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो अपने आर्थिक सिद्धांतों को मानववादी तत्त्वमीमांसा की बुनियाद पर विकसित करते हैं और इसलिए ऐसी किसी भी अर्थ-व्यवस्था की सिफारिश नहीं करते जो मनुष्य के आर्थिक कार्यव्यापारों का संचालन स्वयं मनुष्य को कोई महत्त्व दिए बगैर करती है। वे आधुनिक उद्योगवाद का विरोध एक ओर जहां शुद्ध आर्थिक तर्कों के आधार पर करते हैं, वहीं, साथ ही साथ, इस तथ्य पर भी पूरा बल देते हैं कि वैज्ञानिक और तकनीकी शक्ति के अतिरेक में आधुनिक मानव ने प्रकृति के साथ अनाचार करने वाली उत्पादन-प्रणाली और मनुष्य को विकृत करने वाले समाज की रचना कर ली है। इसीलिए शुमाकर उस समुचित व मानवमुखी प्रोद्योगिकी को तरजीह देते हैं जो मनुष्य के श्रम व सृजनात्मकता पर आधारित हो तथा प्रकृति प्रदत्त ऊर्जा के संसाधनों का अल्प प्रयोग करती हो। लेकिन इसके लिए हमें अर्थशास्त्र में उत्पादन के तर्क को छोड़ना होगा और जीवन में यह मानना होगा कि भौतिक वस्तुओं की उपलब्धि केवल एक सीमा तक सुखकारक है और उसके बाद वे अनेक बुराइयां पैदा करती हैं इसीलिए शुमाकर अपने चिंतन को बौद्ध अर्थशास्त्र कहते हैं क्योंकि तकनीक व लक्ष्यों के बारे में वह मध्यम मार्गी है।
आर्थिक संगठन व स्वामित्व के सवालों पर भी शुमाकर ने विस्तार से विचार किया है। उनकी मान्यता है कि वर्तमान उद्योगवाद का संगठन व्यक्तिगत स्वामित्व पर आधारित और अधिनायकवादी है जबकि निजी उद्यम सार्वजनिक व्यय से खड़ी की गई दृश्य व अदृश्य दोनों प्रकार की आधारिक संरचना का बहुत अधिक लाभ उठाता है और इसीलिए इस प्रकार निर्मित परिसंपत्तियों को निजी नहीं बल्कि सार्वजनिक संपत्ति मानना चाहिए। इसीलिए वे स्वामित्व के ढांचे में परिवर्तन के लिए स्कॉट बेडर कॉमनवैल्थ का नमूना प्रस्तुत करते हैं जहां स्वामित्व एक कॉमनवैल्थ का है, पर उसके अलग-अलग सदस्यों को कोई व्यक्तिगत स्वामित्वाधिकार नहीं दिए गए हैं और इस प्रकार वह सामूहिक स्वामित्व की स्थापना न होकर निजी स्वामित्व का अंत है। यह प्रकारांतर से महात्मा गांधी के न्यासिता सिद्धांत का ही एक रूप है। सही स्थिति यह है कि इस फर्म में स्वामित्व का स्थान परिसंपत्तियों के प्रबंध और प्रयोग के विशिष्ट अधिकारों व उत्तरदायित्वों ने ले लिया है। इसमें फर्म के सामाजिक उत्तरदायित्व भी सन्निहित हैं।
इस प्रकार शुमाकर अर्थशास्त्र को एक तत्वमीमांसीय आधारभूमि देते हुए उत्पादन प्रणाली, आर्थिक-व्यवस्था व स्वामित्व आदि से सबंधित रूढ़िग्रस्त मान्यताओं में क्रांतिकारी परिवर्तन की मांग करते हैं। लेकिन, इसके लिए आधुनिक मानव के दृष्टिकोण में बुनियादी बदलाव की जरूरत है क्योंकि ......बुनियादी संसाधन मनुष्य है, प्रकृति नहीं। समस्त आर्थिक विकास का मूलमंत्र मानव-मस्तिष्क की उपज है और इसीलिए शिक्षा सबसे महान संसाधन है। शुमाकर उन अर्थशास्त्रियों में हैं जो अर्थशास्त्र को बाकी जीवन से काटकर स्वयं भू बनाकर नहीं देखते और इसलिए अर्थ-व्यवस्था व जीवन के अन्य पक्षों के अंतस्संबंधों पर पूर्ण विचार करते हैं। वे ऐसे पहले अर्थशास्त्री हैं जो अर्थशास्त्रीय चिंतन की प्रक्रिया में तत्त्वमीमांसकों, संतों व लेखक-कलाकारों के मंतव्यों को पर्याप्त व उचित महत्व देते हैं और इसी कारण अपने अध्ययन में केवल आंकड़ों और आर्थिक रपटों तथा अर्थशास्त्रियों का ही नहीं बल्कि बुद्ध, कन्फ्यूशियस, रसेल, होइल, गांधी और आर०जी० कालिगवुड तथा कीर्केगार्ड, काफ्का, बायरन, शेक्सपियर व आनंदकुमार स्वामी
(12)