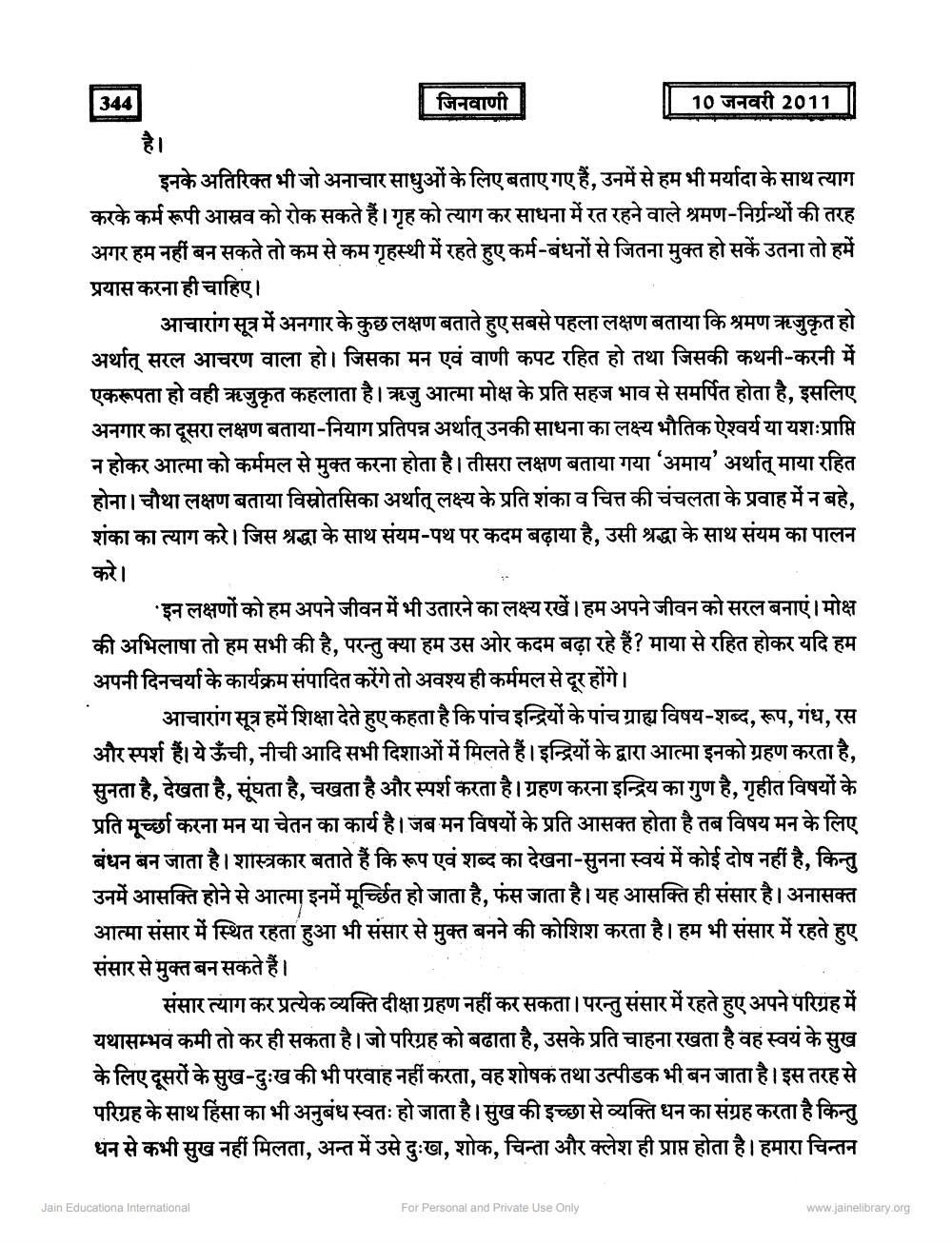________________
344
जिनवाणी
है।
इनके अतिरिक्त भी जो अनाचार साधुओं के लिए बताए गए हैं, उनमें से हम भी मर्यादा के साथ त्याग करके कर्म रूपी आस्रव को रोक सकते हैं। गृह को त्याग कर साधना में रत रहने वाले श्रमण-निर्ग्रन्थों की तरह अगर हम नहीं बन सकते तो कम से कम गृहस्थी में रहते हुए कर्म - बंधनों से जितना मुक्त हो सकें उतना तो हमें प्रयास करना ही चाहिए।
10 जनवरी 2011
आचारांग सूत्र में अनगार के कुछ लक्षण बताते हुए सबसे पहला लक्षण बताया कि श्रमण ऋजुकृत हो अर्थात् सरल आचरण वाला हो। जिसका मन एवं वाणी कपट रहित हो तथा जिसकी कथनी-करनी में एकरूपता हो वही ऋजुकृत कहलाता है। ऋजु आत्मा मोक्ष के प्रति सहज भाव से समर्पित होता है, इसलिए अनगार का दूसरा लक्षण बताया- नियाग प्रतिपन्न अर्थात् उनकी साधना का लक्ष्य भौतिक ऐश्वर्य या यशः प्राप्ति न होकर आत्मा को कर्ममल से मुक्त करना होता है। तीसरा लक्षण बताया गया 'अमाय' अर्थात् माया रहित होना। चौथा लक्षण बताया विस्रोतसिका अर्थात् लक्ष्य के प्रति शंका व चित्त की चंचलता के प्रवाह में न बहे, शंका का त्याग करे। जिस श्रद्धा के साथ संयम पथ पर कदम बढ़ाया है, उसी श्रद्धा के साथ संयम का पालन करे ।
• इन लक्षणों को हम अपने जीवन में भी उतारने का लक्ष्य रखें। हम अपने जीवन को सरल बनाएं। मोक्ष अभिलाषा तो हम सभी की है, परन्तु क्या हम उस ओर कदम बढ़ा रहे हैं? माया से रहित होकर यदि हम अपनी दिनचर्या के कार्यक्रम संपादित करेंगे तो अवश्य ही कर्ममल से दूर होंगे।
आचारांग सूत्र हमें शिक्षा देते हुए कहता है कि पांच इन्द्रियों के पांच ग्राह्य विषय- शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श हैं। ये ऊँची, नीची आदि सभी दिशाओं में मिलते हैं। इन्द्रियों के द्वारा आत्मा इनको ग्रहण करता है, सुनता है, देखता है, सूंघता है, चखता है और स्पर्श करता है। ग्रहण करना इन्द्रिय का गुण है, गृहीत विषयों के प्रतिमूर्च्छा करना मन या चेतन का कार्य है। जब मन विषयों के प्रति आसक्त होता है तब विषय मन के लिए बंध बनाता है। शास्त्रकार बताते हैं कि रूप एवं शब्द का देखना-सुनना स्वयं में कोई दोष नहीं है, किन्तु उनमें आसक्ति होने से आत्मा इनमें मूर्च्छित हो जाता है, फंस जाता है। यह आसक्ति ही संसार है। अनासक्त आत्मा संसार में स्थित रहता हुआ भी संसार से मुक्त बनने की कोशिश करता है। हम भी संसार में रहते हुए संसार से मुक्त बन सकते हैं।
Jain Educationa International
संसार त्याग कर प्रत्येक व्यक्ति दीक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। परन्तु संसार में रहते हुए अपने परिग्रह में यथासम्भव कमी तो कर ही सकता है। जो परिग्रह को बढाता है, उसके प्रति चाहना रखता है वह स्वयं के सुख के लिए दूसरों के सुख-दुःख की भी परवाह नहीं करता, वह शोषक तथा उत्पीडक भी बन जाता है। इस तरह से परिग्रह के साथ हिंसा का भी अनुबंध स्वतः हो जाता है। सुख की इच्छा से व्यक्ति धन का संग्रह करता है किन्तु धन से कभी सुख नहीं मिलता, अन्त में उसे दुःख, शोक, चिन्ता और क्लेश ही प्राप्त होता है। हमारा चिन्तन
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org