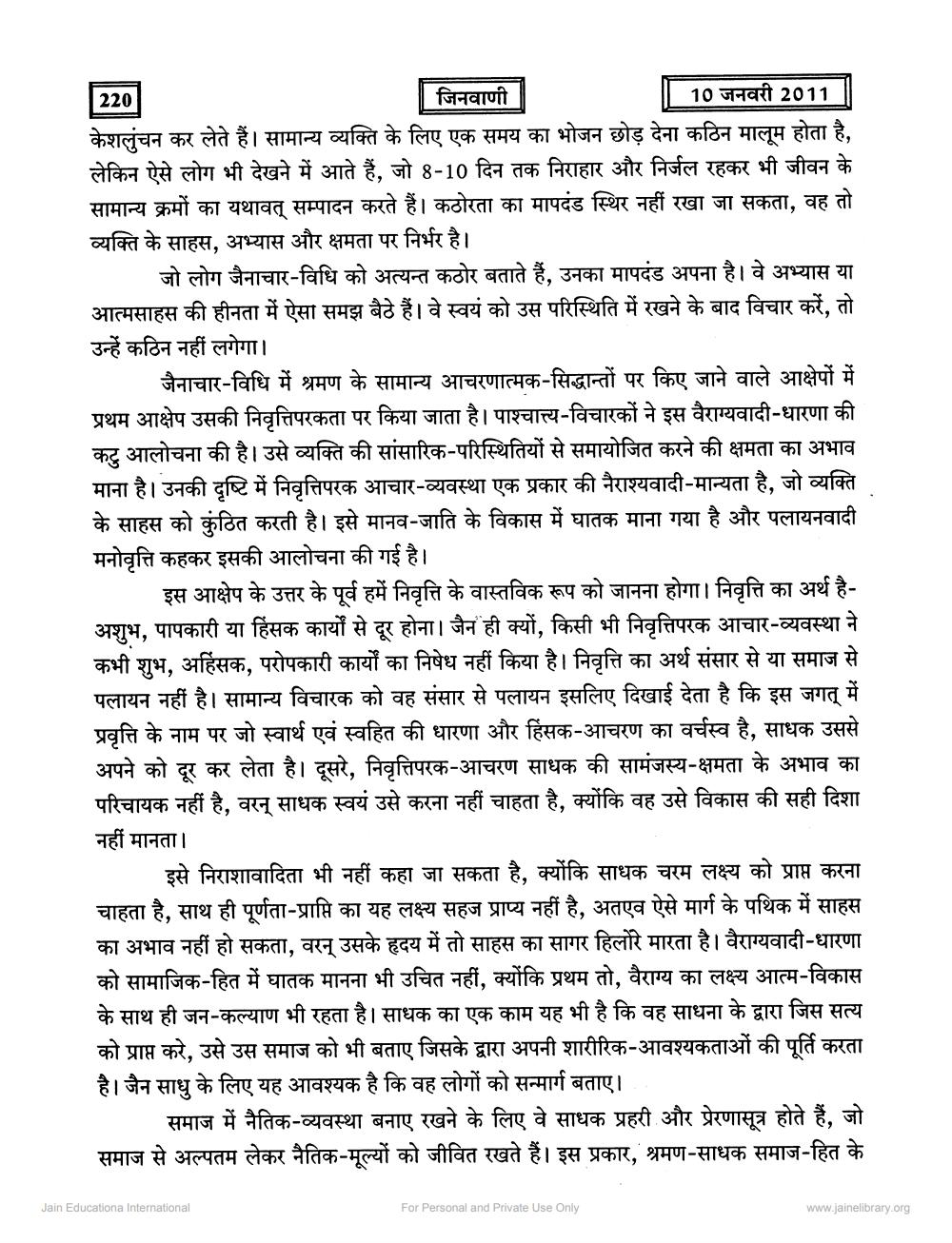________________
220
जिनवाणी
|| 10 जनवरी 2011 || केशलुंचन कर लेते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए एक समय का भोजन छोड़ देना कठिन मालूम होता है, लेकिन ऐसे लोग भी देखने में आते हैं, जो 8-10 दिन तक निराहार और निर्जल रहकर भी जीवन के सामान्य क्रमों का यथावत् सम्पादन करते हैं। कठोरता का मापदंड स्थिर नहीं रखा जा सकता, वह तो व्यक्ति के साहस, अभ्यास और क्षमता पर निर्भर है।
जो लोग जैनाचार-विधि को अत्यन्त कठोर बताते हैं, उनका मापदंड अपना है। वे अभ्यास या आत्मसाहस की हीनता में ऐसा समझ बैठे हैं। वे स्वयं को उस परिस्थिति में रखने के बाद विचार करें, तो उन्हें कठिन नहीं लगेगा।
जैनाचार-विधि में श्रमण के सामान्य आचरणात्मक-सिद्धान्तों पर किए जाने वाले आक्षेपों में प्रथम आक्षेप उसकी निवृत्तिपरकता पर किया जाता है। पाश्चात्त्य-विचारकों ने इस वैराग्यवादी-धारणा की कटु आलोचना की है। उसे व्यक्ति की सांसारिक-परिस्थितियों से समायोजित करने की क्षमता का अभाव माना है। उनकी दृष्टि में निवृत्तिपरक आचार-व्यवस्था एक प्रकार की नैराश्यवादी-मान्यता है, जो व्यक्ति के साहस को कुंठित करती है। इसे मानव-जाति के विकास में घातक माना गया है और पलायनवादी मनोवृत्ति कहकर इसकी आलोचना की गई है।
इस आक्षेप के उत्तर के पूर्व हमें निवृत्ति के वास्तविक रूप को जानना होगा। निवृत्ति का अर्थ हैअशुभ, पापकारी या हिंसक कार्यों से दूर होना। जैन ही क्यों, किसी भी निवृत्तिपरक आचार-व्यवस्था ने कभी शुभ, अहिंसक, परोपकारी कार्यों का निषेध नहीं किया है। निवृत्ति का अर्थ संसार से या समाज से पलायन नहीं है। सामान्य विचारक को वह संसार से पलायन इसलिए दिखाई देता है कि इस जगत् में प्रवृत्ति के नाम पर जो स्वार्थ एवं स्वहित की धारणा और हिंसक-आचरण का वर्चस्व है, साधक उससे अपने को दूर कर लेता है। दूसरे, निवृत्तिपरक-आचरण साधक की सामंजस्य-क्षमता के अभाव का परिचायक नहीं है, वरन् साधक स्वयं उसे करना नहीं चाहता है, क्योंकि वह उसे विकास की सही दिशा नहीं मानता।
इसे निराशावादिता भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि साधक चरम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, साथ ही पूर्णता-प्राप्ति का यह लक्ष्य सहज प्राप्य नहीं है, अतएव ऐसे मार्ग के पथिक में साहस का अभाव नहीं हो सकता, वरन् उसके हृदय में तो साहस का सागर हिलोरे मारता है। वैराग्यवादी-धारणा को सामाजिक-हित में घातक मानना भी उचित नहीं, क्योंकि प्रथम तो, वैराग्य का लक्ष्य आत्म-विकास के साथ ही जन-कल्याण भी रहता है। साधक का एक काम यह भी है कि वह साधना के द्वारा जिस सत्य को प्राप्त करे, उसे उस समाज को भी बताए जिसके द्वारा अपनी शारीरिक-आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैन साधु के लिए यह आवश्यक है कि वह लोगों को सन्मार्ग बताए।
समाज में नैतिक-व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे साधक प्रहरी और प्रेरणासूत्र होते हैं, जो समाज से अल्पतम लेकर नैतिक-मूल्यों को जीवित रखते हैं। इस प्रकार, श्रमण-साधक समाज-हित के
Jain Educationa International
For Personal and Private Use Only
www.jainelibrary.org