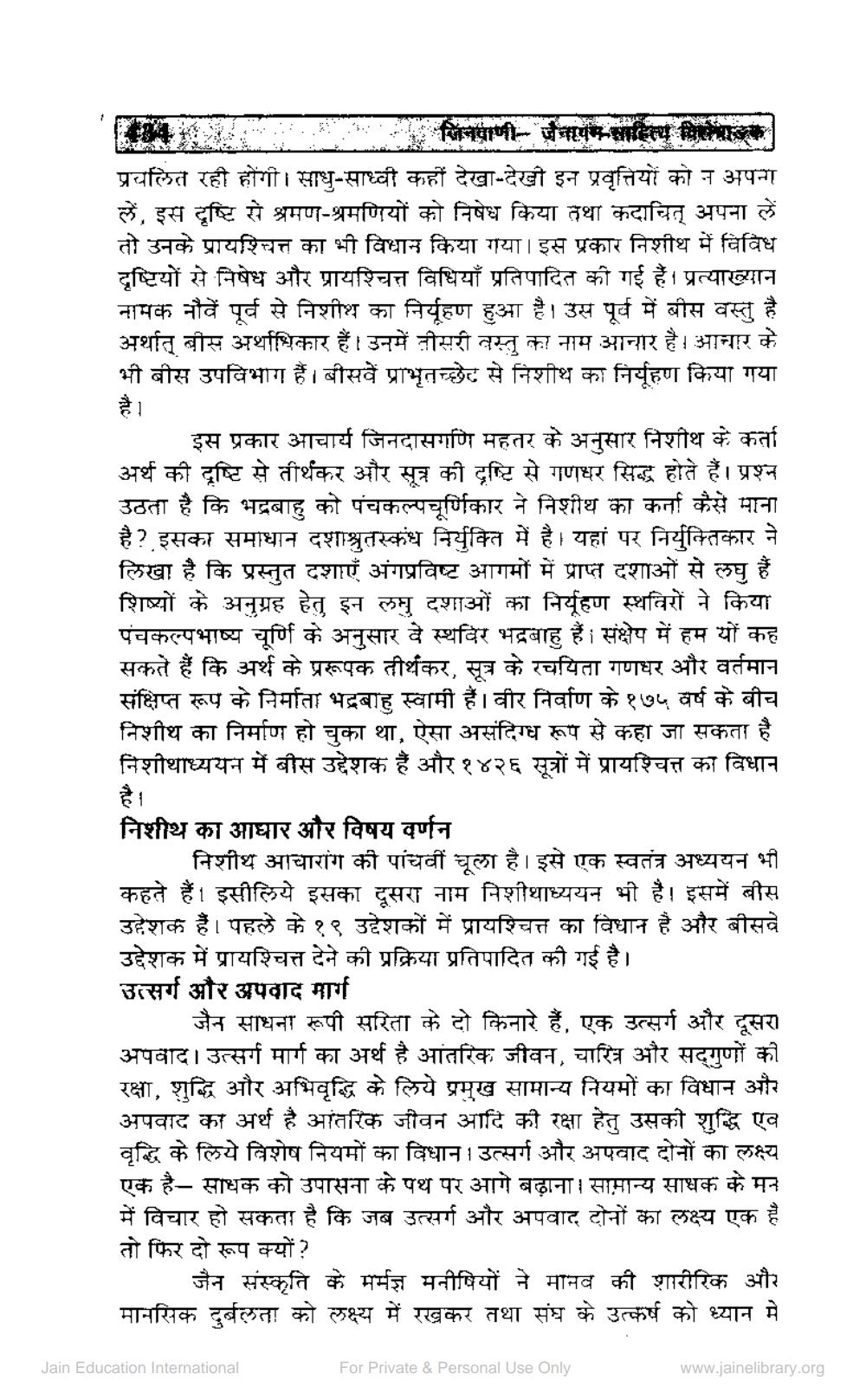________________
प्रचलित रही होंगी। साधु-साध्वी कहीं देखा-देखी इन प्रवृत्तियों को न अपना लें, इस दृष्टि से श्रमण-श्रमणियों को निषेध किया तथा कदाचित् अपना लें तो उनके प्रायश्चित्त का भी विधान किया गया। इस प्रकार निशीथ में विविध दृष्टियों से निषेध और प्रायश्चित्त विधियाँ प्रतिपादित की गई है। प्रत्याख्यान नामक नौवें पूर्व से निशीथ का निर्यहण हुआ है। उस पूर्व में बीस वस्तु है अर्थात् बीस अधिकार हैं। उनमें तीसरी वस्तु का नाम आचार है। आचार के भी बीस उपविभाग हैं। बीसवें प्राभृतच्छेद से निशीथ का निर्ग्रहण किया गया
इस प्रकार आचार्य जिनदासगणि महतर के अनुसार निशीथ के कर्ता अर्थ की दृष्टि से तीर्थकर और सूत्र की दृष्टि से गणधर सिद्ध होते हैं। प्रश्न उठता है कि भद्रबाहु को पंचकल्पचूर्णिकार ने निशीथ का कर्ता कैसे माना है? इसका समाधान दशाश्रुतस्कंध नियुक्ति में है। यहां पर नियुक्तिकार ने लिखा है कि प्रस्तुत दशाएँ अंगप्रविष्ट आगमों में प्राप्त दशाओं से लघु है शिष्यों के अनुग्रह हेतु इन लमु दशाओं का नि!हण स्थविरों ने किया पंचकल्पभाष्य चूर्णि के अनुसार वे स्थविर भद्रबाहु हैं। संक्षेप में हम यों कह सकते हैं कि अर्थ के प्ररूपक तीर्थकर, सूत्र के रचयिता गणधर और वर्तमान संक्षिप्त रूप के निर्माता भद्रबाहु स्वामी हैं। वीर निर्वाण के १७५ वर्ष के बीच निशीथ का निर्माण हो चुका था, ऐसा असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है निशीथाध्ययन में बीस उद्देशक हैं और १४२६ सूत्रों में प्रायश्चित्त का विधान
निशीथ का आधार और विषय वर्णन
निशीथ आचारांग की पांचवीं चूला है। इसे एक स्वतंत्र अध्ययन भी कहते हैं। इसीलिये इसका दूसरा नाम निशीथाध्ययन भी है। इसमें बीस उद्देशक हैं। पहले के १९ उद्देशकों में प्रायश्चित्त का विधान है और बीसवे उद्देशक में प्रायश्चित्त देने की प्रक्रिया प्रतिपादित की गई है। उत्सर्ग और अपवाद मार्ग
जैन साधना रूपी सरिता के दो किनारे हैं, एक उत्सर्ग और दूसरा अपवाद। उत्सर्ग मार्ग का अर्थ है आंतरिक जीवन, चारित्र और सद्गुणों को रक्षा, शुद्धि और अभिवृद्धि के लिये प्रमुख सामान्य नियमों का विधान और अपवाद का अर्थ है आंतरिक जीवन आदि की रक्षा हेतु उसको शुद्धि एव वृद्धि के लिये विशेष नियमों का विधान । उत्सर्ग और अपवाद दोनों का लक्ष्य एक है- साधक को उपासना के पथ पर आगे बढ़ाना। सामान्य साधक के मन में विचार हो सकता है कि जब उत्सर्ग और अपवाद दोनों का लक्ष्य एक है तो फिर दो रूप क्यों?
जैन संस्कृति के मर्मज्ञ मनीषियों ने मानव की शारीरिक और मानसिक दुर्बलता को लक्ष्य में रखकर तथा संघ के उत्कर्ष को ध्यान में
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org