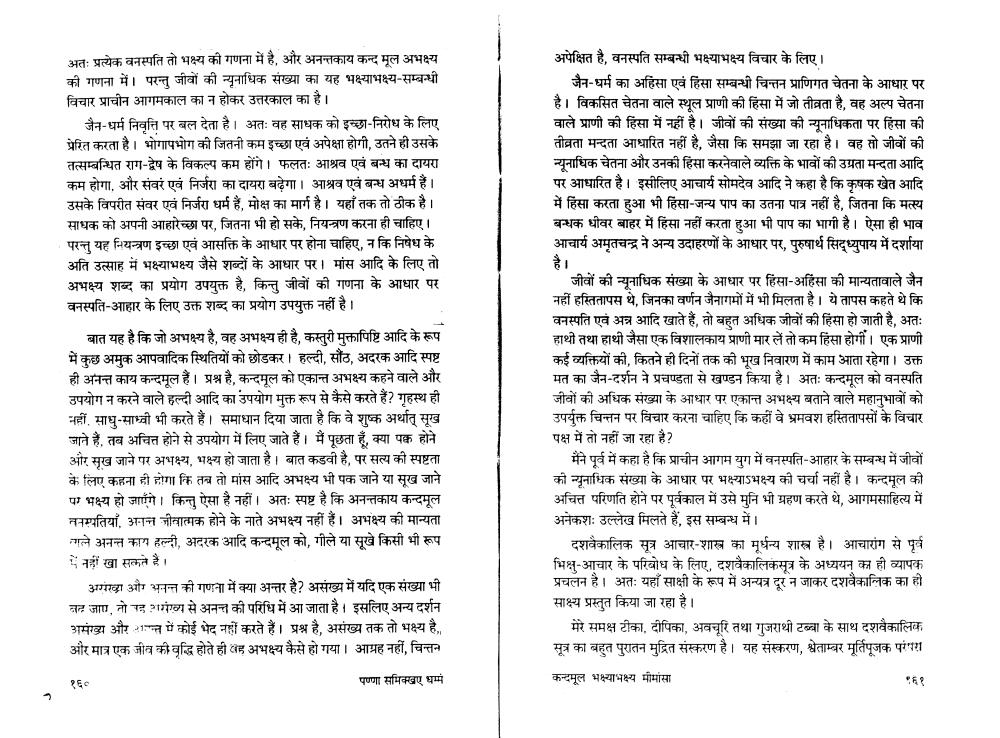________________
अपेक्षित है, वनस्पति सम्बन्धी भक्ष्याभक्ष्य विचार के लिए।
जैन-धर्म का अहिंसा एवं हिंसा सम्बन्धी चिन्तन प्राणिगत चेतना के आधार पर है। विकसित चेतना वाले स्थूल प्राणी की हिंसा में जो तीव्रता है, वह अल्प चेतना वाले प्राणी की हिंसा में नहीं है। जीवों की संख्या की न्यूनाधिकता पर हिंसा की तीव्रता मन्दता आधारित नहीं है, जैसा कि समझा जा रहा है। वह तो जीवों की न्यूनाधिक चेतना और उनकी हिंसा करनेवाले व्यक्ति के भावों की उग्रता मन्दता आदि पर आधारित है। इसीलिए आचार्य सोमदेव आदि ने कहा है कि कृषक खेत आदि में हिंसा करता हुआ भी हिंसा-जन्य पाप का उतना पात्र नहीं है, जितना कि मत्स्य बन्धक धीवर बाहर में हिंसा नहीं करता हुआ भी पाप का भागी है। ऐसा ही भाव आचार्य अमृतचन्द्र ने अन्य उदाहरणों के आधार पर, पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय में दर्शाया
अतः प्रत्येक वनस्पति तो भक्ष्य की गणना में है, और अनन्तकाय कन्द मूल अभक्ष्य की गणना में। परन्तु जीवों की न्यूनाधिक संख्या का यह भक्ष्याभक्ष्य-सम्बन्धी विचार प्राचीन आगमकाल का न होकर उत्तरकाल का है।
जैन-धर्म निवृत्ति पर बल देता है। अतः वह साधक को इच्छा-निरोध के लिए प्रेरित करता है। भोगापभोग की जितनी कम इच्छा एवं अपेक्षा होगी, उतने ही उसके तत्सम्बन्धित राग-द्वेष के विकल्प कम होंगे। फलतः आश्रव एवं बन्ध का दायरा कम होगा, और संवरं एवं निर्जरा का दायरा बढ़ेगा। आश्रव एवं बन्ध अधर्म हैं। उसके विपरीत संवर एवं निर्जरा धर्म हैं, मोक्ष का मार्ग है। यहाँ तक तो ठीक है। साधक को अपनी आहारेच्छा पर, जितना भी हो सके, नियन्त्रण करना ही चाहिए। परन्तु यह नियन्त्रण इच्छा एवं आसक्ति के आधार पर होना चाहिए, न कि निषेध के अति उत्साह में भक्ष्याभक्ष्य जैसे शब्दों के आधार पर। मांस आदि के लिए तो अभक्ष्य शब्द का प्रयोग उपयुक्त है, किन्तु जीवों की गणना के आधार पर वनस्पति-आहार के लिए उक्त शब्द का प्रयोग उपयुक्त नहीं है।
बात यह है कि जो अभक्ष्य है, वह अभक्ष्य ही है, कस्तुरी मुक्तापिष्टि आदि के रूप में कुछ अमुक आपवादिक स्थितियों को छोडकर। हल्दी, सौंठ, अदरक आदि स्पष्ट ही अनन्त काय कन्दमूल हैं। प्रश्न है, कन्दमूल को एकान्त अभक्ष्य कहने वाले और उपयोग न करने वाले हल्दी आदि का उपयोग मुक्त रूप से कैसे करते हैं? गृहस्थ ही नहीं. साधु-साध्वी भी करते हैं। समाधान दिया जाता है कि वे शुष्क अर्थात् सूख जाते हैं, तब अचित्त होने से उपयोग में लिए जाते हैं। मैं पूछता है, क्या पक्क होने
और सूख जाने पर अभक्ष्य, भक्ष्य हो जाता है। बात कडवी है, पर सत्य की स्पष्टता के लिए कहना ही होगा कि तब तो मांस आदि अभक्ष्य भी पक जाने या सूख जाने पर भक्ष्य हो जाएंगे। किन्तु ऐसा है नहीं। अतः स्पष्ट है कि अनन्तकाय कन्दमूल नतस्पतियाँ, अपन जीवात्मक होने के नाते अभक्ष्य नहीं हैं। अभक्ष्य की मान्यता गले अनन्त काय हल्दी, अदरक आदि कन्दमूल को, गीले या सूखे किसी भी रूप
नहीं खा सकते है। __ अपरदा और अनन्त की गणना में क्या अन्तर है? असंख्य में यदि एक संख्या भी बन जाए, तो वह आय से अनन्त की परिधि में आ जाता है। इसलिए अन्य दर्शन असंख्य और २१ त में कोई भेद नहीं करते हैं। प्रश्न है, असंख्य तक तो भक्ष्य है, और मात्र एक जीव की वृद्धि होते ही वह अभक्ष्य कैसे हो गया। आग्रह नहीं, चिन्तन
जीवों की न्यूनाधिक संख्या के आधार पर हिंसा-अहिंसा की मान्यतावाले जैन नहीं हस्तितापस थे, जिनका वर्णन जैनागमों में भी मिलता है। ये तापस कहते थे कि वनस्पति एवं अत्र आदि खाते हैं, तो बहत अधिक जीवों की हिंसा हो जाती है, अतः हाथी तथा हाथी जैसा एक विशालकाय प्राणी मार लें तो कम हिंसा होगी। एक प्राणी कई व्यक्तियों की, कितने ही दिनों तक की भख निवारण में काम आता रहेगा। उक्त मत का जेन-दर्शन ने प्रचण्डता से खण्डन किया है। अतः कन्दमूल को वनस्पति जीवों को अधिक संख्या के आधार पर एकान्त अभक्ष्य बताने वाले महानुभावों को उपर्युक्त चिन्तन पर विचार करना चाहिए कि कहीं वे भ्रमवश हस्तितापसों के विचार पक्ष में तो नहीं जा रहा है?
मैंने पूर्व में कहा है कि प्राचीन आगम युग में वनस्पति-आहार के सम्बन्ध में जीवों की न्यूनाधिक संख्या के आधार पर भक्ष्याऽभक्ष्य की चर्चा नहीं है। कन्दमूल की अचित्त परिणति होने पर पूर्वकाल में उसे मुनि भी ग्रहण करते थे, आगमसाहित्य में अनेकशः उल्लेख मिलते हैं, इस सम्बन्ध में।
दशवकालिक सूत्र आचार-शास्त्र का मूर्धन्य शास्त्र है। आचारांग से पूर्व भिक्षु-आचार के परिबोध के लिए, दशवैकालिकसूत्र के अध्ययन का ही व्यापक प्रचलन है। अतः यहाँ साक्षी के रूप में अन्यत्र दूर न जाकर दशवैकालिक का ही साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है।
मेरे समक्ष टीका, दीपिका, अवचूरि तथा गजराथी टब्बा के साथ दशवैकालिक सूत्र का बहुत पुरातन मुद्रित संस्करण है। यह संस्करण, श्वेताम्बर मूर्तिपूजक परंपरा कन्दमूल भक्ष्याभक्ष्य मीमांसा
पण्णा समिक्खए धम्म