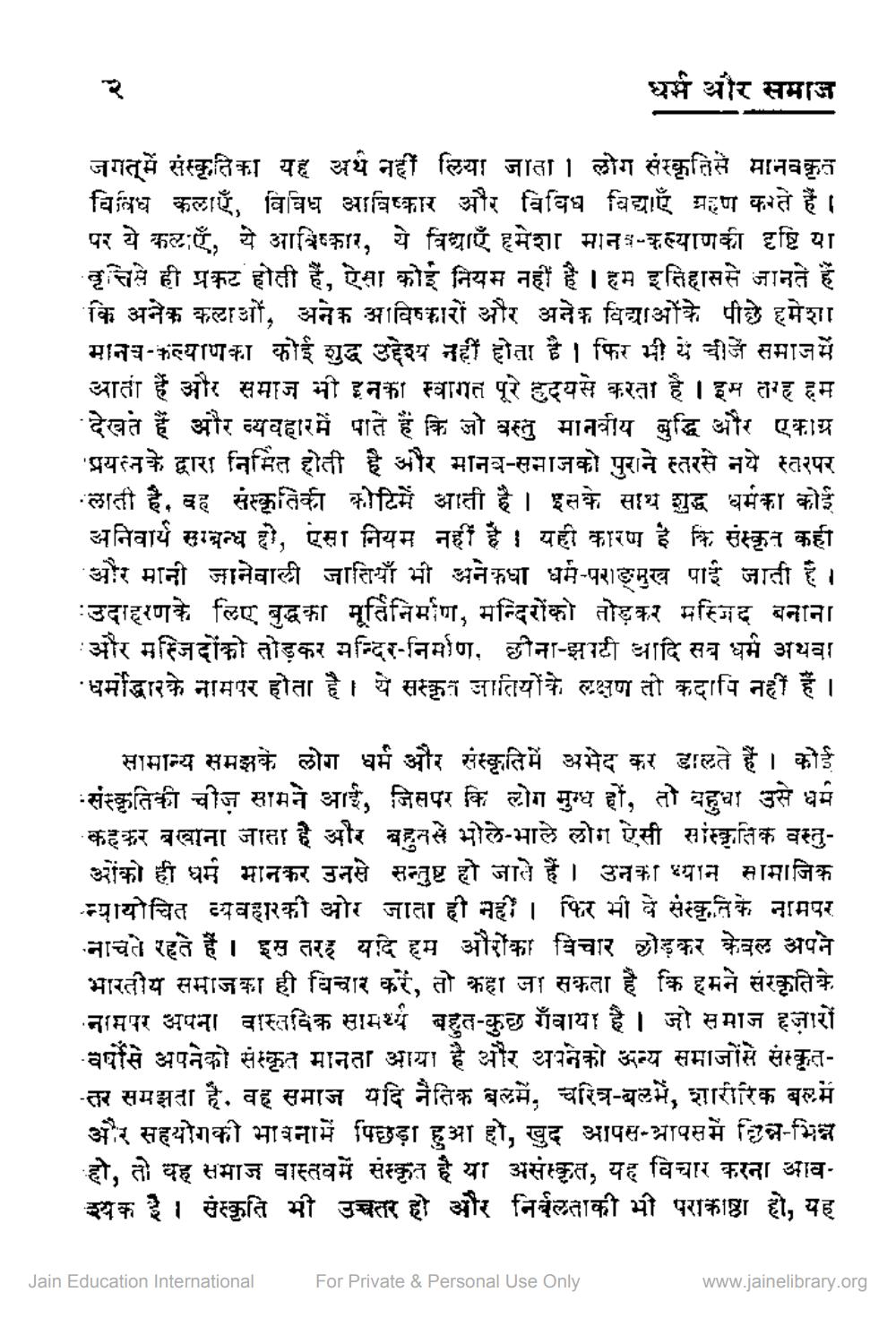________________
धर्म और समाज
जगत में संस्कृतिका यह अर्थ नहीं लिया जाता । लोग संस्कृति से मानवकृत विविध कलाएँ, विविध आविष्कार और विविध विद्याएँ ग्रहण करते हैं । पर ये कलाएँ, ये आविष्कार, ये विद्याएँ हमेशा मान-कल्याण की दृष्टि या वृत्तिले ही प्रकट होती हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। हम इतिहाससे जानते हैं कि अनेक कलाओं, अनेक आविष्कारों और अनेक विद्याओं के पीछे हमेशा मानव-कल्याणका कोई शुद्ध उद्देश्य नहीं होता है। फिर भी ये चीजें समाज में आता हैं और समाज भी इनका स्वागत पूरे हदयसे करता है । इस तरह हम देखते हैं और व्यवहार में पाते हैं कि जो वस्तु मानवीय बुद्धि और एकाग्र प्रयत्न के द्वारा निर्मित होती है और मानव-समाजको पुराने स्तरसे नये स्तरपर लाती है, वह संस्कृतिकी कोटिमें आती है। इसके साथ शुद्ध धर्मका कोई अनिवार्य सम्बन्ध हो, एसा नियम नहीं है। यही कारण है कि संस्कृत कही और मानी जानेवाली जातियाँ भी अनेकधा धर्म-पराङ्मुख पाई जाती है । उदाहरणके लिए बुद्धका मूर्तिनिर्माण, मन्दिरोंको तोड़कर मस्जिद बनाना
और मस्जिदोंको तोड़कर मन्दिर-निर्माण, छीना-झपटी आदि सब धर्म अथवा 'धर्मोद्धार के नामपर होता है। ये सस्कृत जातियों के लक्षण तो कदापि नहीं हैं ।
सामान्य समझके लोग धर्म और संस्कृति में अभेद कर डालते हैं। कोई संस्कृतिकी चीज़ सामने आई, जिसपर कि लोग मुन्ध हों, तो बहुधा उसे धर्म कहकर बखाना जाता है और बहुत से भोले-भाले लोग ऐसी सांस्कृतिक वस्तु
ओंको ही धर्म मानकर उनसे सन्तुष्ट हो जाते हैं। उनका ध्यान सामाजिक न्यायोचित व्यवहार की ओर जाता ही नहीं। फिर भी वे संस्कृति के नामपर नाचते रहते हैं। इस तरह यदि हम औरोंका विचार छोड़कर केवल अपने भारतीय समाज का ही विचार करें, तो कहा जा सकता है कि हमने संस्कृति के नामपर अपना वास्तविक सामर्थ्य बहुत-कुछ गँवाया है। जो समाज हजारों वर्षोंसे अपनेको संस्कृत मानता आया है और अपनेको अन्य समाजोंसे संस्कृत-तर समझता है. वह समाज यदि नैतिक बलमें, चरित्र-बल), शारीरिक बल में
और सहयोगको भावनामें पिछड़ा हुआ हो, खुद आपस-आपस में छिन्न-भिन्न हो, तो वह समाज वास्तव में संस्कृत है या असंस्कृत, यह विचार करना आव. श्यक है। संस्कृति भी उच्चतर हो और निर्बलताकी भी पराकाष्ठा हो, यह
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org