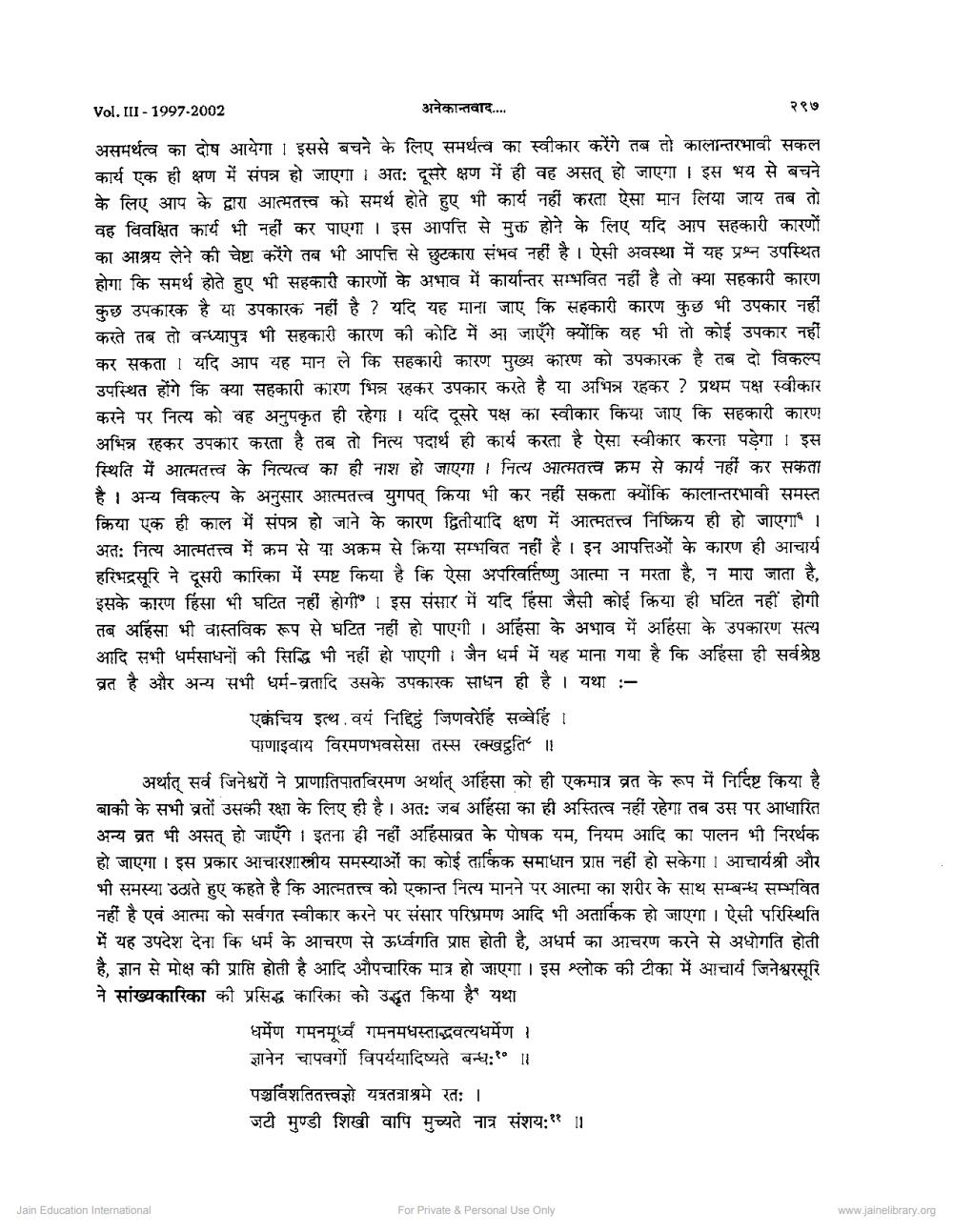________________
Vol. III-1997-2002 अनेकान्तवाद....
२९७ असमर्थत्व का दोष आयेगा । इससे बचने के लिए समर्थत्व का स्वीकार करेंगे तब तो कालान्तरभावी सकल कार्य एक ही क्षण में संपन्न हो जाएगा। अत: दूसरे क्षण में ही वह असत् हो जाएगा । इस भय से बचने के लिए आप के द्वारा आत्मतत्त्व को समर्थ होते हुए भी कार्य नहीं करता ऐसा मान लिया जाय तब तो वह विवक्षित कार्य भी नहीं कर पाएगा । इस आपत्ति से मुक्त होने के लिए यदि आप सहकारी कारणों का आश्रय लेने की चेष्टा करेंगे तब भी आपत्ति से छुटकारा संभव नहीं है। ऐसी अवस्था में यह प्रश्न उपस्थित होगा कि समर्थ होते हुए भी सहकारी कारणों के अभाव में कार्यान्तर सम्भवित नहीं है तो क्या सहकारी कारण कुछ उपकारक है या उपकारक नहीं है ? यदि यह माना जाए कि सहकारी कारण कुछ भी उपकार नहीं करते तब तो वन्ध्यापुत्र भी सहकारी कारण की कोटि में आ जाएँगे क्योंकि वह भी तो कोई उपकार नहीं कर सकता । यदि आप यह मान ले कि सहकारी कारण मुख्य कारण को उपकारक है तब दो विकल्प उपस्थित होंगे कि क्या सहकारी कारण भिन्न रहकर उपकार करते है या अभिन्न रहकर ? प्रथम पक्ष स्वीकार करने पर नित्य को वह अनुपकृत ही रहेगा । यदि दूसरे पक्ष का स्वीकार किया जाए कि सहकारी कारण अभिन्न रहकर उपकार करता है तब तो नित्य पदार्थ ही कार्य करता है ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा । इस स्थिति में आत्मतत्त्व के नित्यत्व का ही नाश हो जाएगा । नित्य आत्मतत्त्व कम से कार्य नहीं कर सकता है। अन्य विकल्प के अनुसार आत्मतत्त्व युगपत् क्रिया भी कर नहीं सकता क्योंकि कालान्तरभावी समस्त किया एक ही काल में संपत्र हो जाने के कारण द्वितीयादि क्षण में आत्मतत्त्व निष्क्रिय ही हो जाएगा । अतः नित्य आत्मतत्त्व में क्रम से या अक्रम से क्रिया सम्भवित नहीं है । इन आपत्तिओं के कारण ही आचार्य हरिभद्रसूरि ने दूसरी कारिका में स्पष्ट किया है कि ऐसा अपरिवर्तिष्णु आत्मा न मरता है, न मारा जाता है, इसके कारण हिंसा भी घटित नहीं होगी । इस संसार में यदि हिंसा जैसी कोई क्रिया ही घटित नहीं होगी तब अहिंसा भी वास्तविक रूप से घटित नहीं हो पाएगी । अहिंसा के अभाव में अहिंसा के उपकारण सत्य आदि सभी धर्मसाधनों की सिद्धि भी नहीं हो पाएगी। जैन धर्म में यह माना गया है कि अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ व्रत है और अन्य सभी धर्म-व्रतादि उसके उपकारक साधन ही है । यथा :
एकंचिय इत्थ वयं निद्दिटुं जिणवरेहिं सव्वेहिं ।
पाणाइवाय विरमणभवसेसा तस्स रक्खट्ठति ।। अर्थात् सर्व जिनेश्वरों ने प्राणातिपातविरमण अर्थात् अहिंसा को ही एकमात्र व्रत के रूप में निर्दिष्ट किया है बाकी के सभी व्रतों उसकी रक्षा के लिए ही है। अतः जब अहिंसा का ही अस्तित्व नहीं रहेगा तब उस पर आधारित अन्य व्रत भी असत् हो जाएंगे। इतना ही नहीं अहिंसाव्रत के पोषक यम, नियम आदि का पालन भी निरर्थक हो जाएगा। इस प्रकार आचारशास्त्रीय समस्याओं का कोई तार्किक समाधान प्राप्त नहीं हो सकेगा। आचार्यश्री और भी समस्या उठाते हुए कहते है कि आत्मतत्त्व को एकान्त नित्य मानने पर आत्मा का शरीर के साथ सम्बन्ध सम्भवित नहीं है एवं आत्मा को सर्वगत स्वीकार करने पर संसार परिभ्रमण आदि भी अताकिक हो जाएगा । ऐसी परिस्थिति में यह उपदेश देना कि धर्म के आचरण से ऊर्ध्वगति प्राप्त होती है, अधर्म का आचरण करने से अधोगति होती है, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है आदि औपचारिक मात्र हो जाएगा। इस श्लोक की टीका में आचार्य जिनेश्वरसरि ने सांख्यकारिका की प्रसिद्ध कारिका को उद्धत किया है। यथा
धर्मेण गमनमूर्ध्वं गमनमधस्ताद्भवत्यधर्मेण । ज्ञानेन चापवर्गो विपर्ययादिष्यते बन्ध:१० ।। पञ्चविंशतितत्त्वज्ञो यत्रतत्राश्रमे रतः । जटी मुण्डी शिखी वापि मुच्यते नात्र संशय:१२ ॥
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org