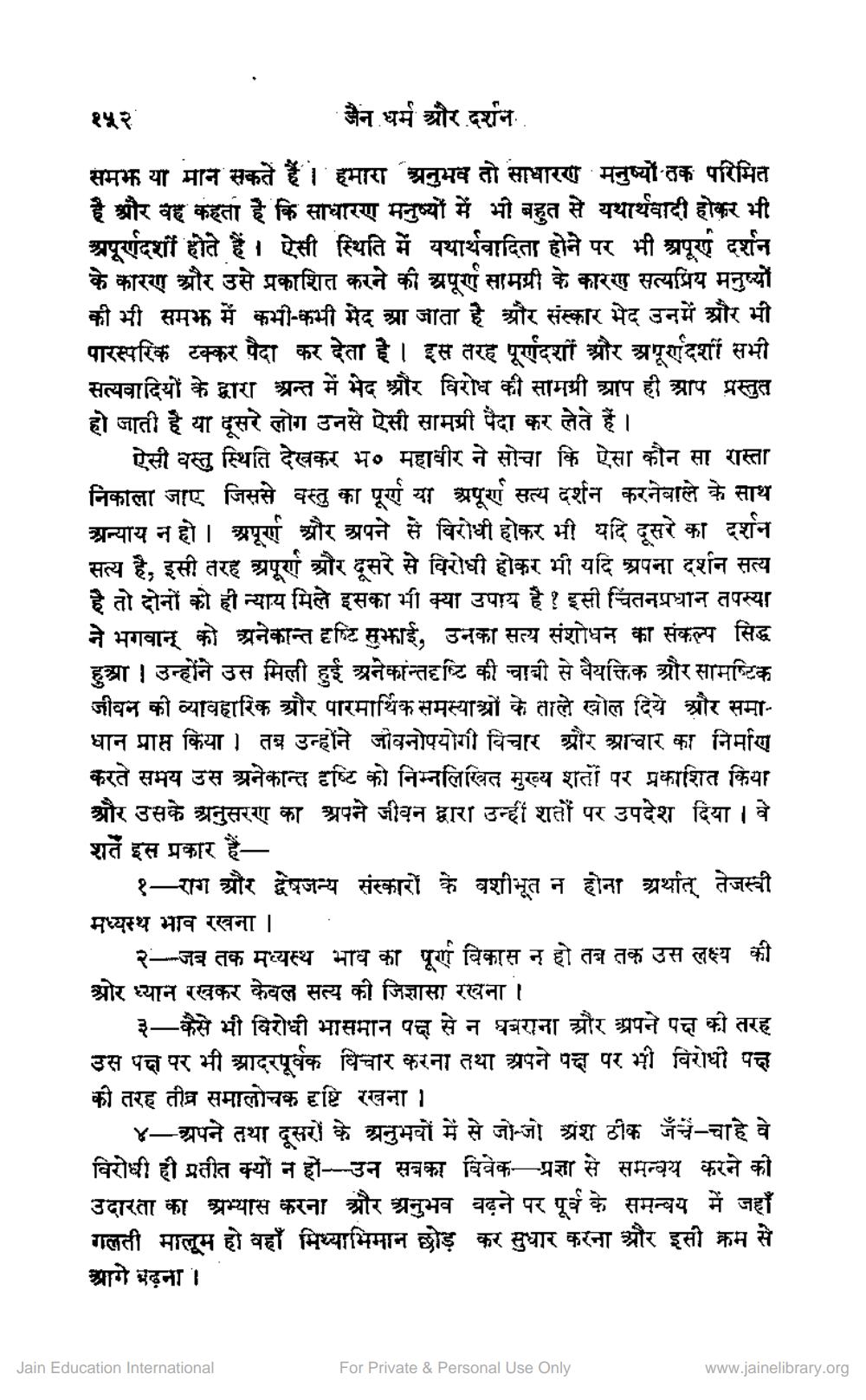________________
१५२
जैन धर्म और दर्शन..
समझ या मान सकते हैं। हमारा अनुभव तो साधारण मनुष्यों तक परिमित है और वह कहता है कि साधारण मनुष्यों में भी बहुत से यथार्थवादी होकर भी पूर्णदश होते हैं। ऐसी स्थिति में यथार्थवादिता होने पर भी अपूर्ण दर्शन के कारण और उसे प्रकाशित करने की अपूर्ण सामग्री के कारण सत्यप्रिय मनुष्यों की भी समझ में कभी-कभी भेद या जाता है और संस्कार भेद उनमें और भी पारस्परिक टक्कर पैदा कर देता है । इस तरह पूर्णदशों और अपूर्णदर्श सभी सत्यवादियों के द्वारा अन्त में भेद और विरोध की सामग्री आप ही आप प्रस्तुत हो जाती है या दूसरे लोग उनसे ऐसी सामग्री पैदा कर लेते हैं ।
ऐसी वस्तु स्थिति देखकर भ० महावीर ने सोचा कि ऐसा कौन सा रास्ता निकाला जाए जिससे वस्तु का पूर्ण या अपूर्ण सत्य दर्शन करनेवाले के साथ अन्याय न हो । अपूर्ण और अपने से विरोधी होकर भी यदि दूसरे का दर्शन सत्य है, इसी तरह पूर्ण और दूसरे से विरोधी होकर भी यदि अपना दर्शन सत्य है तो दोनों को ही न्याय मिले इसका भी क्या उपाय है ? इसी चिंतनप्रधान तपस्या ने भगवान् को अनेकान्त दृष्टि सुझाई, उनका सत्य संशोधन का संकल्प सिद्ध हुआ । उन्होंने उस मिली हुई अनेकान्तदृष्टि की चाबी से वैयक्तिक और सामष्टिक जीवन की व्यावहारिक और पारमार्थिक समस्याओं के ताले खोल दिये और समाधान प्राप्त किया । तब उन्होंने जीवनोपयोगी विचार और आचार का निर्माण करते समय उस अनेकान्त दृष्टि को निम्नलिखित मुख्य शर्तों पर प्रकाशित किया और उसके अनुसरण का अपने जीवन द्वारा उन्हीं शर्तों पर उपदेश दिया । वे शर्तें इस प्रकार हैं
१ - राग और द्वेषजन्य संस्कारों के वशीभूत न होना अर्थात् तेजस्वी
मध्यस्थ भाव रखना ।
२ —जब तक मध्यस्थ भाव का पूर्ण विकास न हो तब तक उस लक्ष्य की ओर ध्यान रखकर केवल सत्य की जिज्ञासा रखना ।
३ – कैसे भी विरोधी भासमान पक्ष से न घबराना और अपने पक्ष की तरह उस पक्ष पर भी आदरपूर्वक विचार करना तथा अपने पक्ष पर भी विरोधी पक्ष की तरह तीव्र समालोचक दृष्टि रखना ।
४
- अपने तथा दूसरों के अनुभवों में से जो जो अंश ठीक जँच - चाहे वे विरोधी ही प्रतीत क्यों न हों उन सत्रका विवेक प्रज्ञा से समन्वय करने की उदारता का अभ्यास करना और अनुभव बढ़ने पर पूर्व के समन्वय में जहाँ गलती मालूम हो वहाँ मिथ्याभिमान छोड़ कर सुधार करना और इसी क्रम से आगे बढ़ना ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org