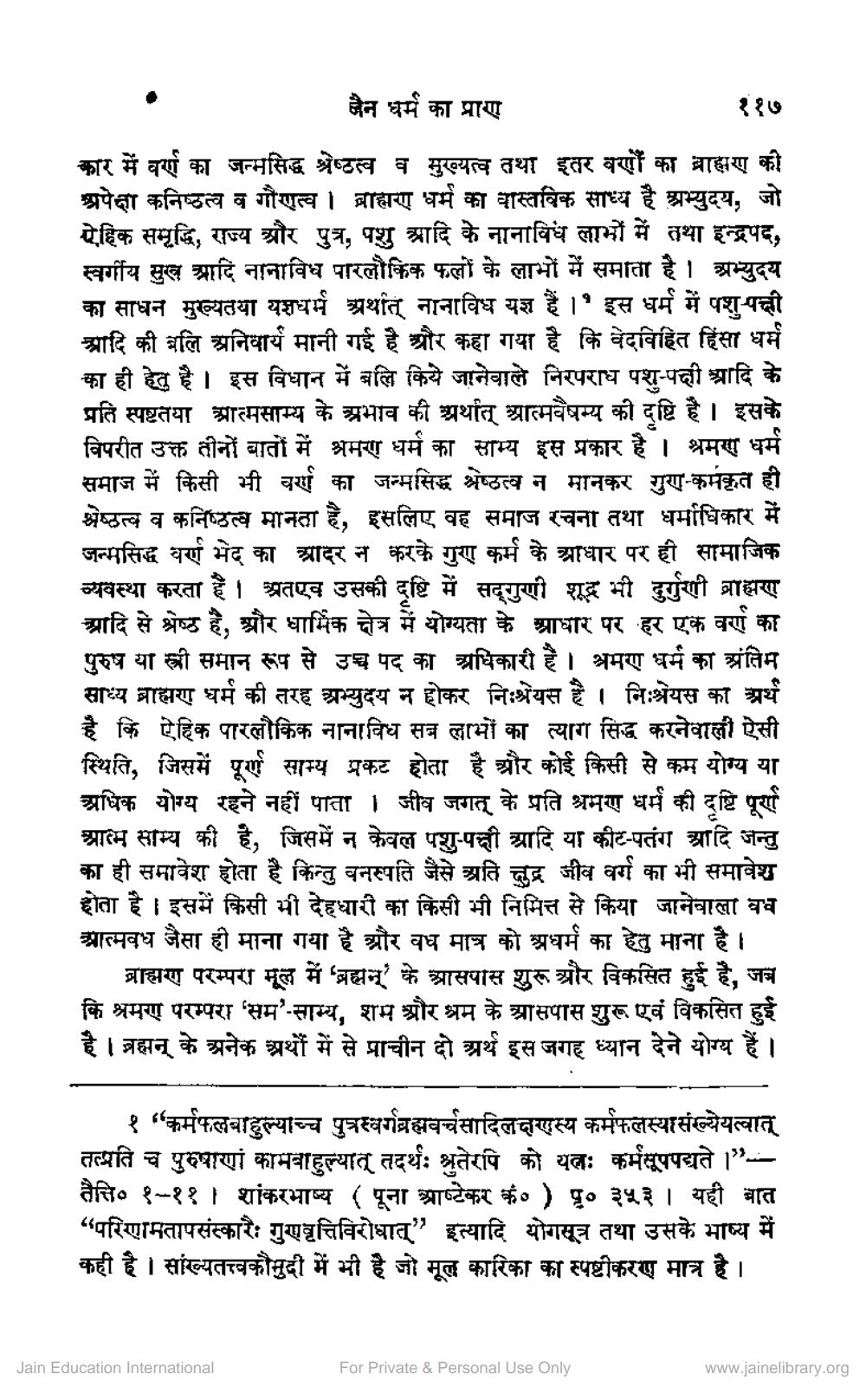________________
जैन धर्म का प्राण
११७
कार में वर्ण का जन्मसिद्ध श्रेष्ठत्व व मुख्यत्व तथा इतर वर्णों का ब्राह्मण की अपेक्षा कनिष्ठत्व व गौणत्व । ब्राह्मण धर्म का वास्तविक साध्य है श्रभ्युदय, जो ऐहिक समृद्धि, राज्य और पुत्र, पशु आदि के नानाविध लाभों में तथा इन्द्रपद, स्वर्गीय सुख आदि नानाविध पारलौकिक फलों के लाभों में समाता है । अभ्युदय का साधन मुख्यतया यशधर्म अर्थात् नानाविध यज्ञ हैं।' इस धर्म में पशु-पक्षी आदि की बलि अनिवार्य मानी गई है और कहा गया है कि वेदविहित हिंसा धर्म काही हेतु है । इस विधान में बलि किये जानेवाले निरपराध पशु-पक्षी श्रादि के प्रति स्पष्टतया आत्मसाम्य के अभाव की अर्थात् आत्मवैषम्य की दृष्टि है । इसके विपरीत उक्त तीनों बातों में श्रमण धर्म का साम्य इस प्रकार हैं । श्रमण धर्म समाज में किसी भी वर्ण का जन्मसिद्ध श्रेष्ठत्व न मानकर गुण-कर्मकृत ही श्रेष्ठत्व व कनिष्ठत्व मानता है, इसलिए वह समाज रचना तथा धर्माधिकार में जन्मसिद्ध वर्ण भेद का आदर न करके गुण कर्म के आधार पर ही सामाजिक व्यवस्था करता है । अतएव उसकी दृष्टि में सद्गुणी शूद्र भी दुर्गुणी ब्राह्मण आदि से श्रेष्ठ है, और धार्मिक क्षेत्र में योग्यता के आधार पर हर एक वर्ण का पुरुष या स्त्री समान रूप से उच्च पद का अधिकारी हैं । श्रमण धर्म का अंतिम साध्य ब्राह्मण धर्म की तरह अभ्युदय न होकर निःश्रेयस है । निःश्रेयस का अर्थ है कि ऐहिक पारलौकिक नानाविध सत्र लाभों का त्याग सिद्ध करनेवाली ऐसी स्थिति, जिसमें पूर्ण साम्य प्रकट होता है और कोई किसी से कम योग्य या अधिक योग्य रहने नहीं पाता । जीव जगत् के प्रति श्रमण धर्म की दृष्टि पूर्ण श्रात्म साम्य की है, जिसमें न केवल पशु-पक्षी आदि या कीट-पतंग आदि जन्तु का ही समावेश होता है किन्तु वनस्पति जैसे अति क्षुद्र जीव वर्ग का भी समावेश होता है। इसमें किसी भी देहधारी का किसी भी निमित्त से किया जानेवाला वध श्रात्मवध जैसा ही माना गया है और वध मात्र को अधर्म का हेतु माना है ।
ब्राह्मण परम्परा मूल में 'ब्रह्मन्' के आसपास शुरू और विकसित हुई है, जब कि श्रमण परम्परा 'सम' - साम्य, शम और श्रम के आसपास शुरू एवं विकसित हुई है । ब्रह्मन् के अनेक अर्थों में से प्राचीन दो अर्थ इस जगह ध्यान देने योग्य हैं ।
१ "कर्मफल बाहुल्याच्च पुत्रस्वर्ग ब्रह्मवर्चसादिलक्षणस्य कर्मफलस्यासंख्येयत्वात् तत्प्रति च पुरुषाणां कामबाहुल्यात् तदर्थः श्रुतेरपि को यत्नः कर्मसूपपद्यते ।" - तैत्ति० १-११ । शांकरभाष्य ( पूना आष्टेकर क० ) पृ० ३५३ । यही बात “परिणामतापसंस्कारैः गुणवृत्तिविरोधात्" इत्यादि योगसूत्र तथा उसके भाष्य में कही है । सांख्यतत्त्वकौमुदी में भी है जो मूल कारिका का स्पष्टीकरण मात्र है ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org