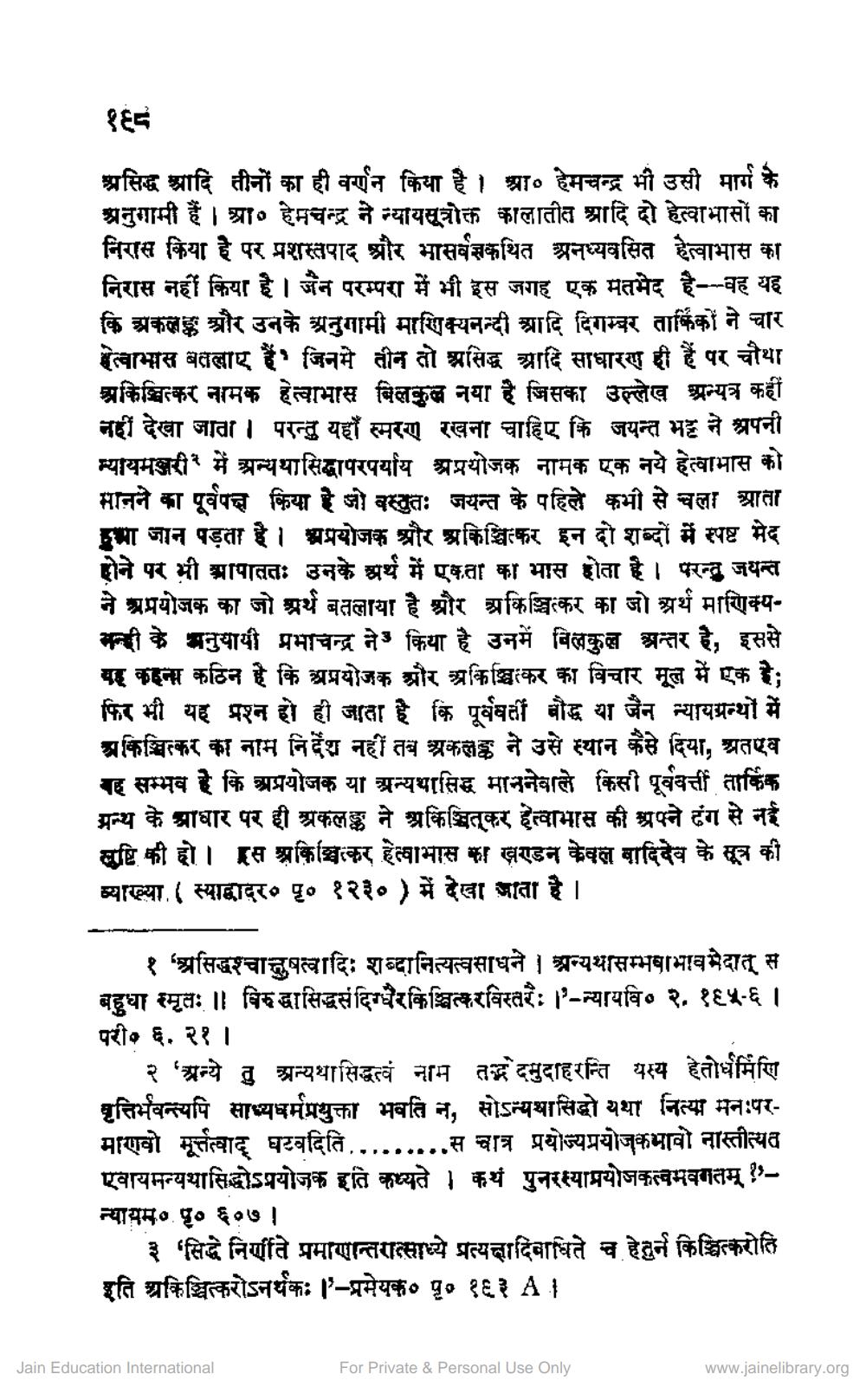________________
१६६
श्रसिद्ध श्रादि तीनों का ही वर्णन किया है। श्रा० हेमचन्द्र भी उसी मार्ग के अनुगामी हैं । श्रा० हेमचन्द्र ने न्यायसूत्रोक्त कालातीत श्रादि दो हेत्वाभासों का निरास किया है पर प्रशस्तपाद और भासर्वज्ञकथित अनध्यवसित हेत्वाभास का निरास नहीं किया है। जैन परम्परा में भी इस जगह एक मतभेद है---वह यह कि अकलङ्क और उनके अनुगामी माणिक्यनन्दी श्रादि दिगम्बर तार्किंकों ने चार हेत्वाभास बतलाए हैं। जिनमें तीन तो प्रसिद्ध आदि साधारण ही हैं पर चौथा अकिञ्चित्कर नामक हेत्वाभास बिलकुल नया है जिसका उल्लेख अन्यत्र कहीं नहीं देखा जाता। परन्तु यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि जयन्त भट्ट ने अपनी म्यायमअरी २ में अन्यथासिद्धापरपर्याय अप्रयोजक नामक एक नये हेत्वाभास को मानने का पूर्वपक्ष किया है जो वस्तुतः जयन्त के पहिले कभी से चला आता हुमा जान पड़ता है। अप्रयोजक और अकिञ्चित्कर इन दो शब्दों में स्पष्ट मेद होने पर भी आपाततः उनके अर्थ में एकता का भास होता है। परन्तु जयन्त ने अप्रयोजक का जो अर्थ बतलाया है और अकिञ्चित्कर का जो अर्थ माणिक्यमन्दी के अनुयायी प्रभाचन्द्र ने किया है उनमें बिलकुल अन्तर है, इससे यह कहना कठिन है कि अप्रयोजक और अकिश्चित्कर का विचार मूल में एक है; फिर भी यह प्रश्न हो ही जाता है कि पूर्ववर्ती बौद्ध या जैन न्यायग्रन्थों में अकिञ्चित्कर का नाम निर्देश नहीं तब अकलक ने उसे स्थान कैसे दिया, अतएव यह सम्भव है कि अप्रयोजक या अन्यथासिद्ध माननेवाले किसी पूर्ववर्ती तार्किक अन्य के आधार पर ही अकलङ्क ने अकिञ्चित्कर हेत्वाभास की अपने ढंग से नई सष्टि की हो। इस अकिश्चित्कर हेत्वाभास का खण्डन केवल वादिदेव के सूत्र की व्याख्या. { स्याद्वादर० पृ० १२३० ) में देखा जाता है ।
१'असिद्धश्चानुषत्वादिः शब्दानित्यत्वसाधने । अन्यथासम्भषाभावभेदात् स बहुधा स्मृतः ॥ विरु द्धासिद्धसंदिग्धैरकिञ्चित्करविस्तरैः। -न्यायवि० २. १६५-६ । परी० ६.२१ ।
२ 'अन्ये तु अन्यथासिद्धत्वं नाम तद्भदमुदाहरन्ति यस्य हेतोमिणि वृत्तिर्भवन्त्यपि साध्यधर्मप्रयुक्ता भवति न, सोऽन्यथासिद्धो यथा नित्या मनःपरमाणवो मूर्त्तत्वाद् घटवदिति .........स चात्र प्रयोज्यप्रयोजकमावो नास्तीत्यत एवायमन्यथासिद्धोऽप्रयोजक इति कथ्यते । कथं पुनरस्याप्रयोजकत्वमवगतम् - न्यायम० पृ. ६०७॥
३ 'सिद्ध निर्णीते प्रमाणान्तरात्साध्ये प्रत्यक्षादिवाधिते च हेतुर्न किञ्चित्करोति इति अकिञ्चित्करोऽनर्थकः।-प्रमेयक० पृ० १६३ AL
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org