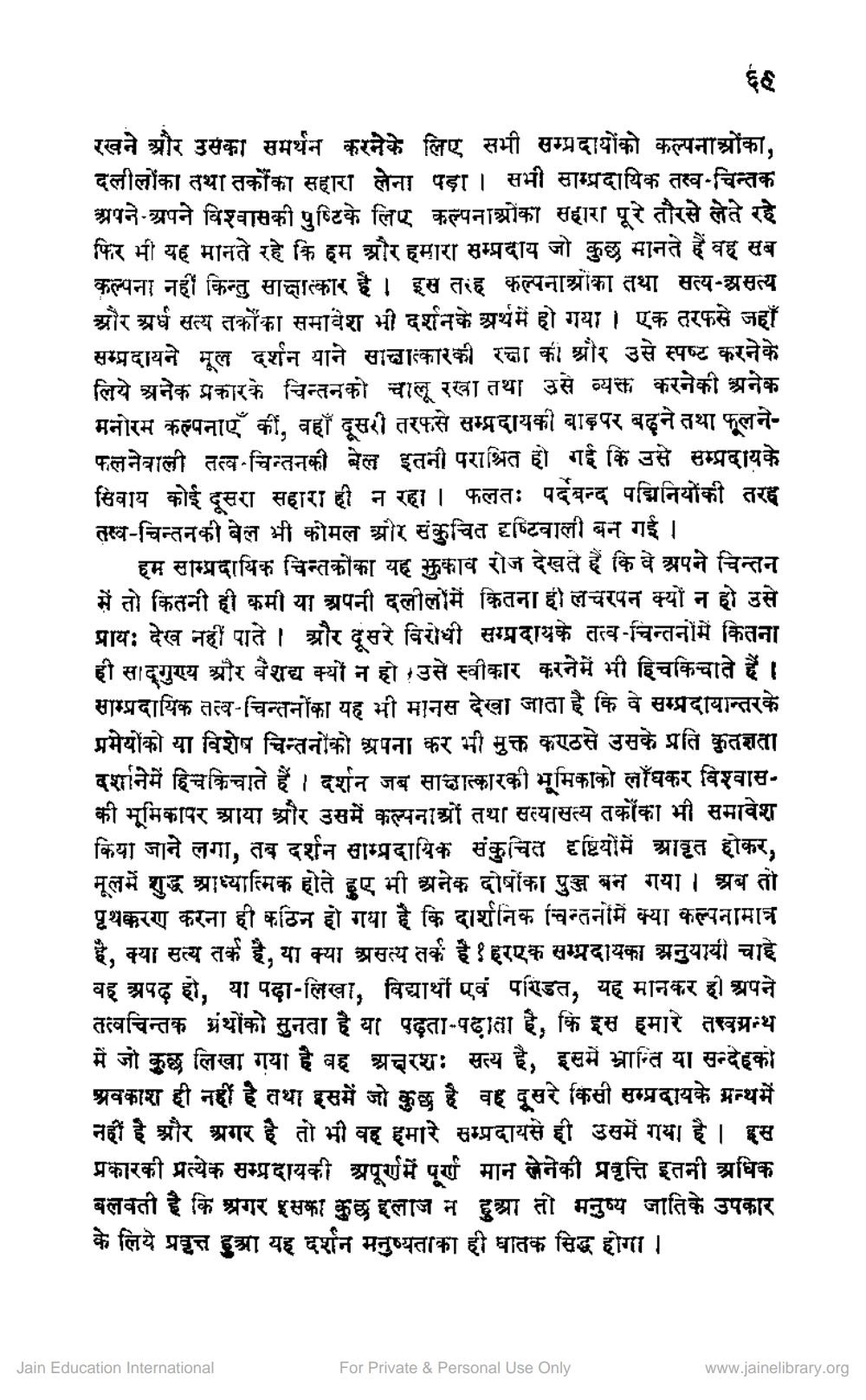________________
६६
रखने और उसका समर्थन करनेके लिए सभी सम्प्रदायोंको कल्पनाओं का, दलीलोंका तथा तर्कों का सहारा लेना पड़ा। सभी साम्प्रदायिक तत्व -चिन्तक अपने-अपने विश्वासकी पुष्टिके लिए कल्पनाओं का सहारा पूरे तौर से लेते रहे फिर भी यह मानते रहे कि हम और हमारा सम्प्रदाय जो कुछ मानते हैं वह सब कल्पना नहीं किन्तु साक्षात्कार है । इस तरह कल्पनाश्रोंका तथा सत्य-असत्य और सत्य का समावेश भी दर्शनके अर्थ में हो गया एक तरफ जहाँ सम्प्रदायने मूल दर्शन याने साक्षात्कार की रक्षा की और उसे स्पष्ट करने के लिये अनेक प्रकार के चिन्तनको चालू रखा तथा उसे व्यक्त करनेकी अनेक मनोरम कल्पनाएँ कीं, वहाँ दूसरी तरफसे सम्प्रदायकी बाढ़पर बढ़ने तथा फूलनेफलनेवाली तत्व- चिन्तनकी बेल इतनी पराश्रित हो गई कि उसे सम्प्रदाय के सिवाय कोई दूसरा सहारा ही न रहा । फलतः पर्देबन्द पद्मिनियोंकी तरह - चिन्तनकी बेल भी कोमल और संकुचित दृष्टिवाली बन गई ।
तस्व-1
हम साम्प्रदायिक चिन्तकोंका यह झुकाव रोज देखते हैं कि वे अपने चिन्तन में तो कितनी ही कमी या अपनी दलीलों में कितना ही लचरपन क्यों न हो उसे प्रायः देख नहीं पाते। और दूसरे विरोधी सम्प्रदाय के तत्व-चिन्तनों में कितना ही सद्गुण्य और वैशद्य क्यों न हो ! उसे स्वीकार करने में भी हिचकिचाते हैं ।
प्रदायिक तत्व-चिन्तनोंका यह भी मानस देखा जाता है कि वे सम्प्रदायान्तर के प्रमेयोंको या विशेष चिन्तनोंको अपना कर भी मुक्त कण्ठसे उसके प्रति कृतज्ञता दर्शाने में हिचकिचाते हैं । दर्शन जब साक्षात्कारकी भूमिकाको लाँघकर विश्वासकी भूमिकापर श्राया और उसमें कल्पनाओं तथा सत्यासत्य तर्कों का भी समावेश किया जाने लगा, तब दर्शन साम्प्रदायिक संकुचित दृष्टियों में आवृत होकर, मूलमें शुद्ध श्राध्यात्मिक होते हुए भी अनेक दोषोंका पुञ्ज बन गया । अब तो पृथक्करण करना ही कठिन हो गया है कि दार्शनिक चिन्तनों में क्या कल्पनामात्र है, क्या सत्य तर्क है, या क्या असत्य तर्क है ? हरएक सम्प्रदायका अनुयायी चाहे वह अपढ़ हो, या पढ़ा-लिखा, विद्यार्थी एवं पण्डित, यह मानकर ही अपने तत्वचिन्तक ग्रंथोंको सुनता है या पढ़ता- पढ़ाता है, कि इस हमारे तस्वग्रन्थ में जो कुछ लिखा गया है वह अक्षरशः सत्य है, इसमें भ्रान्ति या सन्देहको अवकाश ही नहीं है तथा इसमें जो कुछ है वह दूसरे किसी सम्प्रदायके ग्रन्थ में नहीं है और अगर है तो भी वह हमारे सम्प्रदायसे ही उसमें गया है | इस प्रकारकी प्रत्येक सम्प्रदाय की अपूर्ण में पूर्ण मान लेने की प्रवृत्ति इतनी अधिक बलवती है कि अगर इसका कुछ इलाज न हुआ तो मनुष्य जातिके उपकार के लिये प्रवृत्त हुआ यह दर्शन मनुष्यताका ही घातक सिद्ध होगा ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org