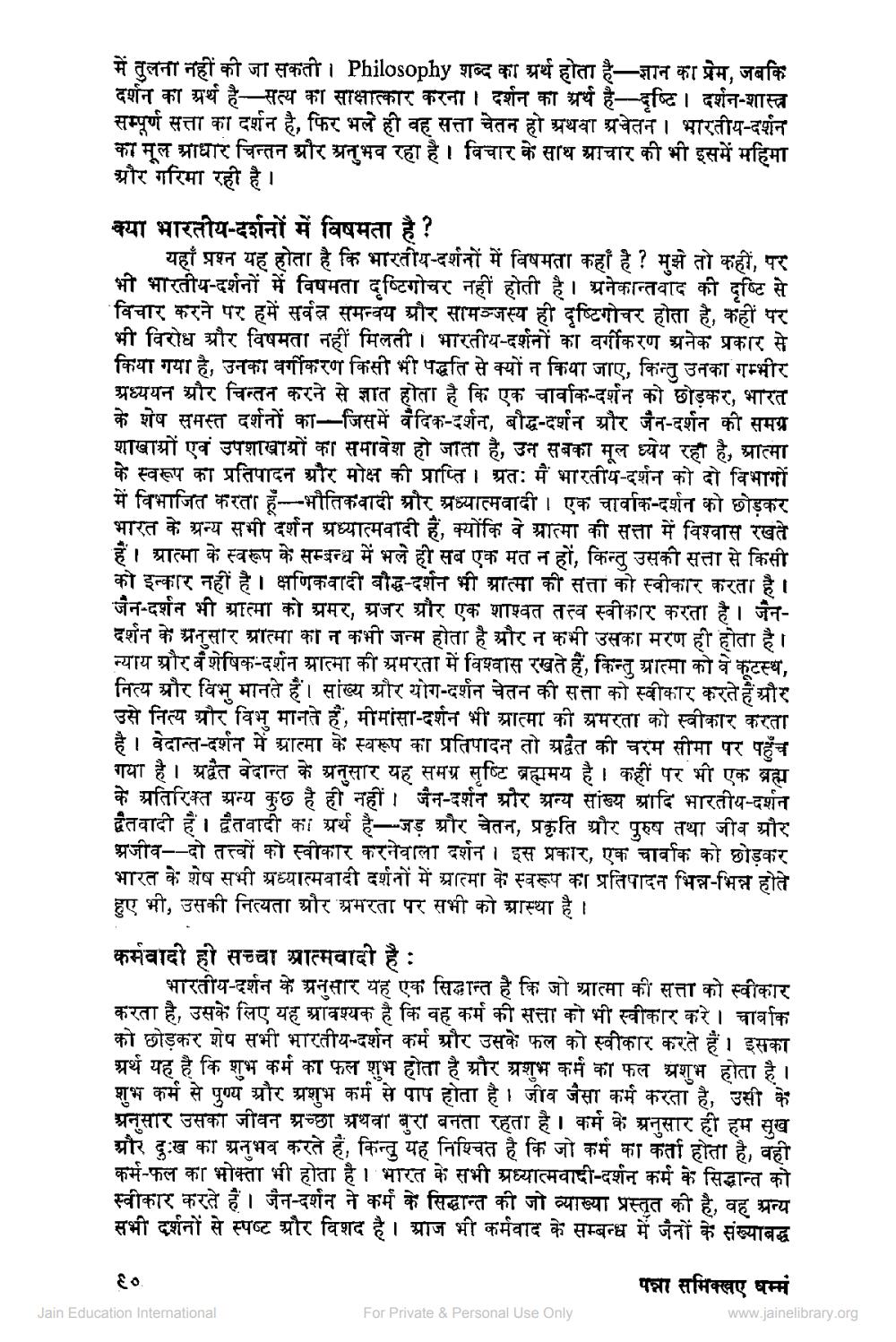________________
में तुलना नहीं की जा सकती। Philosophy शब्द का अर्थ होता है-ज्ञान का प्रेम, जबकि दर्शन का अर्थ है-सत्य का साक्षात्कार करना । दर्शन का अर्थ है-दृष्टि । दर्शन-शास्त्र सम्पूर्ण सत्ता का दर्शन है, फिर भले ही वह सत्ता चेतन हो अथवा अचेतन । भारतीय-दर्शन का मूल आधार चिन्तन और अनुभव रहा है। विचार के साथ प्राचार की भी इसमें महिमा और गरिमा रही है।
क्या भारतीय-दर्शनों में विषमता है ?
यहाँ प्रश्न यह होता है कि भारतीय-दर्शनों में विषमता कहाँ है ? मुझे तो कहीं, पर भी भारतीय-दर्शनों में विषमता दृष्टिगोचर नहीं होती है। अनेकान्तवाद की दृष्टि से विचार करने पर हमें सर्वत्र समन्वय और सामञ्जस्य ही दृष्टिगोचर होता है, कहीं पर भी विरोध और विषमता नहीं मिलती। भारतीय-दर्शनों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया गया है, उनका वर्गीकरण किसी भी पद्धति से क्यों न किया जाए, किन्तु उनका गम्भीर अध्ययन और चिन्तन करने से ज्ञात होता है कि एक चार्वाक दर्शन को छोड़कर, भारत के शेष समस्त दर्शनों का-जिसमें वैदिक-दर्शन, बौद्ध-दर्शन और जैन-दर्शन की समग्र शाखाओं एवं उपशाखाओं का समावेश हो जाता है, उन सबका मूल ध्येय रही है, आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन और मोक्ष की प्राप्ति । अतः मैं भारतीय-दर्शन को दो विभागों में विभाजित करता हूँ-भौतिकवादी और अध्यात्मवादी। एक चार्वाक-दर्शन को छोड़कर भारत के अन्य सभी दर्शन अध्यात्मवादी है, क्योंकि वे आत्मा की सत्ता में विश्वास रखते हैं। आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में भले ही सब एक मत न हों, किन्तु उसकी सत्ता से किसी को इन्कार नहीं है। क्षणिकवादी बौद्ध-दर्शन भी आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है। जैन-दर्शन भी आत्मा को अमर, अजर और एक शाश्वत तत्त्व स्वीकार करता है। जैनदर्शन के अनुसार प्रात्मा का न कभी जन्म होता है और न कभी उसका मरण ही होता है। न्याय और वैशेषिक-दर्शन आत्मा की अमरता में विश्वास रखते हैं, किन्तु आत्मा को वे कूटस्थ, नित्य और विभु मानते हैं। सांख्य और योग-दर्शन चेतन की सत्ता को स्वीकार करते हैं और उसे नित्य और विभु मानते हैं, मीमांसा-दर्शन भी आत्मा की अमरता को स्वीकार करता है। वेदान्त-दर्शन में प्रात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन तो अद्वैत की चरम सीमा पर पहुँच गया है। अद्वैत वेदान्त के अनुसार यह समग्र सृष्टि ब्रह्ममय है। कहीं पर भी एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। जैन-दर्शन और अन्य सांख्य आदि भारतीय-दर्शन द्वैतवादी हैं। द्वैतवादी का अर्थ है-जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष तथा जीव और अजीव--दो तत्त्वों को स्वीकार करनेवाला दर्शन । इस प्रकार, एक चार्वाक को छोड़कर भारत के शेष सभी अध्यात्मवादी दर्शनों में प्रात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन भिन्न-भिन्न होते हुए भी, उसकी नित्यता और अमरता पर सभी को आस्था है।
कर्मवादी ही सच्चा आत्मवादी है :
भारतीय-दर्शन के अनुसार यह एक सिद्धान्त है कि जो आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह कर्म की सत्ता को भी स्वीकार करे । चार्वाक को छोड़कर शेष सभी भारतीय-दर्शन कर्म और उसके फल को स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ यह है कि शुभ कर्म का फल शुभ होता है और अशुभ कर्म का फल अशुभ होता है। शुभ कर्म से पुण्य और अशुभ कर्म से पाप होता है। जीव जैसा कर्म करता है, उसी के अनुसार उसका जीवन अच्छा अथवा बुरा बनता रहता है। कर्म के अनुसार ही हम सुख
और दुःख का अनुभव करते हैं, किन्तु यह निश्चित है कि जो कर्म का कर्ता होता है, वही कर्म-फल का भोक्ता भी होता है। भारत के सभी अध्यात्मवादी-दर्शन कर्म के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं। जैन-दर्शन ने कर्म के सिद्धान्त की जो व्याख्या प्रस्तुत की है, वह अन्य सभी दर्शनों से स्पष्ट और विशद है। आज भी कर्मवाद के सम्बन्ध में जैनों के संख्याबद्ध
१०
पन्ना समिक्खए धम्म
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org