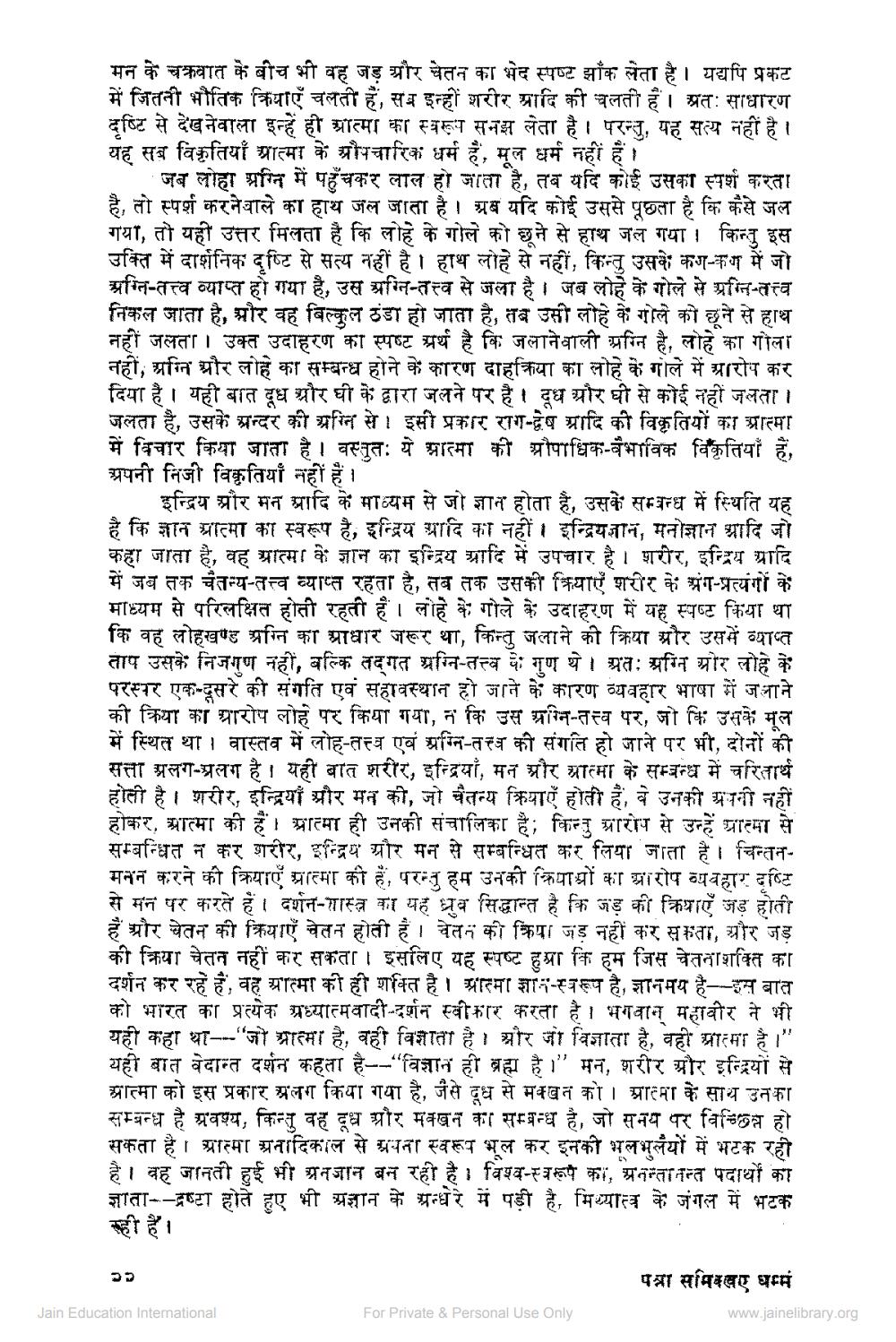________________
मन के चक्रवात के बीच भी वह जड़ और चेतन का भेद स्पष्ट झाँक लेता है। यद्यपि प्रकट में जितनी भौतिक क्रियाएँ चलती हैं, सब इन्हीं शरीर प्रादि की चलती है। अतः साधारण दृष्टि से देखनेवाला इन्हें ही आत्मा का स्वरूप सनझ लेता है। परन्तु, यह सत्य नहीं है। यह सब विकृतियाँ आत्मा के औपचारिक धर्म है, मूल धर्म नहीं हैं।
जब लोहा अग्नि में पहुँचकर लाल हो जाता है, तब यदि कोई उसका स्पर्श करता है, तो स्पर्श करनेवाले का हाथ जल जाता है। अब यदि कोई उससे पूछता है कि कैसे: गया, तो यही उत्तर मिलता है कि लोहे के गोले को छूने से हाथ जल गया। किन्तु इस उक्ति में दार्शनिक दृष्टि से सत्य नहीं है। हाथ लोहे से नहीं, किन्तु उसके कण-कण में जो अग्नि-तत्त्व व्याप्त हो गया है, उस अग्नि-तत्त्व से जला है। जब लोहे के गोले से अग्नि-तत्त्व निकल जाता है, और वह बिल्कुल ठंडा हो जाता है, तब उसी लोहे के गोले को छूने से हाथ नहीं जलता। उक्त उदाहरण का स्पष्ट अर्थ है कि जलानेवाली अग्नि है, लोहे का गोला नहीं, अग्नि और लोहे का सम्बन्ध होने के कारण दाहक्रिया का लोहे के गोले में आरोप कर दिया है। यही बात दध और घी के द्वारा जलने पर है। दध और घी से कोई नहीं जलता। जलता है, उसके अन्दर की अग्नि से। इसी प्रकार राग-द्वेष प्रादि की विकृतियों का आत्मा में विचार किया जाता है। वस्तुतः ये प्रात्मा की औपाधिक-वैभाविक विकृतियाँ है, अपनी निजी विकृतियाँ नहीं हैं।
इन्द्रिय और मन आदि के माध्यम से जो ज्ञान होता है, उसके सम्बन्ध में स्थिति यह है कि ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, इन्द्रिय आदि का नहीं। इन्द्रियज्ञान, मनोज्ञान आदि जो कहा जाता है, वह प्रात्मा के ज्ञान का इन्द्रिय प्रादि में उपचार है। शरीर, इन्द्रिय आदि में जब तक चैतन्य-तत्त्व व्याप्त रहता है, तब तक उसकी क्रियाएँ शरीर के अंग-प्रत्यंगों के माध्यम से परिलक्षित होती रहती है। लोहे के गोले के उदाहरण में यह स्पष्ट किया था कि वह लोहखण्ड अग्नि का प्राधार जरूर था, किन्तु जलाने की क्रिया और उसमें व्याप्त ताप उसके निजगुण नहीं, बल्कि तद्गत अग्नि-तत्त्व के गुण थे। अत: अग्नि और लोहे के परस्सर एक-दूसरे की संगति एवं सहावस्थान हो जाने के कारण व्यवहार भाषा में जलाने की क्रिया का प्रारोप लोह पर किया गया, न कि उस अग्नि-तत्त्व पर, जो कि उसके मल में स्थित था। वास्तव में लोह-तत्त्व एवं अग्नि-तत्त्व की संगति हो जाने पर भी, दोनों की सत्ता अलग-अलग है। यही बात शरीर, इन्द्रियाँ, मन और आत्मा के सम्बन्ध में चरितार्थ होली है। शरीर, इन्द्रियाँ और मन की, जो चैतन्य क्रियाएँ होती है, वे उनकी अपनी नहीं होकर आत्मा की है। प्रात्मा ही उनकी संचालिका है: किन्न प्रारोप से उन्हें प्रात्मा से सम्बन्धित न कर शरीर, इन्द्रिय और मन से सम्बन्धित कर लिया जाता है। चिन्तनमनन करने की क्रियाएँ प्रात्मा की हैं, परन्तु हम उनकी क्रियानों का आरोप व्यवहार दष्टि से मन पर करते हैं। दर्शन-शास्त्र का यह ध्रुव सिद्धान्त है कि जड़ की क्रियाएँ जड़ होती है और चेतन की क्रियाएँ चेतन होती है। चेतन की क्रिया जड़ नहीं कर सकता, और जड़ की क्रिया चेतन नहीं कर सकता। इसलिए यह स्पष्ट हुआ कि हम जिस चेतनाशक्ति का दर्शन कर रहे हैं, वह आत्मा की ही शक्ति है। प्रात्मा ज्ञान-स्वरूप है, ज्ञानमय है-इस बात को भारत का प्रत्येक अध्यात्मवादी-दर्शन स्वीकार करता है। भगवान महावीर ने भी यही कहा था---"जो प्रात्मा है, वही विज्ञाता है। और जो विज्ञाता है, वही आत्मा है।" यही बात वेदान्त दर्शन कहता है---"विज्ञान ही ब्रह्म है।” मन, शरीर और इन्द्रियों से आत्मा को इस प्रकार अलग किया गया है, जैसे दूध से मक्खन को। प्रात्मा के साथ उनका सम्बन्ध है अवश्य, किन्तु वह दूध और मक्खन का सम्बन्ध है, जो सनय पर विच्छित हो सकता है। आत्मा अनादिकाल से अपना स्वरूप भूल कर इनकी भलभुलयों में भटक रही है। वह जानती हुई भी अनजान बन रही है। विश्व-स्वरूप का, अनन्तानन्त पदार्थों का ज्ञाता--द्रष्टा होते हुए भी अज्ञान के अन्धेरे में पड़ी है, मिथ्यात्व के जंगल में भटक
पन्ना समिक्खए धम्म
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org