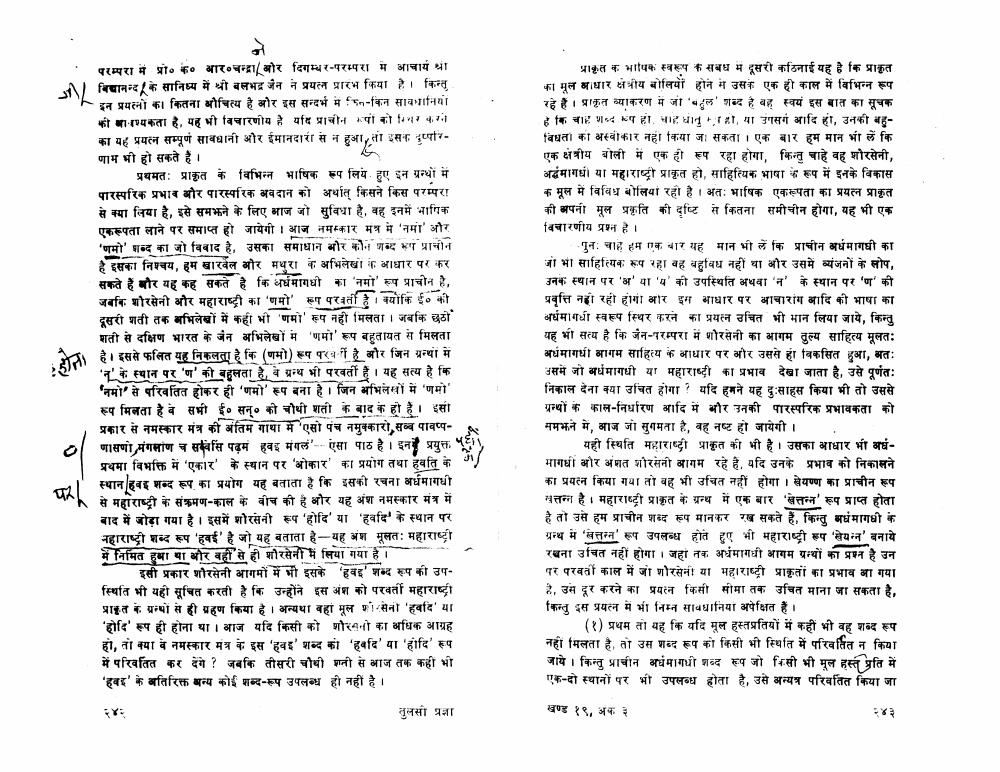________________
परम्परा में प्रो. क० आर०चन्द्रा/और दिगम्बर-परम्परा म आचार्य श्रा बिचानन्द के सानिध्य में श्री बलभद्र जैन ने प्रयत्न प्रारभ किया है। किन्तु इन प्रयत्नों का कितना औचित्य है और इस सन्दर्भ म भन-किन सावधानियां की मा-श्यकता है, यह भी विचारणीय है यदि प्राचीन पा को 14 का यह प्रयत्न सम्पूर्ण सावधानी और ईमानदारी से न हारता सा दुप्पारणाम भी हो सकते हैं।
प्रथमतः प्राकृत के विभिन्न भाषिक रूप लिये हुए इन ग्रन्थों में पारस्परिक प्रभाव और पारस्परिक अवदान को अर्थात् किसने किस परम्परा से क्या लिया है, इसे समझने के लिए माज जो सुविधा है, वह इनमें भाषिक एकरूपता लाने पर समाप्त हो जायेगी । आज नमस्कार मत्र में 'नमा' और 'णमों' शब्द का जो विवाद है, उसका समाधान मोर को शब्द भ प्राचीन है इसका निश्चय, हम बारवेल और मथुरा के अभिलेखांक आधार पर कर सकते हैं और यह कह सकते है कि अर्धमागधी का 'नमो' रूप प्राचीन है, जबकि शौरसेनी और महाराष्ट्री का णमो' रूप परवर्ती क्योंकि की दूसरी शती तक अभिलेखों में कहीं भी णमो' रूप नहीं मिलता। जबकि छठों शती से दक्षिण भारत के जन अभिलेखों में णमो' रूप बहुतायत से मिलता है। इससे फलित यह निकलता है कि (णमो) प पर है और जिन ग्रन्था में 'न' के स्थान पर 'ण' की बहुलता है, वे ग्रन्थ भी परवर्ती है । यह सत्य है कि 'नमो से परिवर्तित होकर ही णमो' रूप बना है। जिन मभिलमों में णमो' रूप मिलता है वे सभी ई. सन्० को चौथी शती के बाद के ही है। इसी प्रकार से नमस्कार मंत्र की अंतिम गाथा में 'एसो पंच नमुक्कारो, सब्ब पावप्पणासणी मंगलाण च सवसि पढ़म हवइ मंगलं'-- एसा पाठ है । इन प्रयुक्त ५७ प्रथमा विभक्ति में 'एकार' के स्थान पर 'ओकार' का प्रयोग तथा हवति के / स्थान हबद्द मन्द रूप का प्रयोग यह बताता है कि इसकी रचना अर्धमागधी से महाराष्ट्री के संक्रमण-काल के बीच की है और यह अंश नमस्कार मंत्र में बाद में जोड़ा गया है। इसमें शौरसेनी रूप 'होदि' या 'हवदि' के स्थान पर नहाराष्ट्री शब्द रूप 'हवई' है जो यह बताता है-यह अंश मूलत: महाराष्ट्री में निर्मित हुमा था और वहीं से ही शौरसेनी में लिया गया है।
इसी प्रकार शौरसेनी आगमों में भी इसके 'हव' शब्द रूप की उपस्थिति भी यही सूचित करती है कि उन्होंने इस अंश को परवर्ती महाराष्ट्री प्राकृत के ग्रन्थों से ही ग्रहण किया है। अन्यथा वहां मूल की सेना 'हवदि' या 'होदि' रूप ही होना था। आज यदि किसी को गोरखनी का अधिक आग्रह हो, तो क्या वे नमस्कार मंत्र के इस 'हव' शब्द की 'हदि' या 'हादि' रूप में परिवर्तित कर देंगे? जबकि तीसरी चौथी पानी से आज तक कही भी 'हवर' के अतिरिक्त अन्य कोई शब्द-रूप उपलब्ध ही नहीं है।
प्राकृत क भाषिक स्वरूप कसबंध में दूसरी कठिनाई यह है कि प्राकृत का मूल माधार क्षेत्रीय बोलियों होने में उसक एक ही काल में विभिन्न रूप रहे हैं। प्राकृत व्याकरण में जा 'बहुल' शब्द है वह स्वयं इस बात का सूचक है कि चार शब्द पहा, पाहधातु+tatया उगसग आदि ही, उनकी बहुविधता का अस्वीकार नहीं किया जा सकता । एक बार हम मान भी लें कि एक क्षेत्रीय बोली में एक ही रूप रहा होगा, किन्तु चाहे वह शोरसेनी, अद्धमागधी या महाराष्ट्री प्राकृत हो, साहित्यिक भाषा के रूप में इनके विकास क मूल में विविध बोलिया रही है । अतः भाषिक एकरूपता का प्रयत्न प्राकृत की अपनी मूल प्रकृति की दृष्टि से कितना समीचीन होगा, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है।
पुनः चाह हम एक बार यह मान भी लें कि प्राचीन अर्धमागधी का जो भा साहित्यिक रूप रहा वह बहुविध नहीं था और उसमें व्यंजनों के सोप, उनक स्थान पर 'अ' या 'य' की उपस्थिति अथवा 'न' के स्थान पर 'ण' की प्रवृत्ति नहीं रही होगा और इस भाधार पर आचारांग आदि की भाषा का अर्धमागधी स्वरूप स्थिर करने का प्रयत्न उचित भी मान लिया जाये, किन्तु यह भी सत्य है कि जैन-गरम्परा में शौरसेनी का आगम तुल्य साहित्य मूलतः अर्धमागधी भागम साहित्य आधार पर और उससे ही विकसित हुआ, अतः उसमें जो मर्धमागधी या महाराष्ट्री का प्रभाव देखा जाता है, उसे पूर्णत: निकाल देना क्या उचित होगा? यदि हमने यह दुःसाहस किया भी तो उससे ग्रन्थों क काल-निर्धारण आदि में और उनकी पारस्परिक प्रभावकता को समझने में, आज जो सुगमता है, वह नष्ट हो जायेगी।
यही स्थिति महाराष्ट्री प्राकृत की भी है। उसका आधार भी अर्धमागधी और अशत शौरसनी बागम रहे हैं. यदि उनके प्रभाव को निकालने का प्रयत्न किया गया तो वह भी उचित नहीं होगा । सेयण्ण का प्राचीन रूप मत्ता है। महाराष्ट्री प्राकृत के ग्रन्थ में एक बार 'खेत्तन्न' रूप प्राप्त होता है तो उसे हम प्राचीन शब्द रूप मानकर रख सकते हैं, किन्तु मधमागधी के ग्रन्थ में सत्तन' रूप उपलब्ध होते हुए भी महाराष्ट्री रूप सेयन्न' बनाये रचना उचित नहीं होगा । जहा नक अर्धमागधी आगम ग्रन्थों का प्रश्न है उन पर परवती काल में जो शोरसेनी या महाराष्ट्री प्राकृतों का प्रभाव आ गया है, उसे दूर करने का प्रयत्न किसी सीमा तक उचित माना जा सकता है, किन्तु इस प्रयत्न में भी निम्न सावधानिया अपेक्षित हैं।
(१) प्रथम तो यह कि यदि मूल हस्तप्रतियों में कहीं भी वह शब्द रूप नहीं मिलता है, तो उस शब्द रूप को किसी भी स्थिति में परिवर्तित न किया जाये । किन्तु प्राचीन अर्धमागधी शब्द रूप जो किसी भी मूल हस्त प्रति में एक-दो स्थानों पर भी उपलब्ध होता है, उसे अन्यत्र परिवर्तित किया जा
तुलसी प्रज्ञा
खण्ड १९, अक३