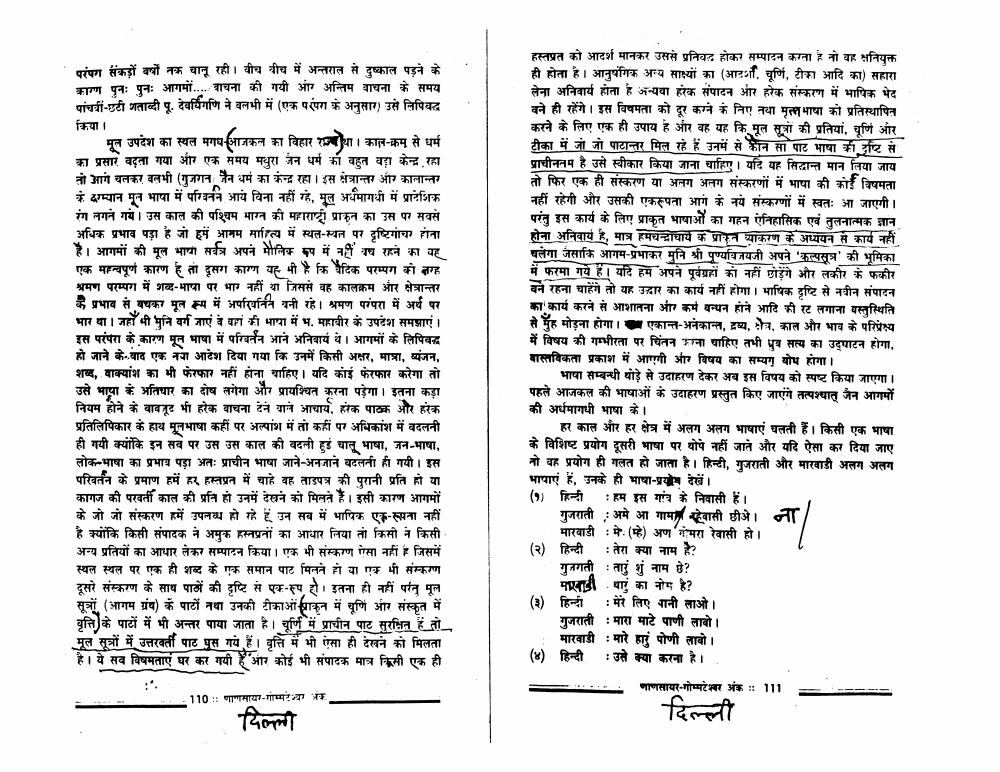________________
परंपरा संकड़ों वर्षों तक चानू रही। बीच बीच में अन्तराल से दुष्काल पड़ने के कारण पुनः पुनः आगमों.... वाचना की गयी और अन्तिम वाचना के समय पांच-छटी जताब्दी पू. देवर्षिगणि ने वलभी में (एक परंपरा के अनुसार) उसे लिपिवद्र
मूल उपदंश का स्थल मगध- आजकल का बिहार राज्याया। काल-क्रम से धर्म का प्रसार बढ़ता गया और एक समय मधुरा जन धर्म का बहुत बड़ा केन्द्र रहा तो आगे चलकर बलभी (गुजगन जैन धर्म का कंन्द्र रहा । इस क्षेत्रान्तर और कालान्तर के दाम्यान मूल भाषा में परिवर्तन आये विना नहीं रहे, मूल अर्धमागधी में प्रादेशिक रंग लगन गये । उस काल की पश्चिम भाग्न की महाराष्ट्री प्राकन का उस पर सवस अधिक प्रभाव पड़ा है जो हम आमम मारित्य में स्थल-स्थल पर द्रष्टिगांचा ना है। आगमों की मूल भाषा सर्वत्र अपने मौलिक रूप में नहीं वष राने का यह एक महत्वपूर्ण कारण है ता दुसग कारण यह भी है कि पैदिक परम्पग की जगह श्रमण परम्परा में शत-भाषा पर भार नहीं था जिससे वह कालक्रम आर क्षेत्रान्तर के प्रभाव से बचका मूल स्म में अपरिवर्तित बनी रहे। श्रमण परंपरा में अर्थ पर भार था । जहाँ भी मुनि वर्ग जाएं वे वहां की भाषा में भ. महावीर के उपदेश समनाएं। इस परंपरा के कारण मूल भाषा में परिवर्तन आने अनिवार्य थे। आगमों के लिपिवद्ध हो जाने के बाद एक नग आदेश दिया गया कि उनमें किसी अक्षर, मात्रा, व्यंजन, शब्द, वाक्यांश का भी फेरफार नहीं होना चाहिए। यदि कोई फेरफार करेगा तो उसे भाषा के अतिचार का दोष लगेगा और प्रायश्चित करना पड़ेगा। इतना कड़ा नियम होने के बावजूद भी हरेक वाचना टेने वाले आचार्य, हरेक पाठक और हरेक प्रतिलिपिकार के हाथ मूलभाषा कहीं पर अल्पांश में तो कहीं पर अधिकांश में बदलती ही गयी क्योंकि इन सब पर उस उस काल की बदली हुई चालू भाषा, जन-भाषा, लोक-भाषा का प्रभाव पड़ा अतः प्राचीन भाषा जाने-अनजाने बदलनी ही गयी। इस परिवर्तन के प्रमाण हमें हर हस्तप्रत में चाहे वह ताडपत्र की पुरानी प्रति हो या कागज की परवर्ती काल की प्रति हो उनमें देखने को मिलते हैं। इसी कारण आगमों के जो जो संस्करण हमें उपलब्ध हो रहे हूं उन सब में भाषिक एक-साना नहीं है क्योंकि किसी संपादक ने अमुक हस्नप्रना का आधार लिया तो किसी ने किसी अन्य प्रतियों का आधार लेकर सम्पादन किया। एक भी संस्करण ऐसा नहीं है जिसमें स्थल स्थल पर एक ही शब्द के एक समान पाट मिलते हो वा एक भी संस्करण दूसरे संस्करण के साथ पाठों की दृष्टि से एक-स्प हो। इतना ही नहीं परंतु मूल सूत्रों (आगम ग्रंथ) के पाटों तथा उनकी टीकाओं याकन में चूर्णि और संस्कृत में वृत्ति के पाटों में भी अन्तर पाया जाता है। चूर्णि में प्राचीन पाट सुरक्षित हैं तो... मूल सूत्रों में उत्तरवर्ती पाट घुस गये हैं। वृत्ति में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। ये सब विषमताएं घर कर गयी है आर कोई भी संपादक मात्र किसी एक ही
हस्तप्रत को आदर्श मानकर उससे प्रनिवट होकर सम्पादन करता है तो वह क्षतियुक्त ही होता है। आनुषंगिक अन्य साक्ष्यों का (आदर्शा, चूर्णि, टीका आदि का सहारा लेना अनिवार्य होता है अन्यथा हरेक संपादन आर हरेक संस्करण में भाषिक भेद वने ही रहेंगे। इस विषमता को दूर करने के लिए तथा मृतभाषा को प्रतिस्थापित करने के लिए एक ही उपाय है और वह यह कि मूल सूत्रों की प्रतियां, चूर्णि और टीका में जो जो पाटान्तर मिल रहे हैं उनमें से कौन सा पाट भाषा की दृष्टि से प्राचीनतम है उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि यह सिद्धान्त मान लिया जाय तो फिर एक ही संस्करण या अलग अलग संस्करणों में भाषा की कोई विषमता नहीं रहेगी और उसकी एकरूपता आग के नये संस्करणों में स्वतः आ जाएगी। परंत इस कार्य के लिए प्राकृत भाषाओं का गहन ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक ज्ञान होना अनिवार्य है, मात्र हमचन्द्रोचार्य के प्रारत व्याकरण के अध्ययन से कार्य नहीं चलेगा जसाकि आगम-प्रभाकर मुनि श्री पूविजयजी अपने 'कल्पसूत्र' की भूमिका में फरमा गये है। यदि हम अपने पूर्वग्रहों को नहीं छोड़ेंगे और लकीर के फकीर बने रहना चाहेंगे तो यह उदार का कार्य नहीं होगा। भाषिक दृष्टि से नवीन संपादन का कार्य करने से आशातना और कर्म बन्धन होने आदि की रट लगाना वस्तुस्थिति से मुँह मोड़ना होगा। - एकान्त-अनेकान्त, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के परिप्रेक्ष्य में विषय की गम्भीरता पर चिंतन माना चाहिए तभी पर सत्य का उद्घाटन होगा, वास्तविकता प्रकाश में आएगी और विषय का सम्यग योध होगा।
भाषा सम्बन्धी बाड़े से उदाहरण देकर अब इस विषय को स्पष्ट किया जाएगा। पहले आजकल की भाषाओं के उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे तत्पश्चात् जैन आगमों की अर्धमागधी भाषा के। ___हर काल और हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं चलती हैं। किसी एक भाषा के विशिष्ट प्रयोग दूसरी भाषा पर थोपे नहीं जाते और यदि ऐसा कर दिया जाए नो वह प्रयोग ही गलत हो जाता है। हिन्दी, गुजराती और मारवाडी अलग अलग भाषाएं हैं, उनके ही भाषा-प्रयोग देखें। (9) हिन्दी हम इस गांव के निवासी हैं।
गुजराती अमे आ गामा रहेवासी छी। ना
मारवाडी : मे (म्हे) अण गंमरा रेवासी हो। (२) हिन्दी तेरा क्या नाम है।
गुतगती : ताशुं नाम छे?
मारवाडी थाएं का नोम है? (३) हिन्दी : मेरे लिए पानी लाओ।
गुजराती : मारा माटे पाणी लावो।
मारवाडी : मारे हासू पोणी लावो । (४) हिन्दी : उसे क्या करना है।
गाणसायर-गोमटेश्वर अंक: 111 - -----
-
.
-110:: णाणमाया गाम्माया र
दिल्ली
दिल्ली