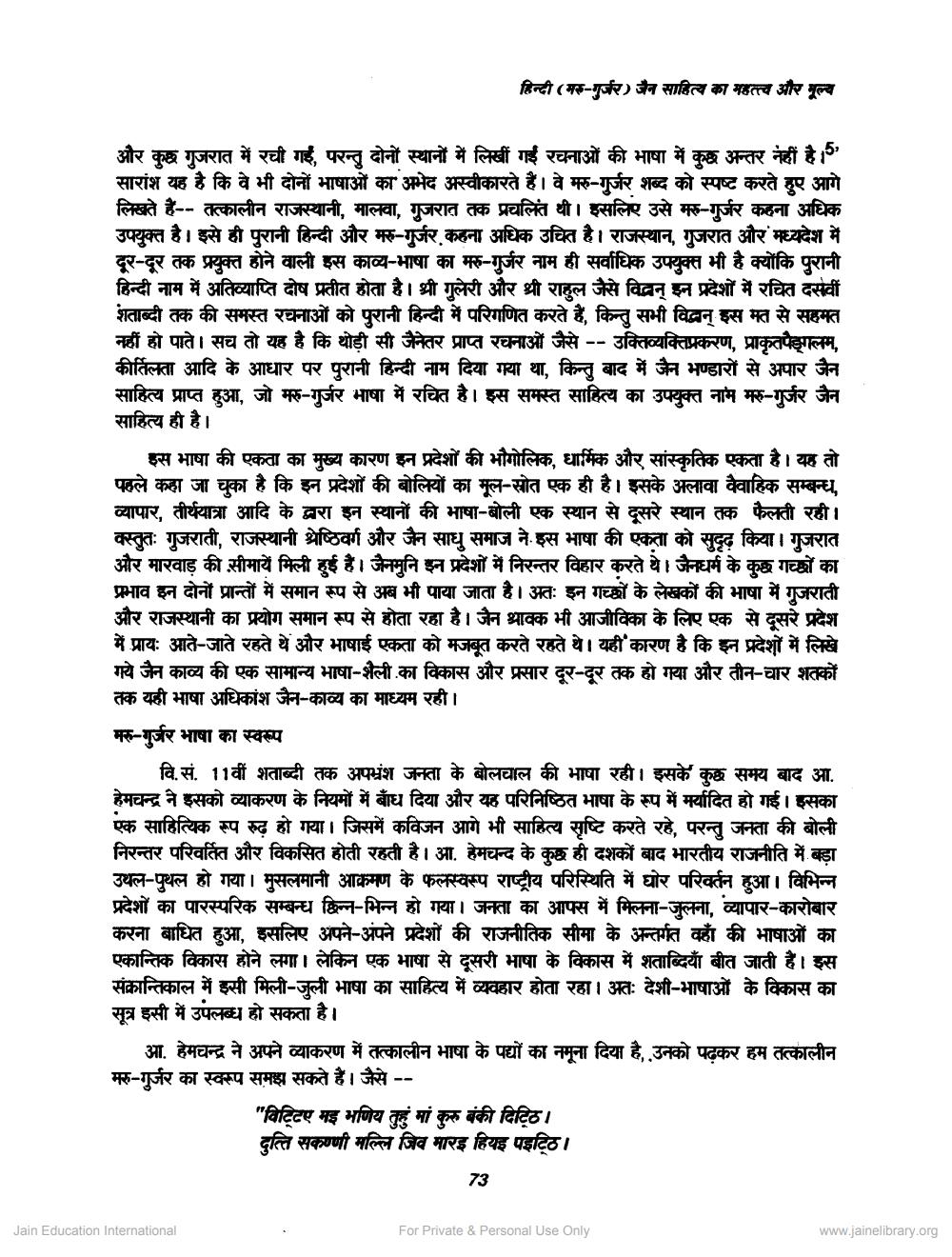________________
हिन्दी (मरु-गुर्जर) जैन साहित्य का महत्त्व और मूल्य
और कुछ गुजरात में रची गईं, परन्तु दोनों स्थानों में लिखी गई रचनाओं की भाषा में कुछ अन्तर नहीं है । " सारांश यह है कि वे भी दोनों भाषाओं का अभेद अस्वीकारते हैं। वे मरु-गुर्जर शब्द को स्पष्ट करते हुए आगे लिखते हैं-- तत्कालीन राजस्थानी, मालवा, गुजरात तक प्रचलित थी। इसलिए उसे मरु-गुर्जर कहना अधिक उपयुक्त है। इसे ही पुरानी हिन्दी और मरु-गुर्जर कहना अधिक उचित है। राजस्थान, गुजरात और मध्यदेश में दूर-दूर तक प्रयुक्त होने वाली इस काव्य-भाषा का मरु-गुर्जर नाम ही सर्वाधिक उपयुक्त भी है क्योंकि पुरानी हिन्दी नाम में अतिव्याप्ति दोष प्रतीत होता है। श्री गुलेरी और श्री राहुल जैसे विद्वन् इन प्रदेशों में रचित दसेवीं शताब्दी तक की समस्त रचनाओं को पुरानी हिन्दी में परिगणित करते हैं, किन्तु सभी विद्वन् इस मत से सहमत नहीं हो पाते। सच तो यह है कि थोड़ी सी जैनेतर प्राप्त रचनाओं जैसे उक्तिव्यक्तिप्रकरण, प्राकृतपैड्गलम, कीर्तिलता आदि के आधार पर पुरानी हिन्दी नाम दिया गया था, किन्तु बाद में जैन भण्डारों से अपार जैन साहित्य प्राप्त हुआ, जो मरु-गुर्जर भाषा में रचित है। इस समस्त साहित्य का उपयुक्त नाम मरु-गुर्जर जैन साहित्य ही है।
इस भाषा की एकता का मुख्य कारण इन प्रदेशों की भौगोलिक, धार्मिक और सांस्कृतिक एकता है। यह तो पहले कहा जा चुका है कि इन प्रदेशों की बोलियों का मूल स्रोत एक ही है। इसके अलावा वैवाहिक सम्बन्ध, व्यापार, तीर्थयात्रा आदि के द्वारा इन स्थानों की भाषा-बोली एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलती रही। वस्तुतः गुजराती, राजस्थानी श्रेष्ठिवर्ग और जैन साधु समाज ने इस भाषा की एकता को सुदृढ़ किया। गुजरात और मारवाड़ की सीमायें मिली हुई हैं। जैनमुनि इन प्रदेशों में निरन्तर विहार करते थे। जैनधर्म के कुछ गच्छों का प्रभाव इन दोनों प्रान्तों में समान रूप से अब भी पाया जाता है। अतः इन गच्छों के लेखकों की भाषा में गुजराती और राजस्थानी का प्रयोग समान रूप से होता रहा है। जैन श्रावक भी आजीविका के लिए एक से दूसरे प्रदेश में प्रायः आते-जाते रहते थे और भाषाई एकता को मजबूत करते रहते थे। यही कारण है कि इन प्रदेशों में लिखे गये जैन काव्य की एक सामान्य भाषा-शैली का विकास और प्रसार दूर-दूर तक हो गया और तीन-चार शतकों तक यही भाषा अधिकांश जैन-काव्य का माध्यम रही ।
मरु-गुर्जर भाषा का स्वरूप
वि.सं. 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश जनता के बोलचाल की भाषा रही। इसके कुछ समय बाद आ. हेमचन्द्र ने इसको व्याकरण के नियमों में बाँध दिया और यह परिनिष्ठित भाषा के रूप में मर्यादित हो गई। इसका एक साहित्यिक रूप रूढ़ हो गया। जिसमें कविजन आगे भी साहित्य सृष्टि करते रहे, परन्तु जनता की बोली निरन्तर परिवर्तित और विकसित होती रहती है। आ. हेमचन्द के कुछ ही दशकों बाद भारतीय राजनीति में बड़ा उथल-पुथल हो गया। मुसलमानी आक्रमण के फलस्वरूप राष्ट्रीय परिस्थिति में घोर परिवर्तन हुआ। विभिन्न प्रदेशों का पारस्परिक सम्बन्ध छिन्न-भिन्न हो गया । जनता का आपस में मिलना-जुलना, व्यापार- कारोबार करना बाधित हुआ, इसलिए अपने-अपने प्रदेशों की राजनीतिक सीमा के अन्तर्गत वहाँ की भाषाओं का एकान्तिक विकास होने लगा। लेकिन एक भाषा से दूसरी भाषा के विकास में शताब्दियाँ बीत जाती है। इस संक्रान्तिकाल में इसी मिली-जुली भाषा का साहित्य में व्यवहार होता रहा। अतः देशी भाषाओं के विकास का सूत्र इसी में उपलब्ध हो सकता है।
आ. हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण में तत्कालीन भाषा के पद्यों का नमूना दिया है, उनको पढ़कर हम तत्कालीन मरु - गुर्जर का स्वरूप समझ सकते हैं। जैसे
Jain Education International
--
"विट्टिए मइ भणिय तुहुं मां कुरु बंकी दिट्ठि । दुत्ति सकण्णी मल्लि जिव मारइ हियइ पइट्ठि ।
73
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org