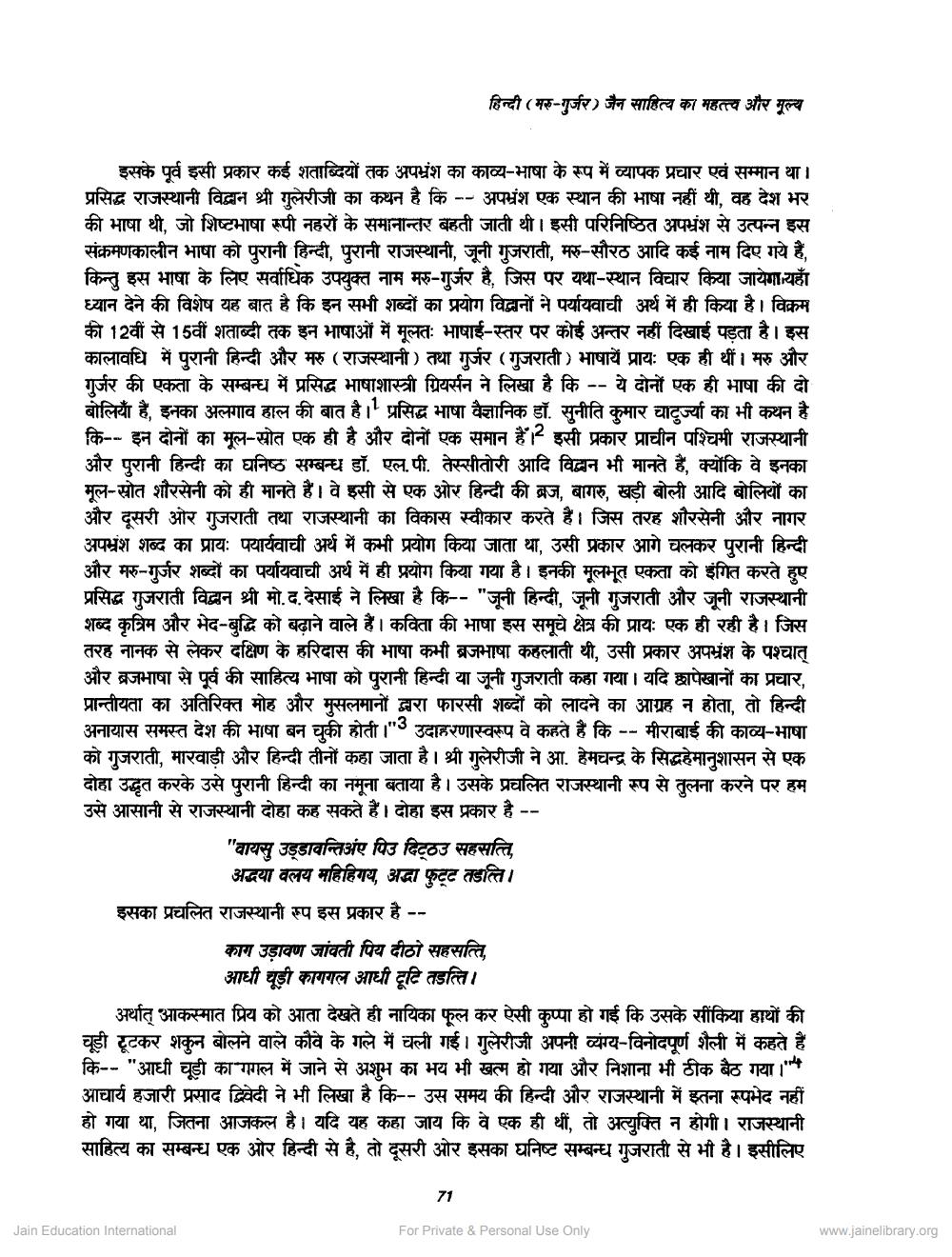________________
इसके पूर्व इसी प्रकार कई शताब्दियों तक अपभ्रंश का काव्य-भाषा के रूप में व्यापक प्रचार एवं सम्मान था ।
प्रसिद्ध राजस्थानी विद्वान श्री गुलेरीजी का कथन है कि अपभ्रंश एक स्थान की भाषा नहीं थी, वह देश भर की भाषा थी, जो शिष्टभाषा रूपी नहरों के समानान्तर बहती जाती थी। इसी परिनिष्ठित अपभ्रंश से उत्पन्न इस संक्रमणकालीन भाषा को पुरानी हिन्दी, पुरानी राजस्थानी, जूनी गुजराती, मरु- सौरठ आदि कई नाम दिए गये हैं, किन्तु इस भाषा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नाम मरु-गुर्जर है, जिस पर यथा-स्थान विचार किया जायेगा. यहाँ ध्यान देने की विशेष यह बात है कि इन सभी शब्दों का प्रयोग विद्वानों ने पर्यायवाची अर्थ में ही किया है। विक्रम की 12वीं से 15वीं शताब्दी तक इन भाषाओं में मूलतः भाषाई स्तर पर कोई अन्तर नहीं दिखाई पड़ता है। इस कालावधि में पुरानी हिन्दी और मरु ( राजस्थानी ) तथा गुर्जर (गुजराती) भाषायें प्रायः एक ही थीं। मरु और गुर्जर की एकता के सम्बन्ध में प्रसिद्ध भाषाशास्त्री ग्रियर्सन ने लिखा है कि ये दोनों एक ही भाषा की दो बोलियाँ है, इनका अलगाव हाल की बात है । 1 प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉ. सुनीति कुमार चाटुर्ज्या का भी कथन है कि-- इन दोनों का मूल स्रोत एक ही है और दोनों एक समान हैं। 2 इसी प्रकार प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी और पुरानी हिन्दी का घनिष्ठ सम्बन्ध डॉ. एल. पी. तेस्सीतोरी आदि विद्वान भी मानते हैं, क्योंकि वे इनका मूल स्रोत शौरसेनी को ही मानते हैं। वे इसी से एक ओर हिन्दी की ब्रज, बागरु, खड़ी बोली आदि बोलियों का और दूसरी ओर गुजराती तथा राजस्थानी का विकास स्वीकार करते हैं। जिस तरह शौरसेनी और नागर अपभ्रंश शब्द का प्रायः पयार्यवाची अर्थ में कभी प्रयोग किया जाता था, उसी प्रकार आगे चलकर पुरानी हिन्दी और मरु-गुर्जर शब्दों का पर्यायवाची अर्थ में ही प्रयोग किया गया है। इनकी मूलभूत एकता को इंगित करते हुए प्रसिद्ध गुजराती विद्वान श्री मो. द. देसाई ने लिखा है कि- "जूनी हिन्दी, जूनी गुजराती और जूनी राजस्थानी शब्द कृत्रिम और भेद-बुद्धि को बढ़ाने वाले हैं। कविता की भाषा इस समूचे क्षेत्र की प्रायः एक ही रही है। जिस तरह नानक से लेकर दक्षिण के हरिदास की भाषा कभी ब्रजभाषा कहलाती थी, उसी प्रकार अपभ्रंश के पश्चात् और ब्रजभाषा से पूर्व की साहित्य भाषा को पुरानी हिन्दी या जूनी गुजराती कहा गया। यदि छापेखानों का प्रचार, प्रान्तीयता का अतिरिक्त मोह और मुसलमानों द्वारा फारसी शब्दों को लादने का आग्रह न होता, तो हिन्दी अनायास समस्त देश की भाषा बन चुकी होती।" 3 उदाहरणास्वरूप वे कहते हैं कि मीराबाई की काव्य-भाषा को गुजराती, मारवाड़ी और हिन्दी तीनों कहा जाता है। श्री गुलेरीजी ने आ. हेमचन्द्र के सिद्धहेमानुशासन से एक दोहा उद्धृत करके उसे पुरानी हिन्दी का नमूना बताया है। उसके प्रचलित राजस्थानी रूप से तुलना करने पर हम उसे आसानी से राजस्थानी दोहा कह सकते हैं। दोहा इस प्रकार है --
इसका प्रचलित राजस्थानी रूप इस प्रकार है -
--
हिन्दी (मरु-गुर्जर) जैन साहित्य का महत्त्व और मूल्य
"वायसु उड्डावन्तिअंए पिउ दिट्ठउ सहसत्ति, अर्द्धया वलय महिहिगय, अद्धा फुट्ट तडति ।
Jain Education International
काग उड़ावण जांवती पिय दीठो सहसत्ति, आधी चूड़ी कागगल आधी टूटि तडत्ति ।
अर्थात् आकस्मात प्रिय को आता देखते ही नायिका फूल कर ऐसी कुप्पा हो गई कि उसके सींकिया हाथों की चूड़ी टूटकर शकुन बोलने वाले कौवे के गले में चली गई। गुलेरीजी अपनी व्यंग्य-विनोदपूर्ण शैली में कहते हैं कि-- "आधी चूड़ी का गगल में जाने से अशुभ का भय भी खत्म हो गया और निशाना भी ठीक बैठ गया ।"* आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है कि-- उस समय की हिन्दी और राजस्थानी में इतना रूपभेद नहीं हो गया था, जितना आजकल है। यदि यह कहा जाय कि वे एक ही थीं, तो अत्युक्ति न होगी। राजस्थानी साहित्य का सम्बन्ध एक ओर हिन्दी से है, तो दूसरी ओर इसका घनिष्ट सम्बन्ध गुजराती से भी है। इसीलिए
71
--
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org